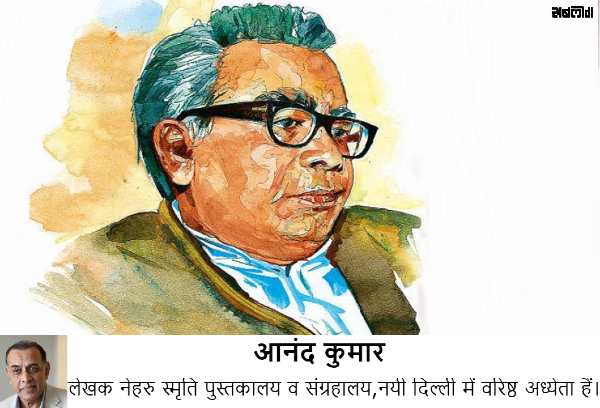चुनावी विसंगतियों से लोकतन्त्र पर आँच
यह देश में आम चुनाव का दौर है। इसे लोकतन्त्र का उत्सव भी कहते हैं। पर ऐसा क्यों कहते हैं? दरअसल, यही वह अवसर है जब लोकतन्त्र अपने पूरे शबाब पर होता है, लोक अपने विराट रूप को प्रकट करता है, उसकी स्वीकृति, उसके अनुमोदन के लिए मदान्ध सत्तासीनों से लेकर राजनीति के धुरन्धर तक उसके सामने नतमस्तक होते हैं।चुनाव एक दिन के लिए ही सही पर तख़्त को पलटने, गर्व से चूर बाहुबली नेताओं तक को धुल चटाने, नया निज़ाम बनाने और यह दिखा देने का अवसर है कि लोकतन्त्र की व्यवस्था में अंतत: सर्वशक्तिमान लोक ही है, सारी शक्तियाँ उसी में निहित हैं।
अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतन्त्र का मतलब है वह व्यवस्था, जिसमें सरकार जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए होती है। लोकतन्त्र में ही ऐसी व्यवस्था है कि जनता ख़ुद उन लोगों को चुनती है, जो सरकार बनाते और चलाते हैं। अभी प्रचलित शासन पद्धतियों में प्रजातांत्रिक प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और हमारे लिए यह संतोष की बात है कि अपने देश में आज़ादी के समय यही व्यवस्था अपनायी गयी और तब से चल रही है । हमारा देश आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और हमारे राजनेता ऐसा कोई मौक़ा नहीं चूकते जब वे इसका ज़िक्र कर वाहवाही ले सकें। इसके बावजूद क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था को लोकतन्त्र की कसौटी पर कसें, तो वो खरा उतर पाएगी? यूँ सरसरी तौर पर देखें और छोटी-मोटी ख़ामियों को नज़रअंदाज़ करें तो लगेगा कि सब ठीक-ठाक ही चल रहा है। पर ऐसा नहीं है। पूरी व्यवस्था पर बारीकी से ग़ौर करें, तो कई गंभीर सवाल खड़े दिखाई देते हैं।
सवालों के इस सिलसिले की शुरुआत तो तभी से हो गयी जब हमने लोकतन्त्र को अपनाया तो ज़रूर पर इसके सही रूप और चरित्र को स्थापित करने के लिए देश में कोई प्रयास नहीं किया गया। शासक और बुद्धिजीवी वर्ग पर अँग्रेजी शासन का ऐसा असर था कि उसने लोकतन्त्र को भी औपनिवेशिक शासन के रंग में रंग दिया, जिसका नतीजा सामने है। देश में जो लोकतन्त्र दिखता है वह खोखला हो चुका है और जनाकांक्षाओं को समझने और तदनुरूप नतीजे देने में असफल है।
अलिस्टर फारुगिया के शब्दों में “आज़ादी तभी है, जब लोग बोल सकें और प्रजातन्त्र तब है, जब सरकार लोगों की बात सुने।” इस कसौटी पर जाँचें तो हमारे देश में लोकतन्त्र बेहद कमज़ोर दिखेगा। आम लोगों के मत से चुने जाने के बावजूद हमारी सरकारों में लोगों के प्रति जवाबदेह होने की प्रवृत्ति घटी है और मनमानी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सरकार और आमजन के बीच संवाद का कम होते जाना लोकतन्त्र के कमज़ोर होने का गंभीर लक्षण है ।
एक स्वस्थ और सही लोकतन्त्र की बुनियाद साफ़-सुथरी, संदेह से परे की हद तक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर टिकी होती है । चुनाव सुधार के लगातार होते रहे प्रयासों के बावजूद हमारी चुनाव प्रक्रिया में गंभीर ख़ामियाँ दिखती हैं । स्वस्थ लोकतन्त्र के लिय इन ख़ामियों का दुरुस्त होना ज़रूरी है जिसकी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग के साथ-साथ राजनीतिक दलों और आमजन की भी है। पर क्या ऐसी कोई कोशिश होती दिखती है?
चुनावी सफलता के लिये लालायित राजनीतिक पार्टियाँ लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई भी समझौता करने में नहीं झिझकती। इसकी शुरुआत चुनाव की घोषणा होने के बाद टिकट बँटवारे की प्रक्रिया से ही हो जाती है। जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने वाले, ईमानदारी और देश चलाने की योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवार चुनने की बजाय चुनाव लड़ रही पार्टियाँ उन उम्मीदवारों को टिकट देने में तरजीह देती है जो किसी भी तरीक़े से ही सही पर चुनाव जीतकर सीट दिला सके। इसी कारण टिकट बँटवारे में उम्मीदवार की क़ाबीलियत की बजाय उसके जातीय आधार, आर्थिक हैसियत, दबंग छवि जैसी अवांछित योग्यताओं एवं भाई-भतीजावाद को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा हो भी क्यों न, लोकतन्त्र में सत्ता पाने के लिए सदन में संख्याबल सबसे ज़रूरी योग्यता जो ठहरी। अल्लामा इक़बाल ने ठीक ही कहा था, “जम्हूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते।”
चुनाव यदि लोकतन्त्र की बुनियाद है तो ऐसी कमज़ोर बुनियाद पर मज़बूत लोकतन्त्र कैसे खड़ा हो सकता है? तो इस तरह चुनाव में ग़लत प्रत्याशियों को उतारने के साथ ही प्रजातन्त्र पर आघात शुरु हो जाता है और उसके कमज़ोर होने का सिलसिला भी। पार्टियों द्वारा चुने गये ऐसे उम्मीदवार जानते हैं कि उनके चयन में जनता के बीच काम करने का ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें जनता, उसकी समस्याओं एवं आकांक्षाओं की दिखावा करने भर से ज्यादा परवाह नहीं होती। वे चुनाव मैदान में तूफ़ान की तरह उतरते हैं और अपने संसाधनों की आँधी में जनता की पसंद-नापसंद को उड़ाकर अपने को जनता पर थोप देते हैं। इसमें प्रायोजित मीडिया ख़बरों की भूमिका भी अब अहम हो गई है। यह चिंता की बात है कि लोकतन्त्र को देश में बचाए, बनाए रखने और इसे मज़बूत बनाने में मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी वह ज़बरदस्त अनदेखी कर रहा है। दरअसल देश में प्रजातन्त्र की स्थिति की चर्चा करते हुए यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि यह मीडिया की विश्वसनीयता का संक्रमण काल है।
दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ऊपर से थोपे गए उम्मीदवारों को सामान्यतः जनता का विरोध भी झेलना नहीं पड़ता। इसके कई कारणों में से एक है, अब भी बड़ी संख्या में मतदाताओं का ग़रीब और अशिक्षित होना। सही चुनाव करने में मतदाता को निष्पक्ष ख़बरों के माध्यम से मदद की जानी चाहिए पर इसके उलट प्रायोजित मीडिया ख़बरों के इस दौर में वह भ्रमित होकर निर्णय लेता है। एक समस्या बहुतेरे मतदाताओं का यह दृष्टिकोण भी है कि कोई जीते, कुछ नहीं बदलने वाला, तो फिर जिससे बेहतर डील हो जाए उसे ही अपना वोट दे दें। एक बड़ी वजह लोगों के बीच वोट को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की समझ का विकसित न हो पाना है।
यह भी देखने में आता है कि धुआँधार प्रचार, संसाधनों एवं अन्य सामर्थ्य देखकर मतदान से पहले ही जीतने वाले और न जीतने वाले उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकरण हो जाता है और जीतने वाले उम्मीदवारों के बीच अधिकांश मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है। स्वभाविक रूप से ऐसे हालात में संसाधनों के अभाव में चुनाव लड़ने वाले ईमानदार एवं योग्य उम्मीदवारों के लिए जीतना तो दूर सम्माजनक मत प्राप्त करना भी टेढ़ी खीर बन जाता है। तो फिर ऐसी हालत में अच्छे लोग राजनीति में कैसे आएँगे, वहाँ कैसे टिक सकेंगे और अच्छे बने रहे सकेंगे, यह एक विचार का विषय है। आज सारे समाज विरोधी तत्व जनतन्त्र का उपयोग अपने को शक्तिशाली बनाने में कर रहे हैं। इनकी उपस्थिति से राजनीति का चरित्र अब ऐसा भयावह हो गया है कि वस्तुत: अच्छे लोगों के लिए यह वर्जनीय हो गयी है।
मतदान के पूर्व मतदाताओं को रिझाने के लिए उनमें रुपये-पैसे एवं शराब का वितरण एवं उन्हें अन्य प्रलोभन दिये जाने की बात जग-ज़ाहिर है। परिस्थितियाँ फिर भी अनुकूल न होने पर दबंग प्रत्याशियों द्वारा मतदान के रुख़ को प्रभावित करने के लिये मतदान क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा कर दिया जाता है। इनसब पर रोक लगाने में चुनाव आयोग अब तक असफल रहा है। इवीएम के साथ छेड़छाड़ और मतगणना में हेर-फेर जैसी आशंकाएँ व्यक्त होती रही हैं। एक स्वस्थ लोकतन्त्र में ऐसी आशंकाओं के लिये कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।
मल्टी पार्टी व्यवस्था, क्षेत्रीय पार्टियों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से चुनाव में प्रत्याशियों की बड़ी संख्या और कम मतदान की स्थिति में मत विभाजन की वजह से कई बार मतदाताओं की संख्या का अति अल्प भाग प्राप्त कर ही प्रत्याशी को जीत हासिल हो जाती है, पर क्या सही मायने में उसे जन-प्रतिनिधि माना जा सकता है? इसी तरह व्यापक मत विभाजन का लाभ लेकर कोई पार्टी चुनाव में ग़ैर-अनुपातिक रूप से बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशी जिताने में सफल हो जाती है। यह सब हमारे देश में लागू ‘फ़र्स्ट पार्ट द पोस्ट’ आधारित चुनाव पद्धति का नतीजा है, जिस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। देश में अब भी लगभग एक तिहाई मतदाता मतदान नहीं करते। मतदान के प्रति इतना ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैया हमारी अपरिपक्व लोकतांत्रिक मानसिकता का ही एक उदाहरण है।
चुनाव नतीजों के बाद प्रजातन्त्र का मखौल उड़ाने का सिलसिला बन्द नहीं होता, यह जारी रहता है। सत्ता हथियाने के लिए जनादेश की सुविधानुसार व्याख्या,दल-बदल, सौदेबाज़ी करने का खेल शुरु हो जाता है और इन सबके बीच जनता से किये गये सारे वादे छूमंतर हो जाते हैं। लोकतन्त्र के साथ खिलवाड़ का यह सिलसिला निरंतर चलता ही रहता है। देश में लोकतन्त्र की आज जो दशा है, उसे न तो स्वस्थ कहा जा सकता है और न ही इस पर संतोष कर चुपचाप बैठा जा सकता है। लोकतन्त्र की इस हालत के लिए काफ़ी हद तक नेतृत्व का दिवालियापन और बौद्धिक वर्ग की वैचारिक ग़ुलामी ज़िम्मेदार है। देश की जनता और संवैधानिक संस्थाओं ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया और चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिये शीघ्र ही आवश्यक क़दम न उठाए गए तो वह दिन भी दूर नहीं जब देश में लोकतन्त्र होने का बस भ्रम ही शेष रहेगा। कहा भी गया है कि सतत जागरुकता लोकतन्त्र की वह क़ीमत है जो नागरिकों को चुकानी पड़ती है।
.