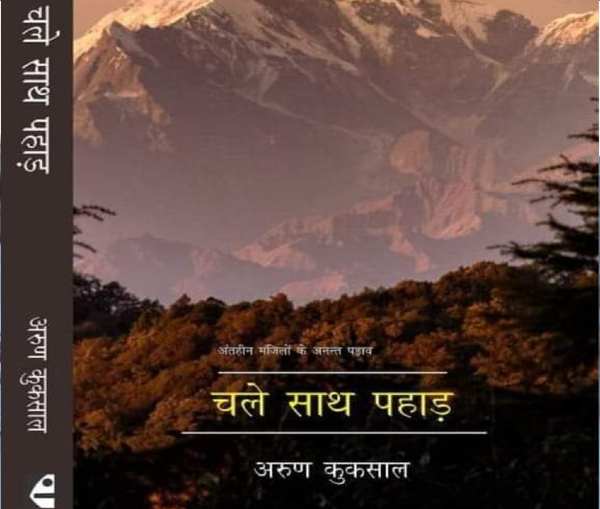शान्त दिखते जल के भीतर की जानलेवा सड़ांध
उत्तराखंड के टिहरी के श्रीकोट गाँव में 26 अप्रैल को जितेंद्र दास नामक एक युवक की सिर्फ इसलिए बुरी तरह पिटाई कर दी गई कि वह एक विवाह समारोह में कुछ लोगों के साथ कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था। उसने उसी काउंटर से प्लेट में खाना लिया जिससे उसके साथ बैठे अन्य लोग खाना ले रहे थे, जिन्हें उसका ऐसा करना गँवारा नहीं था। लात मार कर युवक को कुर्सी से नीचे गिरा देने से भी उन्हें गुरेज नहीं था। प्रतिक्रिया में युवक ने प्रहार करने वाले व्यक्ति के थप्पड़ जड़ दिया तो प्रतिपक्ष गुस्से से आग-बबूला खो कर अपना आपा ही खो बैठा। वह ‘आपा’ क्या इंसान का आपा होगा जो इतनी सहज बात पर किसी का अपमान कर सकता है? किसी मध्यस्थ के बीच-बचाव करने से मामला फौरी तौर पर नियन्त्रण में आया और युवक अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फिर से उस पर जानलेवा प्रहार किए गए जिसके परिणामस्वरूप 9 दिन तक देहरादून के अस्पताल में जीवन-मौत के बीच तड़पते हुए युवक की मृत्यु हो गई।
घटना को अंजाम देने वाले और घटना के शिकार व्यक्ति और मूकदर्शक किसी की भी वर्णगत पहचान अगर घटना पढ़ते ही सबके दिमाग में साफ दर्ज हो जाती है तो क्या इससे यह नहीं दिखता कि देश का एक हिस्सा जो कि काफी बड़ा है, संविधान के दायरे के बाहर है और संविधान की भावना को जीता तो कतई नहीं है। कोई नागरिक शालीन ढंग से अपने मानवाधिकार को, संवैधानिक अधिकार को जीने की कोशिश करता है तो उससे जीने तक का अधिकार छीन लिया जाता है। प्राणिमात्र को मिले हुए अधिकार भी जो समाज अपने सदस्यों को देने के लिए तैयार नहीं है, उसे सभ्य समाज कैसे कहा जा सकता है। बचपन से अहिंसा, उदारता सहनशक्ति और शांतिप्रियता को इसी सभ्यता के लक्षण की तरह पढ़ते-सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। असमानता की जो हिंसा दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों पर लगातार की जा रही है, उसे चुपचाप सहते जाना ही शांति और सौहार्द है?
उसपे सवाल खड़े करना, उसे बदलने की कोशिश हिंसा है? सदियों से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुजन समाज को ब्राहम्णवादी सभ्यता ने मानवाधिकारों से वंचित रखा और अपने पाखण्ड को सत्य की तरह स्थापित करने के लिए जीवन-मूल्यों और आचरण के तौर तरीकों की ऐसी नियमावली रची कि चंद लोग बाकियों को अपने विकास के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते रहे। यह सब काम धर्म के ढाँचे के भीतर बड़े ही सुनियोजित ढंग से सम्पन्न किए जाते रहे। इतिहास जगजाहिर ही है कि कितनी लम्बी प्रक्रिया में आधुनिक बोध और इतिहास बोध के विकास के साथ लोकतन्त्र स्थापित हुआ। समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, बंधुत्व आज संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। किसी भी तरह का भेदभाव गैरकानूनी है। संविधान की नजरों में देश के सभी नागरिक बराबर हैं। पर सवाल है कि संविधान की भावना को जीवन में उतारने की प्रक्रिया में बराबरी क्यों नहीं है?
हाशियाकृत वर्ग तो अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के प्रति निरन्तर सचेत होता जा रहा है। उसकी शुभेच्छाओं के क्रियान्वयन का भरोसा और शक्ति वह संविधान से ग्रहण करता है। किन्तु सवर्ण वर्ग संविधान की अवहेलना करके किसी भी तरह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। संविधान की आत्मा को नागरिक अपने भीतर धारण करें और समानता, स्वतन्त्रता के मूलभूत अधिकारों को जी पाएँ। इसकी शिक्षा लेने-देने में भयानक चूक हुई है। नागरिकों की चेतना में संवैधानिक मूल्यों को भली-भाँति दर्ज करवाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इस शिक्षा का प्रसार और प्रशिक्षण उतना ही जरूरी है जैसे 7-8 दशक पहले तक अंग्रेजी शासन के विरूद्ध भारतीय जनता को जागरूक और एकजुट करने की जरूरत थी। जनता के एक चौथाई हिस्से तक भी अगर संवैधानिक मूल्य अपनी जगह नहीं बना पाए हैं तो बहुसंख्य वर्ग के लिए देश स्वतन्त्र हुआ ही कहाँ। बहुसंख्य नागरिक पराधीन हैं तो फिर देश की स्वतन्त्रता के क्या मायने हैं?
अव्वल तो ऐसी एक घटना का घटित होना भी सारे समाज को प्रश्नांकित करने के लिए काफी था। अफसोस ! जातिगत हिंसा की खबरें देश की अलग-अलग जगहों से लगातार आ रही हैं। ऐसे समय में जब मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तमाम तरह के राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय दवाब हैं। दुनिया भर की संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ हमारे सामने धुनी हुई रूई की तरह बिखरी पड़ी हैं। जिसके चलते मूलभूत आदमियत का अतिक्रमण अब उतना सहज नहीं रहा जैसे धर्म/राज सत्ता से संचालित समाजों में सम्भव था और अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। अपने वैयक्तिक मिजाज के अनुसार उस रूई से जैसे चाहे परिधान बना के पहन लें। स्वीकार भाव हर जीवन-शैली के लिए है।
ज्ञान की तमाम सरणियों को समय के साथ विकसित नई समझ के अनुसार लगातार खँगाला जा रहा है। नई दृष्टि ने यथार्थ को ही बदल कर रख दिया है। ऐसे समय में लोकतांत्रिक देश में मनुष्यता को शर्मसार करने वाली घटनाएँ घटती हैं और कोई बड़ा विक्षोभ इस तरह से नहीं पैदा होता कि सकारात्मक शक्तियाँ मिल कर इसके विरोध में प्रभावी कदम उठाएँ। समूची सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्था में ही इतना बड़ा झोल है जो कि इतनी हिंसा, इतना अत्याचार पैदा होता है। सामाजिक चेतना के अभाव के कारण जनता का बड़ा हिस्सा भेदभावमूलक मानसिकता से अब तक उबर नहीं पाया है। इससे भी बड़ा भयावह सत्य यह है कि निर्णायक भूमिका निभाने वाले पदों पर बैठे हुए वर्चस्वशाली लोगों की भावना में ही खोट दिखता है। बहुजन समाज के विकास के लिए सहयोगी बनना तो बहुत दूर की बात है। अपने बूते पर भी वे कुछ कर गुजरें तो इन लोगों से सहन नहीं होता। दलितों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के साथ उन पर की जाने वाली हिंसा बढ़ रही हैं।
हैरानी की बात यह है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण के दौर में भी समाज के एक हिस्से का घोड़ी पर चढ़ना, बारात ले जाना, साथ में खाना, मंदिर जाना, चश्मा पहनना, कहीं-कहीं तो चप्पल जैसी जरूरत की चीज पहनना तक स्वीकार नहीं किया जा रहा और इसके विरूद्ध हिंसा करने में समाज एकजुट हो जा रहा है। हाल ही में दलित युवक के लग्जरियस कार खरीदने पर युवक को अपने साथ मार-पीट झेलनी पड़ी और कार को भी क्षति पहुँचाई गई। ऐसी जघन्य गतिविधियों को समर्थन देने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, यह कितनी बड़ी विडम्बना है।

जिस गाँव में पूर्वोक्त मर्मांतक घटना घटी। वहाँ सवर्णों की तुलना में दलितों की आबादी काफी कम है। दलित अगर अपने घर के विवाह समारोह में सवर्णों को आमंत्रित करता है तो उनके खाने की प्लेटें और काउंटर अलग होते हैं। पहले सवर्ण खाना खाते हैं। इनका खाना खत्म होने के बाद ही दलित लोग खाना खाते हैं। उनका रसोइया, काउंटर, प्लेटें और खाने का समय भी अलग होता है। यह अपनेआप में कितनी बड़ी खबर है। एक लोकतांत्रिक देश में लोग खुले आम इन असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं। अपराधी और पीड़ित तत्वों को रेखांकित करने में भी कोई उलझन नहीं थी। इसमें खबर के पूरे तत्व मौजूद थे। ऐसे सहज दिखते समय में ही खबरें प्रसारित हों, लेख लिखे जाएँ, सोशल मीडिया में इन अमानवीय रीति-रिवाजों के पालन की घटनाएँ मुख्य समाचार की तरह घर-घर फैलायी जाएँ ऐसा होता तो जितेंद्र दास और रोहिला वेमूला जैसी अनमोल जिंदगियाँ बच सकती थीं। प्रशासन के तन्त्र को सवर्णों पर कार्रवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ता। शासन तन्त्र हरकत में आता।
घटना-विहीन समय को लोग शांत समझते हैं। वस्तुतः हिंसा उसी समय पल और फैल रही होती है। खबर तो एक तरह से गाँधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर अहिंसा का शस्त्र की तरह प्रयोग करने पर उसके विरूद्ध की गई हिंसा की बनी। यानी कि लम्बे समय से अपने ऊपर हिंसा झेलने वाला दलित अपने प्रति अहिंसक होना अथवा हिंसा में सहयोगी न होना जब चुनता है। संवैधानिक अधिकारों पर उसका भरोसा तोड़ने के लिए सवर्णों द्वारा की गई हिंसा की खबर तब बनती है। इस घटना में हमले के तीन दिन बाद जितेंद्र की बहन ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कानून के तहत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। शर्म की बात यह भी है कि शिकायत तो किसी भी उपस्थित व्यक्ति की ओर से हो सकती थी।
मगर शिकायत तो दूर गवाही तक नहीं मिली। खबर को पर्याप्त महत्त्व भी जितेंद्र की मृत्यु के बाद मिला। दलितों का अल्पसंख्या में होना और शहरों से कटे हुए पहाड़ी गाँव के सदस्यों का आजीविका के लिए एक-दूसरे पर निर्भर करना भी इसके पीछे के कारण होंगे। पर फिलहाल इन बातों को जारी रखते हुए इस आवाहन के साथ छोड़ रही हूँ कि क्यों न हम सब मिलकर बाहर से शांत दिखते समय में ही सदियों से की जा रही संगठित हिंसाओं के विरूद्ध लामबन्द हो कर अपने-अपने स्तर पर इनके विरूद्ध सक्रिय हो जाएँ। जहाँ भी ऐसी किसी भी गतिविधि जारी रहने की भनक पड़े। फैला दें उसे आग की तरह। आग का तो स्वभाव ही होता है ऊपर उठना। वह हमें भी ऊपर उठाएगी। सभी का हित सबके ऊपर उठने में ही है। अब हम सभी को ये समझ ही लेना चाहिए।
.