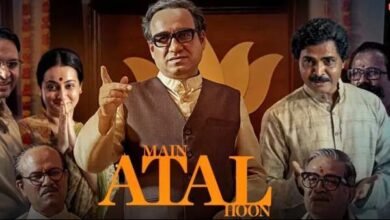ख्वाहिशों के पैबंद सिलती ‘बैकुंठ’
{Featured In IMDb Critics Reviews
निर्देशक – विश्व भानु
कास्ट – विश्व भानु, संगम शुक्ला, विजय ठाकुर, वन्या
क्या वजह है आखिर की आजादी के बाद हम आजाद भारत के पचहत्तर वें बरस में प्रवेश करने वाले हैं और फिर भी निर्माता, निर्देशकों को कालजयी कथाकार, कथासम्राट प्रेमचंद की कहानी ‘कफ़न’ को फिर से फिल्माना पड़ रहा है। दरअसल प्रेमचंद की लिखी अंतिम कहानी ‘कफ़न’ साल 1936 में प्रकाशित हुई थी। जिस पर आज बरसों बाद विश्व भानु ने फ़िल्म बनाई है ‘बैकुंठ’ इस फ़िल्म में प्रेमचंद की कहानी के अलावा भोजपुरी के प्रसिद्ध लोकगीत लिखने वाले तथा रंगकर्मी , लोक कलाकार तथा लोक जागरण के संदेश वाहक रहे ‘भिखारी ठाकुर’ के कुछ गीतों को आधार इस फ़िल्म में बनाया गया है।
प्रेमचंद की कहानी से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे। साहित्य पढ़ने वाले तथा न भी पढ़ने वालों ने कम से कम प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा होगा अपने जीवन में उसी क्रम में अगर उन्होंने यह कहानी भी पढ़ी है तो उन्हें यह फ़िल्म विशेष तौर पर पसंद आएगी। प्रेमचंद की कहानी में उन्होंने जो लिखा उसके मुताबिक झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए दिखते हैं और अंदर झोपड़े में बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़ खाते हुए चीख रही है। रह-रहकर उसके मुँह से निकलने वाली चीत्कार इस कदर हिलाती है कि बाहर बाप बेटे दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात में घीसू कहता है कि वह बचेगी नहीं तो माधव उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती।
कुछ इस तरह का दृश्य हमें 1 घण्टा 10 मिनट की इस ‘बैकुंठ’ फ़िल्म में भी देखने को मिलता है। अपने पेट भर जाने को बुधिया की सद्गति मान लेना। घीसू-माधव का दोज़ख भरते-भरते बुधिया का संसार से चले जाना, बाप को बरसों पुरानी दावत का याद हो आना। जिसमें किस्म-किस्म के पकवान थे और लोगों ने इस कदर उन्हें खाया कि पानी तक न पिया गया इस बात की चर्चा करना। सामाजिक व्यवस्था का जिक्र जिसमें श्रम के प्रति हतोत्साहन पैदा करना क्योंकि उस श्रम में घीसू और माधव को कोई सार्थकता नजर नहीं आती। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रगाढ़ हो रहे अंधेरे पर कथाकार का कटाक्ष। कहानी के समस्त मानवीय मूल्य, सद्भाव, आत्मीयता को रौंदते हुए दिखाना। ये सब फ़िल्म बैकुंठ में जीवंत हो उठता है।
29 मार्च को हंगामा, एयरटेल एक्सट्रीम आदि पर रिलीज होने के बाद एमएक्स प्लयेर पर आई यह फ़िल्म प्रेमचंद के साथ-साथ भिखारी ठाकुर को भी याद करती है। उनके प्रमुख गीतों को अपने में खूबसूरती से समेटती है और बन जाती है आधुनिकता बोध की पहली कहानी मानी जाने वाली ‘कफ़न’ की गवाह। फ़िल्म इससे पहले कई फेस्टिवल्स में भी सराही गई है। और इस कहानी पर इससे पहले भी कई बार फ़िल्म बनी है और नाटक तक भी निर्देशित किए गए हैं। 
उत्तर भारत का एक गांव जहां आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। जैसे कि फ़िल्म कहती है कि हिंदुस्तान आजाद हो गया लेकिन क्या सच में आजाद हुआ है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। जाति से हरिजन और शरीर से ब्राह्मण घीसू माधव की यह कहानी आने वाले दशकों तक यूं ही राम, कृष्ण की कथाओं की भांति कही, सुनी एवं फिल्माई जाती रहेगी। मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी हाथ में आ जाए तो समझ लो समाज सुधर रहा है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है भला। इस बात को भी फ़िल्म सार्थक कर जाती है।
किसी पशु जानवर की तरह बंधे घीसू माधव के दर्शन क्या हमें आज भी दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के रूप में दिखाई नही देते? आए दिन अखबारों की कतरने इन खबरों से तथा दलितों के खून से रंगी, लिखी, छपी नहीं नजर आती? घीसू माधव के ऊपर पेशाब करते फ़िल्म में बच्चे क्या हमें असल समाज में दिखने बंद हो गए हैं? जब सूखी हुई जमीन पर बरसात की पहली फुहार पड़ती है तो उस मिट्टी की महक का आनंद ही कुछ और होता है। ठीक ऐसा ही कुछ दुःख मिश्रित आंनद यह फ़िल्म भी दे जाती है।
‘प्रेमचंद’ की कालजयी रचना ‘कफ़न’ और ‘भिखारी ठाकुर’ के लिखे गीतों को संगीतबद्ध करके जो घीसू और माधव की ख्वाहिशों के पैबंद सिलने की कोशिशें इस फ़िल्म में हुई हैं उसमें निर्देशक के साथ-साथ अभिनय करने वाले कलाकार भी सफल होते दिखाई देते हैं। ‘तेरे बिना भी क्या जीना’, ‘यारा तेरी यारी’ पुराने गानों के साथ-साथ खेल तमाशों, कफ़न के लिए मांगे गए रुपए-पैसों से सिनेमा देखते, ताड़ी पीते हुए बुधिया को याद कर रोते घीसू-माधव, कफ़न के रुपयों से ही दूसरों को पकवान खिलाते और उसके बैकुंठ जाने के लिए दुआएं करते हुए घीसू-माधव अंत में जो सवाल बुधिया के बहाने से खड़े करते हैं क्या प्रेमचंद से पहले किसी ने खड़े किए? इस बात पर हमें विचार करने के लिए फ़िल्म अपने आगोश में लिए, आपको अपने में जज्ब करके सोचने पर मजबूर कर जाती है।
क्या बुधिया ने वाकई सवाल उठाया होगा? मरने के बाद भला कोई कैसे सवाल उठा सकता है? यह तो बुद्धिजीवियों, समीक्षकों का काम ठहरा लेकिन सम्भवतः सवाल तो प्रेमचंद ने ही पहले उठा दिया था। नहीं? फ़िल्म हर कदम पर आपको छूती है लेकिन बावजूद इसके इसमें बैकग्राउंड स्कोर को और मार्मिक किया जाता तो सम्भवतः यह बुधिया की चीख पुकार में आपको इस कदर समो लेती कि आप भी दो आंसू उसके लिए टपका ही देते। फ़िल्म का अंतिम दृश्य दिल दहलाने में सफल होता है। सबकुछ बेहतर होने के बाद भी फ़िल्म कुछ और की गुंजाइश छोड़ जाती है। तिस पर भी सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन, लेखन, गीत-संगीत सभी में यह एक उम्दा फ़िल्म कही जा सकती है।
फिल्म को एमएक्स प्लेयर पर यहाँ क्लिक कर देखा जा सकता है।
अपनी रेटिंग – 3.5 स्टार
.