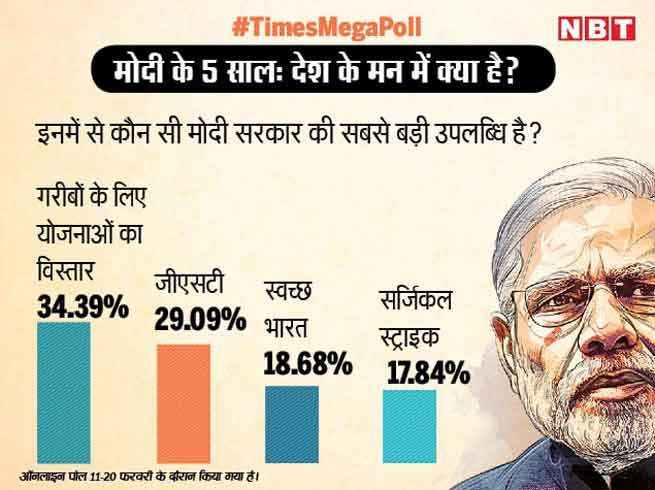प्रशांत किशोर और काँग्रेस के बारे में अटकलबाज़ी पर एक नोट
प्रशांत किशोर के काँग्रेस में शामिल होने की चर्चा गर्म है। कोई नहीं जानता कि सचमुच ऐसा होगा। इस संशय के पीछे प्रशान्त किशोर का अपना इतिहास ही एक बड़ा कारण है। अब तक वे कई पार्टियों के चुनाव प्रबन्धक रह चुके है जिनमें बीजेपी का नाम भी शामिल है। काँग्रेस, सपा और जेडीयू के प्रबन्धक के रूप में उनकी भूमिका को तो सब जानते हैं। इसी वजह से उनकी वैचारिक निष्ठा के प्रति कोई निश्चित नहीं हो सकता है। इसीलिए तमाम चर्चाओं के बाद भी सबसे विश्वसनीय बात आज भी यही प्रतीत होती है कि वे किसी भी हालत में काँग्रेस की तरह के एक पुराने संगठन में शामिल नहीं होंगे।
यदि इसके बावजूद यह असंभव ही संभव हो जाता है तब उस क्षण को हम प्रशांत किशोर के पूरे व्यक्तित्व के आकलन में एक बुनियादी परिवर्तन का क्षण मानेंगे। उसी क्षण से हमारी नज़र में वे महज़ एक पेशेवर चुनाव-प्रबन्धक नहीं, विचारवान गंभीर राजनीतिज्ञ हो जाएँगे।
प्रशांत किशोर चुनाव-प्रबन्धन का काम बाकायदा एक कंपनी गठित करके चला रहे थे। अर्थात् यह उनका व्यवसाय था। इसकी जगह काँग्रेस में बाकायदा एक नेता के तौर पर ही शामिल होना, तत्त्वत: एक पूरी तरह से भिन्न काम को अपनाना कहलाएगा। आम समझ में राजनीति और व्यवसाय, इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक गहरे सम्बन्ध की धारणा है। लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इन दोनों के बीच सहज विचरण कभी भी संभव नहीं है। इनके बीच एक सम्बन्ध नज़र आने पर भी, इनकी निष्ठाएँ अलग-अलग हैं, इनके विश्वास भी अलग है। कोई भी इनमें से किसी एक क्षेत्र को ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना सकता है।
कम्युनिस्ट विचारक अंतोनिओ ग्राम्शी ने इसी विषय पर अपनी ‘प्रिजन नोटबुक’ में एक बहुत सारगर्भित टिप्पणी की है। इसमें एक अध्याय है ‘बुद्धिजीवी और शिक्षा’। इस अध्याय में वे बुद्धिजीवी से अपने तात्पर्य की व्याख्या करते हैं। वे बुद्धिजीवी की धारणा को लेखक-दार्शनिक-संस्कृतिकर्मी की सीमा से निकाल कर इतने बड़े परिसर में फैला देते हैं जिसमें जीवन के सभी आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। बुद्धिजीवी कौन है और कौन नहीं है, इसी सवाल की उधेड़बुन में पन्ना-दर-पन्ना रंगते हुए वे क्रमश: अपनी केंद्रीय चिन्ता का विषय ‘राजनीतिक पार्टी’ पर आते हैं और इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि राजनीतिक पार्टी का हर सदस्य ही बुद्धिजीवी होता है, क्योंकि उनकी सामाजिक भूमिका समाज को संगठित करने, दिशा देने अर्थात् शिक्षित करने की होती है। 
इसी सिलसिले में वे टिप्पणी करते हैं कि “एक व्यापारी किसी राजनीतिक पार्टी में व्यापार करने के लिए शामिल नहीं होता है, न उद्योगपति अपनी उत्पादन-लागत में कटौती के लिए उसमें शामिल होता है, न कोई किसान जुताई की नई विधियों को सीखने के लिए। यह दीगर है कि पार्टी में शामिल होकर उनकी ये ज़रूरतें भी अंशत: पूरी हो जाए।” इसके साथ ही वे यह विचारणीय बात कहते हैं कि यथार्थ में “राजनीति से जुड़ा हुआ व्यापारी, उद्योगपति या किसान अपने काम में लाभ के बजाय नुक़सान उठाता है, और वह अपने पेशे में बुरा साबित होता है। … राजनीतिक पार्टी में ये आर्थिक-सामाजिक समूह अपने पेशागत ऐतिहासिक विकास के क्षण से कट जाते हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय चरित्र की सामान्य गतिविधियों के माध्यम बन जाते हैं।”
जब हम प्रशांत किशोर के काँग्रेस की तरह के एक स्थापित राजनीतिक संस्थान में शामिल होने की गंभीरता पर विचार करते हैं को हमारे ज़ेहन विचार का यही परिदृश्य होता है जिसमें राजनीति का पेशा दूसरे पेशों से पूरी तरह जुदा होता है और इनके बीच सहजता से परस्पर-विचरण असंभव होता है।
अब यदि हम पूरे विषय को एक वैचारिक अमूर्त्तन से निकाल कर आज के राजनीतिक क्षेत्र के ठोस परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो यह कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं होगी कि आज किसी का काँग्रेस में शामिल होने का राजनीतिक अर्थ है खुद को दृढ़ बीजेपी-विरोधी घोषित करना। चुनाव प्रबन्धन का ठेका लेने के बजाय काँग्रेस पार्टी का हिस्सा बनना भी इसीलिए स्वार्थपूर्ण नहीं कहला सकता है क्योंकि अभी काँग्रेस में शामिल होने से ही तत्काल कोई आर्थिक लाभ संभव नहीं है।
प्रशांत किशोर अपने लिए पेशेवर चुनाव प्रबन्धक से बिल्कुल अलग जिस बृहत्तर भूमिका की बात कहते रहे हैं, उनका ऐसा फ़ैसला उनके इस आशय की गंभीरता को पुष्ट करेगा। यह उनके उस वैचारिक रुझान को भी संगति प्रदान करता है जिसके चलते उन्होंने नीतीश कुमार से अपने को अलग किया, पंजाब में काँग्रेस का साथ देने, उत्तर प्रदेश में सपा-काँग्रेस के लिए काम करने के अलावा बंगाल में तृणमूल के लिए काम करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, उनका काँग्रेस जैसे विपक्ष के प्रमुख दल को चुनना भी उनके जैसे एक कुशल व्यक्ति के लिए निजी तौर पर उपयुक्त चुनौती भरा और संतोषजनक निर्णय भी हो सकता है।
बहरहाल, अभी तो यह सब कोरा क़यास ही है। प्रशांत किशोर के लिए अपनी योग्यता और वैचारिकता के अनुसार काम करने के लिए काँग्रेस का मंच किसी भी अन्य व्यक्ति को कितना भी उपयुक्त क्यों न जान पड़े, ऐसे फ़ैसलों में व्यक्ति के अहम् और संगठनों की संरचना आदि से जुड़े दूसरे कई आत्मगत कारण है जो अंतिम तौर पर निर्णायक साबित होते हैं। मसलन, आज यदि हम दृढ़ बीजेपी-विरोध के मानदंड से विचार करें तो किसी के भी लिए काँग्रेस के अलावा दूसरा संभावनापूर्ण अखिल भारतीय मंच वामपंथी दलों का भी हो सकता है। लेकिन वामपंथी पार्टियों का अपना जो पारंपरिक सांगठनिक विन्यास और उसकी रीति-नीति है, उसमें ऐसे किसी बाहर के योग्य व्यक्ति की प्रभावी भूमिका की बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।
वामपंथी पार्टियों के सांगठनिक ढाँचे की यह विडंबना ऐसी है कि इसमें जब बाहर के व्यक्ति के भूमिका असंभव है, तब बाहर के अन्य लोगों के लिए भी वामपंथी पार्टियों की ओर सहजता से झांकना संभव नहीं होता है। इसके लिए कथित संघर्ष की एक दीर्घ प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होता है, भले वह संघर्ष पार्टी के अंदर का संघर्ष ही क्यों न हो। अर्थात् उसके लिए वामपंथी मित्रों के सहचर के रूप में एक लम्बा समय गुज़ारना ज़रूरी होता है। अनुभव साक्षी है कि यह अन्तरबाधा एक मूल वजह रही है जिसके चलते अनेक ऐतिहासिक परिस्थितियों में भी वामपन्थ अपने व्यापक प्रसार के लिए उसका लाभ उठा पाने से चूक जाता है या अपनी भूमिका अदा करने के लिए ज़रूरी शक्ति का संयोजन नहीं कर पाता है। जब 1996 में ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया था तो कुछ ऐसी ही अपनी अन्तरबाधाओं की वजह से, जो सीपीएम के संविधान की एक धारा 112 के रूप में प्रकट हुई थी, वामपन्थ अपनी भूमिका अदा करने में विफल हुआ।
बहरहाल, यहाँ अभी विषय प्रशांत किशोर के अनुमानित निर्णय का है। हम पुन: यही कहेंगे कि अव्वल तो यह बात पूरी तरह से अफ़वाह साबित होगी। प्रोग्राम यह बात सच साबित होती है तो मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर अपनी भिन्न और बृहत्तर सामाजिक भूमिका के बारे में सचमुच गंभीर और ईमानदार है।