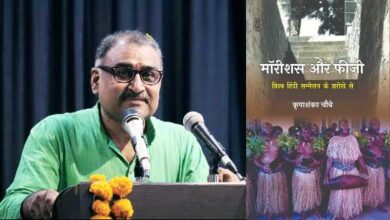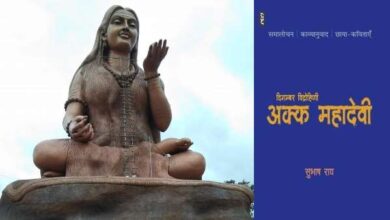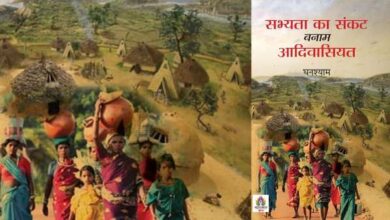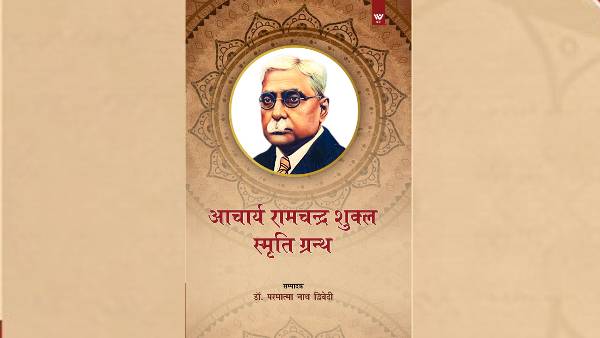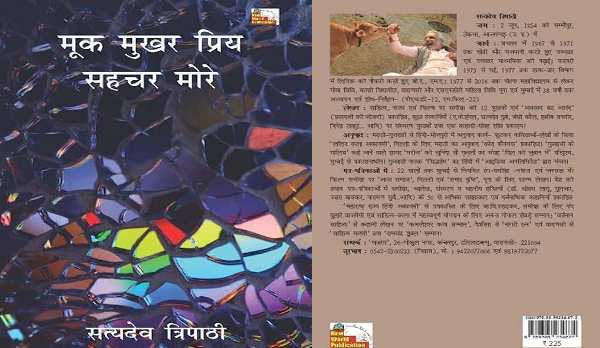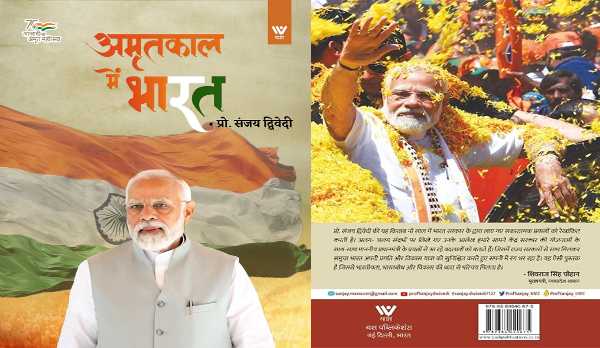स्त्रीवादी विमर्श की नई राहें: पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता
स्त्रीवाद पर पठन-पाठन नया नहीं है, किन्तु हिन्दी जगत में अच्छे विमर्श प्रायः अपनी मूल भाषा में बहुत कम उपलब्ध रहे हैं। ऐसे में सुजाता जी की पुस्तक “पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता” स्त्रीवादी विमर्श के विविध आयामों को समझने के लिए एक उत्कृष्ट कृति है। हिन्दी जगत में ऐसे विमर्शों पर पूरी तरह केंद्रित लेखन बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए यह पुस्तक विशेष महत्व रखती है।
यह पुस्तक तीन खण्डों में विभाजित है, क्रमशः पितृसत्ता कैसे आई?, यौनिकता क्या है? और समलैंगिकता व क्वीयर विमर्श। अकादमिक जगत में जटिलता को अक्सर एक फैशन के रूप में देखा जाता है, जिससे सरल विमर्श को भी दुर्बोधता का जामा पहना दिया जाता है। परन्तु, यह पुस्तक उस प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता के आपसी सम्बन्ध को सहज और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास करती है।
शब्दों के अर्थ का अपना महत्व व उसके पीछे की अपनी राजनीति होती है। इनके अर्थ को ऐतिहासिक संदर्भ के बिना पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन लेखिका ने तीनों खण्डों के अंत में विमर्श की आवश्यक शब्दावली को उचित व्याख्या के साथ स्थान दिया है, जो हिन्दी जगत के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान है। लेखिका किताब की शुरुआत में ही वेगनवाद और इकोफेमिनिज्म के सम्बन्ध पर बहुत बुनियादी सवालों को उठाती हैं कि “मांसाहार पितृसत्तात्मक दमन का ही रूप है। यह समझना कोई दुरूह कार्य नहीं है कि अगर मांसाहार को पितृसत्तात्मक हिंसा और दमन की तरह देखा जाएगा तब महज़ शाकाहार हिंसा और दमन का अन्त नहीं है। इसकी राहें वीगन भोजन के चयन तक जाएँगी और क्या पता इसके बाद भी कुछ और ऐसा आ जाए जो वीगन को भी हिंसा और दमन से जोड़ दे। आख़िर हमारा उद्देश्य क्या था? अवास्तविक, अमूर्त, वायवीय हो जाना?”
आजकल वेगनवाद का प्रचार-प्रसार ख़ूब ज़ोरों-शोरों से चल रहा है लेकिन यह इकोफेमिनिज्म के अतिवाद और उसकी सीमाओं पर सवालिया निशान लगता है। यहाँ वो अपने मूल उद्देश्य से भटक सकती है क्योंकि वेगानिज्म सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो शायद सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का रूप ले ले। यह वर्चस्ववाद विशिष्ट समुदायों की परम्परा, परिस्थितियों और नैतिक मानकों को नज़रअंदाज़ कर रहा है। जनजातीय समुदाय के लिए शिकार महज़ भोजन हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे भी परे यह उनके जीवन- दर्शन और आध्यात्मिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे बेहिसाब शोषण नहीं करते, उनके पास अपने ही नैतिक और इकोलॉजिकल सिद्धांत होते हैं। उनपर बाहर से नैतिकता थोपना सरासर अन्याय होगा।
वेगनवाद को ‘सामान्य’ या ‘मानक’ बनाने की तैयारी की जा रही है और चूँकि इसमें हिंसा का तत्व है तो इसे प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक द्वित्व में बाँटने की कोशिश की जा रही है। प्राकृतिक होने का अर्थ ही वेगनवाद मान लिया जाएगा और समाज से एक अहम तबका छूट जाएगा, वही जिसके लिए शिकार जीवनयापन का ज़रिया है मगर परिस्थितिकीय संतुलन को बिना नुकसान पहुंचाए। आखिर इसी पारिस्थितिक संतुलन को सामान्य बनाने और महिलाओं के हिंसा की बात हमने उठायी थी न? फ़िर यह ट्राइबल समाज को हिंसक मानने पर ख़त्म क्यों हो रही है? क्या एक को सामान्य बनाने के लिए बांकियों का असामान्य या हाशिये पर पहुँच जाना ही हल है? सामान्य होता क्या है? कौन तय करता है कि सामान्य क्या है? इस तरह के सवालों का हमारे सामने अम्बार है मगर एक चीज़ एकदम स्पष्ट है कि सामान्य, मानक और प्राकृतिक द्वित्व को बनाती है, यही द्वैत समाज को दो फाड़ कर करती है।
अगर कोई सामान्य है तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरा उस श्रेणी में फिट न आने वाला असामान्य है, मानक पर ख़रा न उतरने वाला कोई तबका ज़रूर होगा और किसी का अप्राकृतिक बन जाना भी तय होगा। सुजाता जी इन्हीं तीन शब्दों के माध्यम से सत्ता के उन खेलों को उजागर करती हैं, जो चोरी-छिपे न जाने कब चला आ रहा है। वेगनवाद का विमर्श एकदम समकालीन है और इसे हम सब गढ़ते हुए देख रहे हैं, जिस पूँजीवाद को प्राकृतिक तबाही के लिए जिम्मेदार समझा जा रहा था उसी पूँजीवाद ने लैब मीट का विकल्प तलाश लिया है। उस हिंसा से बचाने के लिए लेकिन मूल उद्देश्य से ही हम भटक जाएँगे। विमर्श को उसकी तार्किक परिणीति तक ले जाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विमर्श के व्यावहारिक से अव्यावहारिक दिशा में मुड़ते ही, वह आत्म-विनाश की ओर चला जाता है।
खण्ड-1 में सुजाता जी पितृसत्ता कैसे आयी? इस सवाल को उठाती हैं। जेंडर गैरबराबरी इतना सामान्य हो चुका है कि कोई इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही होता आया है। यह कोई नई बात तो नहीं। लेकिन यह सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। सुजाता जी लिखती हैं कि “रूढ़ भूमिकाओं को निभाते हुए, प्रेम करते हुए, घर और देश चलाते हुए हम कभी समझ नहीं पाये कि दुनिया को एक ताक़त ने बाँट दिया है। यह बँटवारा हमें सहज प्रतीत होता है क्योंकि अब तक यह इतना पुराना पड़ गया है कि इसकी जड़ में जाना आसान नहीं रहा। जड़ तक जाया भी तभी जाता है जब कोई समस्या हो रही हो। समस्या वह होती है जिससे कामकाज रुकता हो।” इसके उलट काम तब ठप्प पड़ सकता है जब इस व्यवस्था में अवरोध पैदा हो।
लेखिका पितृसत्तामक व्यवस्था पर प्रश्न उठाती हैं कैसे यह शक्ति के बंटवारे में पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को निम्नता की श्रेणी में रखता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था कभी भी स्त्रियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि महिलाओं की कोख, श्रम और यौनिकता उनके रास्ते को आसान बनाती हैं। स्त्रियों को नियंत्रित किया जाना पुरुष समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए पितृसत्ता बड़ी ही चालाकी से कुछ महिलाओं को पुरस्कार तो कुछ को सज़ा देकर इस तंत्र को आगे बढ़ाती है। यहाँ रखमाबाई राउत को याद करना ज़रूर हो जाता और लेखिका ने भी इनके बारे में लिखा है। रखमाबाई के केस से पुरस्कार और दण्ड देने की पितृसत्ता की इस चाल को बहुत सरलता से समझा जा सकता है। रखमाबाई इस देश की पहली महिला थी जिसने कोर्ट की दहलीज़ पर खड़े होकर तलाक माँगा था क्योंकि उनकी शादी उस समय के चलन के हिसाब से मात्र 11 वर्ष में कर दी गई थी वो भी उनसे 9-10 साल बड़े दादाजी भीकाजी जी से। बात बस कांसेंट की थी क्योंकि इसमें उनकी सहमति या जिस उम्र में शादी की गयी थी तब शादी की समझ भी नहीं थी।
उस समय के समाज के लिए इस तर्क को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था या यूँ कहें असंभव था और सुधीश चंद्र अपनी किताब “गाँधी के देश में” लिखते हैं कि “उस समय ब्रिटेन में नारी मुक्ति का मसला उभार पर था। इसका नेतृत्व करनेवाली कुछ महिलाओं ने रखमाबाई के प्रतिरोध के व्यापक सन्दर्भ को समझ उनके जीवन और संघर्ष पर गंभीर लेख छापे।” यानी यह मसला केवल भारत तक सीमित नहीं था बल्कि ब्रिटिश संसद तक भी गूँजा था। एक मिया- बीवी का मसला अब एक विमर्श का रूप ले चुका था। और अंत में रखमाबाई पति के पास जाने की बजाए 6 महीने जेल जाने को स्वीकार करती हैं। उस समय भले घर की लड़कियों का अदालत में कदम रखना भी अच्छा नहीं माना जाता था। जेल जाने की कल्पना भी कौन कर सकता था। यह भले घरों की स्त्रियां कुछ और नहीं बल्कि पितृसत्ता के द्वारा पुरस्कार देने का ही तरीका है।
उच्च जाति कि महिलाओं से पतिव्रता होने की उम्मीद की जाती है। पितृसत्ता संरचना को टिकाए रखने के लिए आदर्शो की एक लम्बी सूची तैयार की जाती है। लेखिका ने यहाँ परशुराम के द्वारा अपनी माँ की हत्या करने का प्रसंग भी ज़िक्र किया है। रखमाबाई को भी समाज के द्वारा दण्ड मिला था। यह 19वीं शताब्दी का दौर था और रखमाबाई एकदम अकेली केवल सौतेले पिता का साथ मिला था लेकिन उनकी मृत्यु बीच में ही हो गयी। पूरा समाज नैतिकता का ताना तैयार किये बैठा था। आए दिन मुहल्लों के लोगों की खरीखोंटी सुननी पड़ी थी। दूसरी तरफ़ विरोधी अख़बार और पत्रिकाएँ गंदे और अश्लील लेख छापे जाते थे। हद तो तब हुई जब मराठी में रखमाबाई के चरित्र को पतित बताते हुए पूरा एक नाटक भी छपा था।
उस समय का हिंदू समाज पूरा सकपकाया हुआ था क्योंकि रखमाबाई का जेल जाना उसका व्यक्तिगत चुनाव न होकर पूरे हिन्दू समाज के लिए कलंक का विषय बन जाता। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगानगर तिलक समेत कई रूढ़िवादियों ने दादाजी का समर्थन किया था लेकिन उन्हें रखमाबाई का जेल जाना भी नहीं भा रहा था क्योंकि यह रखमाबाई का मसला भर न रहकर हिन्दू संस्कृति का मसला बन गया था। अंत में रखमाबाई को जेल नहीं ही जाना पड़ा। यह लड़ाई कितनी मुश्किल रही होगी हम इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते। पितृसत्ता को बनाने और चलाने वाले पुरुष ही हैं। आज भी मेरिटल रेप को पूर्ण रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। सहवास जैसे पुरुष का ही अधिकार क्षेत्र है।
सुजाता जी एक और महत्वपूर्ण और बहुपरती पितृसत्तात्मक सच्चाई को प्रकाश में लाती हैं। पितृसत्ता केवल स्त्रियों को ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी एक शक्ति संबंधों के ढांचे में बाँधती है। सुजाता जी यहाँ पितृसत्ता के बहुस्तरीय परत की चर्चा करती हैं और यह चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर यह समझा जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज केवल स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है और सभी पुरुष को इससे समान रूप से लाभ मिलता है किन्तु सच्चाई हमेशा परतों में होती है यहाँ सच्चाई को दो फाड़ में नहीं देखा जा सकता। यहाँ जाति के कोण से इस जटिलता को समझा जा सकता है क्योंकि यह पुरुषों के बीच भी असमानता पैदा करती है। सभी पुरुष एक सी शक्ति और विशेषाधिकार नहीं रखते क्योंकि जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उनका स्थान निर्धारित होता है। उच्च जाति, संपन्न वर्ग या प्रभुत्वशाली पुरुषों को ज़्यादा लाभ मिलता है, जबकि श्रमिक, निम्न जाति, विकलांग या समलैंगिक पुरुषों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
पितृसत्ता एक ख़ास प्रकार की मर्दानगी को उच्च मानती है और जो पुरुष इस आदर्श पर खरे नहीं उतरते, वे भी किसी न किसी रूप में इसके दमन का शिकार होते हैं। इसलिए, पितृसत्ता सिर्फ पुरुष बनाम स्त्री का प्रश्न भर नहीं है, बल्कि शक्ति के बंटवारे की एक अति जटिल संरचना है, जिसमें कुछ पुरुष तो अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं और कुछ पुरुष सोपान में अधीनस्थ रह जाते हैं। मनुस्मृति में भी जाति के आधार पर सज़ा की गंभीरता में बहुत बड़ा फ़र्क है, जहाँ ब्राह्मणों को अन्य जातियों की तुलना में हल्की सज़ा दी जाती है।
लेखिका ने पितृसत्ता के सन्दर्भ में स्त्री, दलित पुरुष और क्वीर कम्युनिटी की बात तो की है लेकिन मेरी नज़र में यहाँ एक और जमात है जो इस तंत्र के शोषण का शिकार है। वो कोई और नहीं बल्कि ख़ुद “मज़बूत” पुरुष समाज। वही पुरुष समाज जिसने इस सत्ता को उत्साह के साथ खड़ा किया मगर वो ख़ुद भी इसका शिकार है। यहाँ हेगेल का मास्टर-स्लेव डायलेक्टिक्स यह बताता है कि दूसरों को दबाकर कोई भी व्यक्ति खुद को पूरी तरह आज़ाद नहीं कर सकता। एक मालिक अपनी पहचान साबित करने के लिए हमेशा दास पर निर्भर होगा। यह निर्भरता मानसिक गुलामी की दलदल में धकेलने लगता है। यानी यहाँ भी सच्चाई परतों में है और सच्चाई हमेशा परतों में ही होती है।
सुधीर कुमार सुथार की किताब “डिलैपिडेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, एंड फार्मर सुइसाइड्स इन इंडिया” और रेविन कॉनेल की “हेजेमोनिक मस्क्युलिनिटी” सिद्धांत भी यही समझाने की कोशिश करता है। सुधीर कुमार सुथार तर्क देते हैं कि किसान आत्महत्या की समस्या को केवल आर्थिक संकट के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। यह संकट दरअसल ग्रामीण समाज में बदलती सामाजिक संरचनाओं, पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव और पुरुषत्व की पारंपरिक भूमिकाओं के टूटने का नतीजा है। हेजेमोनिक मस्क्युलिनिटी के अनुसार, समाज पुरुषों से अपेक्षा करता है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और परिवार के रक्षक बनें। यह पितृसत्तात्मक संरचना पुरुषों को एक “आदर्श पुरुष” की छवि में गढ़ने की कोशिश करती है, जो न केवल महिलाओं और हाशिए के समूहों को कमजोर करती है, बल्कि आम पुरुषों पर भी भारी दबाव डालती है।
ग्रामीण समाज में यह भूमिका और भी कठोर और कड़ी हो जाती है, जहाँ पुरुष किसान को परिवार का पालनकर्ता और संरक्षक माना जाता है। सुधीर कुमार सुथार की पुस्तक में यही तर्क सामने आता है कि किसान आत्महत्याएँ केवल आर्थिक तंगी का परिणाम नहीं हैं, बल्कि एक बहुस्तरीय सामाजिक-मानसिक संकट का हिस्सा हैं। पूंजीवाद जो कि पितृसत्ता का एक अहम रूप है, का शिकार सिर्फ़ प्रकृति, महिलाएँ, या आदिवासी समुदाय ही नहीं हैं, बल्कि मुख्यधारा के किसान भी हैं, जिनके लिए पारंपरिक मर्दानगी की अपेक्षाएँ अब एक असहनीय बोझ बन चुकी हैं। जब एक किसान अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में खुद को अक्षम पाता है, तो उसकी अस्मिता और आत्मसम्मान पर गहरा आघात पहुँचता है। मानसिक तनाव, विषाद और सामाजिक अलगाव के कारण कई किसान आत्महत्या को अंतिम समाधान के रूप में अपनाते हैं।
सुजाता जी ने इन तीनों विमर्शों को समझाने के लिए बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण अपनाया है। जब उन्होंने यौनिकता पर चर्चा की, तो इसे मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण से समझाने के लिए फ्रायड, सिमोन और जूलीयट मिशेल के विचारों का सहारा लिया। स्त्री यौनिकता वास्तव में कोई सरल विमर्श नहीं है, लेकिन सुजाता जी ने भाषा की सरलता बनाए रखते हुए इसे न केवल छुआ, बल्कि इसकी गहराई में जाने का भी सराहनीय प्रयास किया है।
उन्होंने मिशेल फूको के दृष्टिकोण से यौनिकता को शक्ति के संदर्भ में समझाने की कोशिश की है। स्त्रियों की शारीरिक स्वायत्तता (बॉडी ऑटोनॉमी) राज्य की निगरानी में किस प्रकार रहती है, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो भिन्न समाजों—ईरान और भारत—के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वे बताती हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद बुर्क़ा अनिवार्य कर दिया गया, जबकि क्रांति से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। यह परिवर्तन अचानक हुआ था। लेखिका के अनुसार, रज़ा पहलवी और खुमैनी, दोनों ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के समर्थक थे।
दूसरा उदाहरण भारत के मणिपुर का है, जहाँ मैतेई माएं सैनिकों के समक्ष खड़ी होती हैं। यहाँ सैनिक राज्य (स्टेट) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुजाता जी यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि राज्य वास्तव में पितृसत्ता को ही आगे बढ़ाने का कार्य करता है। स्त्री की कोख को सबसे आसान निशाना बना लिया जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि समाज में किसी पुरुष का अपमान करने के लिए उसकी माँ-बहन से जुड़ी गालियों का प्रयोग किया जाता है, और दुर्भाग्यवश, अब कई स्त्रियाँ भी इन गालियों का उपयोग करने लगी हैं, बिना उनके निहितार्थ को समझे। सुजाता जी भारत के संदर्भ में समलैंगिकता को समझाने का प्रयास करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समलैंगिकता को लेकर प्रचलित मिथकों,जैसे कि यह केवल पश्चिमी समाज की देन है, का कोई ठोस आधार नहीं है। असल में, समलैंगिकता भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा रही है, जबकि यह रूढ़ विषमलैंगिक व्यवस्था बाहरी प्रभावों की देन है।
सुजाता जी सरल भाषा में इतने जटिल विमर्श को समझाने में सफल रहती हैं। वे पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता को वेस्टर्न और भारतीय, दोनों दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करती हैं। यही पहलू इस किताब को और भी ख़ास बना देता है, क्योंकि हिन्दी भाषी जगत में एक साथ दोनों दृष्टिकोणों से विमर्श प्रस्तुत किया जाना दुर्लभ है। उनके बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण से यह अध्ययन और भी प्रभावशाली बन जाता है। अक्सर हम उपन्यासों को केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनमें जटिल विमर्शों को भी विभिन्न पात्रों के माध्यम से सहजता से समझाया जा सकता है। सुजाता जी ने भी इन विमर्शों को सरल बनाने के लिए उपन्यासों का सहारा लिया है, जिससे पाठकों के लिए विषय को समझना अधिक आसान हो जाता है। यह पुस्तक हिन्दी भाषी पाठकों के साथ पूरी तरह न्याय करती है।