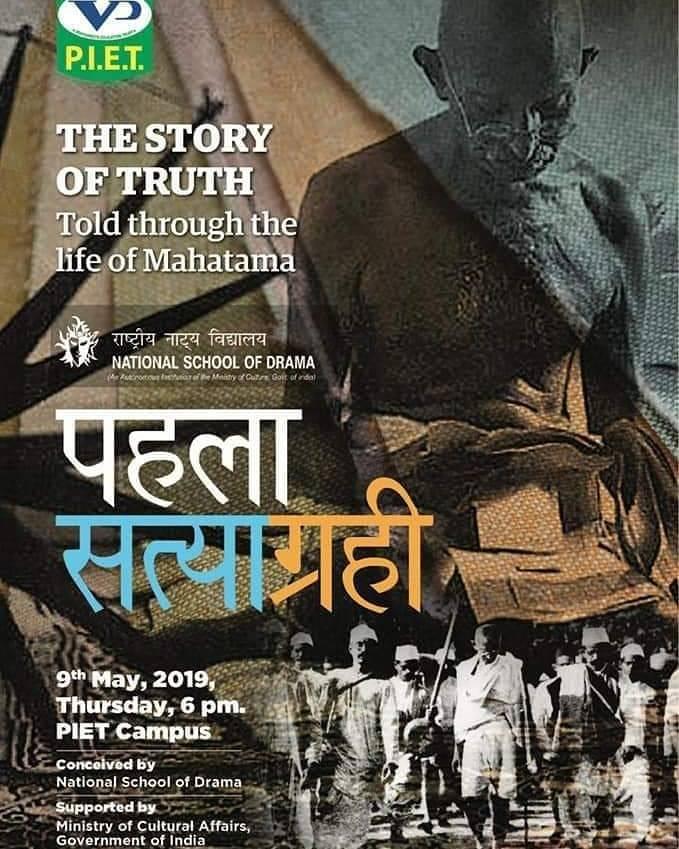हाशिये के समाज का रंगमंच
- राजेश कुमार
हाशिये के लोगों पर चाहे उसके साहित्य पर बातचीत हो या संस्कृति पर, घुमा फिरा कर बहस का कोई न कोई मुद्दा आ ही जाता है। आखिर ये हाशिया है क्या? लोगों को इस शब्द से पाला स्कूल के दिनों में पड़ा होगा जब मास्टर साब कॉपी में हाशिया छोड़कर ही कुछ लिखने का निर्देश दिया करते थे। और ये हाशिया होता कितना था? कुल पन्ना का लगभग एक चौथाई, या उससे भी कम। छोड़ा गया हाशिया मास्टर साब के लिए ही आरक्षित होता था। उस पर मास्टर साब या तो कोई रिमार्क्स देते थे या फिर मार्क्स। समाजशास्त्र या नाट्यशास्त्र में हाशिया की परिभाषा कुछ और है। स्पेस की बात करे तो इसका स्थान चौथाई भर नहीं होता है, बल्कि तीन चौथाई से अधिक ही होता है। राजनीति में हाशिया का जो मतलब होता है, लगभग साहित्य या कहे थिएटर में भी वही होता है।
थिएटर और हाशिया का क्या मतलब है? क्या दोनों में कोई परस्पर संबंध है? संबंध तो जरूर है, अन्यथा बात यूं ही नहीं निकलती? एक मतलब तो ये निकलता है कि थिएटर में हाशिया तो है, पर कहाँ है? फिर सवाल उठता है कि हाशिया क्या है? कौन लोग हाशिए पर हैं, थिएटर में हाशिये के लोग कहाँ हैं? या फिर हाशिये के लोगों का थिएटर कहाँ है, कैसा है? वैसे जब भी हाशिये की बात आती है तो उसके साथ ही एक और शब्द स्वाभाविक रूप से आ जाता है वो है मेनस्ट्रीम। हिंदी में इसका शाब्दिक रूप मुख्यधारा है। दोनों शब्द आजकल समानांतर रूप से प्रयोग में है। दोनों का अर्थ भी अलग – अलग रूप में व्याख्यायित है। दोनों एक दूसरे का पर्याय तो नहीं हैं, पर परस्पर विरोधी हैं, इसमें भी कोई शक नही।
प्रचलन में हाशिया का मतलब ये लगाया जाता है कि जो सत्ता के केंद्र में नहीं है, प्रशासन में जिनकी कोई दखल नहीं है। वोटर लिस्ट में इनका नाम तो है, कहलाने को वो वोटर हैं पर अक्सर इनके वोट का वारा – न्यारा किसी न किसी रूप में कर दिया जाता है। सब्जबाग दिखा कर भटका दिया जाता है या धर्म – जाति के नाम पर पॉलीराइज कर दिया जाता है। अमूर्त रूप में हाशिये के लोगों के कई रूप होते हैं, पर मूर्त रूप में आपको चिन्हित करना हो तो हाशिये के लोग आज के दिनों में किसान, मजदूर, दलित और आदिवासी के रूप में ही नजर आएंगे। हाशिया शब्द से जिन लोगों को एलर्जी होती है या पूर्वाग्रह पाले होते हैं, उनका हाशिया से अभिप्राय प्रायः दलित समाज से ही होता है। हाशिया के दायरे में केवल वर्ण ही नहीं, वर्ग के आधार पर भी जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, सामंती – पूंजीवादी सत्ता से सामाजिक – आर्थिक रूप से शोषित – उत्पीड़ित हो रहे है, आते हैं। हाशिया के लोग में अगर मजदूर – किसान आते है तो इन मजदूर – किसान वर्ग में जो जाति दंश को झेल रहे हैं, वे भी आते हैं। वृहत दायरा है इसका। इसे केवल वर्ण – जाति के खांचे में फिट करना तर्कसंगत, न्यायसंगत नहीं है।
हाशिया का रंगमंच भले सत्ता की दृष्टि में उपेक्षितों का रंगमंच हो…कला के स्तर पर निम्न हो… आर्थिक विपन्नता वाला नाटक हो… शास्त्रीयता, कला की सूक्ष्मता – महीन बुनावट – बारीकी का नितांत अभाव वाला हो…पर यह रंगमंच जंगल के घास – फूल की तरह है, जिसे भले कोई माली सींचता न हो, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हमेशा अपना वजूद बनाये रखती है। शास्त्रीय कला की तरह नहीं है कि गमले में पल्लवित- पुष्पित हो। लेकिन हाशिये का रंगमंच कभी किसी सत्ता के सहयोग के आसरे नहीं रहा। जन – जन के बीच रहने के कारण जन समर्थन ही हमेशा से मजबूत आधार रहा। जन संघर्ष ही मापदंड बना रहा, हाशिये के रंगमंच के उतार – चढ़ाव का।
बरतानिया साम्राज्य द्वारा बंगाल में कृत्रिम अकाल की स्थिति पैदा करने से सांस्कृतिक आंदोलन का जो ज्वार उठा था, वह हाशिये के रंगमंच का ऐतेहासिक उभार था। आज जो हाशिये के थिएटर का अर्थ एक संकुचित अर्थ में लेते हैं, एक खास वर्ण के दायरे तक सीमित करना चाहते हैं, उन्हें बंगाल के अकाल को राष्ट्रीय फलक पर रखनेवाले संस्कृतिकर्मियों के उद्देश्य को जानने की जरूरत है। सन 1940 -42 के भीतर साम्राज्यवाद, फासीवाद एवं युद्धवाद विरोधी चेतना पैदा करने और भारत के मुक्ति संग्राम को नई दिशा देने, सेठों – पूंजीपतियों, मिल- मालिकों एवं जमींदारों के विरुद्ध मजदूर, किसान वर्ग को संगठित करने के लिए, देश के कई नगरों, कस्बों में प्रगतिशील नाट्य संस्थाओं, सांस्कृतिक जत्थों का निर्माण आरंभ हो गया था। सन 43 की 25 मई को इप्टा के गठन के बाद हाशिया का रंगमंच केंद्र में आ गया और उसके साथ तमाम वो लोकनाट्य शैलियां जो कलावादियों की नजर में ओछी समझी जाती थी, कला की दुनिया में जिनका सम्मान नहीं था, प्रमुख हो गयी। किसानों – मजदूरों – दलितों का जीवन जो मंच से दूर था, केंद्र में आ गया। साम्राज्यवादी – पूंजीवादी साजिशों को जनता के बीच रखा जाने लगा। जमींदारों की चाल को लोगों को बताया जाने लगा। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा नहीं चल सका। अंग्रेजों के जाने के बाद जिस वर्ग के हाथों में सत्ता आयी, मूल रूप में उनका चरित्र भिन्न नहीं था। ऊपर से समाजवादी चोला जरूर था, अंदर से वे सामंती – पूंजीवादी – यथास्थितिवादी थे। संस्कृति को लेकर कोई नई नीति या स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। और जनता की वो संस्कृति उन्हें स्वीकार्य भी नहीं था जो उनके लिए प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही थी। ऐसे कइयों उदाहरण मिलते हैं जिसमें सरकार ने नाटक करनेवालों के साथ दमनात्मक कार्रवाई की। नाटक पर प्रतिबंध लगवा दिया, कलाकारों को जेल में डलवा दिया। साथ में एक मुहिम और चलाई गई, सत्ता के संरक्षण में जगह – जगह अकादमी, नाट्य संस्थान और सांस्कृतिक संघटन खड़े किए गए जिसका मुख्य मकसद था, जनपक्षीय संस्कृति को किनारे ठेल देना। अर्थात सत्ता की संस्कृति को केंद्र में ले आना। परिणामतः इप्टा के सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान किसान – मजदूर जो नाटक, कविता, कहानी के केंद्र में था… इन पर हो रहे शोषण – जुल्म फोकस में था…जमींदारों, पूंजीपतियों के विरुद्ध जिस लड़ाई, संघर्ष पर अत्यधिक जोर था; साठ के दशक के प्रारंभ से ही सत्ता की सोची समझी नीति के तहत किनारे करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। उसके स्थान पर मध्य वर्ग के बहाने पाश्चात्य रंग चिंतन लाया जाने लगा जिसमें संघर्ष के स्थान पर कुंठा, संत्रास और हताशा – निराशा पर ज्यादा बल था। रंगमंच की लोक चेतना को तेज करने के बदले उन रंग विचारों को तरजीह दी जाने लगी जो न यहां की जमीन से जुड़ रही थी, न जनता की आवाज तेज करने में सहायक सिद्ध हो रही थी। बल्कि सत्ता के सांस्कृतिक मुहाने पर खड़ा होकर बार -बार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जनता के बीच जो नाट्य शैली व्याप्त है, उसमें रूप और कथ्य दोनों के स्तर पर निम्नता है। उसमें कोई शास्त्रीयता नहीं है। सौन्दर्यशास्त्र के स्तर पर दुर्बल होने के कारण लोक नाटकों का प्रदर्शन कच्चा है। इसमें वो गहराई नहीं है जो दिल को छू सके। उथलापन कहीं ज्यादा है। मनोरंजन करने के प्रयास में श्लील – अश्लील के भेद को समझ नहीं पाती है। अगर एक तरफ वो जनता की लोक संस्कृति को खारिज करती है तो दूसरी तरफ अभिजात्य रंग पद्धतियों को चाहे वो शास्त्रीय रंगमंच हो जो वर्षों से सत्ता से बेदखल था, उसे फिर से सम्मान दिलाना हो या पाश्चात्य की विभिन्न रंग शैलियां जो यथार्थवाद के नाम पर यथास्थितिवाद को स्थापित कर रही थी, को विशेष तरजीह दी जा रही थी। वैसे नाटकों के मंचन पर ज्यादा बल दिया जा रहा था जो व्यक्तिपरक होता था। और इस धारा से जुड़े लोगों और उनके रंगकर्म को प्रधानता दी जा रही थी। इस अभियान में संस्थान, अकादमी से जुड़े आलोचकों, रंगकर्मियों ने सत्ता का खूब साथ दिया। वही किया जिसे करने का उन्हें निर्देश हुआ। सन 67 में नक्सलवाड़ी आंदोलन के दौरान जमींदारों के खिलाफ भूमिहीन किसानों ने जो लड़ाई लड़ी और साहित्य – संस्कृति में जो स्वर सुनाई दिया; सत्ता के सांस्कृतिक मठाधीशों ने अतिवाद का मुलम्मा लगाकर खारिज करने की पूरी कोशिश की। सन 74 में भी देश भर में थोपे गए आपातकाल के विरोध में छात्र आंदोलन उभरा था और जिसके समर्थन में साहित्यकार – संस्कृतिकर्मी नुक्कड़ों पर उतरे थे… रंगकर्मी बंद प्रेक्षागृह से निकलकर खेतों- खलिहानों में जाकर चेतना को जागृत का काम कर रहे थे, उस पर अभिजात्य रंगमंच जिन्हें सत्ता का वरदहस्त प्राप्त था, ने वैचारिक हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नुक्कड़ नाटक के जिस आंदोलन से देश की व्यापक जनता जुड़ी थी, किसान – मजदूर – छात्र अपने संघर्ष की ऊर्जा प्राप्त करते थे; उसको सत्ता के दलाल रंगकर्मियों, आलोचकों ने ‘गटर नाटक‘ से संबोधित किया। जनता की इस प्रगतिशील, जनवादी नाट्य धारा को प्रचारवादी, पार्टी का भोंपू बताकर निकृष्ट जताने का प्रयास किया। सत्ता के साथ मिलकर जगह – जगह दमनात्मक कार्यवाही भी की। लेकिन जिस आंदोलन में बहुसंख्यक लोगों की भागीदारी हो, जिसके साथ शोषित – पीड़ित – संघर्षरत समाज हो, क्या संभव है उस धार को निस्तेज करना? बहुत जल्दी सत्ता के शीर्षस्थों को अहसास हो गया कि जिस रंगमंच में हाशिये का समाज हो, उसे अधिक दिनों तक इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक स्ट्रेटजी के तहत हाशिये के समाज का जो रंगमंच था, उसे सत्ता ने आलिंगनबद्ध कर लिया। उनके स्वर में अपना स्वर मिश्रित कर दिया। साम – दाम – दण्ड – भेद जो भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ी, किया। और कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, वे इस मुहिम में बहुत हद तक सफल भी हुए हैं।
हाशिये के समाज का जो मुखर प्लेटफार्म था, उस पर भी सत्ता का काबिज हो गया। वर्षों से जो लोक नाट्य समाज में रची – बसी थी, वो भी अपनी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही थी, सत्ता के उपेक्षा भाव से लगातार जूझ रही थी। आर्थिक उदारतावाद और उससे उत्पन्न बाजारवाद ने समाज में जिस तरह की विचारधारा को महत्ता दी, उसने भी हाशिये के समाज के रंगमंच के सम्मुख बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। वैश्विक स्तर पर वामपंथ के कमजोर होने के असर से देश की वामपंथी पार्टियां अपने आप को बचा नहीं सकी। बिखराव का शिकार होने के कारण मजदूर – किसान आंदोलन दिनोंदिन कमजोर होता गया। उनसे जुड़ा रंगमंच पर इसका ये प्रभाव पड़ा कि वह निरंतर समाज से विमुख होता गया। जनता से कटते रंगमंच सिकुड़ता गया और उसके स्थान पर वो रंगमंच पैर पसारने लगा जो सत्ता की चाटुकारी में लगा हुआ था। सत्ता को एक ऐसे ही रंगमंच की जरूरत भी थी जो वही करे जो सत्ता चाहती है। सत्ता का अपना एक एजेंडा होता है जो कुछ खुला होता है तो कुछ छिपा हुआ। उसे अपने एजेंडे को लागू करने के लिए संस्कृतिकर्मियों का नया दल तैयार करने की अपेक्षा जो पहले से सक्रिय हैं, उन्हें अपने पक्ष में लाकर, उनसे अपना हित साधना ज्यादा सुविधाजनक लगता है। सत्ता के इस मुहिम में सरकारी अनुदान ने रंगकर्मियों के बीच मारीच की तरह काम किया। प्रारम्भ में यह स्वर्ण मारीच लोमहर्षक साबित होता है। रंगकर्मियों को अपनी अभिव्यक्ति में कोई बंदिश या कहे अवरोध जान नहीं पड़ता है। लेकिन सत्ता को अच्छी तरह से पता होता है कि कब कौन सा पैतरा चलना है। कहाँ तक ढील देनी है और कब टाइट करनी है। जरा भी नानुकुर किया, मक्खी की तरह निकालते देर नहीं लगती है। अन्यथा अधिकतर तो सत्ता की हां में हां मिलाने में ही रम जाते हैं। इस दशा में उनसे जनता के दुःख दर्द की बात सुनना तो बेमानी समझिए। सरोकार से उनका संबंध दूर का हो जाता है। मूल्य, प्रतिबद्धता की बातें किसी हाशिये पर चली जाती है। उनका बस एक ही मकसद होता है, सत्ता की संस्कृति को समृद्ध करना। उस पर किसी तरह का आंच न आने देना। चोट न करना। कोई चुनौती खड़ी न करना ताकि सत्ता के सामने कोई धर्मसंकट न खड़ी हो जाये। और इसके एवज में सत्ता द्वारा जो मुहैया कराया जाता है, वो भी तो कम नहीं है। बड़े – बड़े महोत्सवों में भाग लेने का निमंत्रण, यात्राओं का निरंतर सिलसिला, अभिजात्य रहन – सहन की सुविधा, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की महत्वकांक्षा और उसके प्रभुत्व का आकर्षण छोटे क्या बड़े से बड़े मूल्यवालों – प्रगतिशीलों का ईमान डगमगाने के लिए काफी होता है। इससे इतर हाशिए के समाज के रंगमंच की क्या स्थिति है? वर्तमान में न इनके पास कोई संसाधन है, न प्रदर्शन, पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण या रोजगार जैसी कोई बुनियादी संरचना ही उपलब्ध। आजादी के इतने दिनों बाद भी गांवों में रंगमंच की क्या स्थिति है, ये जाकर ही पता चल सकता है। देश भर में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां शहरों जैसा प्रेक्षागृह हो। जहां आज भी बिजली का संकट है, सड़क की वैसी व्यवस्था नहीं है, रंगमंच का तो सवाल ही नहीं उठता है? कस्बों, शहरों में कहीं – कहीं नाम मात्र के हॉल दिख भी जाये, गांव के लिए तो रेगिस्तान में जल ढूढ़ने सदृश्य है। और इसकी चिंता भी किसे है? जब से देश में सेंट्रलाइज्ड ढांचा विकसित हुआ है, राजधानी – महानगरों को छोड़कर कस्बे और गांव तो हाशिये पर चले गए हैं। आज राजनीति ही नहीं, संस्कृति को भी केंद्रीकृत कर दिया गया है। जो भी होगा, महानगर में ही होगा। मान्य वही होगा जिसकी मान्यता केंद्र देगा। जंगलों में आदिवासी क्या कर रहे हैं, गांवों में कौन सा सौन्दर्यशास्त्र रचा जा रहा है, किस तरह के नए – नए बिम्ब, प्रतीक गढ़े जा रहे हैं, किसे परवाह है जानने की? और कौन तवज्जो दे रहा है? कुछ दशकों में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो इसमें गांव – कस्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा। महानगरों में बैठकर आलोचकों ने भारतीय रंगमंच पर जो भी लिखा है, उसके केंद्र में सत्ता के इर्द -गिर्द की संस्कृति ही पर प्रमुख रही है। उनकी दृष्टि में वही श्रेष्ठ था जो कहीं न कहीं व्यवस्था के पक्ष में खड़ा दिखता हो। अधिकतर उन्हीं नाटकों को मान्यता प्रदान की गई जो अभिजात्य वर्ग के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हो। उनकी दृष्टि में सत्ता के केंद्र में रहनेवाले कलाकार विशिष्ठ थे, अन्य सेकंड ग्रेड के सिटीजन। इसी मानसिकता का परिणाम है कि संस्कृति की महत्तम राशि केंद्र के आसपास ही व्यय होता है। उससे थोड़ा बहुत जो बचता है, कस्बों – देहातों के लिए एहसान कर दिया जाता है। महानगरों में महंगे प्रेक्षागृह के निर्माण का सिलसिला आज भी बरकरार है, लेकिन ये उदारता कभी भी उस समाज के लिए नहीं दिखती है जिनके यहां संस्कृति पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि उनका जीवन है। उनकी ऊर्जा है जो संस्कृति के साथ धड़कती है। अगर संस्कृति उनके जीवन के साथ होती है तो यही संस्कृति संघर्ष के समय कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर जुटी रहती है। कहने को भले मुट्ठी भर कलावादी, यथास्थितिवादी संस्कृतिकर्मियों को सत्ता का एक वर्ग मुख्यधारा के नाम से संबोधित कर ले, लेकिन जिस तेजी से सामाजिक – राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही है…टुकड़ों में बंटे लोग एकजुट हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हाशिये का समाज रंगमंच के सेंटर में आ जायेगा और धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।
राजेश कुमार

लेखक धारा के विरुद्ध चलकर भारतीय रंगमंच को संघर्ष के मोर्चे पर लाने वाले अभिनेता, निर्देशक और नाटककार जो हाशिये के लोग हैं, उनके पुरजोर समर्थक हैं।
+919453737307