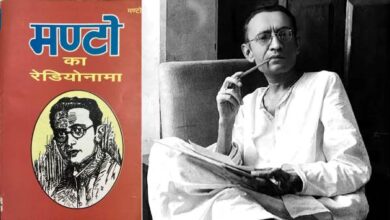अलविदा रणजीत गुहा : तुमसा धीरज वाला इतिहासकार होगा कौन जमाने में!
रणजीत गुहा (1922 -2023) भारतीय इतिहासकारों में सबसे अधिक आयु तक जिए और उनका महत्त्व आयु के बढ़ने के साथ कम नहीं हुआ। देखा जाए तो उनके अधिकतर काम उनके रिटायरमेंट के आसपास या उसके बाद ही आए। ऐसा क्या था रणजीत गुहा में जो उनको एक खास तरीके से विशेष बनाता है। असीम धैर्यवान इस इतिहासकार का जीवन और उसके भीतर चलने वाले संघर्ष के बारे में जाने बिना उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती।
वे एक खास तालुकदार परिवार में पूर्वी बंगाल के कायस्थ परिवार में जन्मे। उनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे और आजादी के बाद ढाका के कोर्ट में जज बने। वह बंगाल (जो पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्ला देश बना) में जन्मे। प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में 1938 में उन्होंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। उनके शिक्षकों में सुशोभन सरकार (यशस्वी मार्क्सवादी शिक्षक और प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार के पिता) शामिल थे। यह दिलचस्प है कि युवा रणजीत गुहा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसी साल जुड़े जिस साल राहुल सांकृत्यायन पार्टी से जुड़े थे। यानि, युवा रणजीत के मन में इतिहासकार बनने का खयाल बाद में आया , इतिहास के निर्माण में अपना राजनीतिक योगदान देने की इच्छा पहले आई।
पार्टी के काम में उनकी संलग्नता के कारण वे इतिहास ऑनर्स नहीं कर पाए और पास ग्रेजुएट हुए। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी सी जोशी ने उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए गंभीर होने के लिए प्रेरित किया।तब उन्होंने एम ए किया। इस बीच वे पार्टी के अखबार के लिए काम करते रहे। जाहिर है युवा रणजीत के ऊपर उस समय की पार्टी में चल रही उथलपुथल, बंगाल की राजनीतिक हलचलों और भीषण अकाल की परिस्थितियों को अपने सामने देखने का मौका मिला और वह इससे प्रभावित हुए। बाद में वह बंबई भी गए और पार्टी के पत्र के लिए काम किया। 1947 में एम ए करने के एक वर्ष बाद उन्हें पार्टी ने यूरोप भेजा। तपन राय चौधरी ने उस समय के बारे में लिखा है कि उनको यूरोप भेजने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे।
उस समय के बहुत सारे कम्युनिस्टों को लगता था कि औपनिवेशिक गुलामी के बाद सत्ता पर काबिज हुआ राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग देश के भीतर के वर्गीय अंतर्विरोधों को मिटा नहीं सकेगा। रणजीत गुहा आजीवन उन मार्क्सवादी चिंतकों में रहे जो राष्ट्रीय बुर्जुआ नेतृत्व (गांधी–नेहरू-पटेल) के प्रति संदेह से भरे रहे और हमेशा उनके प्रति आलोचनात्मक रहे।
जो बात रणजीत गुहा को अन्य बंगाली अभिजन परिवारों से आने वाले कम्युनिस्टों से अलग करती है- वह है बांग्ला भाषा के साथ जुड़ाव। वह अपने बौद्धिक जीवन की शुरुआत बांग्ला भाषा मे लिखकर करते हैं और अपने अंतिम वर्षों में फिर उसी भाषा की ओर मुड़ते हैं। यह बात उनके बौद्धिक व्यक्तित्व की बुनावट को समझने में सहायक हो सकती है।
1947 से 1953 के बीच रणजीत कम्युनिस्ट पार्टी के सौजन्य से पेरिस में रहे। इस दौरान पार्टी के चैनल से उन्होंने सुदूर देशों की यात्राएं की। उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण है उनका चीन जाना। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि गुहा चीन के साम्यवादी बनने के बाद जाने वाले शुरुआती भारतीयों (कम्युनिस्टों)में थे (एक अन्य नाम मोहित सेन का याद आता है।)। उस दौर में उन्होंने देश के बाहर की कम्युनिस्ट पार्टियों व साम्यवादियों के कार्यकलापों को देखने समझने की कोशिश की होगी। इसी दौरान उन्होंने एक पोलिश यहूदी महिला से विवाह किया।
1953 में वह स्वदेश लौटते हैं और कुछ समय तक भारत के अकादमिक माहौल में अपने को लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के अकादमिक माहौल में उन्हें बहुत स्पेस नहीं मिला और उन्होंने जो शोध करने की कोशिश की उसके प्रति उन्हें उत्साह वर्धन नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट पर एक विशेष प्रकार का अध्ययन किया था। कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता त्याग दी। वे रूस के हंगरी पर आक्रमण के आधार पर पार्टी से अलग हुए थे। 1956 के बाद वे तीन वर्ष कलकत्ता में रहे और इस बीच उनके शिक्षक सुशोभन सरकार ने उन्हें जादवपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने का भी मौका दिया।
इस दौरान उन्होंने अपने शोध को बांग्ला पत्रिका परिचय में छापने के लिए तैयार किया। इस पत्रिका को पार्टी से जुड़े लोग निकालते थे। गोपाल हाल्दार इसके संपादक थे। उनको ये आलेख लंबे और पत्रिका के लिए अनुकूल नहीं लगे। गुहा के लेखों को बाद में छपने से रोक दिया गया। इसके बाद वह एक फेलोशिप लेकर यूरोप गए। उनकी थीसिस पर पेरिस के विश्वविद्यालय में भी विचार किया गया और वहाँ भी उनकी थीसिस को पास नहीं किया गया। गुहा के सौभाग्य से उसी समय अमरीकी इतिहासकार डेनियल थॉर्नर पेरिस में थे और उनको थीसिस की कॉपी मिल गई। उनको वह पसंद आई और उन्होंने उसे बाद में छापा भी। 1959 में गुहा के यूरोप जाने के निर्णय के बाद उनकी पत्नी से उनके मतभेद हुए और दोनों अलग हो गए।
इस बार उनको ससेक्स विश्वविद्यालय में रीडर की नौकरी मिल गई और वहाँ उनका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो इतिहास लेखन के क्षेत्र में नई जमीन बनाने की कोशिशों में लगे थे। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण था उनका डी ए लो के साथ संबंध। लो ही उनको बाद में जब वे आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के उपाचार्य हुए तो उन्हें 1980 में कैनबरा ले गए। लो ने 1968 में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक का सम्पादन किया था जिसमें उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान के जटिल प्रश्नों पर विचार किया था। उसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसपर भारत के इतिहासकारों के बीच चर्चा कम हुई लेकिन फिर उसपर कुछ इतिहासकारों का ध्यान गया। आज ऐसा प्रतीत होता है कि गुहा को इससे जरूर प्रेरणा मिली होगी।
सत्तर और अस्सी के दशक में आधुनिक भारत के इतिहास लेखन को लेकर बहस बहुत तेज थी। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण था- कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति दृष्टि का अंतर। मोहित सेन और बिपन चंद्र साम्यवादी होकर भी राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत सकारात्मक थे। उनके ऊपर उन साम्यवादी इतिहासकारों ने आलोचनात्मक रुख रखा जो गांधी नेहरू के प्रति बहुत आलोचनात्मक थे। इसमें बंगाल के इतिहासकार विशेष रूप से आगे थे। बंगाल में गांधी वादी नेतृत्व के प्रति गहरा संदेह शुरु से ही रहा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गांधी के पूर्व ही बंगाल में नई राजनीति शुरु हो चुकी थी और गांधी ने उस धारा को महत्त्व न देकर अपने अनुयायियों को लेकर जो राजनीति शुरू की उससे बंगाल राजनीतिक आंदोलन के केंद्र से हट गया। एम एन राय से लेकर बाद तक लगातार गांधी के ऊपर तीखे हमले बंगाल के इतिहासकारों में आम रहे। नेहरू के प्रति उससे भी अधिक तल्खी के साथ ये पेश आए। रणजीत गुहा भी इसी परंपरा में आते हैं।
1970 के शुरुआती दौर में गुहा एक वर्ष के लिए दिल्ली आए। वे गांधी पर एक अध्ययन करना चाहते थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात नक्सल आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों से हुई। गुहा को नक्सलवाद की हिंसा समर्थन योग्य लगी और उसके बाद वे राष्ट्रीय बुर्जुआ के प्रति आलोचनात्मक होने के साथ साथ इस पूरे मामले में एक ऐसे पर्स्पेक्टिव से जुड़े जिसमें औपनिवेशिक शासक बड़े अभिजन और भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ नेतृत्व छोटे अभिजन थे जो गैर अभिजन का शोषण करते थे। इस गैर अभिजन के लिए ग्रामशी का टर्म ‘सबाल्टर्न’ गुहा को उपयुक्त लगा और इस तरह से सबाल्टर्न हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना। उन्होंने इस काम में जिनको सहयोगी के रूप में पाया वे सभी युवा थे और गांधी नेहरू से चिढ़ने वाले थे।
नक्सलवाद के दौर में रणजीत गुहा के समर सेन संपादित फ़्रंटियर पत्रिका के आलेखों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सत्ता की हिंसा के प्रति प्रतिरोधी हिंसा की उसमें सीधे सीधे वकालत की गई है। इसके बाद आया इंदिरा विरोध का इमरजेंसी का दौर। यह गैर काँग्रेसवाद के उत्थान का समय था जिसने बौद्धिक जगत में कुछ इस तरह का माहौल रचा कि हरिशंकर परसाई जैसे लोगों को लगा कि कांग्रेस तो अब गई ! उस दौर के तुरंत बाद ही गुहा की सबसे महत्त्वपूर्ण किताब ‘एलीमेंट्री आस्पेकट्स ऑफ पेजेन्ट इन्सर्जन्सी’ आई। उसके बाद सबाल्टर्न हिस्ट्री के वॉल्यूम आने लगे। इसके छ: खंडों का सम्पादन गुहा ने बहुत मेहनत से किया।
इस बीच गुहा के लिए 1980 में ससेक्स के बाद कैनबरा में जाने का जो सुयोग लो ने बनाया उससे गुहा को बहुत सुविधा हुई। उनकी दूसरी पत्नी जो जर्मन एंथ्रोपोलोजिस्ट थीं , उनके साथ वे अगले पंद्रह साल कैनबरा में रहे। वहाँ उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं थी। वे अपना काम स्वतंत्रता के साथ करते रहे। इसी दौर में उनकी ख्याति अधिक हुई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सम्पादन का भार त्याग दिया। 1999 में वह आस्ट्रिया के एक जंगल के किनारे एक अपार्टमेंट में रहने लगे। वहीं 2023 की मई तक रहे।
1980 में गुहा की ख्याति इतनी तेजी से क्यों फैली इस पर ठहर कर विचार करना जरूरी है। 1980 के दशक में पोस्ट -कोलोनियल थ्योरी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। दुनिया भर में इस थ्योरी के मूल में यह था कि औपनिवेशिक शोषण असली नहीं है, उससे भी अधिक खतरनाक है यूरोपीय आधुनिकता जो सारी दुनिया में एक खास तरह की विचारधारा को फैलाकर विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक विशिष्टताओं को दबा देती है जिससे हम मानसिक रूप से गुलाम बन जाते हैं। जब औपनिवेशिक शासन खत्म हो जाता है तब भी यह गुलामी बनी रहती है।
यह एक बेहद मन भावन परियोजना थी जिसको लोगों ने इस आशा से स्वीकार किया कि इससे गुलाम हो गई जनता को उसकी खोई हुई सांस्कृतिक आवाज की पुनर्प्राप्ति का सुयोग प्राप्त होगा।
अस्सी और नब्बे के दशक में जब सांस्कृतिक पुनर्वास का यह स्वप्न बौद्धिकों को आधुनिकता विरोधी बना रहा था ,उसी समय क्रांतिकारी स्वप्न का बंध्याकरण कैसे हुआ यह एक बड़ा सवाल है। इस समय भारत के बौद्धिक दो भागों में विभक्त हो गए। वामपंथी कहे जाने वाले लोगों में भी एक तरह का विभाजन हो गया। एक तरफ वे लोग आए जो पोस्ट कोलोनियल स्वप्न के साथ खड़े थे और इस कारण से एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट के विरुद्ध थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जो इस वैश्विक प्रोजेक्ट को छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यह एक बेहद महत्त्वपूर्ण बहस थी जिसके फलितार्थ उस समय स्पष्ट नहीं हुए थे जब ये बहस चल रही थी। बहुत सारे प्रखर युवा इतिहासकारों -दीपेश चक्रवर्ती और ज्ञानेन्द्र पांडे जैसे लोग – जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे , अब एक नई दिशा में चल पड़े और उनके इस हृदय परिवर्तन से भारतीय अकादमिक परिदृश्य बदल गया। इस संदर्भ में यह याद किया जाना चाहिए कि एजाज अहमद क्यों ‘इन थियरी’ लिखकर एडवर्ड सईद के ऑरिएन्टलिज़्म का इतना तीखा विरोध कर रहे थे।
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से दृष्टव्य वे दो आलेख हैं जिन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बिपन चंद्र ने बीबलिओ पत्रिका में एक आलेख में एन्लाइटन्मन्ट प्रोजेक्ट पर एक लेख लिखा था। उसके अलावा इरफान हबीब ने शिलांग विश्वविद्यालय में जो भाषण दिया थे उसके अंतिम हिस्से में सबाल्टर्न हिस्ट्री की जो आलोचना की गयी थी उसको भी देखा जाना जरूरी है। लेकिन इससे भी दिलचस्प है सुमित सरकार का सबाल्टर्न प्रोजेक्ट से जुड़ना और फिर उससे छिटकना। अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक मॉडर्न इंडिया में सरकार ने गुहा के साथ 1977 की एक रात भर की गहन चर्चा का जिक्र किया है जिसने “उनके विचारों में कई परिवर्तन किए”। उसका प्रभाव सुमित सरकार पर जरूर पड़ा और वे भी सबाल्टर्न प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। लेकिन उन्होंने इसके दिशा को समझने के बाद इससे किनारा कर लिया। लेकिन तब तक सब सबाल्टर्न का प्रभाव भारतीय एकेडेमिया पर काफी पड़ चुका था।
आधुनिकता विरोध की आंधी इतिहास में कम साहित्य, समाज शास्त्र और अन्य विषयों पर अधिक पड़ी। एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की अकादमिक जगत में उपस्थित हो गई जो देश विदेश के संस्थानों में आधुनिकता विरोध में अपने अपने देश की सांस्कृतिक अस्मिताओं की खोज में लग गए। पाठकों को याद हो भारतीयता के पुनर्वास पर कितना उत्साह एक समय दिखलाई पड़ता था !
इस प्रक्रिया में रणजीत गुहा को जो यश और मान मिला उसके वे अधिकारी थे। वे उस दौर के थे जब क्रांति का स्वप्न जीवित था। वे इतिहास निर्माण के क्षेत्र से निकल कर इतिहास लेखन में आए थे। उनके अपने तर्क थे और उन्होंने अपनी एक पद्धति का निर्माण किया जिसमें इतिहास लेखन को सिर्फ इतिहासकारों के हवाले वे नहीं छोड़ सकते थे। युगीन यथार्थ को समझने के लिए वे इतिहास से अधिक प्रामाणिक कवि –लेखकों को मानने लगे थे। इसके संदर्भ को भी समझना जरूरी है। जो व्यक्ति मार्क्स के लेखन से इतना प्रभावित हो, वह क्यों कर हायडेगर तक पहुंचा? यह एक गंभीर चर्चा का विषय है। यह सवाल उन सबके लिए जरूरी है जो निर्मल वर्मा या रणजीत गुहा को समझना चाहते हैं। यहाँ उस विषय पर चर्चा का सुयोग नहीं है, बस इसे विचार बिंदु हेतु रख दिया जाना संभव है।
रणजीत गुहा से सीखने की सबसे बड़ी बात है उनका धीरज। वे आजीवन बिना किसी असिस्टेंट के काम करते रहे। एक ऐसा दौर था जब वह अपनी बौद्धिक तैयारी में थे ,वह सेमिनारों में अनुपस्थित से रहे। जर्नल में आलेख भी नहीं लिखे। बस कभी कभी समीक्षाएं लिखीं। रमाशंकर सिंह ने बहुत सही लक्षित किया है कि समीक्षाएं और भूमिकाएं भी उनकी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे लिखने के इस धीरज ने ही गुहा को कई दिशाओं में जाने दिया। उनके धीरज का एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। वे जब किसी छात्र से तर्क करते थे तो उससे आशा करते थे कि वह तुरंत उनकी बात न माने ! वह ये भी सलाह देते थे कि अगर किसी को समझना हो तो वह जिसको पढ़ कर सोच रहा है उसको भी देखा जाना चाहिए। वे अपेक्षा रखते थे कि फूको और डेरीदा को समझने वाला हाइडेगर और नीत्से को पढ़कर समझे, तभी वह तह में जा सकेगा। इतना धीरज बौद्धिक क्षेत्र में आज विरल है।
अंतिम बात : गुहा ने अंत में अंग्रेजी में लिखना छोड़ दिया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। वे अपने कई साक्षात्कारों में इस बात को रखते हैं कि वे सिर्फ बांग्ला में ही अपने को सहज पाते हैं। यह कैसे हुआ होगा ? यह एक संदेश गुहा भारत के बौद्धिकों को दे गए हैं कि बौद्धिक आखिरकार अपनी भाषा में ही अवस्थित होता है। दूसरी भाषा का सम्यक ज्ञान हो तो अच्छी बात है, लेकिन सृजन का संसार अपनी भाषा में ही सम्पूर्ण रूप में प्रकट होता है। हायडेगर के अनन्य शिष्य गादामर ने अपने गुरु से यही शिक्षा पाई थी और इसे वह जीवन भर दोहराते रहे कि जीवन हम अपनी भाषा में ही जीते हैं।
दुर्भाग्य से रणजीत गुहा के प्राइवेट पेपर्स आस्ट्रिया के एक संस्थान को मिलेंगे। अगर वे इसे किसी भारतीय संस्थान को दे देते तो हम लोग इस चिंतक की धारा के विभिन्न पड़ावों के बारे में और अधिक जान पाते।
उनके बांग्ला लेखन पर दो वॉल्यूम में जो सामग्री छपी है उसका मूल्य दो हजार रुपये है और पाठक उसकी तलाश में बार बार दुकान पर जाकर निराश होते थे। मुझे एक दुकान में यह मिली। मैंने खरीदना चाहा, लेकिन दो हजार देखकर छोड़ दिया। इसका उल्लेख अपनी एक शोध छात्रा से किया। उसने कहा प्लीज जैसे भी हो उसे खरीद लें। कहीं नहीं मिल रही ! वह दो तीन बार निराश होकर लौट चुकी थी। फिर, मुझे उसी दिन जाकर खरीदना पड़ा। हिन्दी भाषी समाज के लेखक के लिए यह कुछ अविश्वसनीय जैसी घटना थी।
गुहा साहब के जीवन से आगे की पीढ़ी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे हम अणु बम के लिए आइंस्टीन को दोष नहीं देते वैसे ही उनके बौद्धिक प्रयास को क्रिटिकल मार्क्स वादी धारा या पोस्ट कोलोनीयलिज़्म द्वारा अपने तरीके से इस्तेमाल किए जाने के लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता।