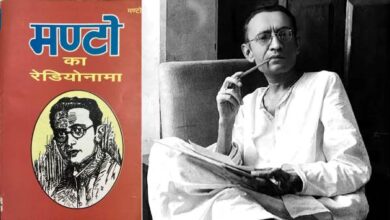राधा बाबू का कहना है ..
- राजेश कुमार
वैसे अकादमिक नाम तो डॉ. राधाकृष्ण सहाय है पर रंगकर्म से जुड़े लोग उन्हें राधा बाबू के नाम से ही संबोधन करते हैं। वो भी सामने नहीं, उनके पीछे। क्योंकि एक तो उनसे उमर में कम है, दूसरे शिष्य भी। विश्वविद्यालय के छात्र व प्रोफेसर उन्हें सर ही कहते हैं। रंगकर्म से जुड़े लोग राधा बाबू का संबोधन इसलिए भी करते हैं कि उनका व्यवहार कभी पारंपरिक गुरु- शिष्य वाला नहीं रहा है। बराबर की हैसियत से बात करते हैं। प्रायः विश्वविद्यालय के माहौल में तर्क करने की परंपरा कम ही रहती हैं। गुरु हमेशा से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए भला उनकी स्थापना को काटने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? लेकिन राधा बाबू के यहाँ अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता रहती है, हरेक को अपनी बात बेफिक्र कहने की छूट है और ये माहौल आज ही नहीं, तब से है जब जर्मन में कुछ वर्ष गुजार कर भागलपुर आये थे। जब रचनात्मकता के स्तर पर जोरदार ढंग से सक्रिय थे, वैचारिक रूप से प्रखर होने के कारण कला-साहित्य को नये अंदाज में देख-परख रहे थे। छोटी खंजरपुर का उनका आवास उन दिनों शाम को साहित्य, रंगमंच और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े एक्टिविस्टों के लिए अड्डा था। और वो सिलसिला आज भी महेश अपार्टमेंट के उनके फ्लैट पर यथावत है। कोई शाम नहीं गुजरती जब कोई न कोई राधा बाबू के ड्राईंग रूप में बहस मुहाविसा करते न मिल जाता हो। आज राधा बाबू की नजर भले कम हो गयी हो, सुनना भी क्षीण हो गया हो लेकिन समय पर उनकी नजर उतनी ही तीक्ष्ण है। अखबार या पत्रिका का कोई हर्फ उनके मैग्नीफाइंग लेंस से शायद ही छूट पाता हो। जहां किसी शब्द पर कन्फ्यूजन होता है, शब्दकोश को उलटने-पलटने लगते हैं, शारलैक होम्स की तरह लेंस से ढूंढ ही निकालते हैं। रोज कोई न कोई उनके यहां धमकता ही रहता है। कोई अपनी कविता सुना रहा है तो कोई अपनी कहानी पर प्रतिक्रिया ले रहा है तो कोई वर्तमान राजनीति व धर्म पर उनके साथ उलझा हुआ हैं। भले वे मूलरूप से छपरा के रहने वाले हो लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने भागलपुर के नाम कर दी है। यहीं भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे और जो भी सृजन किया, यही की जमीन पर रहकर किया। अपने आप को वे लेखक से ज्यादा शिक्षक मानते रहे हैं। और शिक्षक के रूप में छात्रों के बीच हमेशा लोकप्रिय भी रहे हैं। उनके शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का ही ये परिणाम है कि उनके शिष्य आज देशभर में अकादमिक और साहित्यक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं और उन्हीं की परम्परा को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उम्र का असर भले उन पर दीखने लगा है लेकिन विचार के स्तर पर एक्टिव है। आज 85 वर्ष होने के बावजूद उनकी रचना हंस, वागर्थ, पाखी जैसी पत्रिकाओं में दिखती रहती है, मानो कह रही हो कि अभी भी मुझे कुछ कहना है। विचार शेष नहीं हुए हैं। आज जो हालात है उसको देखकर केवल चुप नहीं रहना है। बिस्तर पर लेटे-लेटे निहारना नहीं है, बजावते हस्तक्षेप करना है।
यहीं भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे और जो भी सृजन किया, यही की जमीन पर रहकर किया। अपने आप को वे लेखक से ज्यादा शिक्षक मानते रहे हैं। और शिक्षक के रूप में छात्रों के बीच हमेशा लोकप्रिय भी रहे हैं। उनके शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका का ही ये परिणाम है कि उनके शिष्य आज देशभर में अकादमिक और साहित्यक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं और उन्हीं की परम्परा को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उम्र का असर भले उन पर दीखने लगा है लेकिन विचार के स्तर पर एक्टिव है। आज 85 वर्ष होने के बावजूद उनकी रचना हंस, वागर्थ, पाखी जैसी पत्रिकाओं में दिखती रहती है, मानो कह रही हो कि अभी भी मुझे कुछ कहना है। विचार शेष नहीं हुए हैं। आज जो हालात है उसको देखकर केवल चुप नहीं रहना है। बिस्तर पर लेटे-लेटे निहारना नहीं है, बजावते हस्तक्षेप करना है।
भले अकादमिक लोग उन्हें एक बेहतर शिक्षक के रूप में मानते हो, कहानी-कविता के लोग उन्हें एक सफल कथाकार व भाषाशास्त्री सिद्ध करते हो लेकिन उनकी महारत जो है, सर्वाधिक नाट्य क्षेत्र में है। उनके व्यक्तित्व को देखकर कोई भी छूटते कह देगा कि ये नाटक से जुड़े होंगे। उनके बोलते का अंदाज, चलने का अंदाज, पान को मुंह में हौले से दबाकर बातों को रखने का जो सलीका है, उसमें साहित्य की स्वाभाविकता कम रंगकर्म का वो चमकता भाव आंखों से छुपाये नहीं छिपता है। आंखों में जो मुस्कान होती है, उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। कई सबटेक्सट अंर्तनिहित होते हैं।
बकौल राधा बाबू, वे लम्बे समय तक प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा से जुड़े रहे हैं। और इस बात को वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं। अपने इन्टरव्यू और विचार-विमर्श में चर्चा भी करते रहते हैं। इस चर्चा के बीच कहीं न कहीं उनका दर्द भी उभर पड़ता है। लाजिमी भी हैं जो शख्स इस आंदोलन से प्रारम्भिक दौर से जुड़ा हो, उसे बाद के दिनों में तवज्जो न दी जाए तो दर्द तो सालेगा ही। अपने मुंह से भले राधा बाबू इस प्रतिबद्धता की चर्चा करते हो, इन संगठनों ने कभी किसी मौके पर याद करने की जरा भी मेहरबानी नहीं की। शायद एक कारण यह भी हो कि वे उस मिजाज के हैं भी नहीं जिसकी वजह से लोग पार्टी हो या सांस्कृतिक संगठन ठेल ठाल कर स्पेस बना लेते हैं। खुले मिजाज के हैं और किसी भी ताजी हवा के नथुनों में भर लेने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। इन्हें जो उचित लगना है, बेबाक कह देते हैं। जो लिखना सही जान पड़ता है, बिना किसी दबाव के अभिव्यक्त कर देते हैं। लिखने में इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, न ज्यादा लिखना इनकी आदत में है। जिस तरह इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हैं, साहित्य-सृजन भी उसी के अनुकूल है। नाटक में जमा पूंजी के नाम पर दो मुकम्मल नाटक और आधा दर्जन एकांकी हैं। इसके अलावा नाटय सिद्धांत पर कई लेख हैं जो संकलित हैं, तो कुछ इधर-उधर बिखरी हुई। ’अतः किम्’ इनका पहला नाटक है, ’खेल जारी-खेल जारी ’इसके बाद का है। बीच-बीच में जरूरत के मुताबिक लिखते एकांकी रहे हैं, जो ‘हे मातृभूमि’, ’रंग दृष्य’ के नाट्य संग्रह में संकलित हैं। हिन्दी की कई कहानियों तथा विदेशी नाटकों का अनुवाद अपनी नाट्य संस्था के लिए किया है जिसका मंचन तब कराया जब भागलपुर में बांग्ला थियेटर के अलावा हिन्दी रंगमंच का कहीं नामोनिशान न था। न इस तरह की यथार्थवादी धारा से लोग परिचित थे। सन् 1960 में जब गुलेरी जी की कालजयी कहानी ’उसने कहा था ’ का नाट्यरुप रंगमंच पर उन्होंने प्रस्तुत तो मात्र उस एक मंचन ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी बल्कि नगर में रंगमंच आंदोलन को खड़ा कर दिया। उन्होंने उस समय के युवा कलाकारों को संगठित कर नगर में शौकिया नाट्य संस्था ’अभिनय भारती’ की स्थापना की जिसके अंर्तगत ’एलिस इन वण्डर लैण्ड’ , ’ह्यूअर्स ऑफ़ कोल’, ’विश्प्स कैण्डिल स्टिक’ , ’आकाशदीप’ , ’नाटक का अंत’, ’जय या पराजय ’ ’मरीचिका’, ’मिस्टर अभिमन्यु’, ’गृह प्रवेश’, ’लाल कनेर’, ’साहब ,बीबी गुलाम’, ’कांचन रंग’ जैसे चर्चित नाटकों का सफन मंचन हुआ जिसके साथ वे लेखक, रुपांतरकार और निर्देशक के रुप में जुड़े रहे। कई दशकों तक राधा बाबू वहां के सांस्कृतिक आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। भले आज की पीढ़ी इस इतिहास को न जानती हो, महानगरों के समीक्षक इस योगदान से परिचित न हो, रंगमंच के किसी दस्तावेज में उल्लेख जानबूझ कर या भूलवश छूट गया हो लेकिन उन्होंने रंगमंच पर जो लिखा है, अभिमत प्रकट किया है, उसे बिसराना मुश्किल है। नुक्कड़ नाटक आंदालन के दौर में जब एक ओर महानगरों के आचार्यों, पंडितों, आलोचकों, अभिजान्य रंगकर्मियों ने इसे फूहड़, गंवार कह कर उपेक्षा किया था तो राधा बाबू ने नुक्कड़ नाटक का जम कर पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ या ’जनता का नाटक’ कहीं से आयातित होकर नहीं आया है बल्कि भारतीय रंगमंच की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के रूप में समाज के बीच उपस्थित हुआ है। ये हमने युगीन लोक जीवन की उपज है। इनमें लोक जीवन की आकांक्षायें हैं। यह बात दीगर है कि हमारे समाज के युगीन जीवन में राजनीति के विरोधाभासों का दलदल है इसलिए ये नाटक भी इसी दलदल में फंसे दीखते हैं। फिर भी यह स्वीकारना ही होगा कि इन नाटकों के सड़क पर उतरने के पीछे कोई राजनीतिक दुरभिसंधि नहीं है, बल्कि यदि कुछ है तो वह है भारतीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृति परिवेश की मांग। इसलिए भारतीय रंगकर्म के संदर्भ में नाटक के इस रूप को बड़े गंभीरता से लेना होगा ताकि इसके जरिए राजनीति से लेकर कला और संस्कृति तक भी लड़ाई लड़ी जा सके।
सन् 1960 में जब गुलेरी जी की कालजयी कहानी ’उसने कहा था ’ का नाट्यरुप रंगमंच पर उन्होंने प्रस्तुत तो मात्र उस एक मंचन ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी बल्कि नगर में रंगमंच आंदोलन को खड़ा कर दिया। उन्होंने उस समय के युवा कलाकारों को संगठित कर नगर में शौकिया नाट्य संस्था ’अभिनय भारती’ की स्थापना की जिसके अंर्तगत ’एलिस इन वण्डर लैण्ड’ , ’ह्यूअर्स ऑफ़ कोल’, ’विश्प्स कैण्डिल स्टिक’ , ’आकाशदीप’ , ’नाटक का अंत’, ’जय या पराजय ’ ’मरीचिका’, ’मिस्टर अभिमन्यु’, ’गृह प्रवेश’, ’लाल कनेर’, ’साहब ,बीबी गुलाम’, ’कांचन रंग’ जैसे चर्चित नाटकों का सफन मंचन हुआ जिसके साथ वे लेखक, रुपांतरकार और निर्देशक के रुप में जुड़े रहे। कई दशकों तक राधा बाबू वहां के सांस्कृतिक आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। भले आज की पीढ़ी इस इतिहास को न जानती हो, महानगरों के समीक्षक इस योगदान से परिचित न हो, रंगमंच के किसी दस्तावेज में उल्लेख जानबूझ कर या भूलवश छूट गया हो लेकिन उन्होंने रंगमंच पर जो लिखा है, अभिमत प्रकट किया है, उसे बिसराना मुश्किल है। नुक्कड़ नाटक आंदालन के दौर में जब एक ओर महानगरों के आचार्यों, पंडितों, आलोचकों, अभिजान्य रंगकर्मियों ने इसे फूहड़, गंवार कह कर उपेक्षा किया था तो राधा बाबू ने नुक्कड़ नाटक का जम कर पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ या ’जनता का नाटक’ कहीं से आयातित होकर नहीं आया है बल्कि भारतीय रंगमंच की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के रूप में समाज के बीच उपस्थित हुआ है। ये हमने युगीन लोक जीवन की उपज है। इनमें लोक जीवन की आकांक्षायें हैं। यह बात दीगर है कि हमारे समाज के युगीन जीवन में राजनीति के विरोधाभासों का दलदल है इसलिए ये नाटक भी इसी दलदल में फंसे दीखते हैं। फिर भी यह स्वीकारना ही होगा कि इन नाटकों के सड़क पर उतरने के पीछे कोई राजनीतिक दुरभिसंधि नहीं है, बल्कि यदि कुछ है तो वह है भारतीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृति परिवेश की मांग। इसलिए भारतीय रंगकर्म के संदर्भ में नाटक के इस रूप को बड़े गंभीरता से लेना होगा ताकि इसके जरिए राजनीति से लेकर कला और संस्कृति तक भी लड़ाई लड़ी जा सके।
विदेशों में सालों साल रहने के बावजूद राधा बाबू को अपना कर्मस्थल ही भाता है। वे बातों बात में अक्सर कहते भी रहते हैं, खांटी आदमी हूं… अपनी जमीन को छोड़कर कहीं जाना वाला नहीं हूं। देखने में जितना भी आधुनिक हैं, अंदर से उतने ही देशज हैं। भोजपुरी जमीन को छोड़े अरसा हो गया पर भोजपुरी जुबान अब भी बरकरार रहती है। और कभी-कभी कह भी देते हैं कि भोजपुरिया आदमी कभी डरता नहीं है। और वास्तव में वे कभी डरते भी नहीं हैं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या साहित्यिक, जो उनका दिल कहने को होता है, कह देते हैं। उनके कहने के पीछे उनका एक तर्क भी होता है। बादल सरकार के ’थर्ड थिएटर’ पर शायद ही किसी रंग समीक्षक ने इस नजरिये से सोचा होगा जैसा राधा बाबू ने कहा है। उनका कहना है कि यह अवधारणा चाहे जितनी भी ताजी हो लेकिन यह मूलतः एक अभिाजत्य अवधारणा है जो अन्ततः मध्यवर्ग की मानसिकता से उपजी है। ’एवम इंद्रजीत’ से ’जुलूस’ या ’भोमा’ तक के नाटकों में नाटककार की मुठ्ठी में भारतीय लोक जीवन का सारभूत अंग कहीं नहीं है। अगर कुछ है तो लोकजीवन का धुंआ है- एक गर्म मस्तिष्क की वायवी सृष्टि है। बादल सरकार ‘सिनथीसिस’ की खोज करते हुए अपने नाटकों में केवल भाषा स्तर का ’कोलाज’ तैयार कर पाते है जब कि इसके विपरीत नाटक में जीवन स्थितियों का कोलाज तैयार होना चाहिए था। शायद इसीलिए इनके नाटकों का दर्शक नाटक देखने के बाद हतप्रभ और ठगा-ठगा सा रह जाता है। न तो जीवन स्थितियां उसके हाथ आती है और न जीवन के प्रति उसका कोई स्पष्ट मत बन पाता है। सच कहा जाय तो बादल सरकार के नाटक ‘एब्सर्ड’ नाटक की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते। क्योंकि उनका कहना है कि ‘थीसिस’ से ‘ऐन्टीथीसिस’ या कि ‘सिनथीसिस’ तक की विकास यात्रा एक स्वाभाविक और प्रकृत प्रक्रिया होती है, जो भारतीय रंगमंच के संदर्भ में कभी घटित ही नहीं हुई है। उधार लिए गए वर्तमान नागर थिएटर साम्राज्यवादियों द्वारा हमारे समाज पर बलात् लादे गए थे, आरोपित किए गए थे। वर्तमान नागर थिएटर हमारे लोक जीवन और लोक नाटकों का स्वाभाविक विकास नहीं था इसलिए वर्तमान नागर विस्तार रूप को ‘ऐन्टीथीसिस’ कैसे माना जा सकता है? इतना तो साफ है कि चूंकि नाटक का वर्तमान नागर रूप हमारे लोक मानस की उपज नहीं इसलिए इस वर्तमान रूप को हमारे समाज के विकास का प्रतिफल नहीं माना जा सकता और इसीलिए इस संदर्भ में ‘थीसिस’, ‘एन्टीथीसिस’ और ‘सिनथीसिस’ की बात भी उतनी ही काल्पनिक, रूपानी और बेमानी होगी जितनी कि हमारा नागर थिएटर रूप है।
न तो जीवन स्थितियां उसके हाथ आती है और न जीवन के प्रति उसका कोई स्पष्ट मत बन पाता है। सच कहा जाय तो बादल सरकार के नाटक ‘एब्सर्ड’ नाटक की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते। क्योंकि उनका कहना है कि ‘थीसिस’ से ‘ऐन्टीथीसिस’ या कि ‘सिनथीसिस’ तक की विकास यात्रा एक स्वाभाविक और प्रकृत प्रक्रिया होती है, जो भारतीय रंगमंच के संदर्भ में कभी घटित ही नहीं हुई है। उधार लिए गए वर्तमान नागर थिएटर साम्राज्यवादियों द्वारा हमारे समाज पर बलात् लादे गए थे, आरोपित किए गए थे। वर्तमान नागर थिएटर हमारे लोक जीवन और लोक नाटकों का स्वाभाविक विकास नहीं था इसलिए वर्तमान नागर विस्तार रूप को ‘ऐन्टीथीसिस’ कैसे माना जा सकता है? इतना तो साफ है कि चूंकि नाटक का वर्तमान नागर रूप हमारे लोक मानस की उपज नहीं इसलिए इस वर्तमान रूप को हमारे समाज के विकास का प्रतिफल नहीं माना जा सकता और इसीलिए इस संदर्भ में ‘थीसिस’, ‘एन्टीथीसिस’ और ‘सिनथीसिस’ की बात भी उतनी ही काल्पनिक, रूपानी और बेमानी होगी जितनी कि हमारा नागर थिएटर रूप है।
शायद ही इस नजरिये से महानगरों के नाट्य समीक्षकों ने बादल सरकार की इस अवधारणा को देखा हो। छोटे शहर में राधा बाबू रह जरूर रहे हैं, लेकिन वे जो सोच रहे हैं कही आगे का सोच रहे हैं। भले बड़े बड़े सेमिनारों, नाट्य संस्थानों में प्रायोजित व्याख्यान न दिये हो, लेकिन वे आज भी जहां से अपनी बाते रख रहे हैं, खारिज करना आसान नहीं है। आज जहां शहरों को स्मार्ट शहर में तब्दील करने की होड़ मची है, जिधर जाइए सड़क को चैड़ी कर, पुरानी ईमारतों को ढाह कर नये खड़े किये जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी दूकानों, शोरूम खुलते जा रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह मॉल खोले जा रहे हैं, रंगकर्म की कोई विशेष संभावनाएं सत्ता पक्ष की तरफ से आशान्वित नहीं है। राजनीति के लिए भी रंगमंच कोई वोट उगाहने का जरिया नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां आज गांव का रंगमंच दम तोड़ दिया है, शहरी रंगमंच सरकारी अनुदान और कॉरपोरेट के फेंके गये टुकड़ों का मोहताज है, राधा बाबू निराश नहीं होते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जहां आंखे साथ छोड़ने लगी है, वे हिम्मत नहीं हार रहे हैं। शहर का जो भी युवा सक्रिय रंगकर्मी आता है, उसे जड़ से जुड़ने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि भारतीय रंगमंच की पहचान हमारी जमीन से ही होगी। जो जमीन को जितना जानेगा, उसका रंगमंच उतना ही समृद्ध होगा। वे रंगमंच को जनसाधारण तक पहुंचाने पर जोर देते हैं। कृत्रिम साधनों का कम से कम प्रयोग करने के लिए कहते हैं। उनका कहना है ज्यों नाटक महंगा किया, खर्चीला बनाया, जनता से दूर होता जायेगा। बाजार हावी हो जायेगा। और ज्यों नाटक के अंदर पूंजी का समावेश हुआ कि वह हाथ से सरककर किसी और के पास चला जायेगा। फिर उस पर आपका कोई वश नहीं चलेगा। वह किसी और के द्वारा संचालित होता रहेगा और आप केवल

देखते रह जायेंगे।
राधा बाबू का ड्राइंग रूम में फ्रांस के जैकोबे क्लब से कम नहीं है। उनके यहां कला-साहित्य से जुड़े लोग तो आते ही है, राजनीतिज्ञ और उसमें विभिन्न धारा के लोगों के आने जाने का सिलसिला अभी भी बरकरार है। चाय की चुस्कियों के साथ यूर्निवसिटी की पॉलिटिक्स पर बात होती है तो बहस के जाल से लालू, नीतिश, मोदी भी बच नहीं पाते हैं। लोहिया के मुरीद होने के कारण वर्ण व्यवस्था पर तब से सवाल उठाते रहे हैं जब दलित विमर्श का हिन्दी प्रदेश में कोई चर्चा भी नहीं थी। वे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था को एक विकट समस्या मानते हैं। उनका कहना है इसे नजरअंदाज कर देश में जो लोग वर्ग संघर्ष का सपना देख रहे हैं, वे भ्रम में हैं। वे भारतीय समाज की बेचैनी को दूर करने के लिए नाटक के एक ऐसे रूप की मांग करते हैं जो परम्परागत लोक जीवन से उद्भूत हो। इसलिए वे नाटकों में पात्र की जगह समूह या लोग पर जोर देते हैं। शब्दों की अपेक्षा अभिनय को प्रमुखता देते हैं। उनका नाटक ’खेल जारी- खेल जारी’ उनकी अवधारणा व सोच का एक प्रबल उदाहरण है। उन्हें इस बात को लेकर कतई चिंता नहीं है कि इस नाट्यदृष्टि पर आचार्य, पंडित आलोचक व अभिजत्य रंगकमी क्या कहेंगे? कोई उन्हें गँवार, फूहड़ कहे तो वे डरनेवाले नहीं है, न अपने फैसले से पीछे हटने वाले हैं। उनका मानना है, समय के साथ कौन है, समाज के पक्ष में कौन खड़ा है, ये आने वाला वक्त बतायेगा। वही तय करेगा कि जनता का नाटककार कौन है? किसके सरोकार जनता के पक्ष में थे और किसके सत्ता व्यवस्था के।
राधा बाबू का मानना है कि, रंगमंच से बढ़कर लोक मानस को प्रभावित करने का कोई दूसरा जीवंत माध्यम नहीं। वास्तव में नाटक सृष्टि की प्रतिसृष्टि है। सृष्टि तथा स्थिति, नाटक के दो छोर है। विधाता जो निर्माण नहीं कर सकता, विधाता जो लोक चेतना में बदलाव नहीं ला सकता उसे नाटक कर सकता है।
जो लोग हिन्दी में इस बात का रोना रोते हैं कि नाटक लिखा नहीं जा रहा है या हिन्दी में रंगमंच योग्य नाटक ही नहीं है, इसलिए विदेशी या हिन्दीतर भाषाओं के नाटकों को हाथ में लेना पड़ता है, उनको आड़े हाथों लेते हुए राधा बाबू का कहना है कि पूरी दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में जिस तरह आये दिन घटनाएं घट रही है, उसे आंख बंद कर नहीं देखा जा सकता हैं। यह बदलाव जितना स्थूल स्तर पर है उतना ही सूक्ष्म स्तर पर। तेज ताप या अधिक बारिश के कारण जिस तरह पृथ्वी के ऊपर/नीचे वाले जीव उभचुभ करते हुए कसमसा रहे हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक खांचों के भीतर आज उजबुज करने लगी है और आज का आदमी मुक्ति की खोज में तरह-तरह की राहों को खोज कर रहा है। कला-साहित्य की तरह नाटक भी इसी दिशा में है और ये तलाश खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी जारी है।

लेखक धारा के विरुद्ध चलकर भारतीय रंगमंच को संघर्ष के मोर्चे पर लाने वाले अभिनेता,निर्देशक और नाटककार जो हाशिये के लोगों के पुरजोर समर्थक हैं. +919453737307 rajeshkr1101@gmail.com
.
.
.
सबलोग पत्रिका को फेसबुक पर पढने के लिए लाइक करें|