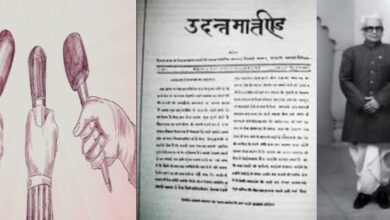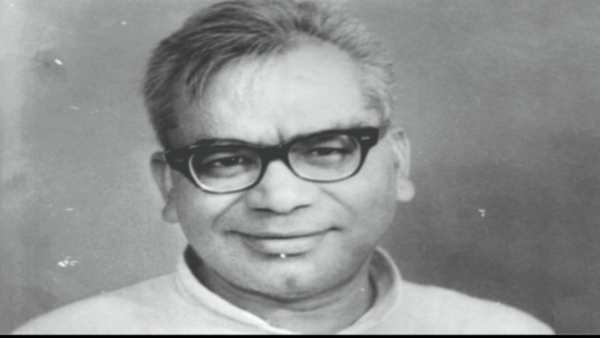हिन्दी सिनेमा का सच
सिनेमा सम्प्रेषण का एक शक्तिशाली माध्यम है, ऐसा शायद इसलिए भी कि इसमें एक साथ अपने श्रेष्ठ रूप में कई कलाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति है। लेखन, अभिनय, निर्देशन, संगीत-संयोजन, गायन, संवाद-अदायगी, सिनेमेटोग्राफी,साज-सज्जा, वेश-भूषा, दृश्यांकन, एडिटिंग आदि मिलकर इसे एक आकर्षक विधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज के फिल्मों की खासियत यह हो गयी है कि इसका प्रदर्शन एक ही समय में तमाम सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों में सम्भव हो गया है। कहना गलत नहीं होगा कि अब के उच्च तकनीक, व्ही एफ एक्स आदि विशेषताओं ने सिनेमा को जो अद्वितीयता प्रदान की है वह अन्य कला रूपों में दुर्लभ तो है ही, इसका सामाजिक प्रभाव भी सबसे ज्यादा है।
मनोरंजन के ही एक माध्यम के रूप में सिनेमा की शुरूआत हुई थी, शायद इसीलिए आज भी इससे मनोरंजन कर वसूला जाता है। सन् 1931 में बनी ‘आलमआरा’ पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें आवाज थी। 18 वर्षों के मूक फिल्मों के दौर के बाद सच्चे अर्थों में हिन्दी फिल्में आवाज दे रही थीं। पहले की तुलना में अब सिनेमा विषय को लेकर ज्यादा सचेत हो गया था।
यही वह दौर था जब अँग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय समाज एकजुट हो रहा था। इस एकजुटता को राजनीतिक स्वरुप देने के लिए पत्रकारिता, साहित्य कला, रंगकर्म और सिनेमा सभी विधाओं की सक्रियता अँग्रेजों के खिलाफ अभिकेन्द्रित थी। राजनीति में जो काम महात्मा गाँधी, लाला लाजपतराय कर रहे थे, साहित्य में वही काम रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चन्द्र, प्रेमचन्द्र और सुदर्शन कर रहे थे। यह सिर्फ संयोग नहीं था कि इन्हीं साहित्यकारों की रचनाओं पर उन दिनों फिल्में भी बन रही थीं।

‘शतरंज के खिलाडी’, ‘मंगल पाण्डेय: दि राइजिंग’, ‘जूनून’ और ‘झांसी की रानी’ जैसी फिल्मों का निर्माण भले भारत की आजादी के बाद हुआ लेकिन इनके कथानक 1857 के आसपास की घटनाओं पर केन्द्रित हैं। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम (जिसमें हिन्दू मुसलमान एक साथ मिलकर अँग्रेजों से लड़े थे) के बाद ही अँग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के काम में तेजी लायी। अँग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति कामयाब हुई। भारत और पाकिस्तान बँटवारे के साथ ही आजाद हुए। बँटवारे और दंगे के अवसाद ने दोनों जगह आजादी के जश्न को फीका कर दिया। आजादी के बाद की फिल्मों में नयी दुनिया और नया समाज बनाने का सपना व्यक्त हुआ है तो विभाजन की त्रासदी से भी यह मुक्त नहीं रही है।
छठे और सातवें दशक में हिन्दी सिनेमा ने सामाजिक मूल्य और रचनात्मकता के सन्दर्भ में नयी ऊँचाई हासिल कर ली थी। दहेज, आवारा, बूटपालिश, जागते रहो, मदर इण्डिया, आनन्द मठ, बैजू बावरा, मुगले-आजम जैसी फिल्मों ने सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं को अपना विषय बनाया। इसलिए यह अकारण नहीं कि एक विशाल दर्शक वर्ग पर हिन्दी सिनेमा का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बढ़ गयी।
फिल्म निर्माण का ढाँचा ही ऐसा है कि यह पैसे वालों का माध्यम बन गया। इसे दूसरे तरीके से यूँ भी कहा जा सकता है कि चूँकि फिल्म एक सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव और इसकी ताकत अपार है, इसलिए इस पर सत्ता वर्ग और पैसे वालों की नजर पहले से ही रही है। इसलिए यह अनायास नहीं हुआ कि पूँजी और पैसे का वर्चस्व फिल्म पर बढ़ता गया। जानबूझकर इसे इतना खर्चीला बनाया गया कि यह प्रभु वर्ग के हाथों में ही रहे। नायक नायिकाओं की ऐसी छवि गढ़ी गयी कि उन्हें साधारण मनुष्य की कोटि में रहने ही नहीं दिया गया। जिस देश के सत्तर प्रतिशत लोग बीस रुपये रोजाना पर गुजर करने के लिए विवश हो उस देश में किसी अभिनेता या अभिनेत्री का एक फिल्म का पारिश्रमिक करोड़ों रुपये में हो, यह अन्याय नहीं तो और क्या है? कहते हैं कि इस देश में सबसे अधिक काला धन फिल्मों में और भवन निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। अभिनेताओं की जब भगवान की तरह पूजा होने लगे तो जनचेतना पर शक होना स्वाभाविक है।

सिनेमा के सन्दर्भ में यह एक स्वाभाविक सवाल बनता है कि कोई नायक फिल्म से बड़ा क्यों हो जाता है? फिल्म तकनीक का माध्यम है और उसका नियन्त्रण निर्देशक के पास रहता है लेकिन वह जानी जाती है अभिनेताओं के नाम से, दूसरी तरफ नाटक अभिनेताओं का माध्यम है लेकिन वह निर्देशक के नाम से जाना जाता है। दरअसल परदे पर अभिनेताओं की मिथकीय महानायकत्व की जो अभिरचना होती है वह दर्शकों के दिल और दिमाग पर स्थायी घर बना लेती है और ऐसे करोड़ों घरों पर ये नायक राज करते हैं।
पूँजी के प्रभाव और प्रकोप के बावजूद हिन्दी सिनेमा में हमेशा एक धारा ऐसी रही है जो सामाजिक प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक मूल्यों से लैश रही है। यह धारा कभी समानान्तर सिनेमा तो कभी नया सिनेमा, कभी कला सिनेमा या प्रतिरोध का सिनेमा के नाम से जानी पहचानी जाती है। इस सन्दर्भ में 1969 में बनी तीन फिल्मों-भुवनशोम (बनफूल के उपन्यास पर मृणालसेन द्वारा निर्देशित), सारा आकाश (राजेन्द्र यादव के उपन्यास पर बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित) और उसकी रोटी (मोहन राकेश की कहानी पर मणि कौल द्वारा निर्देशित) का जिक्र जरूरी है। भुवनशोम के पहले मृणाल सेन बांग्ला में कई फिल्में बना चुके थे। चूंकि मृणाल सेन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरूआत ‘कलकत्ता फिल्म स्टूडियो’ में बतौर ओडियो टेक्नीशियन की थी इसलिए फिल्म निर्माण में तकनीकी तौर पर वे ज्यादा दक्ष थे।
यह फिल्म बंगाली भद्र समाज में व्याप्त अंग्रेजियत पर चोट करती है। इस फिल्म में अभिनय, छायांकन, सम्पादन और साउण्ड ट्रैक, जिस तरह से सन्तुलित था उसने इस फिल्म को ऐतिहासिक बना दिया। ‘फिल्म वित्त निगम’ से मिले ऋण से यह फिल्म बनी थी इसलिए इसका बजट भी सामान्य था। लागत, विषयवस्तु, तकनीक और दर्शकों की स्वीकार्यता के सन्दर्भ में यह एक अभूतपूर्व फिल्म थी। इसलिए समानान्तर सिनेमा का इसे प्रस्थान बिन्दु कहा जा सकता है। बाद में श्याम बेनेगल, प्रकाश झा, गौतम घोष और गोविन्द निहलानी जैसे फिल्मकारों ने भी प्रतिबद्ध सिनेमा की दिशा में सार्थक और महत्त्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया। दलित चेतना को केन्द्र में रखकर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन प्रेमचन्द की कहानी ‘सद्गति’ पर इसी नाम से सत्यजित रे ने 1981 में जो फिल्म बनायी है वह मील का पत्थर साबित हुई है। किसी साहित्यिक कृति के फिल्मी रूपान्तरण का ऐसा सटीक और सुन्दर उदाहरण कोई दूसरा नहीं दिखता।

1990 के बाद नयी आर्थिक नीति और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। साहित्य, पत्रकारिता और संस्कृतिकर्म सब पर इसका असर पड़ा। इसके पक्ष और विपक्ष में बुद्धिजीवी भी बँट गये। हिन्दी सिनेमा पर भी इसका असर होना था और वह हुआ। ऐसा नहीं कि विचार, मूल्यों और सामाजिक चेतना की चिन्ता से आज की फिल्में बिल्कुल खाली हैं, आज भी ‘भीड़’ और ‘कटहल’ जैसी फिल्में बन रही हैं, जो कम पूँजी की फिल्म होकर भी संदेश देने का माद्दा रखती है; लेकिन पिछले तीन दशकों में देश में आर्थिक विचारधारा और उसके स्वरूप में आए परिवर्तन ने जिस नकली और उपभोक्तावादी समाज का निर्माण किया है, फिल्में उनके प्रभाव से अछूती नहीं हैं। इसलिए आज फिल्मों में समाज को लेकर रचनात्मकता और सौहाद्र की चिन्ता कम और अपार धन हासिल करने की लालसा और आतुरता ज्यादा दिखती है।
पिछले दो दशकों के अन्तराल में राजनीति के मंडलीकरण और कमंडलीकरण ने जो परिदृश्य बनाया है वह प्रीतिकर नहीं है, इसे सामान्य और समाजोपयोगी बनाने के लिए राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्कर्म की घोर आवश्यकता है। क्या इस सन्दर्भ में हिन्दी सिनेमा की दिशा और गम्भीरता पर्याप्त है? ‘कश्मीर फाइल्स’, ‘द केरला स्टोरी’ ‘अजमेर 92’ जैसी फिल्में किस भूमिका का निर्वाह कर रही हैं? बावजूद इसके कि इन फिल्मों के आधार हमारे अतीत के कडुवे और क्रूर सच हैं, हमें सोचना यह चाहिए कि इन सच्चाइयों के उत्खनन से हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? कश्मीरी हिन्दुओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ इस तथ्य को झुठलाना असम्भव है।

कश्मीर फाइल्स दिखाती है कि किस तरह का अन्याय हुआ लेकिन फिल्म यह नहीं बताती कि उस भीषण संकट के समय में कश्मीरी मुसलमानों ने अपने हिन्दू पड़ोसियों की किस तरह से मदद की है? यह नहीं दिखाती कि उग्रवादियों और आतंकवादियों से लोहा लेने में कश्मीर के मुसलमान भी शहीद हुए हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद से सच के एक पहलू का उपयोग कला के उद्देश्य को संकीर्ण बनाता है। ऐसे समय में जब दोनों तरफ की कट्टरता मैदानेजंग है, कला को ज्यादा उदार और कोमल होने की जरूरत है। सामंजस्य और सहजीविता, मेल और भाईचारा वे भाव हैं जो समाज को बांधे रखते है और रचनाधर्मिता का यह दायित्व है कि वह इन्हें विकसित करे।
तमाम विसंगतियों और विडम्बनाओं के बावजूद कुछ बातें हैं जो हिन्दी सिनेमा के पक्ष में हैं और लोकतन्त्र के भी पक्ष में। हाल के दिनों में हिन्दी सिनेमा का द्वार नये और प्रतिभाशाली लोगों के लिए खुल गया है। फिल्मी परिवारों का वर्चस्व टूट रहा है। जिसके परिवार में कभी कोई फिल्मों में नहीं था वह भी अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर अपनी जगह बना ले रहा है। यह पहले बहुत मुश्किल था। दूसरी बात यह हुई है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी इस कदर खुली हुई है कि वहाँ तक किसी की भी पहुँच हो सकती है। पहले की तुलना में फिल्म तकनीक थोड़ी सरल और सस्ती हुई है। अब फिल्म बनाना पहले की तरह कठिन नहीं है। किसी ऐसे अछूते विषय पर दस मिनट की डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाकर कोई यू-ट्यूब पर अपलोड कर दे तो पल भर में करोड़ों लोगों तक फिल्म का सन्देश पहुँच सकता है। लेकिन इस तरह के काम के लिए जो निष्ठा और नैतिक बल चाहिए उसे बाजार बढ़ने नहीं दे रहा है। यह बात जगजाहिर है कि लोकतन्त्र भी बाजार के नियन्त्रण में है। बाजार तो यही चाहता है कि कोई मनुष्य और नागरिक नहीं रहे, सारा संसार उपभोक्ता बन जाए। तो क्या हम बाजार की तानाशाही कबूल कर लें?
इसके पहले कि उपभोक्तावाद पूरी तरह से मनुष्यता को मिटा दे हमें विचार पर बाजार के हमले को रोकना होगा। और यह काम वैचारिक चेतना को फैलाए बिना सम्भव नहीं है। विचार को फैलाने के लिए सिनेमा से ज्यादा सटीक और शक्तिशाली माध्यम कोई दूसरा नहीं है। पिछले सौ वर्षों में सिनेमा सम्प्रेषण का एक मुकम्मल माध्यम बन चुका है। लेकिन इस सिनेमा का इस्तेमाल हम बाजार के बजाय मनुष्यता और लोकतन्त्र के पक्ष में करें, इसके लिए क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं तो यह तैयारी कितने दिनों में और कैसे होगी?