
देखा तो हममें ताक़ते-दीदार भी नहीं
रॉयल्टी विवाद और लेखक-प्रकाशक सम्बन्ध
पूरी दुनिया में लेखक और प्रकाशक के बीच के व्यावसायिक रिश्ते में सबसे महत्त्वपूर्ण और विवादी रिश्ता है रॉयल्टी का। यह रिश्ता एक अनुबन्ध के तहत, पूँजी और श्रम का रिश्ता है, न कि सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर, प्रेम, भाईचारे, दोस्ती आदि का, जैसा कि अक्सर प्रकाशक कहते रहते हैं। इसलिए सवाल किसी एक लेखक के हक़ का नहीं है। बल्कि यह उस हर छोटे-बड़े, नये-पुराने लेखक के हक़ का सवाल है, जिसे प्रकाशन उद्योग चला रहे मालिकों को समझना चाहिए और श्रम, पूँजी और उत्पादन के आपसी सूत्र, समीकरण और रिश्ते को विधि-सम्मत, नियमतः पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बरतना चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता कार्य-संस्कृति बननी चाहिए, न कि उसे दिखाने की कोशिश करते हुए दिखाई देना चाहिए।
पर दुर्भाग्य से, जब-जब इस सवाल पर खरा उतरने की बारी आई है, तब-तब प्रकाशकों को बगलें झाँकने और किसी तरह से अपनी गलती को छिपाने और अन्य तरीकों या उपायों से लीपापोती करते देखा गया है। यहाँ पर, सवाल किसी एक या कुछ प्रकाशकों का नहीं है, छोटी पूँजी वाले कुटीर उद्योग की तरह प्रकाशन चला रहे प्रकाशकों से लेकर मोटी पूँजी के बल पर, शीर्ष पर बने रहने की सामराजी सोच वाले प्रकाशन समूहों तक, हर तरह के प्रकाशकों का है। अपनी सीमा और संसाधन की सीमितता का रोना रोने वाला जो प्रकाशक है वह भी येन-केन-प्रकारेण लेखक की रॉयल्टी मार कर उसी मानसिकता को संरक्षित करता हुआ देखा जाता है जिसे बड़े प्रकाशक तरह-तरह के झूठे दावों और उपायों में संरचित करते हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कई तो ख़ुद लेखक भी हैं।
मैं यहाँ उस बहस में नहीं जाऊँगा कि इसके जिम्मेदार एक हद तक, ख़ुद कुछ लेखक भी हैं। बस इस पर इतना ही कहूँगा कि प्रकाशन उद्योग में भी कई कम्पार्टमेंट हैं। साधारण डिब्बे से लेकर फर्स्ट क्लास तक। सबको जल्दी गंतव्य तक पहुँचने की जल्दबाज़ी है। व्यावसायिकता, निजी सम्बन्धों, प्रायोजित पाप्युलरिज़्म, फ़ैशन, लेन-देन की धूर्तताएँ, मध्यवर्गीय तुच्छताएँ आदि-आदि के हवाले से यह बात उठाई जा सकती है। लेकिन, मूल मुद्दा यह नहीं है। उस बहस में जाने से मूल मुद्दा किसी और तरफ़ चला जाएगा। मूल मुद्दा लेखक और प्रकाशक के बीच हुए अनुबन्ध और विधि-सम्मत व्यावसायिकता की ईमानदारी और पारदर्शिता का है। कई बार ‘ईमानदारी’ और ‘पारदर्शिता’ का भ्रामक स्वरूप भी तैयार किया जाता है। आज के उन्नत टेक्नोलॉजी वाले समय में यह और सरल हो गया है।
आज के ‘बेस्ट सेलर’ और ‘पापुलर’ वाली बाजरवादी मानसिकता और बहस को इससे जोड़ कर देखा जाय तो पता यही चलता है कि इस तरह की आधिकांश चर्चाएँ और बहसें प्रायोजित होती हैं। क्योंकि, इनके सर्वेक्षण समूहों, तरीकों, नमूनों, मतों, विचारों, सूचियों को निर्धारित करते समय कोई लोकतान्त्रिकता, समानता और विश्वसनीयता का वैज्ञानिक आधार नहीं होता। हो सकता है कि आज के तकनीकी युग में यह सब जिस तरीके से किया जाता हो वह बाहरी तौर पर बहुत ही पारदर्शी और साफ-सुथरा दिखे, पर चालाकी से निर्मित पारदर्शिता, ईमानदारी की गारंटी नहीं। पारदर्शिता अगर केवल एक ‘टेक्नोलोजी’ भर है, विचार, मूल्य और उत्तरदायित्व नहीं, तो फिर टेक्नोलॉजी का नियोजन और नियंत्रण सबसे आसान होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि अधिकतर ‘बेस्ट सेलर’ की जो विज्ञापित बहसें हैं, उनका ‘एजेंडा’ और ‘एजेंट’ दोनों निर्धारित होते हैं।


वैसे भी हिन्दी में ‘बेस्ट सेलर’ और ‘अग्रिम बुकिंग’ जैसी परिघटनाएँ मेरी जानकारी में नयी हैं। यह अँग्रेजी की नकल और आज के सन्दर्भ से कहा जाय तो ‘बाज़ारवाद’ की डिमांड से पैदा हुई हैं। जैसे कि ‘लिट-फ़ेस्ट’ शुरू हुए। इनमें, तरह-तरह के बाज़ारू साहित्यिक-सांस्कृतिक तरीकों और माध्यमों का योगदान बहुत अधिक है। इधर ऐसी-ऐसी किताबें बेस्ट-सेलर हुई हैं, जिनका सम्बन्ध या तो तथाकथित रूप से ‘राजनीतिक-समय’ के रेटारिक अथवा दबाव व फैशन से है या ‘हिंदुत्वा और धर्म’ के रेटारिक को मिथक और परम्परा के नये कलेवर में परोसने से है। इनमें से कई तो अपने मूल लक्ष्य में प्रतिगामी हैं, समय-समाज की समस्याओं और मूलभूत चिन्ताओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। पर, प्रकाशक को आजकल ऐसी ही किताबों की न जाने क्यों तलाश रहती है।
मुझे जो लगता है वह यह है कि हिन्दी के प्रकाशक ‘बेस्ट सेलर’ और ‘पापुलर साहित्य’ विज्ञापन का तिकड़म, उन बड़ी पूँजी और संसाधन और नेटवर्क वाले अँग्रेजी के प्रकाशकों, पेंगुइन, ऑक्सफोर्ड, हार्पर एँड कॉलिन्स आदि के इधर हिन्दी प्रकाशन में जगह बनाने की कोशिश के दबाव और प्रतिस्पर्द्धा में कर रहे हैं। हिन्दी के एक बड़े प्रकाशक का यह तर्क है ‘हम पुरानी चीजों को नकार नहीं रहे, लेकिन यह तो सोचना होगा कि नयी पीढ़ी की पाठकीय आकांक्षाओं को कैसे सम्बोधित किया जाए, उनकी भाषा क्या है? वे क्या पढऩा चाहते हैं? उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर हम उनके लिए ‘पापुलर’ किताबें ले आते है।’
एक दूसरे बड़े प्रकाशक का दावा है कि सुरेन्द्र मोहन पाठक के उपन्यास के लिए छपने से पहले ही 50,000 प्रतियों के आर्डर आ चुके हैं। अमिष त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक जैसे पापुलर लेखकों के साथ भी इसी तरह के दावे हैं। हिन्दी के प्रकाशकों की होड़ अब इसी तरह के आंकड़ों को छूने की है। इसलिए, असल मसला अब केवल ‘बेस्ट सेलर’ का नहीं है, अब तो छपने और बिकने के पहले ही किताब ‘बेस्ट सेलर’ हो गयी। इसलिए, यह मामला सचाई से अधिक प्रायोजित है। अब ‘प्रिंट कैपिटलिज्म’ के मार्केट में हिन्दी प्रकाशकों की प्रतिस्पर्धा जहाँ एक तरफ़ हिन्दी में उतरे अँग्रेजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से है वहीं दूसरी तरफ़ उसके डिजिटाइजेशन के जरिए विविध रूपों में प्रस्तुत करने की भी है।
बाकी, रुचियों, युवाओं की पसन्द आदि के सन्दर्भ में हम सब को पता है कि बाज़ार उसे कैसे तैयार करता है। अपने ‘संस्कृति-उद्योग’ सम्बन्धी अध्ययनों में अडोर्नो ने इस पर विस्तार से लिखा है। यह रुचियाँ, यह पसन्द किस वर्ग को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं, यह सबको पता है। हिन्दी सिनेमा में ‘राष्ट्रवाद’ के रेटारिक को संरक्षित और पाप्युलर बनाने के लिए जिस तरह की कुछ फिल्में इधर आई हैं, और उनको ‘स्टेट’ ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे न केवल उनकी कमाई में निर्बाध इजाफ़ा हुआ है, बल्कि एक ख़ास तरह का लक्ष्य भी सधता हुआ प्रचारित होता हुआ देखा गया है। आजकल ‘वेब सीरीज’ का जमाना है। इन ‘वेब सीरीज’ में अधिकांश के यहाँ एक ट्रेंड देखा गया कि वे 9 एपिसोड के ही बनाए जाते हैं। उसका दूसरा कोई सीजन जब आएगा तो देखा जाएगा । पर पहला सीजन 9 एपिसोड का लांच किया जाता है।
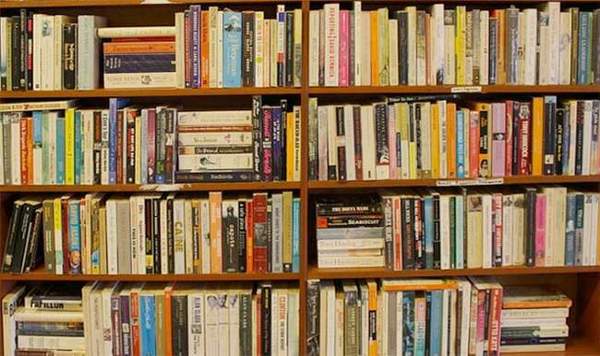
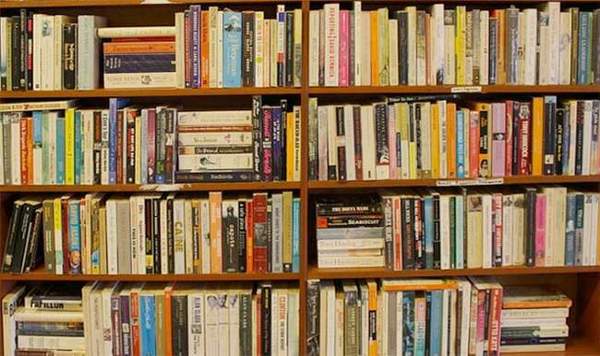
पिछले दिनों हिन्दी के एक प्रकाशक ने ‘वेब सीरीज’ की इस नकल पर एक ‘प्रिंट सीरीज’ शुरू किया और 9 एपिसोड की तर्ज़ पर इस सीरीज का नाम दिया ‘नाइन बुक्स’। इसकी देखादेखी बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए एक दूसरे प्रकाशक ने भी अपनी ‘प्रिंट सीरीज’ शुरू की और उसका नाम रखा ‘पापुलर लिटेरेचर’। जो लोग ‘वेब सीरीज’ से परिचित हैं वे जानते होंगे कि ये ‘वेब सीरीज’ किस वर्ग और समाज के लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं? उनका दर्शक कौन सा वर्ग है? इसलिए, ‘पापुलर साहित्य’ के पूरे खेल को बहुत संजीदगी से समझने की जरूरत है। ‘पापुलर’ किसके बीच? हमें यह समझना होगा कि हिन्दी के पाठक-वर्ग और अँग्रेजी के पाठक-वर्ग की ज़मीन एक नहीं है। इसलिए इधर हिन्दी के कुछ प्रकाशकों और उनके ‘हिट’ लेखकों के करतब देखकर यह कहना पड़ रहा है कि अब वे खुद ही तमाशा हैं और खुद ही तमाशाई।
आज सफलता की परिभाषा बाज़ार ने बदल दी है। व्यावसायिकता की दृष्टि से कोई चीज कितनी सफल है, वही अब हिट है, पापुलर है। इसलिए बिकाऊ और कमाऊ उत्पादों को ही अब सफल माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिनेमा है। अब कोई सिनेमा अपने पहले हफ्ते में 200-300 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर लेता है कि नहीं, वह उसके अच्छे और खराब होने का मानक है। फिल्मों के सिल्वर जुबली और गोल्डेन जुबली का दौर समाप्त हो गया। अब तो ‘मल्टीप्लेक्स’ भी खतरे में हैं क्योंकि अब ‘ओटीटी’ (ओवर द टॉप) का प्लेटफार्म बाज़ार में उतर चुका है, जहाँ सीधे इन्टरनेट के जरिये फिल्में रीलीज़ हो रही हैं। अब किसी गाने को बरसों-बरस नहीं सुना जाता। अब अधिकांश गाने रीमिक्स होते हैं, जिनमें सुनने के लिए कुछ नहीं होता। उनको बनाया और दिखाया ही इस तरह जाता है कि वे सेन्सेशन पैदा करें, फटाफट दिमाग पर चढ़ें, गुदगुदाएँ और फटाफट खिसक जाएँ।
अब किसी पुस्तक के कितने संस्करण छपते हैं और कितने दिनों के अन्तराल पर छपते हैं और कितनी प्रतियाँ छपती हैं, यह मुद्दा नहीं है बल्कि, दो-चार-दस-बीस प्रतियों के संस्करण का बाज़ार से उठ जाना ख़बर है। अब विज्ञापन और विपणन महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसलिए, इस समय लेखकों की एक बाज़ारवादी पीढ़ी भी तेज़ी से उभरकर सामने आई है, उन्हीं की भाषा में कहा जाय तो छा गयी है। उनके लिए ‘लेखक’ होना नहीं ‘लेखक’ कहलाना भर महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए क्या रॉयल्टी, क्या लेखक, क्या लेखक-प्रकाशक के कर्तव्य और अधिकार, सब नैतिकता के तकाज़े से बाहर की चीजें हैं।


इसलिए इस ताज़ा रॉयल्टी विवाद के हवाले से मूल मुद्दे पर बहस करनी है तो ज़ाहिर है कि मूल समस्या उस लेखकीय-प्रकाशकीय नैतिकता से जुड़ा है, उसकी कार्य-संस्कृति से जुड़ा है, जिसमें लेखकीय अधिकार को कोई महत्त्व न दिया जाता है। अगर दिया जाता तो महत्त्व की इसी स्थापना में स्वतः लेखक का सम्मान, उसका आदर, उसकी प्रतिष्ठा अन्तर्निहित होती, उसे अलग से सफ़ाई पेश करते वक़्त कहने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मुद्दा बरसों से ठगे जा रहे हतप्रभ लेखक की उस पीड़ा और दुःख का है, जिसे हिन्दी भाषा के एक अति महत्त्वपूर्ण लेखक विनोद कुमार शुक्ल के रूप में एक 85 साल की उम्र के उस व्यक्ति का है, जो लेखक है। उसकी आजीविका का एक ज़रिया लेखन भी है। लेकिन जब इस ज़रिए की न्यूनतम नैतिकता की भी परवाह न की जाए, तो लेखक होना कितना त्रासद है। कितना अपमानजनक और पीड़ादायी है।
ऐसा नहीं है कि हिन्दी में रॉयल्टी को लेकर लेखक होने की पीड़ा और त्रासदी का यह कोई पहला और आख़िरी वाकया है या होगा। पहले भी रॉयल्टी के मामले में लेखक-प्रकाशक के रिश्ते में विवाद होता रहा है। निराला से लेकर निर्मल वर्मा और अब विनोद कुमार शुक्ल के उदाहरण सामने हैं। इसलिए, इसे किसी एक लेखक या केवल कुछ लेखकों से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। न ही, कि हमें तो मिलता है, उन्हें भी मिलता है की स्पष्टता के आधार पर, प्रकाशकीय बेईमानी के प्रति नरम और सदाशयी सोच की ज़रूरत है, जैसा कि लेखक कहते/करते देखे गए। पर क्या वह इसी तरह आगे मिलती रहेगी?
यह सच है कि ‘हमें’ और ‘उन्हें’ अभी रॉयल्टी मिलती है। इसका प्रमाण भी यदा-कदा, उन्हीं में से कुछ के द्वारा, चेक आदि को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने के करतब में दिख जाता है। लेकिन यहीं पर, इस प्रदर्शन वाली मानसिकता से ही यह सवाल उठता है कि, सचमुच रॉयल्टी का मिलना क्योंकर इतनी बड़ी उपलब्धि हो कि आप ख़ुशी का इज़हार करने से ख़ुद को रोक न पाएँ? क्या इसलिए कि आपको विश्वास नहीं था कि आपकी रॉयल्टी आपको मिलेगी? जैसे वह, पारिश्रमिक नहीं बल्कि पारितोषिक हो। इसलिए मूल समस्या का आधार कहीं और ही है। ज़रूरत है उसको टटोलने, कुरेदने और सामने लाने की। 

दरअसल, हमें यह समझना चाहिए कि नव-उदरवादी पूँजी-तन्त्र और तद्जनित मुक्त वैश्विक-बाज़ार ने शीत-युद्ध के दौर को खत्म कर दिया। नब्बे के बाद का जो दौर आया, देखने में तो वह पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने और बांधने वाला दिखता है पर वास्तविकता कुछ और है। यह केवल और केवल व्यापारिक गठबन्धन है। मानवीय महत्ता और गरिमा की तकाज़े से इसका कोई मूल्य नहीं। इस दृष्टि से से देखा जाय तो यह समय खण्डित-आत्म, खण्डित-चेतना और खण्डित-दृष्टि की मनोदशा वाला एक खण्डित-समय है।
ऐसे समय में लेखन की स्थिति और उपस्थिति पर बात करने से पहले उस पूरे परिदृश्य पर बात होनी चाहिए, जिससे न केवल लेखक-प्रकाशक, बल्कि इस समय का साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश, उसको निर्मित करने वाली, उसका नेतृत्व करने वाली संस्थाएँ किन ताक़तों के दबाव में हैं? उनका प्रबन्धन करने वाली पूँजी कैसे और किस तरह से संचालित और नियन्त्रित होती है? उसका स्रोत क्या है? जैसे सामन्तशाही और पूँजीवाद के दौर में कला, साहित्य और संस्कृति का नेतृत्व करने, उसे सुरक्षित और संरक्षित करने वाले पुरोहितों और अभिजात लोगों का औरा और दबदबा हुआ करता था वैसे ही आज के नव-उदारवादी या उत्तर-पूँजीवादी दौर में बाज़ार के नियमों और जरूरतों के अनुसार एक ख़ास तरह के ‘सांस्कृतिक-बिचौलियों’ का वर्ग बहुत तेज़ी से तैयार हुआ है या यह कहा जाय कि तैयार किया गया है।
यहीं पर गम्भीरता से यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या ‘लेखक’ केवल किसी प्रकाशक के लिए, उसके फ़ायदे के हिसाब से बाज़ार में केवल एक ‘अभिकर्ता’ मात्र है? अगर वह इतना ही भर है तो फिर बाज़ार में फ़ायदे के तर्क और नियम के बदले हुए स्वरूप और तकाज़े से उनकी जगह नये ‘अभिकर्ता’ ले लेंगे। यह ‘व्यापारिक-प्रबन्धन’ के लिए उचित भी है। कहानीकार और मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी कर रहे चन्दन पाण्डेय इसको समझते हैं। रॉयल्टी के मसले पर उठे इस ताज़ा विवाद को उन्होंने बहुत ही साहस के साथ सोशल मीडिया पर बहस के केन्द्र में खड़ा किया। पर, इस बात से तो चन्दन भी इत्तफ़ाक़ रखते होंगे कि ‘लेखक’ मात्र प्रकाशक के लिए ‘अभिकर्ता’ होकर रह जाएगा तो फिर बाज़ार के छल-छद्म से उसे (लेखक को) ख़ुद लेखक ही नहीं बचा पाएगा। जबकि, तमाम बाज़ारू तरीकों और उपयोगिता के प्रायोजित चालाकियों में लेखक शामिल होता देखा जाता है। ज़रूरत ‘लेखक’ नामक संस्था के बने रहने और अस्तित्वमान होकर बने रहने की है।


खासकर, एक ऐसे समय में जब लेखकीय अस्तित्व और उसकी महत्ता पर बार-बार सवालिया निशान लगाए जाते हों। सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रच्छन्न लांछन, अस्पष्ट आरोप, अपुष्ट तथ्य और अतार्किक घामड़पन से आज के साहित्यिक-वातावरण (जिसे साहित्य का समकाल कहा जा रहा है) को निर्भीक, निभ्रान्त सत्य बनाने की पूरी कवायद चल रही है, उसमें लेखक की पहचान विलोपित होती जा रही है। सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत मतभेद और विरोध को सामाजिक मतभेद और विरोध के नाम पर बुर्जुवा छल-प्रपंच का ऐसा मंच दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। उत्तर-पूँजीवादी समाज में मध्यवर्ग के झूठ और प्रवंचना का यह ऐसा जरिया बनता जा रहा है जिसमें हम सुनाना तो अधिक से अधिक चाहते हैं पर सुनना एकदम से पसन्द नहीं करते। सुनाने की इतनी अधीर उग्रता और न सुनने की इतनी उद्धत उपेक्षा का माहौल पहले कभी नहीं रहा। तुरन्त ‘निपटान’ सोशल मीडिया की रहन में है। अभी नहीं निपटाया तो सबकुछ ख़त्म हो जाएगा। पीछे छूट जाने का इतना भय।
जबकि, सच्चाई यह है कि एक लेखक की जो सृजनात्मक चिन्ता होती है वह महज अपनी कलम की चिन्ता नहीं होती, वरन् व्यापक स्तर पर उस ‘सिविल सोसायटी’ की चिन्ता होती है जिसे सरकारें समय-समय पर कभी धर्म के नाम पर तो कभी राष्ट्रीय-स्वाभिमान के नाम पर तो कभी विकास की इजारेदारी के छद्म में छलती रहती हैं। लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी अपने प्रतिरोधी हस्तक्षेप से समय-समय पर असम्भव खतरों की संभावना से इस ‘सिविल सोसायटी’ को ‘एलार्म’ करते रहते हैं। सरकारी तन्त्र और व्यवस्था के लिए किसी भी सिविल सोसायटी में बुर्जुआजी की यह सबसे जरूरी भूमिका होती है। सरकारें उनके इस कार्य-व्यवहार से घबराती हैं। इसलिए केवल मात्र लाभ-लोभ की बाज़ारू राजनीति के तहत किसी ख़ास मक़सद के लिए तैयार किया जाने वाला ‘रेटारिक’ बहुत खतरनाक होता है। ऐसा रेटारिक सार्वजनिक रूप से समाज को भीड़ में तब्दील करने की तैयारी के साथ संचालित और प्रचारित किया जाता है। लोग बालोचित आशावाद में भ्रमित होकर झूठ सुनते हुए अपने को निश्चिन्त और सुरक्षित महसूस करते रहते हैं।
जिस समाज में हम इस कदर भटक जायँ कि खुद से ही झूठ बोलने लगें और उस झूठ पर विशवास भी करने लगें तो उस सामज को कोई नहीं बचा सकता। आज तो यह स्थिति है कि सच कहने भर से ‘सच’ की सत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। यह ‘पोस्ट-ट्रुथ’ का समय है। एक सत्य को काटती हुई समानान्तर सत्य की अनेक-अनेक झूठी छवियाँ आपके सामने परोस दी जाएँगी। बाथ यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन में सोशल एँड पॉलिसी साइंस के प्रोफेसर और समाज-वैज्ञानिक डेविड मिलर के शब्दों में कहें तो यह प्रोपेगैंडा मैनेज्ड डेमोक्रेसी और सोसाइटी का दौर है।
रॉयल्टी विवाद की इस ताज़ा बहस के जरिए हमारी चिन्ता और हमारा कर्तव्य एक ऐसी कार्य-संस्कृति के लिए वातावरण बनाने की होनी चाहिए जो ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करे। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर मुझे कथाकार, सम्पादक और प्रकाशक गौरीनाथ के उस बचावकारी तर्क, कि ऊपर से लेकर नीचे तक, हर जगह उन्हें लोगों को खुश करना पड़ता है, से संवेदनात्मक रूप में साथ होने में कठिनाई है। अतः हमारी चिन्ता उस ‘बाजारवाद’ को लेकर है होनी चाहिए, जिसने आज हर चीज को ‘माल’ में तब्दील कर दिया है। अब हर चीज का मूल्य उसके ‘पण्य’ होने में है। ‘उत्पाद’ के फ़ायदे-नुकसान में है। नव उदारवादी/पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, क्रय और विक्रय के तर्क से हर चीज एक ‘उत्पाद’ है, एक ‘माल’ है, इसके अलावा कुछ नहीं।


क्या साहित्य भी, चूँकि बेचा-खरीदा जा रहा है, इसलिए माल मान लिया जाना चाहिए? अगर मान लिया जाए, फिर तो बात और आसान हो जाती है। माल के रूप में किसी वस्तु को उत्पाद बनाकर जब बाज़ार में, जिस बाज़ार-मूल्य के साथ उतारा जाता है, उसके पहले ही उस उत्पाद का ‘अतिरिक्त-मूल्य’ (सरप्लस) मुनाफ़े के रूप में सेठ और उनके बिचौलियों तक पहुँच जाता है। घर बैठे आज जो ‘अतिरिक्त मूल्य’ पर ‘अतिरिक्त मूल्य’ कमाने की ‘ऑनलाइन’ कोशिश जारी है, वह ‘कॉमोडिटी’ नहीं तो क्या है? उत्पादन के नये रूपों की पहचान, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्तियों के साथ ज्ञान के विनियोजन की पहचान, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विधान (आर्डर) के व्यवहार और विमर्श की जानकारी, राष्ट्रीयता और नागरिकता की नयी समस्यायों पर सूक्ष्म नजर, मिडिया का निरन्तर पूँजी बटोरती और सच को झूठ रचती संस्था की ओर शिफ्ट होने आदि मसलों के साथ हमें लेखन और प्रकाशन के रिश्ते को समझने की आवश्यकता है।
ऐसे में, रॉयल्टी सम्बन्धी इस ताज़ा विवाद पर एक लेखक संगठन में महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाने वाले आलोचक संजीव कुमार के इस कथन से, कि लेखक संगठन ‘ट्रेड यूनियन’ की तरह से फंक्शन नहीं कर सकते, धक्का लगता है। यह ठीक है कि ट्रेड यूनियन जिस तरह से अपने लोगों के हक़ और हितों की लड़ाई गारंटी दिलाने की हद तक जाकर जिस तरह से लड़ते हैं, उसी तरह से एक लेखक संगठन नहीं लड़ सकता। पर, इससे कैसे किनारा किया जा सकता है कि अगर लेखन भी श्रम, पूँजी, उत्पादन, आदि के सूत्र और समीकरण से बंधा है, आजीविका का, एक न्यूनतम ही सही ज़रिया है, तो उसके विधि-सम्मत अधिकार और हक़ की लड़ाई लेखक संगठनों को क्यों नहीं लड़ना चाहिए?
दरअसल, ‘समय’ पर उँगली रखना उसकी नकारात्मता को छीलना और उकेरना भर नहीं होता वरन उन ‘द्वंद्वात्मक-सह-सम्ब्द्धताओं’ को उजागर करना होता है जिससे वह ‘समय’ बन रहा है, बनाया जा रहा है। ऐसे में, आज इसकी ज़रूरत है कि लेखक-प्रकाशक के बीच के व्यावसायिक रिश्ते में हर सम्भव ईमानदारी और पारदर्शिता लाए जाने की पहल की जाए। इसके लिए अगर बड़े पैमाने पर परिवर्तन की दरकार है। इसके लिए लेखक-प्रकाशक दोनों के कर्तव्य और अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अगर सरकार की ओर से एक नियामक संस्था बनाए जाने की मांग की जाये तो उचित होगा।
आज जब ISBN के लिए प्रकाशक की ओर से कवर और टाइटल जमा करने पर ही सरकार ISBN देती है तो इसी के साथ तीसरे दस्तावेज़ के रूप में अगर अनुबन्ध की प्रति भी वह प्रकाशक से जमा कराये, जिसमें साफ तौर पर रॉयल्टी और प्रिंट व डिजिटल रूपों में कितने संस्करण और कितनी-कितनी प्रतियाँ वह छापेगा, का उल्लेख स्पष्ट तौर पर हो। साथ ही उस अनुबन्ध में इस बात का भी उल्लेख हो कि भविष्य में यदि उस प्रकाशन संस्थान का मालिक किसी अन्य प्रकाशन संस्थान को बेचना चाहता है, ऐसे में वह लेखक से पूछेगा कि आप इस प्रकाशन के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। लेखक ‘स्टेक-होल्डर’ है। उससे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? ऐसे और भी सुधारात्मक कदम अनुबन्ध के जरिए उठाए जा सकते हैं।


इस सम्बन्ध में जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष और महत्त्वपूर्ण कथाकार असगर वज़ाहत ने कुछ सुझाव दिए हैं, वह महत्त्वपूर्ण हैं – “समाज में लोगों के बीच होने वाले महत्त्वपूर्ण समझौतों को निर्देशित करने तथा उन्हें सही ढंग से लागू करने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार से लेखक यह माँग कर सकते हैं लेखक-प्रकाशक के प्रकाशन, रॉयल्टी सम्बन्धों पर क़ानून बनना चाहिए। इसके अन्तर्गत ‘रजिस्ट्रार ऑफ रॉयल्टी’ का विभाग खोला जा सकता है। इसके बारे में नियम-क़ानून बनाए जा सकते हैं। इस विभाग को प्रकाशक और लेखक दोनों मान्यता दे सकते हैं तथा यह संस्था दोनों के हितों को देख सकती है। प्रकाशन जगत तथा पुस्तकों के बेचने-खरीदने के लिए भी राष्ट्रीय नीति का होना आवश्यक है। आज यह क्षेत्र पूरी तरह असुरिक्षत है और इसका सीधा प्रभाव पाठकों के ऊपर पड़ता है। क़िताबों के हद से बढ़ते मूल्य तथा दोषपूर्ण वितरण के कारण पुस्तकों तक नहीं पहुँच पाती। हमारे देश में लेखकों के अनेक संगठन हैं और लगभग सभी संगठन कॉपीराइट और रॉयल्टी के मुद्दे को प्रमुख मुद्दा मानते हैं लेकिन आज तक इन दोनों मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस नहीं चली है और न इसको सुलझाने का कोई रास्ता ही नज़र आया है। लेखक संगठनों को आज लेखकों और प्रकाशकों के हितों में रॉयल्टी के मुद्दे पर सार्थक क़दम उठाने की आवश्यकता है।”
अतः जिस संकट को लेकर, जिस अन्याय को लेकर इस्तगासा लगाया जा रहा है, उसके कार्य-कारण सम्बन्ध, उसकी पूरी निर्मिति, उसके उद्देश्य को समझे बिना, वह इस्तगासा सिवाय और धुन्ध व धाँधली फैलाने के और कुछ नहीं साबित होगा। इसलिए, अब विनोद कुमार शुक्ल के ही बहाने सही कॉपी राइट, रॉयल्टी, अनुबन्ध, पुस्तकों की कीमतों का निर्धारण आदि-आदि के सम्बन्ध में लेखक और प्रकाशक के जो कर्तव्य और अधिकार हैं, उसे ठोस अंजाम तक ले जाने की ज़रूरत है। वरना, एक लेखक के अपनी उम्र के आख़िरी पड़ाव में ठगे जाने की त्रासद पीड़ा का कोई पारावार नहीं। सोशल मीडिया से उठी यह बहस लेखकीय हक़ की मुकम्मल लड़ाई में तब्दील होनी चाहिए। वरना तो फिर आगे भी कोई विनोद कुमार शुक्ल जैसा 85 साल का एक लेखक अपनी ठगी की पीड़ा को ज़ाहिर करते हुए सामने आएगा और उस समय आज के हमारे हस्तक्षेप पर शायद यही कहा जाएगा :
