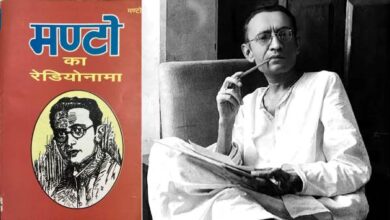जहाँ पर हम रुके वहाँ से तुम चलो
साहित्य की दुनिया से शुरुआती परिचय के दिनों से ही समकालीन हिन्दी आलोचना में नामवर जी की केन्द्रीय भूमिका से परिचित हो चली थी। अनौपचारिक चर्चाओं में भी शोधार्थी और साहित्य सेवी अपनी बात में वजन बढ़ाने के लिए अक्सर उनकी स्वीकृति को अकाट्य तर्क के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आते थे और मैं हक्की-बक्की होकर देखती रहती थी। उनकी प्रखरता और प्रभाव के ऐसे सिलसिले स्वतः मुझे उनके व्याख्यानों और रचनाओं तक ले गये और फिर उनकी ‘दूसरी परम्परा की खोज’, ‘कविता के नए प्रतिमान’ से शुरू करके बाकी रचनाएँ पढ़ती गयी और बीच-बीच में कुछ भाषण भी सुने।
कथा साहित्य में मेरी अधिक रुचि होने के कारण ‘कहानी-नयी कहानी’ ने गहरा असर डाला। उनकी स्थापनाओं और विश्लेषण पद्धति के साथ उनकी प्रखर अभिव्यक्ति से मन्त्र-मुग्ध, मेरी चेतना में ‘फिर’ शब्द खुब सा गया। अब भी घर के बच्चे बाल सुलभ कौतूहल से पूछते हैं कि ‘फिर क्या हुआ ?’, ‘फिर ?’ तो उनकी आँखों में विस्मय की चमक मुझे बेहद लुभाती है। नामवर जी की पंक्तियाँ जेहन में कौंधती हुई कहती हैं कि बच्चों को भविष्य चेतना से, इतिहास बोध से जोड़ने का काम कर रही हो, ध्यान से उत्तर देना। मैं भी बच्चों से मुखातिब होने से पहले उनसे पलट कर पूछ लेती हूँ कि हमने तार्किक चिंतन और इतिहास बोध की लय आप सरीखे विद्वानों से सीखी और यह ज्योति अगली पीढ़ी तक पहुँचे, इसके लिए सजग रह लेंगे, मगर‘फिर?’ के बाद के उत्तर तो इनके अपने हीहोंगे न?
साहित्य के अलावा समाज में बौद्धिक पर्यावरण बनाने का काम जिस ऊर्जा के साथ और जिस व्यापक पैमाने पर उन्होंने किया, दुर्लभ है। देश भर में घूम-घूम कर अपने वर्तमान और समाज को सम्बोधित करने का नतीजा था कि साहित्य से हल्की रुचि रखने वाले दूर-दराज के व्यक्ति के पास भी उनकी कोई न कोई स्मृति अवश्य है। प्रभावी पदों पर होने के बावजूद इतनी सहजता से उपलब्ध रहना कोई छोटी बात नहीं।
अपनी बात कहूँ तो उनके भाषण तो पहले भी सुने थे पर उनका खुद पर क्रमिक असर महसूस करने की शुरुआत हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए होने वाले नवचर्या पाठ्यक्रम के तहत उनकेदिए गए वक्तव्य से। यह वर्ष 2007 या 2008 रहा होगा। मैं छात्रा ही थी पर सुनने की ललक के कारण शिक्षकों के बीच घुस गई। उस दिन उन्होंने कहा था “साहित्य तो साहित्य की शर्तों के साथ ही आएगा और उन्हीं से तय होगा।” और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं जैसे हिन्दी को देश की अन्य भाषाओं के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, अलग-थलग नहीं। मीराबाई की दीप्ति को बहुत ओजस्वी आवाज में सराहा था कि कैसा गजब आत्मविश्वास है खुद पर कि कहती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। कोई और पुरुष दिखता नहीं तो परदा क्या करूं आदि, आदि।
उस दिन में मेरे मन में यह प्रश्न नहीं आया था कि पीना तो पड़ा जहर का प्याला ही आखिर। उनके आत्मविश्वास के साथ समाज में जो गति होनी चाहिए थी, वह मध्यकाल में सम्भव नहीं थी। आज तो दोनों तरफ का विकास ही वांछित हो सकता है। आधुनिक काल में वह अकेला पुरुष हाड़-माँस का सजीव प्राणी ही तो होगा कि अब भी उस अभाव को मिथकों और मूर्तियों से भरा जाना जारी रखें? बहरहाल साहित्य की शर्तों वाली बात उन्होंने इस संदर्भ में कही थी कि साहित्य में दलित और स्त्री के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता। रचनाओं को जाँचने की साहित्य अपनी कसौटी होती है, जो उस पर खरा उतरेगा वही साहित्य कहलाएगा। जो मेरे लिए सम्मानीय थे उनके परम आदरणीय कोई बात बोलें और मैं उन्हें मन्त्रवत ग्रहण न करूँ, यह कैसे सम्भव था? मैं नतमस्तक थी उनके प्रचण्ड ज्ञान और वागवैदिग्ध्य पर। ( नामवर जी मुझे इसके लिए क्षमा करें कि उनसे प्राप्त वैज्ञानिक चेतना का उल्लंघन करके भक्तिकाल के मूल्यों को जीने की नादानी मुझसे हुई।)
उन दिनों घर बैठे-बैठे पत्र-पत्रिकाओं में पते देख कर कुछ लिख कर भेज दिया करती थी। थोड़ा-बहुत कुछ पढ़ती रहती थी। यह सब सुनने के बाद साहित्य की शर्तों को ठीक-ठीक समझने की कोशिश में कई स्थापित विद्वानों को पढ़ गई। फिर जो दलित और स्त्री रचनाएँ सामने आतीं, सबको किनारे रखती जाती। वे मेरी कसौटियों पर खरी उतर ही न पातीं। इस दौरान कई समीक्षाएँ लिखीं-छपीं, कई किताबों की प्रशंसक बनी औरघूम-घूम कर अपने परिजनों को पढ़वाती रही।
कोई इक्का-दुक्का किताब ही उनमें किसी स्त्री रचनाकार की होती। चंद महीने पहले ही सुधीश पचौरी सर ने एक इंटरव्यू में पूछा था कि दलितों और स्त्रियों की जिन्दगी में क्या खुशियों और उत्सवधर्मिता के मौके नहीं आते? उनकी हर रचना रुदन और शिकायतों से भरी रहती हैं। लिहाजा एक बनी बनाई मानसिकता के तहत किताब खोलती औरदस-बीस पन्नों की शिकायतों से ही आजिज आ कर छोड़ देती। लगता जैसे वे कुछ कमतर आत्मविश्वास वाली लेखिकाएँहैं मैं तो वस्तुनिष्ठ, न्यायप्रिय बेहतर स्त्री हूँ न। मैं तो शिकायतें, रोना-धोना और कातरता न पसंद करती हूँ न ऐसा व्यवहार करती हूँ। तब सर्वानुमति की परिभाषा में खरी उतरने वाली भली स्त्री मैं हुआ करती थी। ( मतलब स्वत्वहीन, व्यक्तित्वहीन, चेतनाविहीन स्त्री और जाहिर है उपलब्धिविहीन भी)
साहित्य की शर्तों से डिगने वाले जो लक्षण विद्वानों से सुने थे, वे पुरुष लेखकों में भी दिखने लगे तो धीरे-धीरे समझ बनीकि सिद्धांत और आचरण का द्वैत, क्षेत्रवाद, उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, झटपट बहुत कुछ पा लेनेकी हड़बड़ी, तुरत-फुरत लेखन आदि सब आधुनिक व्यक्ति के द्वंद्व हैं जिन्हें दलित और स्त्री लेखन पर ज्यादा आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनका अनूठापन, नया सौंदर्यबोध जो दरअसलउनकी शक्ति थी, अपरिचय के कारण वह उनकी सीमा लगने लगता है। परिचय से तो प्रेम बढ़ता ही है। जिनका आलोचकीय विवेक इन विमर्शों की पर्याप्त व्याप्ति से पहले बनचुका था, उनका अपरिचय तो स्वाभाविक था – पर इन सबके बीच जीने वाली मैं कैसे इन उभरती ताकतों से अनजान रह गयी ! जबकि व्यवस्था ने लगातार हमारेरास्ते रोके, उपेक्षित किया फिर भी व्यवस्था (बौद्धिक वर्ग के बीच प्रचलित) पोषित विचार ही मेरी चेतनाको घेरे रहे।
नामवर जी के विचारों के आलोक में पुनर्विचार करने पर लगता है कि अगर वह इस समय के होते तो शायद समाज को पुष्ट बनाने वाले आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे होते। बाद में साहित्य में जगह बनाने वाली नवीन सामाजिक शक्तियों के लिए उनका विरोध क्रमशः ढीला पड़ता गया, विचारों में लचक आती गयी। समाज की वर्तमान हलचलों का संज्ञान उनके वक्तव्यों में सुनाई देने लगा था। भीतर के संस्कार ढहने में तोखैर सदियाँ लगती हैं। वेटूटते-टूटते ही टूटेंगे। मगर अगली पीढ़ी भी तो अपने सवाल उतनी मजबूती से अपने समय के मूर्धन्य हस्ती के सामने नहीं रख पाती हैं जिनकी टकराहट से दोनों का माकूल विकास हो।
नामवर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से यही समझी हूँ कि साहित्य की शर्तें अन्ततः जीवन से ही निःसृत होती हैं। वे कहीं शून्य से नहीं आतीं। वे खुद अपने जीवन के उत्तरवर्ती दौर में देश और समाज की हालत से व्यथित होकर या राजनीति के तात्कालिक तकाजों के तहत अपना लिखना स्थगित कर सीधे हस्तक्षेप के इरादे से देशभर में व्याख्यान देते जाते थे तो उनके प्रशंसकों ने इसे साहित्य की शर्तों और लेखकीय भूमिका के विस्तार की तरह ही ग्रहण किया। उन्होंने उनसे वर्तमान से ठोस, सकर्मक जुड़ाव की जरूरत को सीखा और जुड़ाव के सही तौर-तरीकों की चेतना भी ग्रहण की। चेतना जब आती है तो अपने स्रोत की सीमाओं के उल्लंघन का साहस भी साथ लाती है।
दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है। संकटापन्न समयों में कई बार लेखकों को जरूरी लगा है लिखना स्थगित कर लड़ाई में खुद सशरीर उतरना। स्पेनी गृहयुद्ध में दुनिया भर के लेखकों की भूमिका इसका एक उज्ज्वल उदाहरण है। उनकी वह सीधी लड़ाई उनके लेखन का ही हिस्सा थी, उनकी लेखकीय भूमिका का ही विस्तार। विद्यासागर नौटियाल जी तो कहते ही थे कि मेरा लेखन बैठे-ठाले का लेखन नहीं है। संघर्ष के मैदानों से सीधे उतरकर आया है।
सदियों से वंचित और दमित वर्ग संघर्ष के मैदानों में उतरे बिना क्या और कैसे लिखेगा। पन्नों तक पहुँचने में काल के जितने पन्ने लग जाते हैं न पचौरी जी, वे दूसरों के लिए हँसी-खुशी मनाने और उत्सवधर्मिता के रास्ते खोलने के निमित्त ही तो। ‘जलती हुई कुरुपता’ में क्या सौंदर्य नहीं होता? संघर्षरत व्यक्ति तो अक्सर अपनी कोशिकाओं को निचोड़ कर ही आगे के पीढ़ी के लिए जिन्दगी के रास्ते खोल रहा होता है क्योंकि दमित समुदाय के व्यक्ति को करना होता है यह अपने ही बूते।
आज सोचती हूँ कि उस दिन यह सवाल मैंने नामवर जी से किया होता तो उन्हें अच्छा ही लगता। हमारी अगुवाई करने वाले विद्वानों को भीतर से कितनी पीड़ा होती होगी जब उनकी सीमा को हम अपनी भी सीमा बना लेते हैं। अग्रगामी जीवन-मूल्यों को जीता हुआ जो शख्स समाज के निरन्तर विकास के लिए प्रयासरत रहता है वह भविष्य की यात्रा अगली पीढी के माध्यम से ही तो करेगा। इसलिए कि वर्तमान से जो हमारा सम्बन्ध हो सकता है वह पिछली पीढ़ी का नहीं। मगर हम खुद उनके साथ थम कर बैठ जाते हैं। उनके सामने वाजिब चुनौतियाँ न रखी जाने से समय की गति भीझटका खाती है और हमारे प्रगतिशील प्रखर पुरखों की भी गति बाधित होती है।
साहित्यकार की वर्तमान समय में ठोस पकड़ होनी चाहिए। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने बताया था कि उन्होंने ‘आलोचना’ पत्रिका का सम्पादन जब सँभाला तब शुरू के तीन-चार अंक तत्कालीनराजनीति पर केन्द्रित थे, बनिस्बत साहित्य के। यही मोहभंग के उस वक्त की जरूरत थी। इनसारे व्यापक महत्व के कामों को उनके जन्मदिन के अवसर पर याद करते हुए अपने आलोचक गुरु को सादर नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि आपसे मिली वैज्ञानिक चेतना और इतिहास बोध जिस दिशा में ले कर जाए, हम मजबूती से उस ओर ही बढ़ेंगे। आगे की ओर………….
.