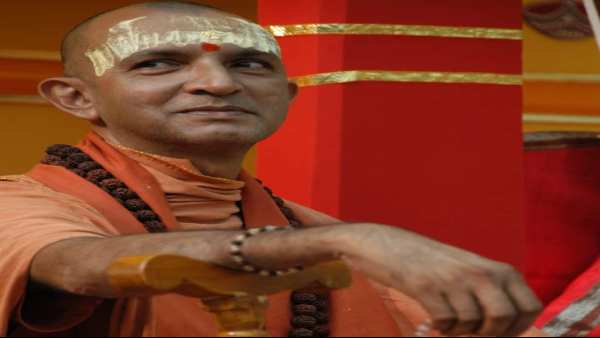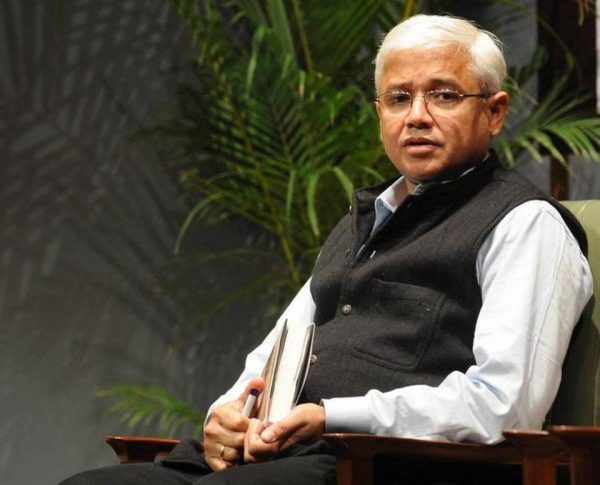लेखन में कल्पना और यथार्थ
लेखन में कल्पना से ज़्यादा यथार्थ को महत्व देना होगा। लेखक तेजस पूनिया से बातचीत
प्रश्न 1. आपने किताब की भूमिका में लिखा है दुनिया में ऐसे बहुत साहित्यकार हैं जिन्हें दो जून की रोटी भी लेखन के कारण नसीब नहीं हो सकी! ऐसे में जो नये साहित्यकार हैं या जो नये साहित्यकार, कहानीकार उभरकर सामने आ रहे हैं। जो लेखन में अभी ताजे तटके है जिन्हें आप अभी कोपलें भी कह सकते हैं उनको आप क्या सन्देश देना चाहेंगे?
उत्तर – साहित्य के मामले में कटु सत्य है कि ऐसे कई साहित्यकार हैं। जिन्हें दो जून की रोटी तक नसीब नहीं हुई। निराला, मंटो जैसे लोग इसका उदाहरण है। ख़ैर पहली बात तो ये कि ये रुचि का विषय है, रोज़गार का नहीं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं कि इससे उन्हें रोजगार मिला हुआ है। लेकिन वो लोग भी कितने हैं? और दूसरी बात तुलसीदास जी ने कहा है स्वान्तः सुखाय तुलसीदास रघुनाथ गाथा। तो स्वान्तः सुखाय लेखन को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात जीवन निर्वहन लायक उपार्जन भी सीखना चाहिए क्योंकि जब तक आप इस भौतिक दुनिया में आत्मनिर्भर नहीं होंगे आपके लेखन को भी प्रचारित करने में कठिनाई आयेगी। तो आत्मनिर्भरता तो जरूरी है। जब आप उस मुकाम पर पहुँच जाओ जहाँ से लेखन के माध्यम से आपकी आजीविका सहजता से चल सके तो आप जिस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं उस क्षेत्र को छोड़ भी सकते हैं। चाहें तो लेखन के साथ बरकरार भी रख सकते हैं। और अंतिम बात जेब की अमावस्या आकाश की अमावस्या से भी अधिक दर्द देने वाली होती है। इसलिए भी आत्मनिर्भरता आवश्यक हो जाती है। और अमावस्या दो तरह की होती है। एक जेब की दूसरी आकाश की। इसलिए जेब की अमावस्या पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र अंकित के हालात भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब वह शहर में आता है।
प्रश्न 2. आपने शहर जो आदमी खाता है कहानी में आदमी खाना या शहर ही खा जाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन शब्दों को प्रयोग करने के पीछे क्या वजह रही? ऐसे क्या कारण थे जो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल इस कहानी में करना पड़ा।
उत्तर – शहर जो आदमी खाता है कहानी पूरी तरह से उस वर्ग को समर्पित है जो किसी न किसी वजह से प्रवासी बन जाते हैं। और उनका प्रवास हमेशा गाँव से शहर के लिए होता है। तो आदमी खाना या शहर खा जाना जैसे शब्द पाश्चात्य संस्कृति की भी देन है। क्योंकि गाँव के या शहर के लोग जब नगर या महानगर की ओर पलायन करते हैं तो वहाँ जाकर वे अपने उन मूल्यों को, संस्कारों को, संस्कृति को सभी को भूलने लगते हैं। इसमें उनके रीत-रिवाज भी शामिल हैं। कुलमिलाकर पूर्ण रूपेण उसका परिवर्तन होकर एक नये आदमी का निर्माण प्रवास के पश्चात हो जाता है। और जब वह अपने उन मूल्यों आदि की तिलांजलि देने लगता है तो उसका एक नवनिर्मित रूप सामने आता है। शहर आदमियों को खा रहा है इसका मतलब ये नहीं की वह मांसाहारी है। इसका मतलब ये है कि वो उनके सामाजिक, नैतिक मूल्यों को समाप्त कर उसे आधुनिक, उत्तराधुनिक बना रहा है। हालांकि ये सब अच्छा है हमें आधुनिक और उत्तराधुनिक होना चाहिए। लेकिन अपने मूल्यों को खोए बिना। तो एक तरह से शहर आदमी को और आदमी ही आदमी को यहाँ चबा जाने को आतुर दिखाई देता है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल से यही दिखाना चाहता था कि शहरों में किस तरह का माहौल है। किसी को किसी से मतलब नहीं। सब अपनी धुन में सवार रहते हैं। जबकि इसके बनिस्पत आप गावों के हालात देख लें वहाँ आज से 100 साल पहले भी और आज भी सात पीढ़ियों तक दुश्मनी या दोस्ती निभाई जाती है। मैं गांव और शहर के इसी अंतर को अपनी कहानी में दिखाना चाहता था। 

प्रश्न 3. आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, पाठकों के तरफ से क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं आपकी कहानियों को पढ़ने के बाद, और जब कोई पाठक आपकी लिखी किसी कहानी की प्रशंसा ना करे बल्कि उसकी आलोचना करे तब आपको कैसा लगता है और जवाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है?
उत्तर – बहुत सारी तो नहीं 10-15 ही लिखी हैं। शुरू में जो 2,3 लिखी थी वो तो कहीं खो गयी, मिली ही नहीं काफी टाइम ढूंढा उन्हें। उस समय मोबाईल स्मार्टफोन नहीं था ना कम्प्यूटर था। तो रजिस्टर में ही लिखी थी कॉलेज के जिसमें नोट्स बनाता था। बाद में परीक्षा खत्म होते ही वो इधर उधर हो गया। लेकिन अब जो छपी हैं पत्रिकाओं में उनको लेकर हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली। इसका एक कारण ये भी है कि मैं अपनी कहानी लिखने के बाद अपनी बहन, मेरे कुछ अध्यापक और एक सीनियर मित्र हैं जो आलोचक भी हैं। उनको कहानी सुनाता हूँ। वो सब जरूरी सुझाव देते हैं उसके बाद कहानी कहीं भेजता हूँ। अभी तक कहानी छपने के बाद तो आलोचना नहीं मिली कहीं से। तो मेरे लेखन की आलोचना उसके प्रकाशन से पूर्व ही हो जाती है। इसलिए मैं पाठकों की आलोचना से बच जाता हूँ। अब जब कहानी संग्रह “रोशनाई” बाजार में आया है तो उसे पाठक बन्धु पढ़ें अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से उसे परखे और एक निश्चित मान मर्यादा के साथ आलोचना करे तो स्वागत है। आलोचना अगर मेरे लिखे की होगी तभी तो उसमें आगे चलकर सुधार कर पाऊंगा।
प्रश्न 4. कहानियाँ तो काल्पनिक होती हैं लेकिन जो आप लिखते हैं उन कहानियों की घटनाओं का कितना सम्बन्ध’ असल जिन्दगी की घटनाओं से होता है?
उत्तर – आपने कहा कहानियाँ तो काल्पनिक होती है इस बात से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। जब से कहानी लेखन आरम्भ हुआ है तब से अब तक और आगे जब तक कहानी लेखन होता रहेगा तब तक उनमें कल्पना का सहारा तो अवश्य लिया जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अधिकांशत: कहानियाँ कल्पनाओं से पूरित होती हैं। लेकिन मेरी बहुत कम कहानियाँ जो हैं कल्पनाओं से परिपूर्ण या कल्पनाओं से पूरित हैं। शहर जो आदमी खाता है, चीख, रूबी का फोन बस यही 2,3 कहानियों में कल्पनाओं का पुट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सभी यथार्थ परक हैं। उसमें भी नग्न यथार्थ है। क्योंकि उनका विषय ही वैसा है कि उन पर आप यथार्थ और नग्न यथार्थ से परे लिखेंगे तो शायद वो उतना प्रभावी ना हो या सहानुभूति न बटोर पाए पाठकों की। बाकी कल्पना का सहारा लेकर भी सहानुभूति बटोरी जा सकती है। लेकिन ज्यादातर कहानी यथार्थ परक हैं कुछ कुछ ही कल्पना है उनमें। बाकी उनको रोचक बनाने के लिए कल्पना का सहारा लिया गया है।
प्रश्न 5. आप सिनेमा पर भी लिखते रहते हैं। फिल्मों की समीक्षा हो या उनसे जुड़े हुए लेख हिंदी सिनेमा के अलावा पंजाबी सिनेमा पर भी लिखा है। आपकी सबसे पसंदीदा फ़िल्म कौन सी है और क्यों? और सिनेमा के भविष्य को आप किस नजरिये से देखते हैं।
उत्तर – फिल्मों की समीक्षाएँ तो खूब की हैं। लेकिन लेख कुछ कम लिखे हैं। पंजाबी फिल्म की समीक्षा भी की उससे जुड़े लेख भी लिखे। लेकिन अगर सबसे पसंदीदा फ़िल्मों की बात करूं तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट हैं। हर साल एक दो फिल्में ऐसी आ ही जाती हैं जो कई बार देखने का मन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा पसन्द है तो मुगले आजम, बागबान, पाकीज़ा, मदर इंडिया जैसी फिल्में। मुगले आजम से याद आया इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सन साठ में मध्य में फ़िल्म आई थी मुगले आजम। जिसका निर्देशन किया था करीमुद्दीन आसिफ ने जिनको के० आसिफ भी कहते हैं और उसी नाम से वे ज्यादा फेमस हैं। ये फ़िल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये फ़िल्म भारतीय सिनेमा के पेशानी पर लिखी गयी एक इबारत है। इस फ़िल्म से जुड़े इतने किस्से हैं जो इतिहास बन गये और कभी उनको दोहराया नहीं जा सकता। मराठा मंदिर में इस फ़िल्म का प्रीमियर हुआ था। जन्म से जवानी तक मुफलिसी में गुजारने वाले आसिफ साहब ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसी बड़ी, भव्य और सफल फ़िल्म बनाई है जो शायद ही कोई बना पायेगा। जब इस फ़िल्म का प्रीमियर हुआ तो लता मंगेशकर, सुरैया, गीता बाली, मीना कुमारी जैसी महान हस्तियाँ शामिल हुई थी। इस फ़िल्म का सेट इतना शानदार बना की लंबे समय तक लोग देश-विदेश से इसे देखने आते रहे। फ़िल्म रिलीज होने के बाद पाकिस्तान से भी भारी मात्रा में दर्शक यहाँ आए थे। इस फ़िल्म को देखने के लिए लोगों में इतनी दीवानगी थी कि लोग टिकट की मारामारी से बचने के लिए रात रात भर वहीं फुटपाथ पर सो जाते थे। और के आसिफ ने इस फ़िल्म को बनाने के लिए जो तपस्या की उसका फल तो उन्हें मिला ही और उस तपस्या की वजह से भारतीय सिनेमा अमर हो गया। यही सब वजह है कि ये मेरी पसन्दीदा फिल्मों में सबसे पहले नँबर पर है। इसके अलावा सिनेमा का भविष्य हमेशा उज्ज्वल है उसमें कोई खतरा नही है।
नोट – लेखक तेजस पूनियाँ का कहानी संग्रह “रोशनाई” अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। लेखक के नाम से अथवा ‘रोशनाई’ नाम से कहानी संग्रह को खोजा जा सकता है।
.