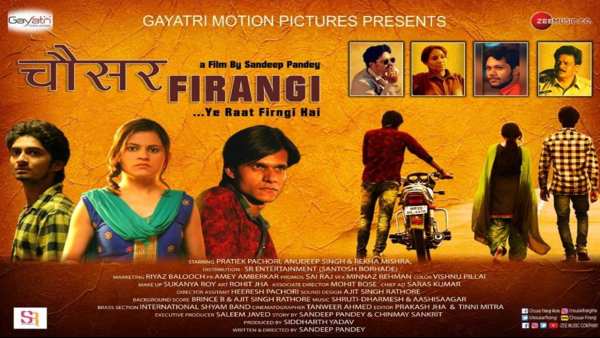अस्पृश्यता का ‘हैंडओवर’
{Featured In IMDb Critics Reviews}
निर्देशक – सौरभ कुमार
कास्ट – विकास कुमार, नूतन सिन्हा, ओरुषिका डे, विजय कुमार आदि
रिलीजिंग प्लेटफॉर्म – एमएक्स प्लेयर
फ़िल्म में दो संवाद है पहला देखो – सरकारी नौकरी वाला जांच के समय महिला से पूछता है तुम कितना कमा लेती हो? महिला कहती है – ठेकेदार सुबह से शाम काम करने के बाद तीन दिन काम करने के हमें सौ रुपए देता है।
दूसरा संवाद देखिए – बीमार पति को डॉक्टर के पास वही महिला लेकर जाती है तो वो डॉक्टर भी यही सवाल करता है तो वह जवाब में कहती है कि हम दोनों को पचास रुपए मिलते हैं।
क्या आपको गणित आती है? अगर आपकी गणित अच्छी है तो गणित लगाकर मुझे भी इस फ़िल्म के बारे में इसे देखने के बाद बताना कि उन्हें कितने रुपए मिलते थे असल में।
अब रिव्यू पढ़ें – एक मजदूर दम्पति जिन्हें तीन दिन काम करने के सौ रुपए मिलते हैं तो उन दोनों को रोज के पचास रुपए कैसे मिल सकते हैं? या फिर रोज के पचास रुपए मिलते हैं तो तीन दिन के सौ रुपए कैसे मिल सकते हैं?
साल 2011 में आई ‘हैंडओवर’ फ़िल्म का यह लेखकीय गणित देखकर मन करता है कि इस फ़िल्म की कहानी और इसे बनाने वालों को ही इसे पुनः हैंडओवर कर देना चाहिए था। और क्या सोचकर ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लयेर ने इसे दिखाने का फैसला किया? मात्र दलितों की कहानी होने के नाम पर आप कुछ भी दिखाएंगे और हम उसे हजम कर लेंगे?
तिस पर तथाकथित फ़िल्म समीक्षकों का यह कहना कि फ़िल्म निःशब्द करती है तो वाक़ई निःशब्द करना चाहिए उन्हें। क्योंकि रुपए लेकर फ़िल्म पत्रकारिता करके जितना नुकसान इन समीक्षकों ने किया है दर्शकों के रुपए का, उन्हें इस बात के लिए उनसे सवाल तलब करके अपने हुए रुपए के नुकसान का हर्जाना मांगना चाहिए।
फ़िल्म की कहानी है बिहार के किसी गांव में दलित परिवार की। जिसमें महिला ने अपने पति के इलाज के लिए अपनी बेटी को बीस हजार रुपए में बेच दिया। और बेचा भी उसे जिसे वो भाई कहती है। अपने पति को बचाने के लिए मां को अपनी कोख बेचनी पड़ जाए। देश में इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है गरीब- गुरबों के साथ। अब उस बच्ची के बेचे जाने की खबर अखबार में छपी तो गांव के मुखिया को पता चला। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची उससे विधानसभा में और वहां से मीडिया में। अब उस बच्ची को तुरंत मां बाप के हवाले किया गया। थोड़े समय बाद बच्ची बीमार होकर मर गई। लो जी खत्म कहानी दलितों की।

फ़िल्म बनाने वालों जितना दुरुपयोग फ़िल्म बनाने में किया। जितनी नाकाम कोशिश और कमअक्ल इस मुद्दे पर संवदेनशील कहानी बनाने में लगाई उतनी कोशिश या उतना धन किसी गरीब की मदद करते तो शायद तुम थोड़ा पुण्य कमा लेते। फ़िल्म में एक्टिंग के नाम पर बस ये दलित दम्पति ही अच्छा अभिनय करते नजर आते हैं। वहीं सरकारी नौकरी वाला आदमी और उसकी पत्नी के बीच बातचीत के दृश्य बस थोड़ा मसाला डालने की कोशिश है। लेकिन अफसोस कि ये मसाला बेढंगेपने से परोसा गया है। जब सरकारी नौकरी वाले की बीवी की नई-नई शादी के बाद कोख हरी हो जाती है तो उसकी सारी कामुकता हवा में घुलनशील पदार्थ बन जाती है।
बैकग्राउंड स्कोर इक्का-दुक्का जगह ठीक लगा। गीत- संगीत ठीक-ठाक है। कैमरामैन ज्यादा कमाल नही करते कुछ जगह ठीक से कैप्चर किया हुआ नहीं लगता है। इस तरह की छोटे बजट की फिल्मों को जो आम फिल्मों की तरह दबी पड़ी रह गईं हैं उन्हें ओटीटी पर लाना बस अपनी लगाई हुई रकम को वापस वसूलने जैसा है। लेखक की कहानी के छेद जो एक बार फ़िल्म देखने की तारतम्यता को बिगाड़ते हैं वो प्रक्रिया अंत तक बनी रहती है। फ़िल्म की मूल कहानी के लेखक हर्ष मंदेर हैं। जिसमें निर्देशक ने भी अपनी तरफ से कुछ जोड़कर फ़िल्म में लेखकीय क्रेडिट हासिल कर लिया है।