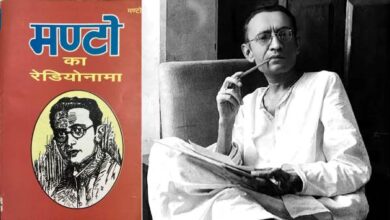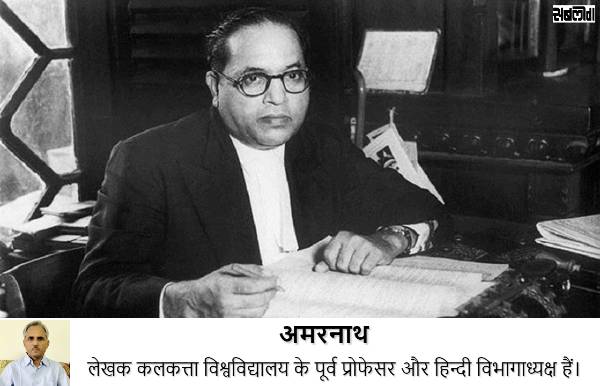सत्यजित राय (2 मई 1921- 23 अप्रैल 1992) की जन्मशताब्दी वर्ष पर विशेष
‘राय का सिनेमा न देखना इस जगत में सूर्य या चन्द्रमा को देखे बिना रहने के समान है।’ – अकिरा कुरोसावा
सत्यजित राय (2 मई 1921- 23 अप्रैल 1992) ने हिन्दी में दो फ़िल्में बनाई हैं। सत्यजित राय अपने उम्र के छपनवें बरस में प्रेमचंद की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ पर 1977 में इसी नाम से और दूसरी प्रेमचंद की ही कहानी ‘सद्गति’ पर अपने उम्र के साठवें पड़ाव पर 1981 में ‘सद्गति’ नाम से हिन्दी सिनेमा के रजत पट्ट पर दो क्लासिक्स प्रस्तुत किया। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म 1977 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म मानी गई। सत्यजित राय ने कुल 38 फिल्मों का निर्माण किया जिनमें से बहुतायत फ़िल्में बांग्ला भाषा की हैं।
उन्होंने पहली फ़िल्म 1955 में पश्चिम बंगला सरकार की मदद से ‘पाथेर पांचाली’ नाम से और अन्तिम फ़िल्म 1991 में राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम की मदद से ‘आगंतुक’ बनाई। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ हिन्दी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद (31 जुलाई 1880 – 8 अक्टूबर 1936) की प्रसिद्ध कहानी है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ की रचना प्रेमचंद ने अक्टूबर 1924 में की थी और यह ‘माधुरी’ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी प्रकाशन के लगभग तिरपन बरस बाद भारतीय सिनेमा के हस्ताक्षर, भारत रत्न से सम्मानित और 32वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्राप्त सत्यजित राय ने लखनऊ के सांस्कृतिक विन्यास को परदे पर उतारा। असल में, परदे पर शतरंज के मोहरे की गतिकी के खास निहितार्थ हैं।
भारत में अंग्रेजो द्वारा बढ़ते औपनिवेशिक छल के परिवेश में अपने ही अंतरद्वन्द्धों के कारण नवाबी और जागीरदारी की मिल्कियत के ढहते जाने की अनुगूंजों को अनसुना करते जाने की जिद के साथ हुक्के का धुंआ, पान की गिलोरी, चाँदी का पीकदान, मुर्गों की लड़ाई, पतंग का खेल दरअसल, अपने ही विरुद्ध कटार, तलवार, तमंचे इस्तेमाल कर लेने की परिस्थति का निर्माण कर रहा था। सत्यजित राय के कैमरे की आंख इन सबको हुक्के से उठते धुँए की लकीर के साथ बड़े ही महीन ढ़ंग से परदे पर उतार रहा था।
भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा के परिदृश्य को उसकी कथा-बुनावट और वस्तु-तत्व के आधार पर यदि देखें तो एकबारगी यह कह देने में अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती कि सिनेमा में यदि कथा-गाम्भीर्य है तो वह साहित्य के रास्ते पहुँचता है। विश्व की अधिकांश क्लासिक सिनेमा साहित्य पर आधारित रहीं हैं। इसकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। सत्यजित राय की सिनेमाई यात्रा को मुक्ममल यात्रा में तब्दील कर देने का काम साहित्य ने ही किया है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ‘साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्मों और फिल्मों की साहित्यिकता के बीच’ [1] फर्क होता है। उनकी पहली ही फ़िल्म ‘पाथेर पांचाली’ बंगला के प्रसिद्ध लेखक बिभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा 1929 में इसी नाम से लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। विभूति भूषण बनर्जी के उपन्यास की कथा पर ‘अपराजितो’ फ़िल्म बनाई गई। ‘पारस पत्थर’ फ़िल्म परशुराम की लघुकथा पर आधारित है। संगीत पर आधारित फ़िल्म ‘जलसा घर’ की कहानी का आधार ताराशंकर बनर्जी की लघु कहानी ‘जलसा घर’ है। ‘अपुर संसार’ फ़िल्म की कथा का आधार भी विभूतिभूषण बनर्जी के उपन्यास ही है।
सत्यजित राय की 1960 में निर्मित फ़िल्म ‘देवी’ प्रभात कुमार मुखर्जी की लघुकथा पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर की तीन लघु कहानियों पर आधारित ‘तीन कन्या’ 1961 में बनाई गई। ताराशंकर बनर्जी के उपन्यास अभिजान पर आधारित फ़िल्म ‘अभिजान’ बनाई गई। नरेन्द्रनाथ मित्र की लघुकथा ‘अबतरनीका’ पर आधारित फ़िल्म ‘महानगर’ बनाई गई। 1964 में सत्यजित राय द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध और चर्चित फ़िल्म ‘चारुलता’ रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास ‘नास्तेनीर’ के आधार पर निर्मित हुई। इसके ठीक एक साल बाद प्रेमेंद्र मित्रा की लघुकथा ‘जानायको कापुरुषेर’ और परशुराम की लघु कहानी ‘बिरंची बाबा’ के आधार पर ‘कापुरुष-ओ-महापुरुष’ बनाई गई।
शरदिंदु बनर्जी के उपन्यास ‘चिड़ियाखाना’ की कथा के आधार पर ‘चिड़ियाखाना’ 1967 में बनाई गई। उपेन्द्र किशोर राय की कहानी पर आधारित फ़िल्म ‘गोपी गायने बाघा बायने’ फ़िल्म बनाई गई। सुनील गाँगुली के सबसे चर्चित उपन्यास ‘अरण्येर दिन रात्रि’ पर इसी नाम से सत्यजित राय की प्रसिद्ध फ़िल्म बौद्धिकों की जमात में खूब सराही गई।‘प्रतिध्वनी’ फ़िल्म सुनील गाँगुली के इसी नाम से लिखे उपन्यास पर आधारित है।
शंकर के उपन्यास ‘सीमाबद्ध’ पर इसी नाम से 1971 में फ़िल्म बनाई गई और 1975 में शंकर के ही उपन्यास ‘जन अरण्य’ पर इसी नाम से फ़िल्म बनाई गई। एक बार फिर से 1973 में सत्यजित राय ने विभूतिभूषण बनर्जी के उपन्यास ‘अशनि संकेत’ पर इसी नाम से फ़िल्म बनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास ‘घरे बाहरे’ पर इसी नाम से 1984 में फ़िल्म बनाई गई। इब्सन के नाटक ‘एन एनिमी ऑफ़ पीपुल’ की कथा के आधार पर ‘गणशत्रु’ नाम से 1989 में फ़िल्म बनाई गई।
प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ और ‘सद्गति’ पर इसी नाम से क्रमशः सत्यजित राय ने फ़िल्म बनाई। दरअसल, सत्यजित राय की सिनेमाई यात्रा साहित्य के सहारे ही मुकम्मल हुई है। सत्यजित राय की सिनेमाई विशिष्टता के बारे में लखनऊ में ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म निर्माण-प्रक्रिया में साथ रहने वाले कुँवर नारायण अपने संस्मरण में जरुरी बात कहते हैं, इस बात के सहारे हम सत्यजित राय के समस्त सिनेमाई रूपबंध को समझ सकते है।
उनकी फिल्मों को याद करें, तो हम एक ऐसी विनम्र मानव-संस्कृति के सम्मुख होते हैं, जिसके वह स्वयं एक जीता-जागता स्रोत और सार थे। सहानुभूति (सिम्पैथी) और समानुभूति (एम्पैथी) उनके व्यक्तित्व का सहज गुण था।’[2] कुँवर नारायण अपने इस मंतव्य के साथ-साथ विस्तार से सत्यजित राय के हिन्दी सिनेमा ‘शतरंज के खिलाड़ी’ के निर्माण से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में लिखते हैं, जिसमें इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि सत्यजित राय को हिन्दी बहुत कम आती थी और वे हिन्दी सिनेमा बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे।[3] कुँवर नारायण के इस कथन के साथ सत्यजित राय के संदर्भ से कहे अकिरा अकिरा कुरोसावा के उपर्युक्त कथन को मिलाकर पढ़ने से सत्यजित राय और उनकी फिल्मों के बारे में एक मुकम्मल समझ बनाई जा सकती है।
सत्यजित राय के सिनेमाई विस्तार और उसके वस्तु-तत्व को अगर देखें तो बड़ी ही आसानी से उसमें निहित प्रगतिशील संदेश की पहचान कर सकते हैं। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण के सामयिक राग-विराग को उनके सिनेमा के प्रथम दृश्य की ताप से ही समझा जा सकता है। उनके सिनेमाई रूपबंध का भाष्य अंततः प्रगतिशीलता के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। सत्यजित राय के सिनेमा को प्रगतिशीलता के संदर्भ से समझने से पहले यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि दर्शक या सिनेमा का रसिक/भोक्ता जब उनकी फ़िल्म की तरफ़ जाए तो वह प्रगतिशीलता के दवाब में अपनी आखें बंद करके नहीं बल्कि तर्क और विवेक के साथ जाए।
यह केवल सत्यजित राय के सिनेमा के लिए ही नहीं बल्कि मोटे तौर पर भारतीय सिनेमा और विश्व सिनेमा की तरफ जाने के लिए भी जरुरी है। दरअसल, सिनेमा के कथा वर्णन का रूपविधान शास्त्रीय पद्धति का रहता आया है। जिसमें, एक प्रारंभ होता है और फिर मध्य के विकास में संघर्ष, इस संघर्ष के बाद अंत में यह समाधान की तरफ आगे बढ़ता है। असल में, यह भारतीय रस-विधान का एक सिद्ध परिदृश्य है, यह अरस्तु के विरेचन का भी विधान है।
यह विधान सीधी रेखा में घटित होती हुई मोटे तौर पर यांत्रिक हो जाया करती है। इसलिए समझ की कसौटी पर यह ठीक दिखलाई तो देती है लेकिन तर्क की कसौटी पर कई बार बाधा उत्त्पन्न कर देती है। हम जानते हैं कि भारतीय चिंताधारा का स्वरुप एकरेखीय की तुलना में हमेशा से चक्रीय रहा है। सत्यजित राय के सिनेमा में इस चक्रीयता की पहचान की जा सकती है। सत्यजित राय की सिनेमाई समझ और उनकी दृष्टि का आधार बहुत व्यापक रहा है इसलिए न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी उनकी सिनेमाई समझ को सराहा गया है।
अपने समय के ख्यात फ़िल्मकार अकिरा कुरोसावा (1910- 1998) ने सत्यजित राय के बारे में कहा है कि, ‘राय का सिनेमा न देखना इस जगत में सूर्य या चन्द्रमा को देखे बिना रहने के समान है।’ एक बारगी कुरोसोवा की यह उक्ति अपने प्रथम पाठ में अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है लेकिन सत्यजित राय के सिनेमाई विस्तार से एक-एक कर गुजरते हुए हमें यह लगने लगता है कि सत्यजित राय के सिनेमा को देखे बिना भारत और उसके वैविध्य को समझने का कोई भी दावा एक अधूरा और अपूर्ण दावा हो सकता है।
अमेरिकी सिने समीक्षक और सिनेमाई इतिहासकार रोजर एबर्ट (1942-2013) ने ‘जलसाघर’ पर लिखे अपने लेख में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि ‘सिनेमा के कई आलोचकों ने सत्यजित राय के सिनेमाई कृतियों को अन्य कई कलाकारों से तुलना की है-अंतोव चेखव, ज्यां रेनुआ, वित्तोरियो दे सिका, हावर्ड हॉक्स, मोत्सार्ट यहाँ तक की शेक्सपियर के समतुल्य पाया गया है।’[4] नाइपॉल ने ‘शतरंज के खिलाड़ी’ के एक दृश्य की तुलना शेक्सपियर के नाटकों से की है- ‘केवल तीन सौ शब्द बोले गए, लेकिन इतने में ही अद्भुत घटनाएँ हो गईं।’[5] दरअसल, सत्यजित राय अपने अध्ययनशील जीवन में ही पहेलियों और बहुअर्थी शब्दों के खेल से बहुत प्रेम करते थे।
सत्यजित राय के तमाम सिनेमाई लेखन और दृश्यों के चित्र में, बिंबों की बहुलार्थता में हम इस बात को रेखांकित किया जा सकता है। सत्यजित राय के बारे में यह बहुप्रचलित तथ्य है कि, वे पूरी फ़िल्म को पहले अपने नोटबुक पर स्केच कर लेते थे फिर उसका फिल्मांकन करते थे। सत्यजित राय की इस पद्धति के बारे में विश्व और भारतीय सिनेमा के पारखी कुँवर नारायण एक दृष्टांत देते हैं, ‘ नेपोलियन कहा करता था कि पूरा युद्ध पहले अपने मस्तिष्क में ही मैं जीत चुका होता हूँ- युद्धभूमि पर तो उसे केवल चरितार्थ करता हूँ।
कुछ-कुछ उसी तरह सत्यजित राय की फ़िल्में पहले उनकी नोटबुकों पर बनती हैं, फिर वे फिल्मों में परिवर्तित होती हैं।’[6] बच्चों की मनोवैज्ञानिक दुनिया और उसके सपने को लेकर सत्यजित राय ने केवल बेहतरीन लिखा है बल्कि उसे सिनेमाई परदे पर संवेदनशीलता के साथ उतारा भी है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ जैसे गंभीर सिनेमा के तत्काल बाद उन्होंने बच्चों के पसंद को ध्यान में रखकर 1978 में ‘जय बाबा फेलुनाथ’ फ़िल्म बनाई। यह कहा जाता है कि ‘शतरंज के खिलाड़ी’ की कथा-भूमि के प्रति सत्यजित राय की प्रतिबद्धता और उसके फिल्मांकन के लिए लखनऊ की परम्परा तथा उसका ‘लोकेल’ ने उनके मन-मस्तिष्क पर एक खास किस्म के सिनेमाई तनाव सृजित कर दिया था।
सत्यजित राय के साथ अपने संस्मरण में कुँवर नारायण कहते हैं कि, ‘पुराने लखनऊ के गली-कुचों में उनके साथ घूमते हुए मैंने कई बार अनुभव किया कि वे एक गुजिश्ता लखनऊ को सिर्फ फ़िल्मकार की निगाह से नहीं देख रहे थे, एक साहित्यकार और कवि की संवेदनशीलता से भी देख रहे थे।’[7] इसी कारण इस सिनेमा का तनाव सिनेमा के बन जाने के बाद भी उनपर रहा। इस सिनेमाई तनाव से बाहर निकलने के लिए सत्यजित राय ने ‘जय बाबा फेलुनाथ’ सिनेमा की रचना की।
असल में, ‘जय बाबा फेलुनाथ’ सिनेमा ‘शतरंज के खिलाड़ी’ के सिनेमाई परिवेश, उसके अर्थ-विन्यास और उसके ऐतिहासिक रूपबंध से सत्यजित राय को एक स्तर पर मुक्ति की तरह ले जाती है। असल में, सत्यजित राय की सेनेमेटिक दुनिया को ‘शतरंज के खिलाड़ी’ ने सघनता के साथ प्रभावित किया था। उनके अबतक के सिनेमाई सफ़र में यह एक भिन्न किस्म के परिवेश का सिनेमा था। मोटे तौर पर सत्यजित राय की लिखी हुई लगभग सभी कथानक बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका ‘एकशान’ में प्रकाशित हुई थी। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ बनाने से पूर्व सत्यजित राय ने सिनेमा पर 1976 में एक चर्चित किताब ‘आवर फ़िल्म्स, देयर फ़िल्म्स’ शीर्षक से लिखी थी।
इस किताब के पहले भाग में भारतीय सिनेमा के परिदृश्य का चित्रण है और दूसरे भाग में हॉलीवुड के सिनेमा का विवरण है। 1976 में ही एक दूसरी किताब ‘विषय चलचित्र’ नाम से सिनेमा के विभिन्न पहलुओं पर अपने चिंतनपरक विचार सत्यजित राय ने प्रस्तुत किए हैं। ‘एकेई बोले शूटिंग’ सत्यजित राय की एक और प्रसिद्ध किताब है। प्रेमचंद की कहानी ‘सद्गति’ पर फ़िल्म बनाने के बाद सत्यजित राय ने 1982 में अपनी आत्मकथा ‘जखन छोटो छिलम’ (जब मैं छोटा था) लिखी।
यह उल्लेखनीय है कि मशहूर भारतीय चिंतक आशीष नंदी ने अपनी किताब The Savage Freud : And Other Essays on Possible And Retrievable Selves (2000) में एक स्वतंत्र अध्याय सत्यजित राय की सिने दृष्टि पर लिखा है। हम यहाँ सत्यजित राय की फ़िल्म ‘शतरंज के खिलाड़ी’ पर स्वयं को केंद्रित करना चाहेंगे।
‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म सत्यजित राय के लिए एक मुश्किल भरा सिनेमाई सफ़र रहा है। बांग्ला भाषी होने के कारण उर्दू नफ़ासत से भरी हुई कहानी तथा उसकी भाषा-योजना और सिनेमा में लखनऊ संस्कृति के साथ तत्कालीन शाही परिवेश का संयोजन[8] उनके लिए चुनौती से भरा और बेहद खर्चीला भी रहा है। इस फ़िल्म की भाषा में लखनवी उर्दू जबान और अवधी बोली का एक सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करना सत्यजित राय के लिए चुनौतीपूर्ण और श्रमसाध्य रहा है।
फ़िल्म की सतह पर भाषाई संरचना में उर्दू और अवधी का प्रयोग सिनेमाई पात्रों के वर्गीय आधार पर संयोजित किया गया है। मोटे तौर पर उर्दू बोलने वाले राज्य-सत्ता से जुड़े हुए हैं और अवधी बोलने वाले लखनऊ के आम लोग। फ़िल्म एक एक पात्र कल्लू लखनऊ के नजदीक सीतापुर की अवधी बोली बोलता है इस अवधी बोली से भिन्न अवधी बेगम खुर्शीद की नौकरानी हिरिया बोलती है। यहाँ अवधी बोली का भी अपना-अपना ‘लोकेल’ है।
ऐसा नहीं था कि बांग्ला संस्कार के कारण सत्यजित राय में उर्दू का संस्कार बिलकुल नहीं था। वे बचपन में एक बार लखनऊ की यात्रा कर आये थे और वहाँ अपने एक नजदीक के रिश्तेदार अतुल प्रसाद सेन जो स्वंय एक संगीतकार थे, के घर पर उर्दू तहजीब और भाषा से प्रथम परिचय प्राप्त कर चुके थे। लखनऊ में उर्दू जबान और तहजीब से नजदीक का रिश्ता सत्यजित राय के लिए एक बार और बना जब वे 1958 में ‘जलसाघर’ फ़िल्म बना रहे थे और उसमें हसन अंसारी की एक प्रसिद्ध ठुमरी ‘भर-भर आई मोरी अखियाँ’ गाने के लिए बेगम अख्तर जो ‘जलसाघर’ फ़िल्म में दुर्गा बाई के नाम से एक गायिका की भूमिका भी अदा कर रही थी के घर लखनऊ पहुँचे।
बेगम अख्तर के पति इसतयाक अहमद अंसारी जो लखनऊ के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, के साथ सत्यजित राय ने लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार की बारीकी सीखी। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ का निर्देशन, पटकथा लेखन और उसके लिए संगीत तैयार करते हुए सत्यजित राय पर लखनऊ की पूर्व के यात्रा में सीखे तहजीब का असर रहा है। उनकी रंगीन फिल्मों में यह ‘शतरंज के खिलाड़ी’ सबसे मंहगी फ़िल्म है। इस फ़िल्म को इस्टमैन कलर में ढालने का कार्य मद्रास के जेमनी कलर लेब्रोटरी में हुआ था। इस फ़िल्म की ग्राफिक्स जेहरा तैयब जी और एनिमेशन राममोहन ने तैयार की है। इस फ़िल्म के लिए स्टूडियो का काम इन्द्रपुरी स्टूडियो, कलकत्ता और बंबई का प्रसिद्ध राजकमल कला मंदिर में संपन्न हुआ है।
‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म की पटकथा स्वयं सत्यजित राय ने लिखी है और इस फ़िल्म के संवाद के निर्माण में भी सत्यजित राय ने अपने साथ शमा जैदी और जावेद सिद्धिकी को जोड़ा है। पटकथा लेखन के बारे में जबकि बहुत पहले सत्यजित राय ने घोषणा कर रखी थी कि वे बांग्ला के अलावा अन्य किसी भी भाषा में न ही पटकथा लिखेंगे और न ही किसी फ़िल्म का निर्देशन करेंगे। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में उन्होंने अपने कथन को झुठलाया। कहा यह जाता है कि पचास के दशक से ही सत्यजित राय को शतरंज खेलने का शौक रहा है। अपनी पहली प्रसिद्ध फ़िल्म ‘पाथेर पांचाली’ के लिए पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अपनी शतरंज के खेल पर आधारित कई किताबें बेच दी थीं।
‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म के दृश्य-दर-दृश्य का संयोजन और संपादन का कार्य दुलाल दत्ता (1925-2010) द्वारा किया गया। दुलाल दत्ता के संपादन कार्य पर सत्यजित राय पर बहुत यकीन रहा है इसलिए सत्यजित राय ने लगभग अपनी सभी फिल्मों का संपादन कार्य दुलाल दत्ता से ही करवाया है। फ़िल्म के कथा-प्रवाह में संपादन का महत्त्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल, संपादन फ़िल्म के दृश्य-विन्यास को एक तारतम्यता में प्रस्तुत करते हुए दर्शक और सिनेमा के बीच संप्रेषण का मजबूत रिश्ता निर्मित करता है। लखनऊ की तहजीब और तत्कालीन परिवेश के मिज़ाज से मेल बैठाते हुए वस्त्र-विन्यास की जिम्मेदारी इस फ़िल्म में शमा जैदी ने निभाई है।
इस फ़िल्म के वार्डरोब का काम हारू दास ने संभाला है। शमा जैदी (1938) प्रसिद्ध पटकथा लेखिका और वस्त्र डिज़ाइनर हैं। वे चर्चित फ़िल्म ‘गर्म हवा’ के ख्यात फ़िल्म निर्देशक एम।एस। (1930) सथ्यु की पत्नी हैं। शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म का नृत्य निर्देशन अपने समय के मशहूर कत्थक नर्तक बिरजू महाराज (1938) ने किया है। इस फ़िल्म में बिरजू महाराज ने रेवा मुहुरी के साथ गायन का कार्य भी किया है। इस फ़िल्म में मेकअप के कार्य का संपादन अनंत दास ने और ध्वनि संयोजन नरेंद्र सिंह ने दुलाल दास के सहयोग से किया है।
इस पूरी फ़िल्म के लखनऊ सहित सभी लोकेशन का संयोजन जेएन श्रीवास्तव ने किया है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म के पहले दृश्य में ही दर्शक के सामने सबसे पहले एक नरेटर की ठोस आवाज उभरती है और यह नरेटर संपूर्ण फ़िल्म के अहम् मोड़ों पर इतिहास के तथ्यों के साथ दर्शक के सामने अपनी आवाज के साथ उपस्थित होता रहता है। नरेटर की यह आवाज अमिताभ बच्चन की है।
सत्यजित राय की ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म की संपूर्ण धुरी एक त्रिकोण पर टिकी हुई है। यह त्रिकोण एक-दूसरे से न केवल जुड़ी हुई है बल्कि कहीं-कहीं एक दूसरे को काटती हुई भी चलती है। इस त्रिकोण में तीन गाँठें हैं। यह गाँठ ज्यों-ज्यों फ़िल्म आगे बढ़ती जाती है क्रमशः खुलती जाती है। सचेत दर्शक इन गाँठों को आसानी से खुलता हुआ फ़िल्म में देख लेता है। यह गाँठें प्रेमचंद की कथा में जिस तरह से खुलती हैं उससे अलहदा सत्यजित राय की फ़िल्म में प्रभावी ढंग से खुलती हैं। दृश्यों के संचरण और उसके अभिग्रहण की एक अपनी मनोरचना होती है। दृश्यों का संयोजन इसे और भी अधिक प्रभावी बना देता है। इस त्रिकोण के एक कोण पर हम दो जागीरदार के शतरंज के खेल को रख सकते हैं।
जब लखनऊ को लार्ड डलहौजी की नीति की पृष्ठभूमि में रौंदे जाने की कवायद की जा रही थी तब यह दो खिलाड़ी अपने इस खेल के लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा रहे थे। वे शतरंज के लिए बीस तिकडम कर सकते थे किसी की जान ले सकते थे, रक्त बहा सकते थे लेकिन अपनी मातृभूमि अवध के लिए अपने रक्त का एक कतरा भी नहीं बहा सकते थे। दूसरे कोण पर इन जागीरदारों की बेगमें हैं।
एक की बेगम अपने पति से प्रेम पाने के लिए शतरंज के खेल से चिढ़ती रहती है और दूसरे की बेगम अपने पति से इतर अपने घर के एकांत में प्रेमी से प्रेम पाने के लिए घर में खेले जा रहे शतरंज से चिढ़ती है। दोनों जागीरदारों की दिनचर्या में शतरंज और दोनों बेगमों का अपना-अपना यौन-प्रहसन सामंती व्यवस्था के भीतर की सड़ांध को रेखांकित करता है। दोनों जागीरदारों को हर कीमत पर शतरंज का खेल चाहिए और दोनों बेगमों को यौन-प्रेम। फ़िल्म में जागीरदारों के लिए शतरंज के खेल और उनकी बेगमों के लिए यौन-प्रेम का आधार धीरे-धीरे खिसकता चला जाता है। जागीरदार और बेगमें जीतनी तन्मयता से अपनी आकांक्षा को पूरे करना चाहते हैं।
उतनी ही तेजी से उनकी आकांक्षा उनसे दूर होती चली जाती है। दोनों के आधार खिसकने का तनाव पूरी फ़िल्म की संरचना में हमें दृश-दर-दृश्य दिखलाई देता है। दोनों बेगमों के प्रेम की वरीयताओं और उससे उत्पन्न विरोधाभास के कारण दोनों जागीरदारों के बीच तल्खी उत्पन्न कर देता है। तीसरे कोण पर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम और नवाब वाजिद अली शाह की माँ आलिया बेगम का संवाद है।
इस कोण में तनाव तब उत्पन्न होता है जब फ़िल्म के एक दृश्य में दोनों के बीच एक परदा झूलता रहता है और दोनों अवध की किस्मत पर बात कर रहे होते हैं। आलिया बेगम से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम के चेहरे में एक असीम पीड़ा का भाव पैदा लेता है। सत्यजित राय के कैमरे ने जेम्स ऑउटरेम के चेहरे पर पीड़ा से उभरने वाली सूक्ष्म रेखाओं को बड़ी ही बारीकी से परदे पर उतारा है।
एक दूसरे दृश्य में जब वाजिद अली शाह के सामने लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम लखनऊ के करारनामे पर दस्तख़त करने का प्रस्ताव रखता है तब इस प्रस्ताव को सुनने के बाद वाजिद अली शाह अपनी जलती मासूम और ठहरी निगाह से लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम को देखते हुए उसके सामने अपना ताज पेश करते हुए कहता है, कि वे ताज तो दे सकते हैं लेकिन अपने महबूब शहर लखनऊ के लिए समझौते के करारनामे पर दस्तख़त नहीं कर सकते हैं। अपनी धरती के प्रति नवाब की प्रतिबद्धता को देखकर लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम की आखें नवाब वाजिद अली शाह के सामने झुक जाती हैं।
खुद्दार आलिया बेगम के सामने जनरल जेम्स ओउटरेम के चेहरे पर असीम पीड़ा का भाव और वाजिद अली शाह के स्वाभिमान के सामने झुकी हुई आखों के कोण और उसपर उभरती हुई रेखाओं की हरकत को अपने कैमरे में कैद करने वाले सोमेन्द्र राय के कैमरा संचालन को सिर्फ इस दृश्य के लिए पूरे अंक दिए जाने चाहिए। पूरी फ़िल्म में सोमेन्द्र राय का कैमरा संचालन बेहतरीन रहा है। जनानखाने में अपनी रानियों के बीच बैठे हुए वाजिद अली शाह के चेहरे पर पसरती हुई विलासिता का सौंदर्य और ठीक उसके विपरीत एक दूसरे दृश्य में अपना ताज अंग्रेज के सामने पेश करते हुए चेहरे पर लाचारी, बेबसी और कराह को जिस बेहतरीन ढंग से कैमरे की आँख पकड़ती है वह अपने आप में विलक्षण है।
ख़ामोशी से गतिशील कैमरे के कोण और दृश्यों के संयोजन से वाजिद अली शाह द्वारा ब्रितानी हुकूमत को उसकी नीचता का अहसास करा देने के दृश्य में एक भाषाई विन्यास उपस्थित हो जाता है। वैश्विक स्तर पर कैमरे का कमाल सधे हुए ढ़ंग से हम प्रसिद्ध फ्रेंच फ़िल्म निर्देशक ज्याँ रेनुआ (1894-1979) की फ़िल्म ‘द रिवर’ (1951) के दृश्यों में देख सकते हैं। यह कह देना गैरजरूरी नहीं होगा कि सत्यजित राय पर ज्याँ रेनुआ का असर रहा है और ज्याँ रेनुआ के कलकत्ता आगमन पर सत्यजित राय की मुलाकात भी ज्याँ रेनुआ से रही है। सत्यजित राय की एक घंटे सतावन मिनट की ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म में यह त्रिकोण अपनी गति में कथा के कई गांठों को सुलझाता चलता है।
‘शतरंज के खिलाड़ी’ कहानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह (1822-1887) के शासन व्यवस्था के बीच उन्नीस सौ सत्तावन की क्रांति से ठीक एक बरस पहले लखनऊ के सामाजिक परिवेश को चित्रित करता है। नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब की छठी पीढ़ी के नवाब थे, वाजिद अली शाह के पिता का नाम अमजद अली शाह और माता का नाम मलिका किश्वर बहादुर फ़क्र-उज-जमानी ताज आरा बेगम जिसे लोग आदर से जनाबे आलिया कहकर पुकारते थे।
अपने पति अमजद अली शाह की मृत्यु के बाद यह एक ताकतवर महिला के रूप में अवध में जानी गई और अपने चार बेटों में से बड़े बेटे वाजिद अली शाह के तख़्त की सलामती के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम के साथ संवाद कायम करती हुई एक खुद्दार स्त्री के चरित्र में लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम के कारनामों के कारण उसे लज्जित करती है। वह लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम द्वारा मुआवजे के प्रस्ताव को ठुकरा कर इंसाफ की माँग करती है और लखनऊ को लेकर बनाए गए करारनामे पर दस्तख़त से असहमत होते हुए ब्रिटिश रानी विक्टोरिया से मिलने लंदन की यात्रा पर चली जाती है।
ब्रिटिश लेखिका और लखनऊ की संस्कृति की जानकर रोजी लिवेलं जोंस ने नवाब वाजिद अली शाह की जीवनी ‘द लास्ट किंग इन इंडिया वाजिद अली शाह’ में रानी विक्टोरिया से जनाबे आलिया की मिलने की तारीख 4 जुलाई 1857, दिन-शनिवार,समय-2।45[9] बताई है। भारत का इतिहास वाजिद अली शाह को एक विलासी नवाब के रूप में स्थापित करता है एक ऐसा नवाब जिसे राज-पाट सँभालने में कोई रूचि नहीं थी। दरअसल, इतिहास में इस नवाब के मूल्यांकन में हमें अन्याय दिखलाई देता है। वास्तव में वाजिद अली शाह एक कला-प्रेमी नवाब रहे हैं। नृत्य, नाटक, संगीत और गीत लेखन में उनकी निजी रूचि रही है।
वे एक प्रगतिशील शायर के रूप में याद किए जाते तो हैं ही उसके साथ सभी धर्मों का एक सामान आदर करने वाले एक विनम्र नवाब के रूप में भी याद किए जाते हैं। 1847 में जब नवाब की ताजपोशी की गई थी तब उन्हें ‘कैसरे-जमाना’ की उपाधि दी गई थी। नवाब बनने से पूर्व उन्होंने दो रोमानी मसनवियाँ भी लिखी थीं। एक का नाम ‘दरिया-ए-तअश्शुक’ (प्यार का दरिया) और दूसरे का नाम ‘बहरे इश्क’ (प्यार का सागर) था। ‘इश्कनामा’ नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है।
वाजिद अली शाह द्वारा भारत में लोक-नाट्य परम्परा को काफी आगे बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है। विशेषकर कृष्ण की गाथा कहने की परम्परा का।[10] फ़िल्म के अड़तालीसवें मिनट पर बिरजू महाराज के नृत्य निर्देशन में एक ठुमरी ‘कान्हा मैं तोसे हारी, छोड़ो मोरी सारी’ कत्थक नृत्यांगना शास्वती सेन के साथ गीतांजली और कत्थक कला केंद्र, नई दिल्ली की टीम द्वारा कत्थक नृत्य के साथ प्रस्तुत हुआ है। वाजिद अली शाह बड़ी ही तन्मयता से नृत्य के भाव के साथ गतिमान हैं और ठुमरी में कृष्ण के वर्णन को सुन रहे हैं। हिन्दू देवता कृष्ण से वाजिद अली शाह का लगाव इतिहास की सच्चाई है। अमजद खान ने इस दृश्य में अपनी पारंपरिक खलनायक की छवि से एकदम बाहर एक के कलाकार लगते हैं।
इस दृश्य में अमजद खान की बोलती आँखें क्लोज शॉट में यही सबसे अधिक प्रभावीशाली हुई है। असल में, बोलती आँखों का यह कमाल सिर्फ अमजद खान का ही नहीं बल्कि कैमरा मैं सोमेन्द्र राय का भी है। फ़िल्म में जनाबे अलिया की दमदार भूमिका वीना (1926-2004) ने निभाई है। वीना का नाम हिन्दी फ़िल्म में अदब से लिया जाता है, इनका वास्तविक नाम ताजौर सुल्ताना था। ‘चलती का नाम गाड़ी’ फ़िल्म में यह कामिनी नाम से भूमिका निभाई थी, वीना, ताजमहल फ़िल्म में नूरजहाँ और पाकीज़ा फ़िल्म में साहेबजान से ख्यात हुईं।
प्रेमचंद की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में नजाकत-नफ़ासत का लखनऊ शहर सामंती ढ़ांचे के भीतर भोग-विलास में डूबा, राजनीतिक-सामाजिक यथार्थ से विलग चेतनाशून्य अवस्था में अपनी सुबह और शाम करता है। शहर के इस भूगोल का प्रमाण सत्यजित राय की फ़िल्म के पहले ही दृश्य में दिखलाई देता है। सिनेमा के पहले ही दृश्य में इमामबाड़े की पृष्ठभूमि में कबूतरों का उड़ना, पतंगे लड़ाना और मुर्गे लड़ाने का दृश्य लखनऊ की 1856 की बेपरवाह आबो-हवा का परिचय देती है। इस दृश्य की आबो-हवा में 1857 के आसन्न खतरों और ब्रितानी हुकूमत द्वारा अवध के लिए बुने जा रहे षड्यंत्रों की कोई गंध नहीं है। संघर्ष और विरोध का कोई सिरा हमें दिखलाई नहीं देता। यहाँ हमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक द्वैत दिखलाई देता है जिसकी प्राथमिकता केवल भोग-विलास है।
हम यहाँ प्रेमचंद की कहानी और सत्यजित राय की फ़िल्म के कथानक की एक साझी तस्वीर आपके सामने इस उद्देश्य से रखना चाहते हैं जिससे यह समझा जा सके कि इस कहानी और फ़िल्म में शतरंज के मोहरे सिर्फ निर्जीव मोहरे नहीं हैं बल्कि ये मोहरे अपनी प्रतीकात्मकता में समय की पूरी चाल को व्याख्यायित करती है, राज्य-तंत्र की कीमियागिरी और उसके खोखलेपन को उजागर करती है, दो व्यक्तियों (जागीरदारों) के बीच संबंधों की छद्म और ईर्ष्यालु दुनिया, झूठी शान-शौकत आत्म-अभिमान से ग्रस्त और अपने फर्ज से च्युत समाज के ढ़ांचे को समझ सकें।
इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं – मिरज़ा सज्जाद अली, सिनेमा में जिसकी भूमिका संजीव कुमार (1938-1985) और मीर रौशन अली सिनेमा में जिसकी भूमिका सईद जाफ़री (1929-2015) ने निभाई है। दोनों वाजिद अली शाह के बड़े जागीरदार हैं। जीवन की बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ एशो-आराम की सभी ज़रूरतों के लिए उन्हें न कोई चिंता है और उसके लिए न ही कोई अलग से काम करना है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है और दोनों का साझा शौक भी है। शौक है शतरंज खेलना है।
शतरंज के खेल के लिए वे दोनों कोई भी इम्तहान देने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों दोस्तों की बेगमें और नौकर-चाकर उनके इस शौक से परेशान रहते हैं। कथा और सिनेमा के अन्य पात्र अपनी-अपनी भूमिका में दोनों दोस्तों के कार्य-व्यापार के वातावरण को और अधिक प्रगाढ़ कर देता है। समानांतर और व्यावसायिक सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आज़मी (1950) ने मिर्ज़ा सज्जाद अली की बेगम खुर्शीद की भूमिका निभाई है। चरित्र भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध फरीदा जलाल (1949) ने मीर रोशन अली की बेगम नफ़ीसा की भूमिका अदा की है।
अपने समय के मशहूर अभिनेता अमजद ख़ान (1940-1992) ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई है। फ़ारुख़ शेख़ (1948-2013) ने मीर रोशन अली की बेगम के प्रेमी के रूप में अक़ील की भूमिका निभाई है। हॉलीवुड की दुनिया में चर्चित अभिनेता और ‘गाँधी’ (1983) जैसी प्रसिद्ध फ़िल्म के निर्देशक रिचर्ड एड्नबेरो (1923-2014) ने इस फ़िल्म में लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ऑउटरेम (1803-1863) की भूमिका निभाई है।
मिर्जा सज्जाद अली के मुंशी की भूमिका हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता डेविड अब्राहम (1908-1981) ने मुंशी नन्दलाल के नाम से निभाई है। प्रेमचंद की कथा से अलग ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म में मुंशी नंदलाल पात्र की सृष्टि सत्यजित राय की अपनी रचनात्मक छूट है। डेविड अब्राहम सत्तर के दशक की अधिकांश फिल्मों के अनिवार्य चरित्र अभिनेता रहें हैं। फ़िल्म के बीसवें मिनट में मुंशी नन्दलाल, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली के संवाद को ध्यान से सुना जाना चाहिए।
मुंशी नंदलाल शतरंज के खेल को हिन्दुस्तानी इजाद बताते हुए उसके खेलने के हिन्दुस्तानी तरीके और ब्रितानी तरीके में जब फर्क बता रहे होते हैं तब वे महज शतरंज के खेल के तरीके के बारे में फर्क नहीं बता नहीं रहे होते हैं बल्कि हिंदुस्तान पर ब्रितानी हुकूमत के बढ़ते हुए दवाब और बदलते हुए समय का संकेत कर रहे होते हैं। दोनों जागीरदारों को मुंशी नन्दलाल के इस कथन में छिपे संकेत से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जब मुंशी नन्दलाल सीधे-सीधे कहता है कि ‘मुझे तो लार्ड डलहौजी की नियत पर शक है।’ तब भी दोनों जागीरदार बेपरवाही में अपनी झूठी शान के कसीदे पढ़ते रहते हैं। दोनों जागीरदारों को इस बात पर हँसी आती है कि ब्रिटिश कैसे मूर्ख हैं जो रेल और तार की व्यवस्था हिंदुस्तान में ला रहे हैं। एक अदूरदर्शी जागीरदार की यह छवि तत्कालीन अवध समाज में भी दिखलाई देती है और यही छवि सत्यजित राय की इस पूरी फ़िल्म में गति करती है। सिनेमा में शतरंज के मोहरे और मोहरे की सतह पर फिसलती अंगुलियों का क्लोज शॉट एक संजीव पात्र की तरह सिनेमाई कथा को एक नई भाषा प्रदान करता है।
कहानी और सिनेमा के कथानक के एक मोड़ पर मिर्जा सज्जाद अली के घर में मिर्जा और मीर रोशन अली के बीच शतरंज बिछी हुई है। दोनों तन्मयता के साथ अपनी-अपनी चाल चल रहे हैं। मिर्जा की बेगम खुर्शीद अपनी नौकरानी हिरिया जिसकी भूमिका हिन्दी फ़िल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला मिश्रा (1908-1988) ने निभाई है, जिसे हम अनेक भूमिकाओं में से एक ‘शोले’ फ़िल्म की मौसी के रूप में स्मरण रखते हैं, को बार-बार मिर्जा के पास यह कहलवाने के लिए भेजती है कि, बेगम बीमार है और उसके सर में तेज दर्द हो रहा है।
मिर्जा साहब शतरंज के मोहरे और उसकी हर आने वाली बाजी को शह और मात के रूप में बदल देने की फ़िराक में हैं और इस चक्कर में वे अपनी बेगम के बुलावे को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन फिर बार-बार बुलाने पर और रोशन अली के कहने पर वे अपनी बेगम के पास जाते हैं। बेगम को न कोई बीमारी है और न ही कोई सर में दर्द। बेगम मिर्जा साहब के जिस्म में प्रेम के आवेग में लिपट जाती है। मिर्जा के ज़ेहन में प्रेम और और उतेजना नहीं है बल्कि उसके ज़ेहन में शतरंज के मोहरे हैं जिसे वह बिसात पर छोड़ आया है।
लिहाजा मिर्जा में प्रेम का कोई आवेग उत्पन्न नहीं होता और यौन आवेग में बेगम को तड़पता छोड़ वह फिर शतरंज की बिसात पर जा बैठता है। यौन-प्रेम के इसी आवेग में एक दिन बेगम गुस्सा करती हैं और तंग आकर उन दोनों को खरी-खोटी सुनाती हुई खेल के सारे ताम-झाम को ड्योढी के बाहर फेंक देती है। दोनों दोस्तों के लिए खेल का अब नया ठिकाना मीर रोशन अली का घर बन जाता है। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक-ठाक खेल चलता है लेकिन धीरे- धीरे मीर रोशन अली की बेगम नफ़ीसा को दिक्कत होने लगती है।
असल में इस दिक्कत का कारण भी प्रेम है। जब मीर रोशन अली घर में नहीं हुआ करते थे तब नफ़ीसा से मिलने उसका प्रेमी अकील आया-जाया करता था जिसके साथ वह अपना यौन-व्यवहार स्वछंद रूप से कर लेती थी। अब घर में ही शतरंज के खेले जाने के कारण प्रेम-व्यवहार में बाधा उत्पन्न होने लगती है। प्रेमचंद की कहानी में यह यौन-संदर्भ एकदम खुले रूप में नहीं बल्कि कुछ संकेतों के माध्यम से आया है।
कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं कि, ‘मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। इसलिए वह उनके शतरंज खेलने के प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी-कभी मीर साहब को देर हो जाती तो उन्हें याद दिला देती थी।’ प्रेमचंद के इस कथन में जो ‘अज्ञात कारण’ है उसी के अवकाश से सत्यजित राय ने अपनी फ़िल्म के लिए मीर की बेगम नफ़ीसा और शकील के बीच के प्रेम संदर्भों की कल्पना की।
असल में, सत्यजित राय के बारे में यह धारणा रही है कि वे मूल रचना की बुनियादी पहचान से कोई छेड़-छाड़ नहीं करते हैं। वे मूल कृति की पहचान बनाए/बचाए रखने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन, अपनी इस पक्षधरता का निर्वाह वे मोटे तौर पर ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में नहीं कर सके हैं। प्रेमचंद की कहानी के कुछ प्रसंगों को उन्होंने अपनी फ़िल्म में बदल दिया है। जिन दिनों सत्यजित राय यह फ़िल्म लखनऊ में रहकर बना रहे थे, उन दिनों उनकी मुलाकात कुँवर नारायण से हुआ करती थी।
इस फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया को नजदीक से कुँवर नारायण ने देखा था। प्रेमचंद की कहानी के कुछ प्रसंगों के फ़िल्म में बदलाव को लेकर कुँवर नारायण की एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी है, ‘… इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमचंद की कहानी के बारीक रेशे फ़िल्म की इतिहास-सामग्री की दंद-फंद के नीचे बहुत कुछ दब भी गए। पुरानी लखनवी तहजीब के प्रति सत्यजित राय के मन में किंचित भावुक-सा लगाव था।’[11] प्रेमचंद और सत्यजित राय की दृष्टि का प्रस्थान बिंदु दरअसल अलग-अलग है।
प्रेमचंद की दृष्टि में यथार्थ को कहने की एक बेबाकी है और सत्यजित राय की दृष्टि में एक खास किस्म की लायात्कता है। इसलिए, कहानी के ट्रीटमेंट में कुछ दृश्यों में बदलाव दिखलाई देते हैं। बहरहाल, मीर रौशन अली के घर में रहने और शतरंज खेलने के कारण नफ़ीसा को यौन-व्यवहार में दिक्कत होने लगती है। इसके लिए नफ़ीसा और उसका प्रेमी शकील एक जुगत लगाता है। दोनों दोस्तों के बीच जब एक दिन शतरंज की बाजी बिछी हुई होती है तब उसी समय नफ़ीसा और अकील की जुगत से शाही फ़ौज का एक छद्म अफ़सर नफ़ीसा के घर पर मीर को ढूंढता हुआ पहुँचता है। उसे देखते ही मीर रोशन अली के होश उड़ जाते हैं।
वह शाही अफसर मीर साहब के नौकरों को खूब डराता-धमकाता है और मीर को ढूंढता है। नौकरों द्वारा झूठ बोल देने पर कि मीर घर में नहीं हैं, वह अफसर फिर अगले दिन आने की बात करके चला जाता है। नफ़ीसा द्वारा रचे इस तमाशे का असर मीर पर होता है। दोनों दोस्त चिंतित होते हैं और शतरंज के खेल के लिए दूसरे ठिकाने की तलाश में भटकने लगते हैं। नफ़ीसा स्वछंद हो कर अपने प्रेमी से मिलती रहती है।
दोनों जागीरदारों की बेगमों की यौन-आकांक्षा और यौन- संतुष्टि के लिए अपनाई जाने वाली विधि इस कथा की एक ऐसी गाँठ है जिसे सामंती परिवेश में स्त्री की वास्तविक स्थितियों और तत्कालीन समय के कार्य-व्यवहारों में स्त्री की स्थिति के परिदृश्य में देखा और समझा जा सकता है। निर्बाध शतरंज खेलने की नई जगह ढूंढते हुए दोनों जागीरदारों की यह तलाश ख़त्म होती है शहर से दूर, गोमती के किनारे एक विरान मस्ज़िद में। दरअसल, वहाँ किसी शाही फौज का खतरा नहीं रहता। वहाँ कोई आता-जाता भी नहीं है। दोनों एक दिन अलसुबह अपने साथ जरूरी सामान- हुक्का, चिलम, दरी आदि लेकर गोमती के किनारे मस्जिद में शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ जाते हैं।
सत्यजित राय की फ़िल्म में दोनों जागीरदार मस्जिद की तलाश में निकलते तो हैं लेकिन यह मस्जिद उन्हें नहीं मिलती है। फ़िल्म में दोनों दोस्त जब उस मस्जिद की खोज में गोमती किनारे पहुँचते हैं, तब मीर रोशन अली मिर्जा साहब से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि दरअसल जिस मस्जिद की वे बात कर रहे थे वह तो उन्होंने बचपन में कानपूर में देखी थीं। यह सुनकर मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली पर नाराज होते हैं। इधर-उधर देखते हुए उनकी नज़र एक किशोर बच्चे पर पड़ती है। फ़िल्म में इस बच्चे का नाम कल्लू है जिसकी भूमिका समर्थ नारायण ने निभाई है। फ़िल्म में कल्लू पात्र की सृष्टि भी सत्यजित राय की अपनी मौलिक सृष्टि है।
दुर्भाग्य से समर्थ नारायण की कोई भी जानकारी ठीक से अब उपलब्ध नहीं है। यहीं पर यह कह देना जरुरी समझता हूँ कि हिन्दी फिल्मों में ऐसे सैंकड़ों कलाकार रहें हैं जो अपना काम कर एक दिन गुमनामी में खो जाते हैं। ऐसे गुमनाम पात्रों का हिन्दी फ़िल्म की दुनिया में कोई अस्तित्व दिखलाई नहीं देता। हिन्दी फिल्मों का यह सबसे काला पक्ष है। ऐसे गुमनाम कलाकारों पर वक्त ने जो राख फैलाई है उसे हटाना और उसपर ठीक से लिखा जाना अब भी शेष है। बहरहाल, कल्लू उन दोनों दोस्तों को अपने वीरान मिट्टी के टूट-फूटे घर में शतरंज खेलने के लिए ले आता है और उन दोनों की तीमारदारी करता है।
असल में इस विराने में कल्लू अकेला इसलिए है क्योंकि कल्लू के घर के लोग अंग्रेजो के डर के कारण घर छोड़कर चले जाते हैं। कल्लू सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि वह ब्रिटिश फ़ौज को लाल ड्रेस पहने देखना चाहता है। यह लाल ड्रेस उससे बहुत अच्छी लगती है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ फ़िल्म के घुमाव-तंत्र को सत्यजित राय स्वयं द्वारा आविष्कृत पात्र कल्लू के माध्यम से बदल देते हैं। कल्लू की उम्र अभी खेलने,पढ़ने की है।
वह अपने परिवार के साथ सिर्फ इसलिए नहीं जाता है कि उसे ब्रिटिश फ़ौज की लाल ड्रेस देखनी है। उसके परिवार ब्रिटिश फ़ौज से डरकर घर से चले जाते हैं। कल्लू ब्रिटिश फ़ौज से डरता नहीं है बल्कि उसके सामने खड़े होकर उसकी ड्रेस देखना चाहता है। कल्लू से जुड़ा यह संपूर्ण प्रकरण फ़िल्म की ताप को एक भिन्न धरातल पर समझे जाने की वकालत करता है। फ़िल्म का यह दृश्यबंद बेहद मारक है। जहाँ एक ओर दोनों दोस्त, मिर्जा और रोशन जिस ब्रितानी फ़ौज से बचने के लिए इस वीराने का सहारा ले रहे हैं, एक बच्चा कल्लू इस वीराने में सिर्फ इसलिए रुका है कि वह ब्रितानी फ़ौज और उसके लाल ड्रेस को देख सके।
फ़िल्म के तमाम त्रासद दृश्यों में से एक दृश्य के रूप में इसे भी समझा जा सकता है। फ़िल्म में कथा की एक गाँठ बच्चे कल्लू के माध्यम से भी लक्षित किया जा सकता है। इस गाँठ के कई माइने इस फ़िल्म में और फ़िल्म के परिवेश से बाहर भी खुलते हैं। सत्यजित राय की इस फ़िल्म में ऐसे ढ़ेरों दृश्य हैं जो इतिहास के एक ‘पाठ’ की तरह हमारे सामने आते हैं। इसी कारण सत्यजित राय की इस फ़िल्म के बारे में चिदानन्द दास गुप्ता ने अपनी किताब ‘सत्यजित राय का सिनेमा’ में यह कहा है कि, ‘शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली और उनके लखनऊ के पतन और ब्रिटिश शक्ति से पहले इसके ढह जाने की ऐतिहासिक अपरिहार्यता की तस्वीर को स्पष्ट: देखती है, तथापि यह उत्कृष्टता, स्वाभिमान और उस नवाबी त्रासदी के संकेत की भी पहचान करती है जो इस पतन को आच्छादित दिए हुए है।’[12]
बहरहाल, कल्लू के घर में बाजी बिछती है। दोनों दोस्त मगन होकर अपनी-अपनी मोहरे चलते हैं। कोई एक पर भारी पड़ता है तो अगले ही पल दूसरा भारी पड़ जाता है। फ़िलहाल, मीर रोशन अली मिर्जा साहब पर भारी पड़े हुए हैं। फ़िल्म में यहीं पर दृश्य अपनी अन्तिम करवट लेता है। परदे पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वीरान और उदास आखें उभरती हैं। उनके दरबार में आज जनरल जेम्स ऑउटरेम अपने दुभाषिए कैप्टन वेस्टन फ़िल्म में जिसकी भूमिका टाम आल्टर (1950-2017) ने निभाई है, को लेकर उपस्थित हुए हैं। वे अवध के विलय के समझौते पर दस्तख़त करने के लिए नवाब को समझाने के लिए आए हुए हैं।
अवध के नवाब को तीन दिनों के भीतर फैसला लेने की मोहलत दी जाती है। नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका में अमजद खान के चेहरे पर अवध की विरासत को खो देने का बेशुमार दर्द उभरता है। वाजिद अली शाह अपने सिंहासन से उठते हुए अपने ताज को सर से उतारकर जनरल जेम्स ऑउटरेम के सामने कर देता है। जनरल जेम्स ऑउटरेम कहता है, यह मेरे किसी काम की चीज नहीं है। वह केवल अवध के विलयन के करारनामे पर दस्तख़त चाहता है।
नवाब वाजिद अली शाह, जनरल जेम्स ऑउटरेम से कहता है आप मेरा ताज ले सकते हैं लेकिन दस्तख़त नहीं। हम जानते हैं कि बाद में नवाब को मृत्युपर्यंत कलकत्ता निर्वासित कर दिया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह फिर कभी अपने वतन लखनऊ नहीं लौट पाते हैं। फ़िल्म फिर लौटती है दोनों दोस्तों के बीच बीछे शतरंज की बिसात पर। कैमरा मोहरों पर केंद्रित हो जाता है। मिर्जा पर भारी पड़े मीर के मोहरे ने मिर्जा को बैचैन कर रखा है। इसी बेचैनी में मिर्जा सज्जाद अली, मीर रौशन अली पर मीर की पत्नी के गैर मर्द के साथ संबंध पर तंज कसते हैं।
मीर क्रोधित होते हुए कहता है कि यह इल्जाम आप मुझपर इसलिए लगा रहे हैं कि मेरा दिमाग भटक जाए और मैं बाजी हार जाऊं। दोनों एक दूसरे से उलझ जाते हैं, एक दूसरे के खानदान और हैसियत को कोसते हुए अचानक मीर अपने साथ लाया तमंचा मिर्जा पर तान देता है और मिर्जा के तमंचे को दूर फेंक देता है। प्रेमचंद की कहानी में दोनों पात्रों के पास कटार और तलवारे होतीं हैं जिससे लड़ते हुए दोनों लहूलुहान होते हैं और अंत में मर जाते हैं। असल में, जिसने अपने नवाब के लिए, ब्रिटिश से अपनी मातृभूमि अवध की रक्षा के लिए कभी तलवारें नहीं उठाई वह शतरंज के खेल के लिए आपस में लड़ कर मर जाते हैं। कथा की एक गाँठ यहाँ भी खुलती है।
सामंती व्यवस्था के विरोधाभासों से भरे परिवेश में व्यक्ति का अंत ऐसे ही होता है। प्रेमचंद की कथा में तलवार और कटार सत्यजित राय की फ़िल्म में तमंचे के रूप में बदल जाता है। मिर्जा, मीर को समझाते हैं कि वे उनकी बेगम को लेकर कोई गलतबयानी नहीं कर रहे हैं इसलिए मीर को अपना तमंचा हटा लेना चाहिए। मिर्जा तमंचा हटाने की अपील करते हैं। ठीक इसी समय कल्लू अचानक आकर सूचना देता है कि, गोरी पलटन आ रही है। हड़बड़ाहट में मीर के तमंचे से गोली छूट जाती है और मिर्जा साहब के बाँह को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। ठीक इसी समय परदे परदे पर दृश्य बदल जाता है। यह दृश्य भारतीय इतिहास की सच्चाई से सृजित है।
ब्रिटिश हुकूमत के लहराते झंडे और उसकी फौज, गारद करते हुए लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत अवध के नवाब वाजिद अली शाह को तीन दिन बाद 7 फ़रवरी 1956 को गिरफ्तार करके कलकत्ता ले जा रहे होते हैं। कल्लू सूचना देता है कि चौक में भगदड़ मच गई है कोई अपने नवाब के लिए नहीं लड़ता है, सब भाग रहे हैं। अवध का तत्कालीन सामंती समय भोग-विलास में इतना डूबा हुआ था कि ब्रिटिश फ़ौज से संघर्ष का कोई आत्मबल तक उनमें बचा नहीं था।
शतरंज के दोनों खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी में आपस में लड़कर मर जाते हैं लेकिन अपने नवाब के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते। सत्यजित राय की फ़िल्म में दोनों आपस में लड़ते तो हैं लेकिन अपने नवाब के लिए न लड़ पाने का अफ़सोस भी जताते हैं। वे अपनी कायरता को जानते हैं इसलिए घर लौटने के लिए अँधेरे का इतंजार करते हैं। मिर्जा कहते हैं, मुँह छिपाने के लिए अँधेरे की जरूरत होती है। मीर अपने लिए कहते हैं जो अपनी बीबी न संभाल सका वो भला मुल्क के लिए क्या लड़ेगा। दोनों शतरंज की बाजी फिर बिछा लेते हैं। मिर्जा मोहरे उठाता हुआ घोषणा करता है महारानी विक्टोरिया पधार रहीं हैं। फ़िल्म यहीं समाप्त हो जाती है।
प्रेमचंद की कहानी दोनों जागीरदारों की मृत्यु पर समाप्त होती है। प्रेमचंद की कहानी में आपसे में लड़ते हुए जागीरदारों की मृत्यु एक तरह से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य खात्मे की घोषणा है। प्रेमचंद के यहाँ शतरंज के मोहरे आखिर में बिखर जाते हैं लेकिन सत्यजित राय की फ़िल्म में शतरंज के मोहरे बिखरते नहीं हैं बल्कि फिर से सज जाते हैं। अब इन मोहरों को ब्रिटिश नियम के तहत चलाया जाएगा। जिसका अंदाजा मुंशी नंदलाल को बहुत पहले ही हो गया था। दरअसल, शतरंज के मोहरे अब सिर्फ मोहरे नहीं रह गए हैं बल्कि ये ‘मोहरे’ अपनी प्रतीकात्मकता में ‘देश’ के अर्थ में घटित हो गया है जिसे अब ब्रिटिश नियमों के अधीन रहना है। ‘शतरंज के खिलाड़ी’ की कहानी में इस प्रकार के बदलावों को लेकर सत्यजित राय से कुँवर नारायण ने एक संक्षिप्त बातचीत[13] भी की थी।
दरअसल, सत्यजित राय अपनी फ़िल्म को एक खुले निष्कर्ष के रूप में ख़त्म करते हैं, वे अवध की संस्कृति का अंत दिखाना नहीं चाहते थे। वे अवध की संस्कृति को एक विरासत की तरह अपनी फ़िल्म में सहेजना चाहते थे इसलिए उनकी फ़िल्म में दोनों जागीरदार की मृत्यु नहीं होती। सत्यजित राय की फ़िल्म को और प्रेमचंद की इस कहानी को केवल दो जागीरदारों मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली की निगाह से ही देखना, पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उन दोनों की बेगमों और नवाब वाजिद अली शाह की कलाप्रिय निगाह से भी देखना, पढ़ना चाहिए। नवाब वाजिद अली शाह जिसने अपने महबूब शहर लखनऊ से बेइन्तहां प्यार किया, हजारों बार सज्दे में सर झुकाया, उसे आज छोड़ते हुए वह बेहद गमगीन था। वह लखनऊ को छोड़ते हुए अपने ही लिखे को गा रहा था-‘बाबुल मोरा, नैहर छुटो ही जाय’।
संदर्भ और टिप्पणियाँ :
[1] लेखक का सिनेमा (2017) कुँवर नारायण, (संपादक-गीत चतुर्वेदी), राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 170
[2] वही, पृष्ठ 177
[3] ‘मुझे पता था कि राय को हिंदी बहुत कम आती है, हिंदी साहित्य के बारे में उनका ज्ञान उससे भी कम है और मेरे साहित्य के बारे में तो वह कुछ भी नहीं जानते. जिंदल (कुँवर नारायण जी का रिश्तेदार), जिनका खुद का हिंदी साहित्य- ज्ञान बेहद दुर्बल था, ने संभवत: राय को बताया था कि मैं शायद हिंदी का कोई कवि या साहित्यकार हूँ. जब हम मिले, तो अगर राय ने अपने मन के भीतर मेरी छवि किसी खाँटी हिंदीवाला जैसी बना रखी हो, तो इसके लिए मैं उन्हें कोई दोष नहीं दूँगा. मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि जब वह यहाँ से लौटे होंगे, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोच रखा होगा और वह खास हिन्दीवालों से कितना अलग रहा होगा. यह मैं इस तथ्य के बावजूद कह रहा हूँ कि उन्हें अमृतलाल नागर से काफी ‘हैवी डोज’ मिला था, जो कि लखनऊ से भी ज्यादा लखनऊ हैं. नागर जी से हमारी मुलाकात उसी रोज होनी थी. मैंने समय लेने के लिए उन्हें फ़ोन किया. तुनकमिजाज बुजुर्गवार पर्याप्त कुपित हो गए, क्योंकि पहले उन्हें यह लगा, मैं उन्हें राय से मिलने के लिए अपने घर बुला रहा हूँ. मेरी मंशा यह कतई नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से, और पता नहीं क्यों, उन्होंने यही समझ लिया और राय के मुकाबले अपनी महत्ता के दावे दागते हुए मुझ बेचारे पर बरस पड़े. मैंने उनके सारे प्रहार बर्दाश्त किए, जो कि भयानक होने से ज्यादा मनोरंजक थे. मैंने उनसे आग्रह किया कि आप अपने किले में ही बने रहें, राय अभी थोड़ी देर में आपको सजदा करने पहुँचेंगे. मुझे लगता है कि राय, जिनमें पुराने की पड़ताल करने की बेहद सूक्ष्म दृष्टि है, जो कि कम लोगों में होती है, उन्हें लखनऊ का प्रमाणिक पुरातात्विक-दृष्टांत अवश्य ही प्रशंसनीय लगा होगा.’ लेखक का सिनेमा (2017) कुँवर नारायण, (संपादक-गीत चतुर्वेदी), राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 180
[4] इसका उल्लेख हमें एंड्रू रॉबिंसन द्वारा अँग्रेजी में लिखे लेख ‘सत्यजित राय: सिनेमा का दर्शन में मिलता है । रॉबिन्सन की किताब और सत्यजित राय पर लिखे अन्य निबंधों के लिए इस लिंक पर जाया जा सकता है –https://trove.nla.gov.au/result?q=subject%3A”Ray%2C+Satyajit%2C+1921-1992.”
[5] इसका उल्लेख हमें एंड्रू रॉबिंसन द्वारा अँग्रेजी में लिखे लेख ‘सत्यजित राय: सिनेमा का दर्शन में मिलता है . रॉबिन्सन की किताब और सत्यजित राय पर लिखे अन्य निबंधों के लिए इस लिंक पर जाया जा सकता है – https://trove.nla.gov.au/result?q=subject%3A”Ray%2C+Satyajit%2C+1921-1992.”
[6] लेखक का सिनेमा (2017) कुँवर नारायण, (संपादक-गीत चतुर्वेदी), राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 169
[7] वही, पृष्ठ 176
[8] 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ की संपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थिति को समझने के लिए अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास ‘ग़दर के फूल’ को पढ़ा जा सकता है.
[9] रोजी लिवेलन जोंस (हिंदी अनुवाद–सुधीर निगम, 2018),भारत में आखिरी बादशाह वाजीद अली शाह, संवाद प्रकाशन,पृष्ठ-44
[10] रोजी लिवेलन जोंस (हिंदी अनुवाद–सुधीर निगम, 2018),भारत में आखिरी बादशाह वाजीद अली शाह नाम की किताब में वाजिद अली शाह के सेकुलर चरित्र को काफ़ी उभरा गया है. इस किताब में एक रोचक प्रसंग है कि, ‘बीस वर्षीय युवा वाजिद अली शाह की मंचीय प्रतिभा उस समय सामने आई जब उन्होंने 1843 में अपने छोटे भाई सिनर हसमत केलिए निजी समारोह की व्यवस्था की. इस अवसर के लिए, वाली अहद ने भगवन कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा से संबंधित एक नाटक का निर्देशन किया. ब्राहम्ण कलाकारों का एक दल मथुरा से आमंत्रित किया गया था और वाजिद अली शाह की पत्नियों में से चार चहेती बीवियों ने नाटक में मुख्य भूमिका निभाई, जबकि यस्मिन पर और हर परी ग्वालिनें बनी. भारतीय रंगशाला के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण था. प्रथम बार एक मुसलमान बादशाह भगवन कृष और उनके प्रेम-प्रसंगों से संबंधित नाटक का निर्देशन कर रहा था, जिससे केवल हिंदू जतना ही प्रसन्न होने वाली थी.’ पृष्ठ – 57
[11] लेखक का सिनेमा (2017) कुँवर नारायण, (संपादक-गीत चतुर्वेदी), राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 171-172
[12] चिन्दानद दास गुप्ता (1995) सत्यजित राय का सिनेमा (अनुवाद-अवध नारायण मुद्दगल), नेशनल बुक ट्रस्ट, पृष्ठ – 14
[13] इस बातचीत में कुँवर नारायण, सत्यजित राय से पूछते हैं – शतरंज के खिलाड़ी की ऐसी कौन सी खासियत ने आपको आकर्षित किया ? सत्यजित राय कहते हैं – पुराने लखनऊ की पृष्ठभूमि . अवध कू जीतने के लिए ब्रिटिशों द्वारा शतरंज जैसी चालों ने. दो नवाबों का शतरंज के खेल में मुब्तिला रहने का पार्टिक. जीतने की दोनों की अति-व्याकुलता, जबकि असली खेल तो वे चालक ब्रिटिशों से हार रहे थे . यही बुनियादी ढ़ांचा है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ. कुँवर नारायण फिर पूछते हैं- आप कहानी के ढ़ांचे में जो बदलाव कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कते आ रहीं हैं ? सत्यजित राय जवाब देते हैं – पृष्ठभूमि की मूल कथा में जोड़ने के लिए सही बिंदुओं की तलाश-पतनशील नवाब बनाम महत्त्वाकांक्षी ब्रिटिश – और वह अग्रभूमि, यानि कि दो शतरंज के खिलाड़ी – इन सबको खोजना. आप जानते हिं हैं, यह सब मैं अपनी सिनेमाई शर्तों पर करना चाहता हूँ. – लेखक का सिनेमा (2017) कुँवर नारायण, (संपादक-गीत चतुर्वेदी), राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 180-181