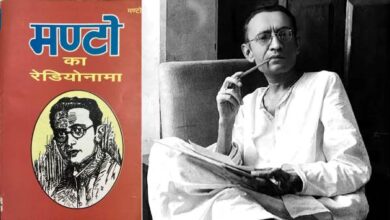हम तुझे वली हैं समझे – गोकि बादाख़्वार है तू…!!
थिएटर के मरजीवा : अरुण पाण्डेय
अरुण पांडेय अपने थिएटर-कर्म के 50 साल पूरे कर रहे हैं, सुनकर कैसा लग रहा है, के अपने जज़्बात को यदि मै शब्दों में उतारूँ, तो वह नग़्मात (कविता) की मदद के बिना सम्भव न होगा –
‘हूँ आज प्रवाहित मैं ऐसे, जैसे कवि के हृदयोदगार।
मै रोक नहीं सकता इसको, कर नहीं सकूँगा इसे पार’।
लेकिन पार करने की कोशिश अब अटाल्य है। यह संस्मरण वर्षों से अपने मन का खुद से वादा था, अरुण व उसके रंगकर्म से अपने इश्क़ का तक़ाज़ा था, लेकिन वह तीसरा घटक अब आ गया है कि मिसरा पूरा हो जाये–‘रस्म-ए-उल्फ़त भी है, वादा भी है, मौक़ा भी है…।
आज 19 अगस्त, 2021 है, जब यह लिखना शुरू कर रहा हूँ…। और वो 11 अगस्त, 1999 था, जब अरुण पाण्डेय से पहली बार हमारी भेंट हुई थी। 22 साल हो गये…। और उनके सक्रिय रंगकर्म के 40 साल आगामी अक्तूबर में पूरे हो रहे हैं। याने उनके रंगजीवन के 28 सालों बाद हम मिले थे। तब भारतीय रंग जगत में जबलपुर शहर को जिस रंग-संस्था ‘विवेचना’ के नाम से जाना जाता था, उसी के बैनर तले अरुण पांडेय काम करते थे। अब वही रंग जगत जबलपुर को अरुण पाण्डेय के नाम से जानता है, जो ‘विवेचना रंग मंडल’ चलाते हैं।
‘विवेचना’में से ‘विवेचना रंग-मंडल’ बनने की चर्चा शायद आगे आये… लेकिन यहाँ अभी यह कि मै इन पचास सालों के लिए भगवान को हाज़िर-नाज़िर करके कह सकता हूँ कि उनके रंगकर्म ने यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा और व्यक्तित्त्व किसी रंग समूह के मोहताज नहीं होते, बल्कि अरुण पांडेय जैसे व्यक्तित्त्वों से चलते हैं रंग मंडल, सरनाम होता है कोई शहर…गर्वोन्नत होता है उस कला का मस्तक…। शंभू मित्र व हबीब तनवीर जैसे तमाम रंगकर्मी तथा उनके समूह इसके प्रमाण हैं, लेकिन किसी सरकारी अनुदान, सम्मान व तमग़े…आदि के बिना सिर्फ़ अपनी कर्मठता के बल पर पूरे जीवन इतना विपुल रंगकर्म करने वाले अरुण पांडेय जैसे बहुत कम (प्राय: नहीं के बराबर) लोग होंगे, जिसमें शामिल हो – लगभग चार दशकों से रंगमंडल का कुशल संचालन, पूर्ण से लेकर एक-अंकी, एकल एवं नुक्कड़…आदि सभी प्रदर्शन-रूपों (फ़ॉर्म्स) में शताधिक नाटकों के निर्देशन, दर्जनाधिकि नाटकों के लेखन-रूपांतरण, शुरुआत में काफ़ी और बाद में कभी-कभार अभिनय भी और हज़ारों शोज़…। और ये सब जीवंत हों – एक से एक अनूठी प्रयोगधर्मिता से एवं ज्वलंत हों गहन वैचारिकता से सम्पन्न सामाजिक सरोकारों से…।
ऐसे अरुण पाण्डेय आज अपने आप में एक रंग संस्था हैं। इसका प्रमाण उनको मिले सम्मान-पुरस्कार, उन पर लिखे लेख व उनके साक्षात्कार…आदि नहीं देंगे, बल्कि जबलपुर की सड़कें, गलियाँ व चौराहे-चौबारे देंगे, वहाँ की मिट्टी देगी, उस मिट्टी से निकले वे सैकड़ों-सैकड़ों रंग-रत्न देंगे, जो पूरे देश में अपनी आभा बिखेर रहे हैं –मंच से लेकर छोटे-बड़े पर्दों तक…। और वे जब कभी लौटकर अपने घर जबलपुर आते हैं, अरुण के स्नेहाशीष व हार्दिक शुभकामनाएँ पाके निहाल होते हैं, लेकिन अरुण का जबलपुर उनके ‘हरि हारिल की लकरी’है। उनके रंगपट पर लिखा सनातन सूत्र है –‘स्वागत होता यहाँसभी का, नहीं किसी की यहाँ प्रतीक्षा’।
इसका प्रमाण यह है कि संस्थापकों एवं रंगमंडल के कुछ स्थायी रंगकर्मियों के अलावा इनके साथ 30-34 युवा हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसी नाट्यकर्मी चेतना वाले अरुण पांडेय अपने जबलपर से यह संदेश दे रहे हैं कि अपना ‘लोकल ही ग्लोबल है’। और कह दूँ कि अपनी कर्मभूमि (जी,उनकी जन्मभूमि बनारस है) जबलपुर के प्रति ऐसी एकनिष्ठता के साथ रंगकर्म का ऐसा अलख जगाने वाले अरुण जैसे ‘वर पुरुष बहुत जग नाहीं’, वरना तो सारे के सारे अपने अंचलों को छोड़-छोड़ कर यूँ गये कि कबीर के शब्दों में ‘जो जो गये, बहुरि नहिं आये’…। पूरे देश में यदि ऐसे अरुण पांडेय दस-बीस भी होते, तो अपने देश का तमाम लोक ‘रंग’ विहीन मही मैं जानी’ न होता…!
अरुण पाण्डेय ने रंगकर्म और सिर्फ़ रंगकर्म किया है… बल्कि कहें कि उन्होंने रंगकर्म को जीया है। नाटक ही उनका जीवन रहा है– हाँ, जीवन बिलकुल भी नाटक नहीं रहा, बल्कि एक अदद-खाँटी जीवन रहा है। ऐसा कुछ, जो रंगकर्म से रत्ती भर भी हट के हो, रंगेतर हो, उनकी ज़ेहन में आया नहीं। शुरुआत फ़ुल टाइम पत्रकारिता से की थी, जो फिर कभी गाहे-बगाहे करते भी रहे –विद्युत् माध्यम वाली भी किया – इसीलिए कि वह सब करके रंगकर्म कर सकें…।

नाटक से अरुण ने कुछ चाहा नहीं। चाहा भी हो, तो कभी कहा नहीं। और नाटक से उन्हें बहुत कुछ मिला अकूत…, पर नाटक के लिए वैसा कुछ नहीं मिला – न कोई बड़ा पुरस्कार-सम्मान, न कोई बड़ा ओहदा, जो कि अमूमन सबको मिलता है। उनके काम के दसवें हिस्से जितना भी करनेवाले बहुतों को वह सब मिला है। नाटक का एक बड़ा संभार उनके मन-मस्तिष्क में समाया रहा, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसे वे मंच पर नाट्य रूप में तो उँड़ेलते रहे, लेकिन प्रचारित करना उन्हें आया नहीं। ‘अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी, बार अनेक भाँति बहु बरनी’ की कला में वे बेहद फिसड्डी सिद्ध हुए हैं और दुनिया आज इसी की है। फिर अपने रंगकर्म के ज़रिए अभिजनों से सम्पर्क बनाने-बढ़ाने का काम तो कैसे होता उनसे!! यह उनको आया नहीं। आता भी रहा हो, तो करना भाया नहीं। सो, किया नहीं। गरज ये कि अपने किये का विज्ञापन-प्रदर्शन उनसे हुआ नहीं। उनका किया हुआ गुलदस्ता बनके नाट्य-मेलों, नुमाइशों में सजा नहीं…हाँ, रंगकर्म से उन्हें एक भरापूरा जीवन मिला है – ईमानदार व कर्मनिष्ठ जीवन। हम उनके लिए फ़ख़्र से और वे खुद के लिए शान से कह सकते हैं –
बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे, खुले मेरे ख़्वाबों के पर धीरे-धीरे…
किसी को गिराया, न खुद को उठाया, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे-धीरे…
कहीं जब गिरा, तो अकेले ही रोया, यूँ ही गया घाव भर धीरे-धीरे…
पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूँ ही सर धीरे-धीरे…
और यह सर न कहीं झुका, न कभी लटका…। उठा है – गर्वोन्नत, शान से…। इसीलिए मै अपने मन में अरुण पांडेय को नाटक का ‘मरजीवा’ कहता हूँ। मरजीवा का सामान्य व शाब्दिक अर्थ मर के जीने वाला ही है और अरुण नाम का बंदा यही तो करता है – नाटक के लिए मर-मर के नाटक में ही जीता है। ‘मरजीवा’ को लक्ष्यार्थ बनाकर दुनियावी भाषा में सुविधा के लिए ‘पनडुब्बा’ याने ‘गोताखोर’ कहते हैं और अरुण रँग-समुद्र के गोताखोर ही तो हैं। लेकिन अरुण के लिए जिस अर्थ-प्रक्रिया में यह शब्द मेरे मन में उठा और समाया है, वह कबीर के नाम पर प्रचलित एक दोहे में मिलता है –
‘मोती उपजे सीप में, सीप समुंदर मांहि। कोइ मरजीवा काढ़ेसि जीवन को ग़म नाहिं’। ।
हालाँकि मानक ग्रंथावलियों में दोहा ऐसे ही नहीं, पर प्रच्छन्न मिलता है। लेकिन नाटक में यही करते मैंने अरुण को देखा है – दुनिया के समुद्र में पड़ी सीपी में छिपे नाटक के मोती को ‘जीवन (मरने) को ग़म नाहिं’ की क़ीमत पर रंगजीवन में आकंठ डूबकर ‘काढ़ता’ है…। और किसे शक होगा कि ऐसा करने वाला ‘मरजीवा’ शब्द के एक व्यंज्यार्थ में ‘अमर’ न बनेगा?
अब आयें संस्मरण की श्रिंखला में उक्त 19 अगस्त, 1999 के उस प्रथम मिलन पर, जिस दिन की शाम मुंबई के ‘इस्कॉन सभागृह’ (हरे राम हरे कृष्ण) में उनके बहुप्रसिद्ध, बल्कि कहें कि ‘विवेचना’ व अरुण पांडेय की पहचान वाले (सिग्नेचर) नाटक ‘निठल्ले की डायरी’ का मंचन होने वालाथा। वही हमारे मिलन व अब तक के आजीवन सम्बन्ध का मूल बना। लेकिन ठीक एक दिन पहले ही ‘बिड़ला क्रीड़ा केंद्र’ सभागृह (चौपाटी) में इसी नाटक का पहला मंचन मैं देख भी चुका था। तब तक मैंने न अरुण पाण्डेय को देखा था, न उनका कोई नाटक…। नाम अलबत्ता सुन रखा था। लेकिन ‘निठल्ले की डायरी’ ऐसा नाटक था कि हमें बीसों साल पहले छूटे अपने गाँव में लेके चला गया…, हमारा गाँव मंच के गाँव जैसा न था, लेकिन मंच पर जो हो रहा था, वह हमारे गाँव जैसा था।
इसका औरा हमारे लिए ऐसा रहा कि इसने ही अरुण व ‘विवेचना’ तथा जबलपुर शहर से मिलवाया और आगे चलकर जब अरुण से हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हुए और उन्हें इस बात का पता चला, तो मेरे गाँव आकर ‘निठल्ले की डायरी’ करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, बल्कि मेरी हसरत को साकार करने के लिए बार-बार कोंचते रहे कि किसी तरह नाटक मेरे गाँव में हो जाये…। ऐसे यार क़िस्म के आदमी तो हैं ही अरुण पांडेय, लेकिन धीरे-धीरे मालूम पड़ा कि यह उनकी रंग-चेतना का एक प्रमुख मक़सद है कि देश में ऐसे नाट्य समूह होने चाहिए, जो सिर्फ़ गाँवों में नाटक करें – गाँव-दर-गाँव जा-जाकर…। मेरे यहाँ तो मेरी काहिली से नहीं हुआ, पर इसकी तड़प आज तक नहीं गयी…और होने की आस आज तक नहीं टूटी।

लेकिन परिहार स्वरूप ‘विश्व भोजपुरी सम्मेलन’ के सालाना उत्सव में नागपुर में अवश्य इसका मंचन हो पाया, जिसमें पूरे देश से आये लोगों को मिलाकर एक बड़ा भोजपुरी समाज इसे देख पाया और देखते-देखते लहालोट होता रहा…। वह भी अरुण पांडेय की रंग-निष्ठाव संकल्प ही रहा कि मेरे प्रस्ताव पर भोजपुरी में रचे-बसे अपने पिताजी से उस एक प्रदर्शन के लिए उन्होंने पूरा नाटक लिखवाया। जबलपुर की रंगयात्राओँ में उनके घर पे रहने के दौरान सुबहें व रातें पिताजी के सानिध्य में बीतती थीं और उसी का सुपरिणाम व उनके पितृत्त्व का ही जादू है कि इतनी कम मुलाकातों के बावजूद मुझ धुर बचपन से पितृविहीन को एक पिता का असधार मिल गया है। जब से उनके छोटे बेटे बॉबी (विवेक पांडेय) ने नया घर लिया है, पिताजी महामार्ग से सटे व खुले परिवेश में वहाँ रहते हैं और अब इतने सक्रिय-समर्थ नहीं कि नाटक देखने आ पायें, तो उनसे मिलने जाना मेरी जबलपुर-यात्रा का अनिवार्य अनुष्ठान होता है – बल्कि अल्लाह झूठ न बोलवाये, तो कई बार नाटक के बहाने उन्हीं से मिलने के लिए ही आने का मन होता है। और अरुण या अरुण-परिवार क्या, पूरे ‘विवेचना’से बिना ज़रूरी काम के फ़ोन पर कभी बात नहीं होती, लेकिन हर 14-20 दिन पर पिताजी से बात ज़रूर हो जाती है। तो आजकल अरुणादि के हालचाल पिताजी से मिलते हैं। बहरहाल,
उनके अनूदित ‘निठल्ले की डायरी’ के लिए अरुण ने अनथक श्रम से सारे अभिनेताओं को भोजपुरी में तैयार कराया। और कक्का की केंद्रीय भूमिका करते-करते सच के कक्का बन गये नवीन चौबे के उस दिन सुलभ न हो पाने या भोजपुरी उच्चारण व लहजे में रवाँ न हो पाने के कारण अपने छोटे भाई विवेक पांडेय उर्फ़ बॉबी को सिर्फ़ एक शो के लिए ही तैयार किया। यहाँ यह भी ऊल्लेख्य है कि अरुण का लगभग पूरा परिवार ही नाट्यमय है। और इसके जनक अरुण ही हैं। विवेक व उसकी पत्नी प्रगति तो फ़ुल टाइम नौकरी धंधे के साथ ‘होल टाइमर’ नाट्यकर्मी हैं– मंच से लेकर मंच-परे तक नाट्य के हर रूप, हर महकमे में सक्रिय, बल्कि अब तो एक हद तक कर्णधार भी। और इतनी निजी बात बताने की नहीं होती, पर यह मर्म तो छिपाने की भी बात नहीं कि प्रगति पिछले एक दशक से असाध्य रोग से ग्रस्त है। लेकिन निरंतर इलाज व एकाधिक शल्यक्रिया से गुज़रते हुए भी उसे धता बताकर अपने जीवन व नाट्यकर्म में सक्रिय है। और कौन कहेगा कि उस ‘किरकिट’ पर क़ाबू पाने में इस कलामय जीवन की ऊर्जा भी कारगर भूमिका नहीं निभा रही है– ‘पहुँच तेरे अधरों के पास हलाहल काँप रही है देख…!!
और अरुण-भार्या मीनू पांडेय यूँ तो फ़ुल टाइम अध्यापिका और फ़ुल टाइम गृहिणी हैं, लेकिन अरुण का घर ही फ़ुल टाइम नाट्यघर है– विवेचना-परिवार का घर हो गया है। वही कार्यालय है, वही बैठक कक्ष है। वही स्टोर रूम है, वही नाट्य-अतिथि-गृह है। और इसलिए ‘इक प्रबिसहिं इक निर्गमहिं भीर भूप दरबार’ सरीखा वह घर कभी बंद नहीं होता…उस घर को ताले-कड़ी की क्या, दरवाज़े तक की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे घर की गृहिणी नाटक से असंपृक्त कैसे रह सकती है, आराम कैसे कर सकती है!! और दर्जनाधिक बार वहाँ रहकर मै चश्मदीद ही नही, भोक्ता भी हूँ कि मेरे घर-परिवार का सब कुछ मीनूजी जानती ही नहीं हैं, उनकी याद में भी रहता है। हर आगमन पर वहीं से आगे के हाल-चालका आदतन ही लेना-देना (अपडेट्स) हो जाता है। और यही हर आने-जाने वाले के साथ होता है…फिर यह क्या कम रंगकर्मी होना है!! मीनूजी ही एक बार कुछ घंटों के लिए मेरे मुंबई वाले घर पहुँच भी गयी हैं, वरना नाट्यदल के कई लोग तो आ गये, पर अरुण नहीं…। जब से बनारस भी रहने लगा हूँ, हर मुलाक़ात में उनके बनारस आने और दस-पाँच दिनों रहने के मंसूबे बनते है, पर 12 साल में आ नहीं पाये कभी। और यह भी क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि नाट्यकर्मी अरुण की नारखेड़ी जबलपुर में ही गड़ी है…। अपने शहर और रंगकर्म के प्रति यह समर्पण भी अद्भुत है। ख़ैर,
नागपुर में भोजपुरी का शो ऐसा हुआ कि सम्मेलन के लोग मिलने और नाटक की बात निकलने पर आज भी अरुण पांडेय के ‘निठल्ले की डायरी’ को याद करते हैं – वह है ही ऐसा…। गाँव के किसी ठीहे-नुक्कड़ पर चौपालनुमा मजमा लगा है। फुरसती लोग जुटे-जमे हैं…आते-जाते भी रहते हैं। कक्काजी जम के बिराजमान हैं। यहाँ न किसी को अफ़रातफ़री है, न रोज़ी-रोटी की फ़िक्र। रोज़ी कोई ख़ास है नहीं, पर रोटी मिल जाती है – कैसी, की चिंता नहीं, चर्चा नहीं। न पत्नी पर शक, न प्रेमिका की खोज। न द्वयअर्थी संवादों व बनावटी दृश्यों से खींच-तान के निकाले जाते हास्य, जिसे नागरी भाषा में ‘हिलैरियस कॉमेडी’ कहते हैं और जिन्हें मुम्बई में देख-देख के सिठा गये थे हम…।

वहाँ चौपाल में चर्चा या शग़ल है, तो दुनिया जहान का। और संवाददाता है प्रतीक रूप में एक सायकल वाला बंदा, जिसे तब नरोत्तम बेन ने साकार किया था, जो आज मुम्बई में गायन-अभिनय…आदि में जम चुका है। जब मैं ‘बतरस’ का मासिक आयोजन चलाता था, नरोत्तम नियमित प्रतिभागी ही नहीं, अपने लहकते लोकगीतों के चलते ‘बतरस की शान’ रहा। नाटक में वह गाँव की ही नहीं, देश-विदेश की खबरें भी देता है। याने वहाँ अख़बार नहीं, आदमी पढ़े जाते हैं…। इस पूरे संभार को नाटक के ही शब्दों में –‘निट्ठले की डायरी’ है – नक़्शा हिंदुस्तान का’। और है हर खबर पर कक्काजी की टिप्पणी, बल्कि तब्सिरा – जैसे उन्हें दुनिया का सब कुछ हस्तामलक हो और जिस पर है श्रोता-मंडली को अखंड विश्वास…। जैसे वे दुनिया के सबसे बड़े ख़बरगो व तत्त्ववेत्ता ‘मिस्टर आल नो’ (सर्वज्ञ) हों…। उनकी यह अदा बहुत मक़बूल हुई कि हर ख़बरके तब्सिरे पर कक्का अपनी नाक से एक बाल ठह के उखाड़ते हैं, फ़ट से फेंकते है – गोया सारी खबरें हों उनके नाक की बाल…और यह है अरुण पांडेय का कमाल…।
इसे बिड़ला क्रीड़ा केंद्र में पहली बार देखते हुए ही अचानक महसूस होने लगा था कि महानगर की जिस ज़िंदगी में हम रम गये होने का अहसास कर रहे हैं, वह कितनी बँधी-बँधी हुई एकरस है। घड़ी की सुइयों से संचालित, चाकचिक्य भरी ज़िंदगी, जिसमें अपनी रोज़ी-रोटी के सिवा कोई गति नहीं। और डेढ़ दशकों से देख रहा था ऐसे ही नाटक, जिनमें सजा-सजाया दीवानखाना (ड्राइंग रूम), जहां या तो सौदे हो रहे हैं या पति-पत्नी के एक दूसरे से छिपके किसी तीसरे-तीसरी से प्रेम चल रहे हैं…आदि-आदि। गरज ये कि सहज-स्फूर्त्त जीवन नदारद है। ऐसे में ‘निट्ठले की डायरी’ उस गाँव में उठा ले गया, जहां तब समय ही समय था। जहां उपयोगिता से कोई वास्ता नहीं। काम की कोई बात नहीं – बस, मस्ती ही मस्ती है। और शहर में अपने और अपने कमाने के अलावा कुछ नहीं होता, शेष सब कुछ बेकाम का – शहर की भाषा में फ़ालतू।
कुल मिलाकर यूँ अनुभव हुआ जैसे ‘तपन में शीतल मंद बयार’ आ गयी हो और लगा कि जैसे हमारी आँखें खुल गयी हों– हाय अल्ला, नाट्यकर्म ऐसा भी होता है!! और वहीं तय किया कि कल दूसरा प्रदर्शन भी देखना ही है। यह दूसरा प्रदर्शन जिस इस्कॉन में घोषित था, वह मेरे घर के पास भी है। इसीलिए पहली शाम ‘क्रीड़ा केंद्र’ से नाटक के तुरत बाद किसी आवश्यक कार्य वश भाग लिया था। न पात्र-परिचय देखा, न नेपथ्य में मिलने गया, जो एक रंग-संस्कृति है तथा नाट्यप्रेमियों व ख़ास तौर पर कलाकारों से परिचित लोगों के लिए उत्साह व कला-प्रेम का सबब भी। हम समीक्षकों के लिए तो नाट्य-विषयक कुछ विवरण या स्पष्टीकरण…आदि पाने का प्रयोजन भी – याने नाट्य-प्रेम व सरोकार दोनो ही। और यह सब हुआ दूसरे दिन 10 अगस्त की शाम इस्कॉन में। पहले तो नाटक के बाद तालियाँ रुक ही न रही थीं…। फिर कलाकार-परिचय शुरू हुआ, तो मंच पर बुलाये गये ‘इस नाटक के लेखक-निर्देशक अरुण पांडेय…’।
वही मेरा पहली बार अरुण को देखना हुआ। पूरे पात्र-परिचय में वे नामालूम से खड़े रहे…उनका नाम लिया गया, तो बस हाथ जोड़ दिये – तालियाँ बजती रहीं…और वे नत-नयन, स्थिर काया लिए स्तंभवत…। यह अदा-हीन अदा भी बड़ी भायी मुझे…। किसी तरह मंच निपटा, तो नेपथ्य की तरफ़ बढ़े…मिलने वालों की भीड़ बड़ी थी। पूरे सभागृह को नाटक बहुत भाया था। और तमाम लोग उमड़ पड़े थे अपने प्रिय कलाकारों से मिलने के लिए…। कक्का बने भाई नवीन चौबे से गलबहिंया होते, बधाइयाँ देते हुए अरुण की तरफ़ बढ़ा…। नाम बताते ही हहा के मिले…तो लगा कि जानते हैं (या मुम्बई आने पर जान गये हों)। ‘भीषण सुंदर’ (उन दिनों किसी बंगालन के प्रभाव में तारीफ़ का यही शब्द था मेरा) – कहते हुए मैं गले लगाने चला कि अरुण पाँव छूने की अदा में अधलटके होने लगे…तो गाँव फिर जी उठा–लगा कि ‘हेलो-हाय’ वाले शहर से अचानक गाँव में आ गये हैं।
यह क़यास भी हुआ कि अरुण उम्र में मुझसे छोटे हैं। भीड़ देख के और समय की नज़ाकत समझ के मैं चलने को हुआ, तो बोले – ‘अरे रुका भैया, जल्दी का हौ’? और तब से यह ‘भैया’ शब्द उनका चिर सम्बोधन ही नहीं बना, जीवन में ढल गया है। फिर तो सम्बंधों में कभी जल्दी आयी नहीं। आपसी बात भोजपुरी में ही होने, जो मुझे भी बहुत प्रिय है, का अनकहा करार बन गया। भीड़ कुछ छँटी, तो एक सिरे से बात शुरू हुई…और शुरू हुई, तो बढ़ती गयी…फिर लगा कि बातें उस नीले कमरे (ग्रीन रूम) में समा नहीं रहीं,तो हम बाहर निकल आये। ‘हरे राम, हरे कृष्ण’ का परिसर काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ टहलते हुए… फिर सदर दरवाज़े के सामने सड़क पर खड़े-खड़े किसी टपरी की चाय पीते हुए और फिर मंदिर के सामने की गली में टहलते-टहलते समुद्र के मुहाने तक घूमते हुए बतियाते रहे…। बातें ही बातें – कभी न ख़त्म होने वाली बातें…, जो पारस्परिकता की जान व गँवईं संस्कृति की ख़ास पहचान हैं और जिससे शहर की सभ्यता बहुत बिदकती है। और अंत में लगभग डेढ़ घंटे बाद भविष्य में मिलते रहने की कई-कई योजनाओं व बराबर सम्पर्क में रहने के वायदों के साथ विदा हुए।
अब क्या कहना होगा कि उन्हीं योजनाओं व वायदों के निभने-निभाने के दौरान बने सम्बन्धों की गाथा है यह संस्मरण…।
‘विवेचना’ के साथ अरुण के जाने के बाद धीरे-धीरे पता लगा कि नाटक का दीवाना मैं ही नहीं हुआ, वरन ‘इस शहर में हम जैसे दीवाने हज़ारों हैं’…दर्जनाधिक नाट्यप्रेमी तो मुझे ही मिले, जिन्होंने दोनो शोज़ देखे और अरुण पांडेय के दीवाने हुए। यह भी पता लगा कि दो-तीन नाट्यकर्मियों ने तो तुरत ही नाट्यालेख की छाया-प्रतियाँ भी करा लीं कि वे मंचन करेंगे। लेकिन समय गवाह है कि कर कोई न पाया। ऐसा ही एक नाटक मराठी का हुआ था –जयंत पवार (जिनका दुर्दैव से अभी चंद दिनों पहले ही अवसान हुआ है) लिखित ‘अधांतर’, जिसमें गाँव तो न था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली मुंबई की रुक्खागीरी-गुंडागर्दी व चाल-निवासियों के जीवन वाली मुम्बई की खाँटी ज़िंदगी का नग्न यथार्थ यूँ नुमायाँ हुआ था कि उससे लरज कर हिन्दी के एकाधिक रंगकर्मियों ने नाट्यालेख लिये थे, पर उसे भी कर कोई न सका।

अरुण पाण्डेय के इस नाटक ने मुम्बई के नाट्य-विमर्श में यह आयाम जोड़ दिया कि हिन्दी में मूल नाटकों के अभाव की तोहमत तो किसी हद तक ठीक भी हो सकती है, लेकिन इसके चलते अंग्रेज़ी-मराठी…आदि के नाटक खेलने को सही साबित करना रंगकर्मी की अपनी काहिली व परमुखापेक्षिता से बनी रचनाहीन वृत्ति है। वे व्यर्थ का अरण्य-रुदन करते हैं कि हिन्दी में अंधायुग, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे आदि चंद नाटकों के सिवा मंचेय नाटकों का अभाव है। अरुण ने तो अपने शहर जबलपुर के एक शीर्ष लेखक हरिशंकर परसाई के लेखन से ही कुल पाँच नाटक लिखे और खेले, जिनका भी शीर्ष है – ‘निठल्ले की डायरी’। अन्य चार हैं –‘मै नरक से बोल रहा हूँ’, ‘चौक परसाई’, ‘परसाई नामा’ और ‘प्रवचन परसाई’।
इसी तरह अपने अंचल के विख्यात लोककवि ईसुरी के जीवनवृत्त पर ‘हंसा उड़ चले देस बिराने’ लिखा और पेश किया। यह वह नाटक है, जो अरुण को बड़े रंग-निर्देशकों के समकक्ष खड़ा कर गया। ये नाट्यकर्म व्यक्तित्व-केंद्रित ही नहीं, इतिहास-संचालित भी हुए। बुंदेला विद्रोह को लेकर बुंदेली में भी नाटक लिखा – तैयार किया – ‘हंसा कर ले किलोल’। यह अरुण की लोकपैठ व लोक में गहरी अनुरक्ति ही है कि लोक कथाकारों के सरताज विजयदान देथा की कहानी ‘फ़ितरी’ को ‘भोले भड़या’ नाम से बुंदेली में ही किया। इसे देखकर कहने का मन होता है कि हर रंगकर्मी का कोई न कोई लोक होता है। यदि वह महानगर की उपज या निवासी है, तो महानगर का भी एक लोक होता है – ‘अधांतर’ मुम्बई का लोक ही तो है। सवाल है पैठ का। महानगरों का रंगकर्मी अपने सज़े-धजे ड्राइंग रूम से बाहर तो निकले, शामों को स्कॉच-पास्ता का मोह छोड़कर पातल भाजी-चपाती न सही, झुणका-भाखर तो खा सके और उस लोक को देख-समझ सके…। हबीब साहब की राह का भी यही परतोख है। और अरुण उसी राह के रहबर हैं।
फिर अपने बुंदेलखंड ही नही, काशी अंचल पर लिखी काशीनाथ सिंह की संस्मरणात्मकव अदामयी (स्टाइलिश) कहानी ‘देख तमाशा लकड़ी का’ को इसी नाम से रूपांतरित किया, लेकिन किन्हीं कारणों से नाटक न बन पाया। उनकी इस वृत्ति से आकर्षित होकर एक बार मैंने भी एक सरकारी प्रस्ताव का मौक़ा हाथ में आते ही मैत्रेयी पुष्पा के अपने पसंदीदा लघु व तेज उपन्यास ‘झूलानट’ का रूपांतर कराया, जो अपनी तेज कर्मनिष्ठा के चलते अरुणजी ने तीन दिनों में ही करके भेज दिया था, लेकिन अफ़सरी पेचोखम को न सुलझा-संवार पाने के कारण शो उसका भी न हो सका। उदय प्रकाश की लोकेतर व तेज-तर्रार कहानी ‘और अंत में प्रार्थना’ का अरुण ने रूपांतर किया और उसका प्रदर्शन भी ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। उसके पहले शो की शाम मै जबलपुर में मौजूद था। मुझे तो कुछ भनक न थी, लेकिन अरुणादि को मालूम था कि शो के दौरान कुछ प्रदर्शन-उपद्रव हो सकता है।
पुलिस का बंदोबस्त तो था ही, संयोगन या योजना के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे ज़िलाधीश, जो औपचारिक उद्घाटन के बाद शो देखने के लिए अगली पंक्ति में बिराजमान भी थे। मंचन 14-20 मिनट चला होगा कि दर्शक-दीर्घा में दाहिनी तरफ़ बिलकुल पीछे से पटाखे फूटने की आवाज़ आयी। आधा हाल धुआँ-धुआँ हो गया। नाटक रुक गया। लेकिन पुलिस ने स्थिति पर चंद मिनटों मेंक़ाबूकर लिया। इसमें ज़िलाधीश की उपस्थिति का भी निर्णायक लाभ मिला। 14 मिनट नाटक रुका रहा, फिर पूर्ववत हुआ और शो भी बड़ा अच्छा हुआ। उस दिन नाटक का जीवट अच्छी तरह समझ में आया। मैं तो रोमांचित हो गया…। नाटक का ऐसा प्रत्यक्ष असर पड़ता है, यह सुनने-पढ़ने को मिला था, देखने को नहीं। बाद में कभी रायगढ़ में हबीब साहब के ‘पोंगा पंडित’ को लेकर पंडितों का पंगा देखने को मिला, लेकिन उसका मामला इतना उग्र व व्यापक न था तथा हबीब साहब ऐसे पंगे को लेकर खेले-खाये शख़्स थे। याने मेरे लिए प्रदर्शन परक कला के इतने जीवंत-ज्वलंत होने का साखी बना अरुण पांडेय का रंगकर्म और जबलपुर।
बेशक कहा जा सकता है कि अरुण-लिखित व मंचन के लिए चयनित नाटकों के मूल स्वर अवांच्छित व्यवस्थाओं की क्रूर सत्ताओं से विरोध के हैं – माध्यम चाहे प्रेम हो या संघर्ष व लड़ाई। उन दिनों मैं ‘जनसत्ता’ में स्तम्भ की तरह नाटक पर लिखता था। प्रदीप सिंह सम्पादक थे। उन्हें फ़ोन करके चेता दिया और लम्बा आलेख भेजा, जो पहले पन्ने पर नीचे छपा –‘बॉटम न्यूज़’ की तरह। बाद में वह पूरा आलेख नामवरजी की सम्मति से ‘आलोचना’ में भी छपा। चर्चा खूब हुई। और नाटक के हिट होने में इस पटाखा-कांड ने भी आग में घी का काम किया। तो जबलपुर जैसे शहर में चुपचाप अपना काम करने वाले अरुण पांडेय के चहरे का स्थायी भाव तो है – गम्भीर-गमखोर होना-रहना, लेकिन वे ऐसे बख़ौफ व क्रांतिकारी रंगकर्मी भी हैं…, जिसका पता उनके साथ रहते, उनसे बात करते हुए बिलकुल नहीं चलता, क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें करना व ज्वलंत योजनाओं के ढिंढोरें पीटना अरुण की आदत नहीं – बल्कि इसमें वे काफ़ी शर्मीले हैं। हाँ, बिना कहे उसे कर दिखाना इस नाट्यवीर की कूबत है।
‘हरे राम हरे कृष्ण’ की पहली भेंट के बाद ‘विवेचना’ के सालाना उत्सव के लिए जबलपुर की पहली जवाई में ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे अपनी किसी रिश्तेदारी के शादी-व्याह जैसे आयोजन में आये हों…और तब से दर्जन भर बार जाना हुआ, लेकिन उस भाव में कोई कमी नहीं आयी। सब कुछ वैसे ही अपनापे की लज्जत से भरा हुआ… जबलपुर स्टेशन पर आधी रात को लेने चार लोग आये – स्वयं अरुण, नवीन चौबे,हिमांशु रॉय व बाँकेबिहारी ब्यौहार। ऐसी अगवानी और कहीं हुई हो – याद नहीं आती। जैसा कि कहा गया, जबलपुर में स्थायी रूप से रहना होता अरुण के घर में। क्या खाने का मन है, पूछकर मीनूजी खाना बनवातीं और फिर कुछ खास बना देतीं अपने हाथ से…। हर बेला एक-दो-चार आगंतुक जुड़ ही जाते, जिसका सनातन अन्दाज़ मीनूजी को रहता…।
जबलपुर में दादा कहने की संस्कृति ज़बरदस्त है और मेरे देखते बीसों साल हो गये, बदल नहीं रही। याने अरुण के ‘भैया’ के अलावा बच्चों से बड़ों तक सभी का गोया राष्ट्रीय सम्बोधन ‘दादा’ भी इतना अपनापा भरा कि अन्य सभी जगहों -खासकर मुम्बई- का ‘त्रिपाठीजी’ बड़ा बेतुका लगने लगा। यह आज भी चल रहा है…। इसी रौ में अरुण का बारम्बार आग्रह होता – ‘भइया, भौजियो के लेके अउता एक बेर…’ लेकिन वह तो ‘उनकी भउजी’ (कल्पनाजी) की बाहर न निकलने -ख़ासकर आयोजनो…आदि में शरीक न होने- की अंतर्मुखी मूल वृत्ति से सम्भव होना ही न था, वरना ये नाट्य-यात्राएँ बिलकुल न रहकर पारिवारिक सम्मिलन हो जाता। फिर भी ऐसा होने से बचा कहाँ!!
…पहली बार जब चलने लगा था, मीनूजी ने दो कुर्त्ते सामने रख दिये – ‘पाण्डेय जी ने ख़ास आपके लिए सिलवा के रखे हैं’…तो हो गया न बड़ी अपनापे वाली रिश्तेदारी का सच्चा सिला। इस पर मैं तो पानी-पानी…लेते बनता न था और ‘ना’ कहना तो कैसे होता!! ‘भइ गति साँप-छछून्दर केरी’ वाला हाल था। बल्कि कहें कि तुलसी की इस पंक्ति से ज्यादा सटीक वह है, जो मेरी निरक्षर माँ जोड़ (इम्प्रोवाइज कर) देती –‘लीलत-उगिलत प्रीति घनेरी’। लेना पड़ा, लेकिन धीरे-धीरे बड़ी तटस्थता के साथ इस भेंट-भाव को मैंने परम्परा नहीं बनने दिया। लेकिन इन सबके पीछे कार्यरत अरुण के गहन संवेदन-सिक्त मानुष भाव, जो नाट्यकर्म से बना है और जिसने नाट्यकर्म को इतना मानवीय बनाया है, ने बिना भेंट-उपहार लिये-दिये व बिना ‘भउजी’ को लाये भी वही कर दिया है कि ऐसे ‘कच्चे धागे के साथ जिसे बांध दिया जाये, वह बैरी क्या छूटे, वहीं पर जिये वहीं मर जाये’…।
उत्सव के दौरान देखने को मिला कि अगवानी के लिए आये उक्त चारो ‘विवेचना’ के चार स्तम्भ हैं। और मुझे अपने ख़ानदान के चार काकाओं की याद आयी, जो बहनों की शादियों से लेकर ख़ानदान के अन्य सभी आयोजनों में अपने-अपने हिस्से के दायित्व को यूँ सम्भाल लेते थे कि किसी को कुछ पता ही ना चले। यहाँ भी कोई एक दूसरे से ज्यादा बात करते दिखता नहीं था, लेकिन आपसी समझ ज़बरदस्त और ग़ज़ब की सहयोगी सहभागिता (कोऑर्डिनेशन)।
सब देखते हुए बिना बताए ही समझ में आ गया कि सबकी सहमति से मंचेय नाटकों के चयन के बाद अपने नाटक की तैयारी एवं उत्सव में आमंत्रित नाटकों के मंचन की व्यवस्था का सारा दारोमदार अरुण के समर्थ कंधों पर होता। जनसम्पर्क का सारा कार्य नवीन जी देखते। अति महत्त्व का आर्थिक मामला हिमांशु रॉय के ज़िम्मे होता। मंचन के पूर्वापर का मंच-संचालन व गोष्ठियों के आयोजन…के कार्य बाँके बिहारी जी सम्भालते। इनके अनुदेशों-इशारों पर पूरा नाट्य-दल गतिशील रहता…। सर्वाधिक स्पृहणीय लगा था मुझे नाटक देखने के लिए आते शहर के मानिंदों-बुजुर्गों को दिया जाता माकूल सम्मान, जिसमें आचार की भारतीय पद्धति जीवंत होती। कुल मिलाकर सारा प्रबंधन इतना सुचारु (स्मूथ) होता कि ‘ता रख न सके कोई किसी ‘काम’ पे अंगुश्त’!!

यहीं अरुणजी के नाट्य-नियोजन -ख़ासकर मंच तैयार करने- के ग़ज़ब के कौशल का एक उदाहरण दे दूँ…। उत्सवों में बड़े-बड़े सेट मंगाने और भाड़ा-किराया खर्च करने-कराने के बदले वे अपने मौजूद साधनों में उसी प्रभाव का मंच तैयार करके दे देते हैं और उन्हें अपने मौजूद उपकरणों की बहुविध उपयोगिता व शहर में ऐसे सामानों की सुलभता का पूरा पता होता है। इस कौशलपूर्ण विधान पे नाटक करके लोग ख़ुशी-ख़ुशी जाते…। यह सब देखकर मैंने कहीं लिखा था कि मुम्बई में जया बच्चन के एक दिन के पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) पर जितना पैसा खर्च होता है, उतना भर दे दिया जाये, तो अरुण पांडेय एक नाटक बना सकते हैं। उन दिनों स्टार कलाकारों का चलन शुरू हुआ था।
छोटी जगहों पर उनकी माँगें ज्यादा भी होती थीं, जिसका शहर और इसीलिए वहाँ के रंगकर्म पर असर भी पड़ता था और इसीलिए अरुण जैसे नाटक वालों को न चाहते हुए भी ‘जनता की माँग’ पर वैसा करना पड़ता था। इसी रौ में एक बार मैंने नीना गुप्ता को जबलपुर आने के लिए तैयार कर दिया था। नाटक के नशे में वे ट्रेन से जा रही थीं, पर उस रात ट्रेन कैंसिल हो गयी। दूसरे दिन नागपुर तक हवाई यात्रा हुई। तब जबलपुर में हवाई अड्डा न था। ‘सूर्य की अंतिम किरण…’ का सेट ले जाने की समस्या थी। अरुण ने चित्र देखकर कहा – ‘आप आ जाइए, सेट मैं बनवा दूँगा’। नीनाजी को संदेह तो बहुत था, पर मेरी ललकार और ले जाने के खर्च व ज़हमत के चलते जोखम उठाने की हिम्मत (डेयरिंग) की। मै न आया था, पर अरुण-निर्मित सेट ऐसा कामयाब रहा कि नीनाजी अरुण की मुरीद बनकर लौटीं।
नाट्योत्सव में हर दिन नाश्ते के बाद व दोपहर के भोजन के पहले चर्चा-गोष्ठियाँ होतीं, जो मै महाराष्ट्र में बहव: देख-कर चुका था। सो, यह मेरे लिए बड़े शौक़ का सबब होता। फ़र्क़ यह ज़रूर है कि वहाँ प्राय: विगत शाम हुए नाटक पर केंद्रित होती चर्चा, जिसमें निर्देशक भी बैठता और सवालों के उत्तर देता। इसके बदले ‘विवेचना’ में नाट्य से सम्बंधित विषयों पर चर्चा होती। और कहना होगा की विवेचना’ में चर्चा अच्छी होती। लेकिन ख़ास बात यह कि यहाँ हर नाटक के मंचन के बाद पूरी टीम के साथ मंच पर बुलाकर भी कुछ-कुछ कहा-कहलवाया जाता…, जो सदा से मेरी प्रकृति व सोच के विरुद्ध रहा।
नाटक देखके या कोई किताब पढ़ के तुरत उस पर कुछ बोलने को मैं ‘अधकचरे अध्ययन का अकस्मात् वमन कहता’। इसीलिए मुम्बई में ‘जनसत्ता’ शुरू होने के बाद कुछ दिनों में जब नियमित साप्ताहिक समीक्षा लिखने की बात हुई, तो तत्कालीन सम्पादक श्रीयुत अच्युतानंद मिश्र से निवेदन करके मैंने बुधवार का दिन तय कराया था, ताकि शनि-रवि को हुए ख़ास नाटकों पर सोचने-पचाने के लिए कम से कम दो दिन तो मिले। लेकिन यह जबलपुर के रंग-समाज का प्रेम ही है कि उनके स्नेहाधिकार भरे इसरारों के वशीभूत अपनी सारी सोच-समझ को परे रखकर नाटक के तुरत बाद मेरी वाचा को फूटना पड़ा। इसका भी एक वास्ता नितांत पारिवारिक है। नाटक के बाद रात को घर में खाते हुए नाटक की चर्चा होनी स्वाभाविक होती, जिस दौरान कभी मंच से ज़बरदस्ती मेरे कुछ कहे को पिताजी ने ऐसा सराहा कि गोया मैं न बोलता, तो नाटक का जो असर उन पर पड़ा, वह न पड़ता।
निश्चितत: यह पिताजी की सदाशयता रही, पर बक़ौल मोहन राकेश ‘प्रतिभा तो एक तिहाई व्यक्तित्त्व का निर्माण करती है – बाक़ी दो तिहाई तो लोगों की सराहना से हो जाता है’– और वह पिता हो, तो बात ही क्या!!। शायद नाटक के बाद तुरत बोलने में पिताजी के सहार और उस पर मीनूजी की फुहार ने ही मुझे तुरत बोलने लायक़ बना दिया हो। इस प्रसंग का एक उपसंहार भी है कि जबलपुर में देखे सारे नाटकों में अब तक का अरुणजी का जो अंतिम नाटक देखा है कबीर पर, उस पर एकाधिक इसरार-आग्रह के बाद भी मैं मंच से कुछ न बोला। दूसरे दिन गोष्ठी में खुलकर जो बोला – फिर लिखा भी, वही उस रात न बोलने का कारण भी था। और इस पर मंच से उतरने के बाद मेरे न बोलने को लेकर मीनूजी की गाढ़ी स्मित के साथ उपालम्भ भरी टिप्पणी अपनी बेहद मार्मिकता में अविस्मरणीय है – ‘हमारे लिए दो-चार वाक्य बोल देते नाटक पर, तो क्या कुछ नुक्सान हो जाता आपका?’
लेकिन इन सबके बीच मूल बात यह है कि समीक्षक की सहभागिता का जो संतोष जबलपुर में मिलता, जो कद्र होती है,वैसा और कहीं होता नहीं दिखा। और यह अरुण-रचित ‘विवेचना’ का प्रेम ही नहीं, एक समूची नाट्य-संस्कृति है, जो सचमुच उदाहरणीय है। कहीं-कहीं तो खूब बड़े आयोजन में पहले दिन मंच पर बुलाकर फूल-माला से स्वागत व दो-चार वाक्यों के शुभेच्छा जैसे औपचारिक सम्बोधन करा लेने के बाद सिर्फ़ नाटक देखना और दिन में ख़ाली बैठे रहना ही होता। ऐसे में जबलपुर का आयोजन ख़ास तौर पर यादगार रहता है। दिनभर कुछ न कुछ चलता रहता है। कोई न कोई साथ होता है। टीमों के अभ्यास ही देखते रहते। वैसे अपनी टीम के साथ अरुण को देखना भी एक नाट्यानुभव है।
जब किसी नये नाटक की तैयारी या नियोजित शो के लिए अभ्यास का प्रयोजन नहीं भी होता है, अपनी टीम के साथ शामों को अभ्यास-स्थल पर होना उनकी आदत में शुमार है। एक बार ऐसा भी अवसर बना, जब मैं किसी और कार्यक्रम में जबलपुर गया। अरुण से तो मिलना ही था, लेकिन समय की क़िल्लत कुछ ऐसी हुई कि शाम का ही वक्त बचा, और हम अभ्यास-स्थल (कोई विद्यालय था) पर ही मिले। बड़ा मज़ा आया, जब बच्चों ने विविध प्रकार का कुछ करके दिखाया –काव्यपाठ, किसी कविता की प्रस्तुति, संवाद या नाटक के दृश्य, एकल व समूह गान…आदि। भेंट भी नाट्यमय रही – अरुण के जीवन की तरह। पता चला कि नाट्य पर लिखे विवेचनात्मक लेखों के पाठ भी वहाँ होते हैं। इस क्रम में डॉ श्रीराम लागू पर लिखे मेरे लम्बे लेख का पाठ भी हुआ था, ऐसा बताया गया। याने उनका प्रशिक्षण एक मुकम्मल रंगकर्मी ही नहीं, एक सुशिक्षित, सुरुचि-सम्पन्न पूर्ण मनुष्य बनाने की कार्यशाला होती है – मात्र शो करके निकल जाने की खानापूर्त्ति नहीं। लेकिन कहना होगा कि यह मुम्बई जैसे महानगर में सम्भव नहीं, लेकिन छोटे शहरों में भी अमूमन सुलभ नहीं।
‘विवेचना’ में कुछेक बार तो उत्सव के आख़िरी शो के बाद बच्चे गाते-बजाते बैठ गये और सुबह हो गयी। अरुण को भी मैंने जबलपुर और उसके अलावा भी जागृति के जोश भरे गीत गाते-गवाते सुना है – पीछे कोरस में बच्चे दुहराते। ऐसे खुलेपन-मस्ती व सामुदायिकता का मुख्य कारण है –पाश्चात्य सभ्यता, शहरीपन व तथाकथित आधुनिकता (जिन्हें फैलाने में एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है) से दूरी व भारतीय लोकजीवन से गहरी सम्पृक्ति। ख़ुदा करे, यह कभी ख़त्म न हो – ‘विवेचना रंगमंडल’वैसा ही रहे…। रातों को खाने पर अरुण साथ होते और देर रात तक गप्पें होतीं। उनका अध्ययन कक्ष ही प्रायः मेरा शयन कक्ष बनता, जहां ढेरों पुस्तकें व पत्रिकाएँ सुलभ होतीं।
कई बार मन होता कि काश एकाध दिन कोई न मिलता, कहीं जाना न होता और इन किताबों केसाथ दिन बीतता…पर ऊपर उल्लिखित बेहद नाट्यधर्मी आयोजनों, जिसका रसिया मेरा मन भी है, के कसाव में ऐसा हो न पाता। लिहाज़ा दो-एक किताबें हर बार लेके आता। अरुण का पुस्तकालय उनके व्यक्तित्त्व का सबसे पारदर्शी आईना है। उन्हें जानना हो जिसे, वह और कुछ भले करे, उनके पुस्तकालय में ज़रूर चला जाये। उनके गहरे बामपंथी सोच का ठीक पता मुझे पहली जवाई में घर जाके ही लगा, जो उनके काम को देखते-देखते धीरे-धीरे पुष्ट होता गया। वरना तो उनकी पारिवारिकता-मावीयता-व्यावहारिकता व आचारधर्मिता में वह छिपी रह जाती। उम्र में बड़े होने का जो आदर मुझे अरुण व विवेचना से मिला, वह मेरे लिए अनमोल निधि है। यूँ मुम्बई में विकसित मेरा एक व्यावहारिक मन इन सबसेकुछ अनखाता भी, लेकिन घुट्टी में बसे गँवईं मन को यह सब खूब भाता…।
जबलपुर में नाटक देखने का एक वाक़या ऐसा भी है कि मै घर से मुम्बई आने वाला था। पता लगा की जिस अपराह्न मेरी गाड़ी जबलपुर से गुजरेगी, उसी शाम इन लोगों का एक शो है – प्रेम निशीथ की कविता ‘क़िस्सा-ए-बड़के दा’ की विवेक पांडेय निर्देशित-अभिनीत एकल प्रस्तुति। अरुण व उनके जबलपुर तथा वहाँ की ‘विवेचना’ से प्रेम के साथ नाटक देखने की मेरी लत तो थी ही, सबसे ऊपर कविता मेरी इतनी पसंदीदा कि मेरे परिचय के दायरे में कोई ऐसा न होगा, जिसे बिठाके मैंने ‘क़िस्सा-ए-बड़के दा’ ज़बरदस्ती न सुनायी हो – कुछ को तो कई-कई बार।
जब से कविता पढ़ी – शायद अक्तूबर, 2002 के ‘हंस’ में, तब से अपनी एम.ए. की कक्षा का कोई छात्र बिना यह कविता सुने एम.ए. न कर पाया होगा – हर दूसरे साल प्रथम-द्वितीय वर्ष के छात्रों को इकट्ठा बिठाके पाठ करता। और अब बता ही दूँ कि मुम्बई के कुछ बड़े मंचों ने आग्रह करकेमुझसे यह कविता सुनी और क्यों न बताऊँ कि इससे मैंने हज़ारों रुपए कमाये…। तो बस, जबलपुर उतर गया। अरुण वैसे भी जान जाते, तो दस मिनट के ठहराव (हाल्ट) में भी मिलने आ जाते और ताज़ा खाना बनवा के अवश्य लाते – मैं उनके पुस्तकालय से एकाध किताब भी मँगा लेता, जिसे लौटानी में वापस करता। लब्बोलुबाब यह कि इतने आसंग के बीच विवेक की उस प्रस्तुति ने उस शाम को इतना यादगार बनाया व संवेदन-तंत्र को इतना समृद्ध किया कि वैसी शामें कम ही बीती होंगी। रात की ट्रेन से फिर चल निकला –‘जीवन चलने का नाम’…!!
इसी तरह एक वाक़या नाटक करने का भी है। किसी सदाग्रह वश मैंने एक नाटक में काम किया था – दोपात्रीय नाटक ‘बूढ़ा चाँद’ में एक बूढ़े की पूरक-सी भूमिका। पूरा नाटक केंद्रित था उस दसेक साल की बच्ची के पात्रत्व पर। अरुण ने सुना, तो बस, उत्सव में बुला लिया। और हम भी अधिक से अधिक शो करना चाहते थे। शो ठीक-ठाक हुआ। बच्ची की भूमिका के लिए अस्मिता शर्मा खूब सराही गयी। नाटक की फ़ीस वग़ैरह कुछ तय न थी। मुझे लेना था नहीं। लेकिन बच्ची को चाहिए था। वह अच्छी अभिनेत्री…और यही उसकी रोज़ी-रोटी थी। वह अड़ गयी – और एक ख़ास रक़म के लिए, जो हमारी लियाक़त से ज्यादा थी। मेरा आवेश तो उस पर था, लेकिन उसी रौ में रक़म की राशि मुँह से निकल गयी अरुण के सामने। और उन्होंने बैग से निकाल के उतना पैसा दे दिया। उनकी ऐसी फ़राखदिली व वक्त की नज़ाकत की सम्भाल की याद आने पर मै आज भी फ़िदा एवं अपनी मजबूरी पर शर्मिंदा हो जाता हूँ…।
यह मेरा सौभाग्य है कि देश के कई शहरों को वहाँ के खुत्थे रहिवासियों की नज़रों से देखने-जानने का मौक़ा मिला। इस शृंखला में अपनी हर अवाई में मिलाकर जबलपुर शहर को मैंने अरुण की आँखों से देखा है…और क्या लाजवाब कि प्राय: देर रातों को भटक-भटक कर…। पूरे शहर के बसने-विकसने के इतिहास-भूगोल का उनका ज्ञान व स्मृति अद्भुत है। रामलीला के समय गोविंदगंज ले गये, तो पूरा क्षेत्र घुमाते हुए रामलीला की शुरुआत से लेकर उसकी प्रसिद्धि, उसकी खूबियों के साथ उसमें आती कुछ अनिवार्य व कुछ थोपी जाती ख़ामियों का पूरा विवरण देते गये…। शहर की मशहूर मिठाई ‘खोए की जिलेबी’ है, यह बताया – वहाँ ले जाके व खिलाके…।
फिर यह भी कहा कि यह दो जगहों की मशहूर है – यह आज करमचंद चौक वाली खा रहे है, कल फुहारा की खिलाऊँगा और जो ज्यादा अच्छी लगे, वह भौजी व बेटे के लिए भी ले जाइएगा। और कहा ही नहीं, किया भी – कुछ भी हो जाये, जिलेबी तो हर जवाई में लेके आना ही पड़ता। जो देखना मेरे लिए तीर्थ की तरह हुआ, वह टाउनहाल में परसाईजी का घर। ‘विवेचना’ नाम उन्हीं का दिया हुआ है, जिसमें तब नाटक नही होते थे, लेकिन नाटक शुरू कराने में भी उनकी भूमिका निर्णायक रही। वे भाड़े पर जिस घर में रहते थे, उसमें रहने वालों में परसाईजी के समय के लोग ज़िंदा थे। उनकी ज़ुबानी कई आँखों देखे जीवंत व रोचक वाक़ये सुनपाने का सौभाग्य बना। नाटककार गोबिंद सेठ की भव्य व बड़ी कोठी में ले गये। उनके वारिसों से मिलवाया और पता लगा कि अपने पूर्वज के नाम-काम को लेकर वे लोग कितने सजग-सक्रिय हैं।
पहली बार के जाने में बड़ी हौंस के साथ सबसे पहले उन्होंने अपने ‘ज्ञानदा’ (ज्ञानरंजनजी) से मिलवाया था। वे भी ‘विवेचना’ के पुरस्कर्त्ताओं में हैं। अरुण के रंगकर्म तथा जबलपुर के रंगमंच के बनने-बढ़ने में उनका बड़ा योगदान है –पूरे साहित्य में तो है ही। इस तरह अरुण का उनसे जुड़ाव बड़ा गहरा है। असर भी बड़ा गहरा है। वे कुछ कह दें, तो अरुण अरबदा के करना चाहते हैं। एक बेहद ऊटपटाँग नाटक कर दिया कबीर पर। जब की खिंचाई मैंने, तो पकड़े गये शारारती बच्चे के अन्दाज़ में सफ़ाई दी – ज्ञानदा ने कहा था, तो मैंने कर दिया। प्रियता का यह पैमाना मानवीय भले हो, कलात्मक क़तई नहीं।
लेकिन जो पर्यटन स्थल के रूप में सबसे मशहूर जगह है भेंड़ा घाट, वहीं मैं अरुण के बिना गया और एक ही बार – वह भी बहुत बाद में। उस बार का जबलपुर जाना इसलिए विरल व ख़ास रहा कि किसी दैव-योग से अरुण को खबर हो गयी कि उनके लिए नया नाटक तैयार करने का अनुदान (प्रोडक्शन-ग्रांट) मंज़ूर हो गया है। फिर तो क्या, तबियत अपने ‘अरुण राम’ को अच्छी मिली है – बस, सुलभता के दरिद्दर हैं, वरना कुलाँचे आसमान से कम क्या मारने!! तो तय किया कि आधुनिक क्लासिक करेंगे – ‘आषाढ़ का एक दिन’।
फिर प्रतिबद्ध लोगों को कार्य-संहिता के अनुसार चलने और अपनी क्षमता में सर्वोत्तम देने की धुन होती है। सो, पाठ को ठीक से समझाने-व्याख्यायित करने के पहले सोपान पर अरुण महोदय को मेरे आषाढ़-प्रेम – बल्कि दीवानगी की याद आयी। घनघनाता हुआ फ़ोन आया। आवाज़ में बच्चों-सी मासूमियत और बड़ों-सा सपना था –‘भैया, ए दाईं हमहूँ के एक ठो ग्रांट मिल गइल हौ (जो शायद बाद में मिली भी नहीं)। त ‘आषाढ़…’ फ़ानत हई। तोहंके आवे के हौ – पाठ विश्लेषण बदे, तीन दिन ख़ातिर’। फिर हहाते हुए स्वर में -हवाई जहाज़ से मँगाइब एदाईं’…तब तक बन गया था हवाई अड्डा। इस अरमान व उत्साह पर कौन न बलि जाये…!! मैं जबलपुर उतरा, तो अपनी गाड़ी लिये नवीनजी और साथ में अरुण मौजूद।
डेढ़ इंच ऊपर दौड़ रहे थे पहिए…। ‘ऊँच रुचि आछी’ के मुताबिक़ तय हुआ कि कुछ भी रूटीन नहीं होगा। तो कक्षाएँ खुले वातावरण में जंगलों-पहाड़ियों के बीच रखी गयीं – बहते झरने के किनारे। नाश्ता-पानी सब मिनी बस में लेके जाते। समूह के बच्चों के साथ बड़े भी बैठते…उस सुरम्य प्राकृतिक माहौल में बार-बार खोली-खुली आषाढ़ की परतें फिर नये सिरे से खोली गयीं और वही हुआ, जो हर अच्छी कला की हर आवृत्ति में होता है –‘हाफ़ कंसील्ड, हाफ़ रिवील्ड’। सो, जैसे राजा रघु के राज्य में वर्षा भी ज्यादा होती, ‘विवेचना रंगमंडल’ के परम उत्साही मंसूबों की मानिंद इस बार ‘आषाढ़’ ने अपने को कुछ ज़्यादा ही ‘रिवील’ किया…। और अंतिम बातचीत सिर्फ़ बच्चों के साथ भेंड़ाघाट पर रखी गयी, जिसमें कोई बड़ा शख़्स नहीं गया – सिर्फ़ मै औरभूमिकाओँ के लिए चयनित कलाकार तथा स्वेच्छा से आये समूह के कुछ उत्साही बच्चे। ‘आषाढ़…’ के संवादों-प्रसंगों-दृश्यों-व्याख्याओं के साथ पूरे दिन के दर्शन-प्रदर्शन ने दर्जनों यात्राओं में भेंड़ाघाट न जा पाने के वर्षों के अभावों को असीम भाव-समृद्धि में बदल दिया।
अरुण के साथ कुछ यात्राएँ भी हुईं, जब हम जबलपुर से बाहर मिले। स्वाभाविक ही है कि वे यात्राएँ भी रंगकर्म के चलते ही हुईं – इसी की पूरक। मैं जब ‘काशी विद्यापीठ’ पढ़ाने पहुँचा, तो दो-तीन महीने के अंदर ही मार्च, 2010 में ‘साहित्य और बाज़ार’ पर बड़ा सेमिनार किया और अरुण को थिएटर में बढ़ते बाज़ार पर बोलने बुलाया। अरुण ने लिखित पर्चा पढ़ा और नाटक वाले आदमी का अन्दाज़ बिलकुल अनाटकीय – बल्कि अन्दाज़ ही न था। मुझे उम्मीद थी – बोलेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई अवसर याद नहीं आ रहा, जब मैंने उन्हें कुछ देर मंच से बोलते सुना हो।
वहाँ ऐसा हुआ कि मै नयी जगह पर अपने आयोजन में व्यस्त और अरुण के तो बचपन का शहर बनारस…वे अपने दोस्तों से मिलने में मस्त! और दोस्तियाँ भी कैसी कि रावण बना बीहड़ दोस्त धमकी देता कि पतंग काटने का बदला मंच पर लूँगा, क्योंकि अरुण सीता बने थे। वे खुद न बतायें, तो आज के स्थूलकाय पक्खड़ अरुण को देखकर कोई कहेगा कि कभी ये इतने सुकुमार भी रहे होंगे कि सीता की भूमिका की होगी!! बनारस की रामलीलाओं ने ही उनके थिएटर-कर्म का बीज-वपन किया है। फिर विद्यापीठ से दो किमी पर उनका अपना हरिश्चन्द कॉलेज और विद्यापीठ से दो मिनट पर स्थित मेरा आवास… फिर भी द्वार तक आके घर में न आ सके और मै समझ सका–‘मैं नहीं लौटा तुम्हारे द्वार से, पथ ही मुड़ गया था’। सो, यात्रा की सिर्फ़ गिनती हुई, कोई दस्तावेज न बना।
दूसरी यात्रा दिल्ली की हुई। कभी नामवरजी को सुनते हुए मुझे पता चला कि बनारस में रहने के दौरान उस अंचल के तत्कालीन थिएटर को लेकर उनकी स्मृति में कुछ बुनियादी सामग्री है। बस, अरुण से राय की। थिएटर के लिए तो हमेशा उनकी ‘नसों में खून, दिल में जोश, आँखों में सजा सपना नया…’होता है। तुरत दिल्ली चलने की हामी भर दी। नामवरजी से बात की, तो उन्होंने तीन दिनों अपने घर पर मिलकर बात करने की तारीख़ें दे दीं। हम परम प्रसन्न। तीन दिनों की बात से तो अरुण को पूरी किताब तैयार होने के सपने आने लगे। रामबख्शजी से सम्पर्क किया – ‘गोमती’ गेस्ट हाउस में कमरा बुक हो गया। हमने नियत तिथि पर पहुँच के फ़ोन किया, तो नामवरजी अचकचा उठे।
हमारा भी माथा ठनका, लेकिन सुबह 10 बजे घर पे बुला लिया। फिर बड़ी विनम्रता व पछतावे के साथ उन्होंने खेद व्यक्त किया कि किसी बड़े आयोजन के लिए ‘हाँ’ कहते हुए उन्हें हमारी तारीख़ें याद न आयीं। लेकिन वह दिन पूरा हमें दिया। बातें सचमुच बड़ी उपयोगी और विरल थीं – भिखारी ठाकुर की मसर्रत भरी यादें व नाट्यकर्म के कुछ जीवंत संदर्भ व अद्भुत व्याख्यायें मिलीं। दिन सार्थक हुआ। नामवरजी भी बाक़ी बातें करने के लिए उत्सुक थे – पुन:-पुन: दुबारा आने के इसरार भरे आदेश दिये। ख़ास बात यह थी कि उन दिनों वे सपत्नीक थे। चाय के लिए पूछा, तो मै जाके बना लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बड़ी मसृणता से उन्होंने कहा –‘बैठो, बन जाएगी’। खुद अंदर जाके तश्तरी (ट्रे) सहित उठा के ले भी आये। अरुण तो बाहर आकर बल्लियों उछल रहे थे –‘भैया, फ़ोन करिहा। हमहन फिर चलल जाई – बड़ी उम्दा (उनका प्रिय शब्द) चीज़ तैयार होई’…।
लौटना साथ में तय हुआ था जबलपुर होते हुए, लेकिन वहीं मुझे मां की बीमारी की खबर लगी। मैंने दूसरी रात फ़रक्का पकड़ ली। अरुण ने स्टेशन तक आके विदा किया। यह दुर्भाग्य है कि बहुत चाहकर भी अरुण के साथ हमारी कोई लम्बी यात्रा आज तक साथ में न हो पायी। रेल-यात्रा में निर्द्वंद्व गप का जो आनंद है, वह और कहीं नहीं। इसके कुछ दिनों बाद जब नामवरजी से समय लेने की याद दिलाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने हिम्मत करके कहा कि अब मैं नामवरजी से बात करने न जाऊँगा, तो अरुण बड़े निराश हुए। तब तक उन्हें पता न था शायद कि ‘नीति विरोध सोहात न मोहीं’ की तरह ज़रा भी बात इधर-उधर लटकी, तो मेरा मन बुरी तरह बिदक जाता है।
समय देकर मुम्बई से दिल्ली बुलाये और यूँ भूल जाये कि हमारे आने तक याद न आये कि एक फ़ोन करके रोक ही दे। आप बहुत बड़े होंगे, पर क्या हमारे छह दिन इतने फ़ालतू हैं!! हम इतने नाचीज़ हैं, तो समय दे ही क्यों –‘दाता से सोम भला कि ठावें देय जवाब’। फिर अरुण से आगे कहा ‘मैं समय ले देता हूँ। आप जाके बात कर आइए – काम होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा…। लेकिन मुझे पता था कि अरुण भी यारों का यार है…इस तरह जायेगा हरगिज़ नहीं। हाँ, पहले दिन की बात को अरुण ने लिपिबद्ध किया और हम दोनो के नाम से छपाया भी, लेकिन मेरी रुचि उसमें से निकल गयी, तो आज मुझे यह भी याद नहीं कि किस पत्रिका में छपा – ‘अक्षरा’ थी या ‘आलोचना’ या कोई और…।
लेकिन इन दोनो यात्राओं के पहले हुई थी ‘इप्टा’, रायगढ़ के नाट्योत्सव में शरीक होने की सहयात्रा, जो हर दृष्टि से बड़ी मुफ़ीद रही। हबीब साहब के सात नाटकों के शोज़ का सात दिनों काउत्सव था। हम सप्ताह भर साथ रहे…। हबीब साहब के समूह के लगभग सारे कलाकारों से भी अरुण का अपनापा देखा – यह भी कि किसी को गाँजा पिला रहे हैं, किसी को बीड़ी। और उनसे गीत सुन रहे हैं – गपिया रहे हैं। उसी में से एक ने हबीब साहब का कैरीकेचर बनाते हुए उन पर एक व्यंग्य कविता लिखी थी, वह भी निकाल लिया, जिसे मैं उन पर लिखे आलेख में उद्धृत कर पाया और जिसे पढ़ने का सबने खूब लुत्फ़ लिया। बाद में पता लगा की वह कविता हबीब साहब ने भी सुनी थी और मज़े लिये थे…।
तब देखा कि रंगकर्म करने-कराने काअरुण का दायरा व इसके लिए उनकी क्षमता वनिष्ठा सिर्फ़ ‘विवेचना’व जबलपुर तक सीमित नहीं, सार्वदेशिक है। इप्टा, रायगढ़ के आयोजकों (अजय-उषा आठले) व पूरी टीम के साथ भी उनके सलूक-सौहार्द्र ऐसे ही – गोया उनके भी संचालक हों। वहाँ पहली बार रंगकर्मी के रहन-सहन का बिलकुल ज़मीनी अनुभव शब्दश: हुआ। रंगकर्म अरुण का भी तो शतश: ज़मीनी है, पर वहाँ उनके सज्जित (फ़र्निश्ड) घर में रहने से उतना बजाहिर ‘फ़ील’ नहीं होता। लेकिन यहाँ मिट्टी-निर्मित घर के कमरों में ज़मीन पर गद्दे बिछाके पूरा दल सोता। सिर्फ़ तनवीर-दम्पति को होटल मिला था। बाक़ी हम सब खुले में नल पर नहाते और वहीं चूल्हों पर नाश्ता-खाना बनता…।
इसलिए बच्चों सहित पूरे रंग समूह से एक दिन में सम्बन्ध घरेलू-से हो गये। और अरुण तो सारे बच्चों तक के साथ पहले से ही घुले-मिले थे। उनके साथ इनके उस्ताद व मित्र के मिले-जुले सहज रिश्ते, जिसमें न कोई आग्रह, न अपेक्षा…बस – सब कुछ देना व सब कुछ ग्रहण करना। ऐसे अरुणके साथ से मैंने हर बार बहुत कुछ सीखा है – विश्वविद्यालय के छात्रों से सम्बंधों की बावत अपने अंदर कुछ-कुछ नया उगा के (ग्रो होके) आया हूँ। अब आज के तथाकथित प्रगत (ऐडवांस) समय में ऐसा सम्भव नहीं, वरना मेरी चले, तो नाट्योत्सवों की व्यवस्था स्थायी तौर पर ऐसी ही हो– सामूहिक और सार्वकालिक रूप से खुली। लेकिन आगे चलकर रायगढ़ ने भी अपने को ‘मॉडर्न’ बना लिया – होटेल-निवास…आदि की अभिजात सुविधाओं वाली भी यात्राएँ वहां की हुईं। अरुण को वहाँ जब सम्मानित किया गया, मैं मंच पर मौजूद रहकर खूब गर्वान्वित हुआ। उस पहली यात्रा की लौटानी में याद आता है कि हम दोनो किसी जंक्शन तक साथ आये थे – सामान्य डब्बे में धंसकर खड़े-खड़े भी खूब गपियाते हुए।
रायगढ़ के इस उत्सव के बरक्स देखें, तो आज के नाट्योत्सवों में कुछेक समीक्षक(!) तक ऐसे स्टार हो गये हैं कि फ़्लाइट से आने के बाद किस होटल में ठहरेंगे, कौन सी ब्रैण्ड का पीएँगे और किस होटल का मटन खाएँगे…आदि भी पहले से तय करके आते हैं। फिर शो के दौरान सभागार से बाहर मोबाइल पर लगे रहते हैं और अख़बार में जो छपता है, उसके लिए पंडित ह.प्र. द्विवेदी के शब्दों में कहें, तो ‘पुस्तक छुई तक नहीं और आलोचना ऐसी लिख दी कि ‘त्रैलोक्य विकम्पित’!! लेकिन इस वृत्ति के चलने एवं ऐसे अतिचारों के पीछे एक बाज़ार-तंत्र सक्रिय है, जिसमें अफ़सरशाही से लेकर दलाल तक की कड़ियाँ जुड़ी हैं। इसी की एक कड़ी को एक बार मैंने अरुण के यहाँ देखा। यह उसी ‘आषाढ़ का एक दिन’ के पहले शो का अवसर था, जिसे पढ़ाने मै तीन दिनों के लिए गया और उतनी मधुर यादें लेकर आया था। उसे जबलपुर के साथ मेरे रंग सम्बंधों का चरमोत्कर्ष सोपान कह सकते हैं, क्योंकि शो देखने के लिए आहूत वाली यात्रा में मिली उस कड़ी के बाद कुछ दिनों के लिए बात कुछ बदल-बदल गयी…।
लेकिन मैं तो इस बार मधुरता की और उमंगें सँजो के आया था। शो की इस तामीर में कुछ मेरा भी योगदान था, जिसे देखने का हुलास कुछ और भी था। उसमें और चार चाँद लगाते हुए सतना से मेरे परम मित्र व सरनाम सिने-चिंतक प्रह्लाद अग्रवाल भी जुड़ गये थे, जो जबलपुर के ही मूल निवासी हैं। सतना से उन्हीं की कार में सुहानी यात्रा करके हम एक दिन पहले ही पहुँच गये थे। मल्लिका बनी बालिका की तबियत खराबी की खबर पाकर थिएटर भी गये। मुख्य भूमिका के रूप में यह उसका पहला ही मौक़ा था। सो, तबियत की बदहाली के बावजूद बच्ची के उत्साह व दृढ़ संकल्प में रत्ती भर भी कमी न थी। हम निश्चिंत-से होके, सभी कलाकारों को शुभेच्छाएं देके व बक़ब करके निकले। रात को देर तक भटके।
प्रह्लादजी अपने भाइयों के इसरारों को नज़रंदाज़ करके सोने के लिए मेरे साथ अरुण के घर ही आ गये। सुबह हम दोनो को किसी शिक्षा संस्थान के समारोह में अतिथि होना था। हम नाश्ता करके आयोजन के वाहन का इंतज़ार कर रहे थे कि अरुण-नवीन उस कड़ी को हवाई अड्डे से लिए हुए घर में दाखिल हुए। शाम से साथ रहते हुए भी आगमन की मुझे भनक तक न लगी थी। सहसा देखके लगा कि शायद भनक लगने न दी गयी हो…। इस बालिशता पर हँसी भी आयी –‘निहुरे-निहुरे कहुं ऊँट की चोरी’!!इस युति के परिणाम में थोड़े दिनों बाद ‘विवेचना रंग मंडल’ में ‘सिने आस्वाद’ का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। लेकिन मुझे तो उनके नमूदार होते ही गोयालिफ़ाफ़ा देखते ही मजबून समझ में आ गया था। इन सब बातों से अरुण अनजान न थे। ऐसे खाँटी प्रतिबद्ध से ऐसी उम्मीद कदापि न थी– ब्रूटस, यू टू!! वरना तो इस युग में ऐसी चिंताओं-विस्मयों से रू-ब-रू होना आम है। इसे सहने के संतोष के लिए क़तील शिफ़ाई का एक शेर मेरे लिए सुमिरनी है –
‘तोड़ गये पैमाने वफ़ा, इस दौर में कैसे-कैसे लोग, ये मत समझ कतील कि बस इक यार तेरा हरजाई है। बहरहाल, शो अच्छा हुआ। मंच पर बुलाया गया– उस कड़ी को भी। बोलने की इच्छा बिलकुल न थी। और अपवाद स्वरूप उस दिन आग्रह भी नहीं, बल्कि पूछा गया – बोलना चाहेंगे। ‘ना’ में सर हिला दिया –‘जान बची लाखों पाये’ और ‘लौट के बुद्धू घर को आए’ – मंच से उतर कर सीधे। तय कर लिया –‘ऊधौ, अब न बसौं यहि गाँव’। शायद संयोग पहले से ही जानता था कि देर रात को ज़रूरत पड़ेगी…सो, वाहन सहित प्रह्लादजी को भेज दिया था।
लेकिन एक ही कार्यक्रम से समझ में आ गया और फिर अपने अरुण ‘मियाँ ठौर के ठौर’। वह कड़ी वहीं से छूट भी गयी। मैं नज़र लगाये था कि यह वारदात फिर होती है या नहीं। फिर एक-दो सालों के अंतराल पर सब जस का तस हो गया। तन से ही थोड़ा दूर हुए थे – मन तो उतने ही क़रीब था। इस बात को लेकर ‘कहिहैं सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात’ के सिवा कभी हमारी कोई बात नहीं हुई और सुबह का भूला शाम तक घर आ जाये, तो भूला नही कहा जाता। लेकिन युधिष्ठिर के ‘नरो वा कुंजरो’ जैसा एक स्खलन (मेरी जानकारी में) अरुण का होना था।
और अब इस संस्मरण का समापन जबलपुर की जानिब से… अरुण के शहरे जबलपुर के एक रसिया ने अपने सैलानी सुर में उनके व्यक्तित्त्व को ग़ालिब का अन्दाज़ देते हुए कहा है – ‘तुझे हम वली समझते, जो न बादाख़्वार होता’। यह बात कहने में बड़ी अच्छी, सुनने पर बड़ी हिट लगती है, लेकिन मै जितना अरुण को जानता हूँ – शराब उसके कलाकार की प्रेरणा (उद्भव) नहीं, उपसंहार है। वह पीके नाटक नहीं करता। नाटक तो यूँ भी उसमें भरा हुआ है। जब नाटक शुरू किया, पीता न था – बनारस के बड़े पक्के ब्राह्मण ख़ानदान से है, जिसके तीन पितृव्य या पितामह (चाचा या दादा) कर्मकाण्डी हुआ करते थे। अब पीता है – नाटक कर लेने के बाद (इधर कुछ सालों में बदला है, तो नहीं कह सकता)। और पीने के बाद फिर होश में आने तक किसी काम का नहीं रहता।
कलाकार का अपने शहर को बनाने में एक अहम योगदान होता है। दिल्ली जो है, उसके बनने में कौन कहेगा कि ग़ालिब का योगदान नहीं!! आज के जबलपुर में अरुण का योगदान क्या बताने की बात है!! लेकिन कलाकार के बनने में शहर का योगदान भी कम नहीं – कौन कहेगा कि ग़ालिब के शायर और शराबी बनने में उनके शहर (मुहम्मद ज़ौक़ और बादशाह) का योग नहीं!! जब तीन दिनों अरुण मेरे साथ दिल्ली में था, मैंने अपने न पीने व दोस्तों के साथ महफ़िली निभाने के लिए जाम थाम लेने की आदत का ज़िक्र करके दो पेग से ज्यादा पीने न दिया। यह काम जबलपुर भी कर सकता था। और उस अरुण को भी मैंने देखा है, जो पीता था, लेकिन होश नहीं खोता था- ‘पीने के बाद होश में आना हराम है’ वाली बादाख़्वारी के कारणों का मुझे पता से ज्यादा क़यास है, जो उसके शहर से ही बावस्ता है।
जिस ‘विवेचना’ को अरुण ने अपना जीवन बना लिया और जिसे उसने अपने जीवन का सर्वोत्तम देकर एक वक्त में उस प्रस्थान बिंदु तक पहुँचा दिया था, जहां से वह ‘नया थिएटर’ व ‘कोरस’ जैसे मुक़ाम तक पहुँचने की यात्राएँ कर सकता था…। लेकिन जैसा कि आम है, परिवार हो या संस्थाएँ, टूटती हैं प्रायः आर्थिक कारणों से, लेकिन निर्णायक होते हैं काग़ज़– फ़ाइलें। और मुख्य कर्त्ता होकर भी अरुण ने ये दोनो अपने पास न रखे। बात विश्वास की थी…और पहले वही टूटता है – फिर बाकी का टूटना क्या!! लिहाज़ा दाम तो गया ही, नाम भी न मिला। अरुण को ‘विवेचना रंगमंडल’ बनाना पड़ा। लेकिन नाम में क्या रखा है –‘लुत्फ़ है लफ़्ज़-ए-कहानी में…’!! और ‘विवेचना रंगमंडल’ अपनी कहानी आप कह रहा है…। लेकिन उस मोड़ पर न अनुदान के पैसे आये होते, न विवेचना टूटती। इसके ब्योरे आज तक किसी ने सरे आम नहीं दिये – जानते सभी हैं, पर न कहने का दुनियावी चलन है।
विवेचना के साथ मेरे मन में जमी चार काकाओं वाली ख़ूबसूरत छबि टूटी। दुख सभी को हुआ बहुत, लेकिन अरुण तो अवसाद (डिप्रेशन) में ही चला गया। किसी से बात ही करनी बंद कर दी थी– शायद बात करने लायक़ कुछ बचा न था। कहीं शून्य में ताकते बैठा रह जाता था। उन दिनों उसका सबसे ज़्यादा वक्त शौचालय में बीतता। जिस दुनिया से छला जाकर वह एक चोटी से अतल घाटी में गिर-घिर गया था, उससे दूर रहने का एकांत उसे कमोड पर ही मिलता। उसी अवसाद में वह अरुण, जो पीके बाहोश बना रहता था – बेहोश होने के लिए पीने लगा। यही उसकी बादाख़्वारी का इतिहास है – पीता नहीं है, पिलायी गयी है। छोटे भाई विवेक के नेतृत्व में परिवार न होता, तो इस अवसाद से उबरना न हो पाता। विवेक के मित्र आशीष द्विवेदी ने भी ‘आपद्गतं च न जहाति ददाति काले’के सन्मित्र को सच कर दिखाया…और यह सब प्रच्छन्न रूप से मेरी नज़रों से गुजरा है। कवि के शब्दों में अरुण की तरफ़ से मै कह सकता हूँ – ‘हाय बॉबी, सिर्फ़ तुम भाई न हो, तुम दाहिनी हो बाँह मेरी’।
लेकिन शहर तो हमेशा बहती गंगा में हाथ धोता है। अरुण के साथ पीया-पिलाया भी और फिर उस दौरान रातों को उसके ‘जुनूँ में बकता हूँ जाने क्या-क्या’ को सुबह तीन में तेरह मिला के उक्त ‘बादाख़्वार होता…’ की गवाही में ‘दुश्मनों की क़तार’ खड़ी कर दी…। दुश्मन तो ग़ालिब ने भी ललकार के बनाये –‘बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता’, लेकिन उसमें लहर को सर झुका के ऊपर से बहा देने का हुनर भी था। तभी तो ‘बगर्ना शहर में ग़ालिब की आबरू क्या है’ कहके अपने किये पर सरेआईना राख भी डाल देता था और पशे आईना वो आग आँच भी देती रहती थी। तो अपना अरुण ऐसा ‘वली’ है, जिसे राख डालना आया भी नहीं और भाया भी नहीं।
फिर इसीलिए जैसे ग़ालिब को आख़िरी दिनों में वह दर्जा मिला भी और उसे पाके वे झींके भी –‘वो दिन गये कि कहते थे नौकर नहीं नहीं हूँ मैं’…वैसा अरुण के साथ न होगा। मुझे यक़ीन है कि न वह वैसा (दरबारी) बन पायेगा, न उसे झींकना पड़ेगा –‘ये हौसला मुझको तेरी आँखों ने दिया है’…उन बड़ी-बड़ी आँखों ने रात की कथा के दिनी परिणामों को बिना पलकें झपकाये एक टक देखा है और रात वाली ज़ुबान ने उफ़ तक नहीं किया है…। और इन सब रूपों में वह सचमुच ‘वली’ है। इसीलिए चचा ग़ालिब से मुआफ़ी के साथ मैं अरुण के लिए कहूँगा – ‘तुझे हम वली हैं समझे, गोकि बादाख़्वार है तू’। और कला देवता व कालदेवता से गुज़ारिश करूँगा कि वे तुझे ऐसा ही ‘वली’ बनाये रखें…आमीन!!