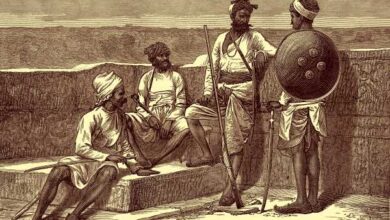चुनावी तपिश में गुम होता हुआ पर्यावरण का मुद्दा !
- महेश तिवारी
जिस लोकतांत्रिक देश में बीते सात दशकों से लगातार जाति, धर्म के नाम पर चुनाव जीता जाता रहा हो। वहाँ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनावी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन उस देश की दुर्गति देखिए जिसके संविधान में मूल कर्तव्य के अंतर्गत वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण का ज़िक्र है। वहीं पर्यावरण जैसा देश का सबसे बड़ा मसला चुनावी घोषणा-पत्र में जगह तक नहीं पाता, और शामिल भी होता तो घोषणा पत्र में ही सिमटकर रह जाता। तभी तो अमेरिका के हेल्थ इफ़ेक्ट इंस्टिट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वायु प्रदूषण से विश्व में 50 लाख मौत हुई। जिसमें 12 लाख मौत अपने देश में हुई। ऐसे में यहाँ गौरतलब हो कि देश में हर जाति और महजब के लोगों की जान दूषित हवा लेती है, लेकिन कोई दल या जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई बयानबाजी तक नहीं करता।
पिछले वर्ष केरल में आई असाधारण बाढ़ भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम थी। ऐसे में आशा और उम्मीद सियासतदानों से की जानी चाहिए कि वे पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सज़ग और निष्ठावान दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आता। आज के दौर में जब देश चुनावी सरगर्मी में उलझा हुआ है। तो वहीं दिल्ली और ऑस्ट्रिया के दो नामी शोध संस्थाओं की रिपोर्ट यह कहती है, कि हमारे देश मे प्रदूषण की रोकथाम के मौजूदा कायदे-कानून के सही तरीके से क्रियान्वयन के पश्चात भी 2030 तक 67.4 करोड़ से अधिक लोग बेहद दूषित हवा में सांस लेने के लिए अभिशप्त होंगे। आगे यही रिपोर्ट कहती कि प्रदूषण की समस्या कमोबेश समूचे देश में है, लेकिन सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में जहरीली हवा की जद में ज्यादातर आबादी है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के हिस्से शामिल हैं। इतना ही नहीं अन्य राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर मानक से ऊपर है, लेकिन सुकून यह कि स्थिति यहाँ की बाक़ी राज्यों के मुकाबले बद्दतर और भयावह नहीं हुई है। वहीं जब आंकड़ों के महासागर में गोते लगाएं तो ग्रीनपीस के अध्ययन के मुताबिक, दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से सात भारत में हैं। तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है।
वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के दौरान जहरीली हवा की वजह से देश में पाँच साल से कम उम्र के लगभग 1 लाख 10 हजार बच्चों की मौत हुई। यही रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण की वजह से भारत में 20 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है जो वैश्विक परिदृश्य में इस वजह से होने वाली मौतों का एक-चौथाई है। वहीं डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में वातावरण में तेज गर्मी और सर्दी देखने को मिल रही है। बारिश के मौसम भी छोटे-बड़े होने लगे हैं। जिसके कारण ही कहीं न कहीं 2006 में राजस्थान, गुजरात में बाढ़ की भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इसके इतर यही रिपोर्ट कहती कि जलवायु परिवर्तन के कारण 1973 के बाद हमारे मुल्क में 28 नए प्रकार की बीमारियाँ सामने आई और उनका प्रकोप बढ़ रहा है ।
ऐसे में बात जब राष्ट्रीय वन नीति की होगी। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भू-भाग का तैंतीस फीसद हिस्सा वनों से आच्छादित होने के बजाय भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान दौर में देश का मात्र 21.54 प्रतिशत भाग वन आच्छादित क्षेत्र है। तो यह शिक्षित और आधुनिक होते समाज की उस कड़ी को रेखांकित करता है, जहाँ पर मानव समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सज़ग दिखता है। पर वहीं संवैधानिक कर्तव्यों को भूल जाता है। साथ में शायद सरकारें भी विकास के आगे विनाश को देखना नागवार समझती हैं। 2018 में एक सुनवाई के दौरान नाराज सुप्रीम कोर्ट की बेंच यह न कहती कि कार्यपालिका अदालत को बेवकूफ बना रही है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमा की गई राशि को अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है।
ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अनदेखी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है?, कि एक तरफ़ पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं सियासी व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए जमा धन का उपयोग सड़कें बनाने, बस स्टैंडों की मरम्मत और कॉलेजों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने जैसे कामों में कर रहीं हैं। स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरणीय संरचना मानव जीवन की पहली प्राथमिकता है। सड़कें आदि बाद की आवश्यकताएं है। तो फ़िर सरकारें सिर्फ़ सड़क आदि बनवा कर आज के दौर में अपनी पीठ जरूर थपथपा सकती है। लेकिन यह भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक 2017, 167 वर्षों में तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। यह रिपोर्ट काफ़ी कुछ सवाल ख़ड़े करती है, कि आख़िर हम समय पर नहीं चेते, तो यह धरती हमारे रहने लायक नहीं बचेंगी। जिसका कारण घटते पेड़-पौधे ही हैं। आज हमारे देश में हर व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ़ 24 पेड़ ही बचे है। ऐसे में सिर्फ़ रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों के चलन को कम करके ही तापमान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसके लिए अन्य उपाय भी करने होंगे। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ईंधन, पौधे और पशु-पक्षी शामिल हैं। इन संसाधनों की देखभाल करना और इनका सीमित उपयोग करके ही प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है, और आने वाली पीढ़ी को सुंदर प्राकृतिक परिवेश दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में विकास की अंधी दौड़ में इनके संरक्षण के प्रति न रहनुमाई व्यवस्था सज़ग दिख रही। न लोग ही इसके प्रति वफादार समझ में आ रहें। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है, कि 73 लोग देश में प्रति घण्टे स्वच्छ पानी ने मिलने के कारण मौत को गले लगा रहे। इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट कहती है, कि हमारे देश में रोपे जाने वाले पौधे में से 35 फ़ीसदी पौधे बढ़ नहीं पाते, तो यह चिंताजनक स्थिति तो अभी से निर्मित हो गई है, फ़िर भविष्य कैसा होगा। इसका सहज आंकलन किया जा सकता है। जंगल की कटाई का मुख्य कारण खेती के लिए वन की कटाई, डूब क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए, शहरों का विस्तार, हाईवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने औऱ वैध-अवैध माइनिंग है। सरकारी आंकड़ों की मानें, तो बीते तीन दशकों में करीब 24 हजार औद्योगिक, रक्षा और जल-विद्युत परियोजनाओं के कारण 14 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का सफाया देश में हो चुका है। इसके अलावा 15 हजार वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र अतिक्रमण के कारण नष्ट हुआ है, और वर्तमान में सिर्फ़ देश के 21.54 फीसद हिस्से में वन बचे हैं।
ऐसे में जब 2019 का आम चुनाव कई मायनों में अहम रहने वाला है। जिसमें पहली बात यह शामिल है, कि इस बार 90 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी लेंगे। दूसरा यह कि इस बार चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक लगभग साढ़े चार करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो इक्कीसवीं सदी में जन्म लेकर पहली बात अपने मत का दान करेंगे। तो नौकरियों, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के साथ पर्यावरण संरक्षण भी राजनीतिक दलों के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा होना चाहिए। हाँ यहाँ हम कह सकते कि भाजपा सरकार ने अपने बीते कार्यकाल में सौर, पवन और हाइड्रो ऊर्जा पर बल दिया है। लेकिन यह प्रयास ऊँट के मुँह में जीरे से ज़्यादा कतई नहीं। आज भारत भले पाँच अक्षय ऊर्जा वाला देश बन गया है और चौथा पवन ऊर्जा वाला देश। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस देश में अमूमन 60 फ़ीसदी से ज्यादा बिजली की मांग कोयला आधारित ताप संयंत्रों के इस्तेमाल से पूरी की जाती है। तो उसे इस प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा। साथ में अन्य तरीकों से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की कवायद करनी होगी। तभी बेहतर और स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना चरित्रार्थ होगी। ऐसे में देश की अवाम को पर्यावरणीय मुद्दे को ध्यान में रखकर दलों से प्रश्न चुनाव प्रचार के दौरान पूछने चाहिए कि सत्ता में आकर पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके पास क्या विजन है, क्योंकि जब बात विकास की होगी तो पर्यावरण को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। तभी कुछ स्थिति हमारे देश की आबोहवा की बदल सकती है।
लेखक टिप्पणीकार है तथा सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लेखन करते हैं|
सम्पर्क- +919630377825, maheshjournalist1107@gmail.com
.