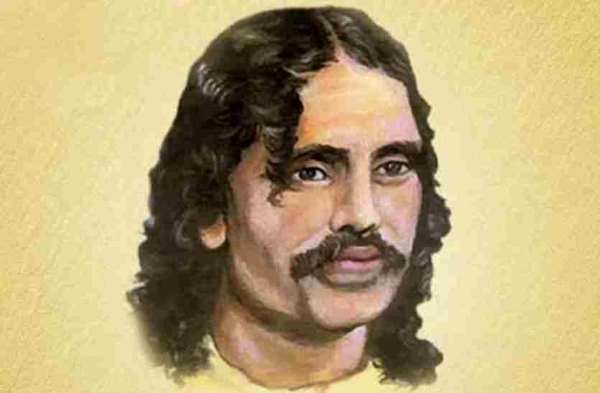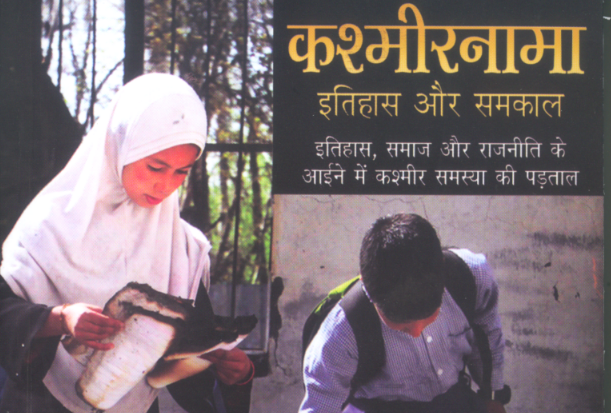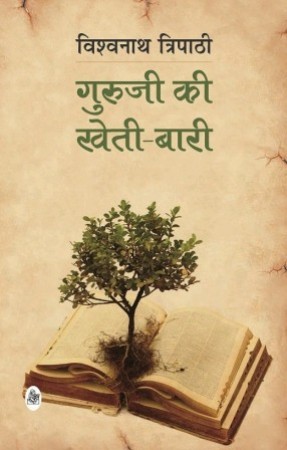
इन दिनों एक नियमित अंतराल पर हिन्दी में आत्मकथाओं और संस्मरणों के प्रकाशन का सिलसिला चल निकला है। हर गुजरते साल के साथ ऐसी एकाध दर्जन रचनायें सामने आ रही हैं। कहना ना होगा कि दलित आत्मकथाओं के लगातार प्रकाशन ने इस विधा को प्राणवान बनाने का काम किया है। अन्यथा गद्य विधाओं में उपन्यास और कहानी जैसी विधा ही चर्चा के केन्द्र में रहती आई थी। संवाद प्रकाशन ने विदेशी रचनाकारों की जीवनियों और आत्मकथाओं के अनुवाद के जरिये इस दिशा में एक बड़ी कमी को दूर करने की पहल काफी पहले आरंभ कर दी थी।
पर अब हिन्दी के प्रकाशकों ने वरिष्ठ का दर्जा प्राप्त कर चुके साहित्यकारों की आत्मकथा और संस्मरणों को सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने की दिशा में एक तेजी लाई है। राजकमल प्रकाशन इस दिशा में अग्रणी है। बीते वर्षों में इस दिशा में उसने विश्वनाथ त्रिपाठी की ‘गुरुजी की खेती बारी’ (2015), निर्मला जैन की ‘जमाने में हम’ (2015), धीरेन्द्र अस्थाना की ‘जिंदगी का क्या किया’ (2017) प्रकाशित की है। वाणी प्रकाशन इसी बीच मुनव्वर राना की आत्मकथा ‘मीर आ के लौट गया’ छापी है।
इस ढंग से अगर गौर किया जाये तो पहले की तुलना में अब इस विधा में एक वैविध्यपूर्ण रंगत लौटी है। तद्भव ने तुलसीराम की आत्मकथा ‘मुर्दहिया’ और ‘मणिकर्णिका’ धारावाहिक छापी थी। इसी क्रम में अरुण कमल और विनोद कुमार शुक्ल भी अपने आत्मकथ्यों के साथ इस सिलसिला को आगे बढ़ाते रहे। हिन्दी-उर्दू की वह पीढ़ी जो अपनी पारी खेल चुकी है अब बिना किसी ओट के अपने ‘आत्म’ के गठन की कहानी सीधे-सीधे कहने को तैयार है। इनसे होकर गुजरना बेहद ही सुखद है।
एक तो उस दौर के परिवेश को आप महसूस कर सकते हैं। उनकी शख्सियतें किन गलियारों, पगडंडियों से होती हुई इस मुख्य मार्ग तक पहुँची है। उसे जानना बेहद प्रेरक है। कोई इसे संस्मरणात्मक बना कर पेश कर रहा है तो कोई आत्मकथा के रुप में। इन किताबों के जरिये आप चरित्रों के ऐसे बीहड़ में दाखिल हो जाते हैं कि कई बार यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे यारबाश, घरफूंक मस्ती से ओत-प्रोत, फक्कड़ लोगों की ऐसी पीढ़ी भी अब लुप्तप्राय होने को है।
जिन शहरों में उनका जीवन गुजरा उसकी जो तस्वीरें वे शब्दों में खींच रहे हैं। गर आप थोड़े भावुक और रोमानी किस्म के इंसान हैं तो यह दुनिया आपको सम्मोहित करने के लिए काफी है। उनके जीवन की दुश्वारियों ने उनके ललाट पर जो चिंता की रेखायें उभारी थीं, इन आत्मकथाओं और संस्मरणों में सर्जक उन गुजरे वक्तों को जिस हैरतंगेज अंदाज में परोस रहा है, वह गजब की पठनीयता से लबरेज है।
इन किताबों में अजब-गजब खुलासे हैं। अप्वांइटमेंट की कहानियाँ हैं तो जुगत या जुगाड़ के किस्से भी हैं। लेकिन यह सब शख्सियतों के सच कहने के साहस पर निर्भर करता है। जैसे निर्मला जैन की आत्मकथा ‘जमाने में हम’ एकेडमिक पॉलिटिक्स को जिस ढंग से संबोधित करती है, इससे उनकी साहस का पता चलता है। और उनका यह ‘गट्स’ और ‘करेज’ इस किताब को एक अलग ऊँचाई दे जाती है। विश्वनाथ त्रिपाठी की ‘गुरुजी की खेती बारी’ निर्मला जैन की किताब के मुकाबले शाकाहारी किस्म की किताब है, जिसमें मसाला कम है। विश्वनाथ त्रिपाठी की सदाशयता, भलमनसाहत और निरीहता को पग-पग पर उद्घाटित करती यह किताब एक ओर तो अपने गद्य के कारण पढ़े जाने की मांग करता है।
वहीं दूसरी ओर यह संभवतः पहली किताब है जिसे एक गुरू ने अपने छात्रों को याद करते हुए लिखा है। गुणा-गणित में पारंगत सेटिंगबाज छात्रों के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी ने इस किताब में एक बड़ा खूबसूरत शब्द दिया है – नक्शेबाज छात्र। इसके उलट छोर पर एक किताब ऐसी भी है जिसमें छात्रों ने अपने गुरु के बारे में लिखा है और उस किताब का नाम है ‘जेएनयू में नामवर सिंह’, जिसे सम्पादित करने का काम सुमन केसरी ने किया है। बहरहाल इन किताबों में संस्मरण और आत्मकथात्मकता के तत्व घुल-मिल के नमूदार हो रहे हैं। अब भी संस्मरणों के मामले में काशीनाथ सिंह का जोड़ नहीं है, ‘याद हो कि ना याद हो’ और ‘घर का जोगी जोगड़ा’ जैसी किताबें इस विधा में नजीर की तरह हैं।
इसमें अचानक भस्म लगाये औघड़ की तरह रवीन्द्र कालिया अपनी ‘गालिब छूटी शराब’ के साथ दाखिल हो गये थे। ‘गालिब छूटी शराब’ उस नोक पर टिकी किताब है जहाँ संस्मरण और आत्मकथा में धागे भर का अंतर रह जाता है। धागा खींच दो तो वह फर्क मिट जाता है। इन किताबों से गुजरते हुए इन रचनाकारों के प्रति मन एक अलग सम्मान से भर जाता है, उनकी दिपदिपाती संघर्षशीलता अभिभूत करती है। लगता है कि तपे बगैर कुंदन नहीं बना जा सकता है।
यह एक विधा के बतौर उभार ले रही है। आज हिन्दी में एक साथ पाँच-सात पीढियाँ सक्रिय हैं। इनमें से जो सबसे वरिष्ठ पीढ़ी है, उनके बारे में और उनके दौर के बारे में जानने का चाव इस विधा को लंबे समय तक जीवंत बनाये रखेगा। उनकी रचनाधर्मिता को समझने की कुंजियाँ इन आत्मकथाओं में बिखरी पड़ी रहती हैं। उनके रचना संसार की निर्मिति के मूल में जो परिवेश रहा है, उसकी जानकारी इफरात में मौजूद रहती है।
जैसे हाल ही में आई धीरेन्द्र अस्थाना कि आत्मकथा ‘जिंदगी का क्या किया’ को देखें तो उनकी कहानियों से लेकर उनके उपन्यास तक के कथासूत्रों को उन्होंने सविस्तार बताया है। ऐसी ही एक अलग ढंग की प्यारी-सी किताब है शिवमूर्ति की लिखी ‘सृजन का रसायन’। जिसमें उनकी रचना प्रक्रिया और रचना संसार को समझने का हैंडबुक कह सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन इस श्रृंख्ला को आनेवाले दिनों में समृद्ध करते हैं। आत्मकथाओं के मुकाबले जीवनियाँ कहीं नहीं ठहरती हैं। शायद उसकी प्रामाणिकता को लेकर मन के किसी कोने में संशय बचा रह जाता है। बल्कि आत्मकथा में थोड़ी मिलावट भी जादू-सा असर करती है।
कवि वीरेन डंगवाल की मृत्यु के बाद उनके साथ बिताये वक्तों को उनकी कविता के मार्फत् याद करने का एक सिलसिला पंकज चतुर्वेदी ने अपने फेसबुक वॉल पर शुरु किया था। वीरेन डंगवाल के साथ गुजारे गये वक्त को जिस शीद्दत ओर संवेदनशीलता के साथ पंकज चतुर्वेदी ने फेसबुक पर जिया। उसके बाद सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है, इसका आशय बदल गया। बाद में उनके फेसबुक पर लिखे इन शताधिक पोस्ट्स को पहल ने अलग से किताब के रुप में प्रकाशित किया।
यों तो उस किताब को आये काफी वक्त हो गया पर इस विधा में जितनी तोड़-फोड़ उस अकेली किताब ने मचायी थी, वैसा फिर दुबारा देखने को नहीं मिला। वह किताब थी, स्वदेश दीपक की ‘मैंने मांडू नहीं देखा’। उस किताब को याद करें तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आनेवाले दिनों में इस विधा की उड़ान देखने लायक होगी। इंच-दर-इंच अपने दायरे का विस्तार करती यह विधा अनंत संभावनाओं से भरी है, आनेवाले दिनों में इसकी खूबसूरती और सुगंध को हम और विस्तारित होता हुआ पायेंगे।