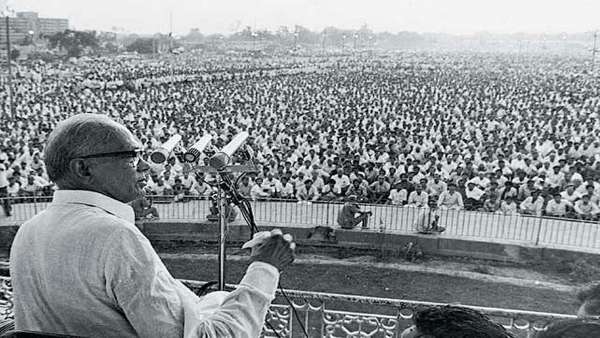सिर्फ कुंवर सिंह ही नहीं थे ‘1857’ के विद्रोही
ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ कुंवर सिंह ने ही अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई लड़ी थी। बिहार में ऐसे अनेक छोटे-बड़े जमींदार थे, जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से देश को मुक्त कराने का प्रयास किया और या तो अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते शहीद हुए या अंग्रेजों के द्वारा पकड़ कर फांसी पर लटका दिये गए। यह बात हवा में नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हैं। ‘1857’ के समय के सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करने पर तथा बिहार के गांव-गांव में फैले लोककथाओं और किंवदंतियों से गुजरने पर कोई भी अध्येता इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बिहार में 1857 का सम्बन्ध सिर्फ कुंवर सिंह, अमर सिंह, दानापुर के कुछ सैनिकों और पीर अली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे बिहार के सैकड़ों छोटे-बड़े जमींदार और लाखों आम जनता की भावनाएँ जुड़ी हुई थी।
फर्ग्युसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने पटना से बंगाल सरकार के सचिव को 9 अगस्त 1859 को लिखे पत्र में इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले हजारों जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे या तो अंग्रेजों ने बेंच दिया या वैसे लोगों को दे दिया, जिन्होंने विद्रोहियों को कुचलने में उनकी मदद की थी। पटना और तिरहुत की छोटी इस्टेटों को जब्त किया गया और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा गया। इस तरह से जमींदारों की संपत्ति जब्त करके उसे बेचने से अंग्रेजी सरकार के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई। अंग्रेजों द्वारा हजारों जमींदारों की संपत्ति जब्त करना इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का सम्बन्ध सिर्फ कुंवर सिंह से ही नहीं था। जमींदारों की संपत्ति जब्त की गई, इससे यह तो पता चलता है कि जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया या नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता चलेगा अंग्रेजों द्वारा जमींदारों और आम जनता को दी गई सजा से।
सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन से यह साफ पता चलता है कि ‘‘बिहार में विद्रोह के दौरान 18 हजार से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए।’’1 इनमें से अधिकांश लोग आम नागरिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म और शोषण से तंग आकर उनके दफ्तरों और आवासों को आग के हवाले कर दिया था। यह सच है कि बिहार में कुछ जमींदारों और सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। लेकिन ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखा। छपरा का एक व्यक्ति जिसका नाम शेख बहादुर था, वह मेरठ डिवीजन की 11वीं नेटिव इंफैंट्री में मेजर था। विद्रोह को कुचलने में उसने अंग्रेजों का साथ दिया। मेरठ के कमिश्नर एफ- विलियम्स ने इस सम्बन्ध में सरकार को पत्र लिखकर बताया कि शेख बहादुर को उनके गांव के अपने लोगों ने जाति से निकाल बाहर कर दिया है। आम आदमी अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में कई तरह से शामिल हो रहा था- जमींदारों का तन मन और धन से साथ देकर, अंग्रेजों के दफ्तरों और आवासों में आग लगाकर, अंग्रेजों को खाने-पीने का समान देने से मना करके, और किसी भी प्रकार के सरकारी कर चुकाने से मना करके।
बिहार के मधेपुरा नामक प्रखंड में दुनियाही नामक एक गांव है। इस गांव के आशा मण्डल नामक व्यक्ति ने आसपास के गांवों में लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार का सरकारी कर नहीं देना है, अब अंग्रेजी राज खत्म हो गया है। इसी तरह से कई छोटे-छोटे किसानों ने भी विद्रोह में भाग लिया- ‘‘मधेपुरा के मनहरा नामक गांव के किसान छोटी यादव ने भी अपने क्षेत्र के कृषकों को संगठित कर सरकारी लगान देना बंद करवा दिया और शंति का बिगुल फूंक दिया। सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई। किंतु उस जमाने में ग्राम्य रक्षा और क्रांतिकारी दल का गठन कर उन्होंने जन जागरण के अनेक कार्य किये। पूर्णिया से 15 किलोमीटर पूर्व लाल बालू का ईदगाह और बड़ा मैदान इसका साक्षी है कि वहां 17 दिसंबर 1857 को राष्ट्रभक्तों एवम् भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर यूल के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। सम्प्रति यह मैदान राष्ट्रीय स्मारक के रूप में चिन्हित है।’’2
1857 के विद्रोह की किसी न किसी घटना से जुड़े हुए स्थलों की संख्या बिहार में पर्याप्त है। ‘‘सरकारी दस्तावेजों में यह नोट किया गया कि जून महीने में शाहाबाद के विद्रोहियों ने सोन नदी को पार कर बिक्रम तथा मसौढ़ी में सरकारी भवनों को जला दिया और ध्वस्त कर दिया।’’3
आज भी पटना से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित बिक्रम के लोग उस जगह के बारे में बताते हैं, जहां 1857 में सरकारी बंगले में आग लगा दी गई थी। इस स्थल पर यह सवाल उठता है कि विद्रोही सरकारी बंगलों में आग क्यों लगाते थे? दरअसल सरकारी बंगलों में आम आदमी और जमींदारों से संबंधित वैसे दस्तावेज रखे होते थे जिनके माध्यम से अंग्रेज इनका शोषण करते थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि मौका मिलते ही ऐसे दस्तावेजों को जला देने का काम किया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध लेखक जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है कि ‘‘बलवे में दूसरे भवनों के साथ सार्वजनिक रिकार्ड कक्ष भी जला दिया गया और इसके सभी बहुमूल्य सामान लूट लिये गये या नष्ट कर दिये गये।
1857 के पहले के एकमात्र शासकीय अभिलेख नवादा सबडिवीजन के बचे हैं, जिसे देशी कर्मचारियों ने उस समय पास की पहाड़ी की एक गुफा में छिपा दिया, जब बलवाईयों ने स्थानीय कार्यालयों को नष्ट कर दिया था। वे अभिलेख अब भी हैं, लेकिन अपने अस्थायी गुप्त स्थान से अस्तव्यस्त अवस्था में लाये जाने के बाद उन्हें कभी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया गया। अतः उनमें जो कुछ है उसका विस्तृत विवरण असंभव है। वर्तमान लेखक ने ऐसा बहुत देखा है, जिससे वह कह सकता है कि वे भविष्य में किसी ऐसे स्थानीय इतिहासकार को बेशकीमती जानकारियां उपलब्ध करायेंगे, जिसके पास ढेर सारा खाली समय हो।’’4
बिहार के प्रसिद्ध जिला गया में भी आम जनता ने विद्रोह कर दिया। मेरठ और दिल्ली में विद्रोह की जो शुरुआत हुई उसकी खबर जल्द ही गया पहुंच गई। जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है कि ‘‘शहर (गया) के भीतर ही, देश के सारे हिस्से में फैले अलगाव को फैलाने के लिए ब्राह्मण पूरी कर्मठता से लगे हुए थे, जिसके तहत बाजारों में आटे में सूअर तथा बैल की हड्डियां तथा लहू मिले होने की बात की जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक वहां नियुक्त सिख सैन्य टुकड़ी को इन अफवाहों से बरगलाकर उन्हें विद्रोहियों के प्रयोजन हेतु तैयार करना था। जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने सिखों को ईसाई घोषित करते हुए जाति से बहिष्कृत कर दिया। इस प्रक्रिया को मजबूती से दमित किया जाना आवश्यक हो गया था। इसलिये एक बढ़ई को जिसके खिलाफ सिखों को बरगलाने की कोशिश का कोई सबूत नहीं था, वहां की सारी पुलिस और सेना के सामने बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस उदाहरण का शहर पर काफी अच्छा असर हुआ।’’5
गया में जिन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया उसमें जीवधन सिंह, हैदर अली खान, कुशल सिंह प्रमुख थे। इन लोगों का साथ बाद में सैनिकों ने भी दिया। ‘‘भागलपुर में मैक्डॉनल्ड और यूल पर हमले के साथ तनाव की शुरुआत हुई, मुंगेर में भी बागियों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। पूर्णिया में गदर की शुरुआत एक अफवाह से हुई और अधिकारी उन्हें कोई हानि पहुंचाने में असफल रहे। मुजफ्फरपुर में सिपाहियों का विद्रोह कोई बड़ा आयाम ग्रहण नहीं कर पाया, उसे दबा दिया गया और उनमें से कई सरहद पार नेपाल चले गये। चम्पारण, सारन और दरभंगा में भी विद्रोह का बिगुल बजा।’’6
ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या बहुत है कि अंग्रेजों के आने से भारत की न्याय-व्यवस्था सुधर गई। लेकिन कोर्ट-कचहरी का नाम सुनते ही आम जनता में जिस तरह का भय व्याप्त हो जाता था, उससे तो यह कहीं से भी नहीं लगता कि अंग्रेजों ने भारत की न्याय व्यवस्था सुधार दी। अंग्रेजों की न्याय-प्रणाली से आजिज आकर वैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में वकीलों को वेश्या कहा था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यास ‘परख’ में लिखा है -‘‘वकालत में क्या है? अपने देश का सत्यानाश है, और आत्मा का सत्यानाश है।—- ओ हो! तो आप ईमानदार वकील बनेंगे। तब तो म्यूजियम के लायक होंगे आप, क्योंकि अभी तक ऐसा जानवर देखा नहीं गया।’’7
अंग्रेजों की इस न्याय-व्यवस्था पर आम जनता ने भी अपने गीतों और लोककथाओं के माध्यम से खूब कटाक्ष किया है। इस सन्दर्भ में एक लोक कवि की एक कविता का यह अंश देखने लायक है –
समुझि परी जब जाएब कचहरी
खाइल पीयल लेल देल कागज बाकी सब निकसी
धरमराज जब लेखा लीहन लोहा के सोटबार मार पड़ी
आगे पीछे चोपदार ढाई वी मुगदर जय के फांस पड़ी
आगिन खंब में बांध के रखिहें, हाजरी जमिनी कोइ न करी।8
बिहार में 1857 की गतिविधियों पर बात करते हुए यह कैसे संभव है कि वहाबी आन्दोलन पर बात न की जाय। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. के. के. दत्त ने अपनी पुस्तक ‘बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास’ में लिखा है कि ‘‘तथाकथित वहाबी आन्दोलन का 19वीं सदी के बिहार के स्वातंत्र्य-संघर्ष में महत्त्वपूर्ण स्थान था। 46 वर्षों तक (1822 से 1868) पटना इसका एक प्रमुख केंद्र था।— वहाबी आन्दोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा आरंभ किया गया था। किंतु उस युग के राजनैतिक परिवेश में इसने भारत में अंगरेजी राज को समाप्त करने के उद्देश्य से एक धार्मिक राजनीतिक रूप ले लिया तथा उसी रूप में उसका विकास हुआ।’’9
डॉ. के. के. दत्त ने ‘वहाबी आन्दोलन’ के लिए ‘तथाकथित’ शब्द का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है कि अंग्रेजों ने इस शब्द का इस्तेमाल इस आन्दोलन को सीमित करने के लिए किया था। यह सच है कि वहाबी आन्दोलन का आरंभ में उद्देश्य धार्मिक ही था, लेकिन अंग्रेजों के शोषण से तंग आकर, और उनके द्वारा लगातार धार्मिक भावनाएँ आहत किये जाने की वजह से वहाबी आन्दोलन से जुड़े हुए लोगों ने यह तय किया कि अंग्रेजों का हर मोर्चे पर विरोध करना है। फलस्वरूप पटना में वहाबी आन्दोलन से जुड़े लोग 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरूद्ध आम जनता की भावनाएँ भड़काने लगे।
बिहार और बंगाल में शाह मोहम्मद हुसेन ने वहाबी आन्दोलन की बागडोर संभाली। इस आन्दोलन में दो भाइयों विलायत अली और इनायत अली ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। वहाबी आन्दोलन के बारे में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 1857 के विद्रोह के पहले से ही यह आन्दोलन जारी था, और इसके नेता अंग्रेजों को काफिर मानकर उनसे नफरत करते थे। इसका प्रमाण रावेनशॉ की रिपोर्ट है। बंगाल सरकार को भेजे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘1852 में पंजाब के अधिकारियों ने एक राजद्रोहात्मक पत्रचार पकड़ा। उससे पहाड़ियों के हिंदुस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा रावलपिंडी स्थित नेटिव इनफैंटरी के चौथे रेजीमेंट को फोड़ने के प्रयत्न का रहस्योद्घाटन हुआ। इस षड्यंत्र की मूल योजना पटना में बनाई गई थी- यह विदित हुआ।’’10
जैसे ही 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, पटना के तत्कालीन आयुक्त विलियम टाइलर ने वहाबी नेताओं के विरूद्ध अत्यंत कठोर दमनात्मक कारवाईयां की। उसने इन नेताओं को गिरफ्रतार करने के लिए तमाम कायदे-कानून ताक पर रख दिये।

बिहार में 1857 के विद्रोह के नायकों में वीर कुंवर सिंह के बाद पीर अली का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। पीर अली लेखक और पत्रकार होने के साथ ही साथ सच्चे अर्थों में बुद्धिजीवी थे। अंग्रेजों के विरूद्ध पटना की सड़कों पर जो पहला जुलूस निकला, उसका नेतृत्व पीर अली ही कर रहे थे। पीर अली को गिरफ्तार करके पटना के तत्कालीन आयुक्त विलियम टेलर ने उनसे अन्य विद्रोहियों का नाम और पते बताने को कहा। टेलर ने उसके बदले में पीर अली को छोड़ देने का लोभ दिया। हमलोग खुदीराम बोस या भगत सिंह के बारे में कहते हैं कि उन दोनों ने फांसी के तख्ते पर झुलने से पहले कहा था कि तुम (अंग्रेजों) एक खुदीराम या एक भगत सिंह को फांसी दोगे तो हजारों खुदीराम या भगत सिंह पैदा हो जाएँ गे। लेकिन 7 जुलाई 1857 को जब पीर अली को फांसी पर लटकाया गया तो उससे पहले उन्होंने जो कहा, वह 1857 के विद्रोह के महत्त्व को हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देता है- ‘‘तुम लोग (अंग्रेजों) मुझे और मेरे साथियों को फांसी की सजा दे सकते हो, लेकिन हमारे खून से हजारों वीर पैदा होंगे और अंग्रेजी राज का खात्मा कर देंगे।’’11
पीर अली का यह कथन वैसे लोगों को करारा जवाब है जो 1857 को सामंतों का विद्रोह मानते हैं। पीर अली लखनऊ के रहने वाले थे और पटना में आकर बस गए थे। पटना का तत्कालीन आयुक्त विलियम टेलर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीर अली ही विद्रोह का मुखिया था। उसने ही लायन को खुद गोली मारी थी। पीर अली का सम्बन्ध वहाबी आन्दोलन से भी बहुत ही गहरा था। कयामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक ‘वहाबी मूवमेंट’ में वहाबी आन्दोलन से पीर अली के संबंधों की विस्तार से चर्चा की है। पीर अली अपने प्रगतिशील विचारों और फौलादी हिम्मत की वजह से सच्चे बुद्धिजीवी और महान देशभक्त के रूप में याद किये जाते हैं। 1857 के विद्रोह में पीर अली जैसे सच्चे देशभक्तों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। 1857 के विद्रोह के महत्व को समझते हुए अंग्रेज लेखक लार्ड क्रोमर ने लिखा कि ‘‘मैं चाहूंगा कि अंगरेजों की तरूण पीढ़ियां भारतीय विप्लव के इतिहास को पढ़े, समझे एवं उसे आत्मसात करे तथा उससे शिक्षा ले। इसमें हमारे लिए अनेक संदेश एवम् चेतावनी भरी हुई है।’’12
इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘1857’ में लिखा है ‘‘बिहार के भूमि-पति बराबर अंग्रेज सरकार के साथ रहे। एक बार दरभंगा, डुमरांव और हथवा के महाराजाओं की स्वामिभक्ति पर शक किया गया लेकिन उन्होंने और उनके साथी जमींदारों ने सरकार को जन और धन की सहायता दी।’’13 सुरेंद्रनाथ सेन का उपर्युक्त कथन बिहार में 1857 के महत्व को कम करके आंकता है।
प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत की महत्वकांक्षी किताब ‘1857 बिहार-झारखंड में महायुद्ध’ से गुजरने के बाद कोई भी पाठक सुरेन्द्रनाथ सेन के उपर्युक्त कथन से सहमत नहीं हो सकता।
इस स्थल पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि जिस तरह से कुंवर सिंह और अमर सिंह से संबंधित लोकगीत जनमानस में अंकित हैं, उस तरह से विद्रोह में शामिल बिहार के अन्य जमींदारों से संबंधित लोकगीत बहुत ही कम उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं भी उसे अब तक लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है।
सन्दर्भ
1- प्रसन्न कुमार चौधरी, श्रीकांत, 1857 बिहार-झारखंड में महायुद्ध, पृ. 145
2- वही, पृ. 170
3- वही, पृ. 172
4- वही, पृ. 261
5- वही, पृ. 129
6- वही, पृ. 130
7- जैनेन्द्र कुमार, परख, पृ. 11-12
8- विश्वमित्र उपाध्याय, लोकगीतों में क्रांतिकारी चेतना, पृ. 162
9- डॉ0 के0 के0 दत्त, बिहार में स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास, भाग- 1, पृ. 79
10- वही, पृ. 81
11- श्रीकांत, पीरअली (लेख) प्रगतिशील वसुधा-76, जनवरी-मार्च 2008, पृ. 374
12, वही
13– सुरेंद्र नाथ सेन, अठारह सौ सत्तावन, पृ. 310