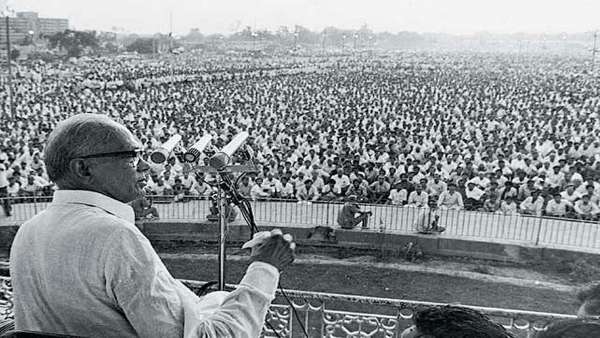मध्यकाल में भारत में स्थापित मुस्लिम सल्तनतों के रवैयों में भिन्नता
इस्लामी शासकों के भारतीय अनुभव के सम्बन्ध में यद्यपि कुछ इतिहासकार सामान्यीकरण का प्रयास करते हैं, परन्तु ऐतिहासिक अभिलेखों को देखने से भारत के इस्लामी दरबारों के रवैयों में काफी भिन्नता प्रगट होती है। दिल्ली में स्थापित सबसे पहले की सल्तनतें, हिन्दू और भारतीय मूल के मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण थीं। जबकि भारत में ही पैदा और बढ़े शासकों द्वारा स्थापित कुछ सल्तनतें व्यवहार में ज्यादा उदारवादी थीं और राजपूत तथा हिन्दूओं की सहकारिता के ज्यादा इच्छुक थे।
विदेशी विजेताओं द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत मध्य एशिया के अप्रवासी एवं तुर्क कुलीनवंशी मुस्लिमों की ओर विशेष झुकाव रखते थे। बाद में, अफगान कुलीन और अबीसिनियन हपसी वंश के दास योद्धा भी उभर कर आये। ईरानी शियाओं ने सुन्नी तुर्को एवं अफगानों के विरूद्ध एक धड़ा संगठित किया और परशियन नमूने को पेश करते हुए शक्ति के लिए स्पर्धा भी की। जो भी हो, अल्पसंख्यक और सीमित अधिकार प्राप्त इन सल्तनतों को हिन्दू मध्यस्थों और परिवर्तित मुसलमानों पर करों की वसूली तथा कानून व्यवस्था के लिए आश्रित रहना पड़ता था।
इस तरह ब्राह्मण, कायस्थ, खत्री और अन्य जातियों से हिन्दू और मुसलमान जमींदार एवं प्रशासक इस्लामी दरबारों के अपरिहार्य औजार बने और कभी कभी वे ऊंचे पदों पर भी पहुंचे। ये दरबार विदेशी व्यापारियों, वाणिज्यिकों और सभी जातियों के साहूकारों यथा हिन्दू, जैन और परिवर्तित मुसलमानों यथा खोजा, बोहरा, और गुजरात के मैमन पर भी आश्रित हुआ करते थे।
इन सल्तनतों की स्थिरता कमाबेश हिन्दू और स्थानीय जन्मे मुसलमानों के मध्यस्थों की मौन सम्मति और राजभक्ति पर टिकी हुआ करती थी। जब कभी इनको उकसाया जाता ये प्रमुख सल्तनत के खिलाफ सत्ता पलट और राजद्रोह में सहयोगी बनते और भड़क जाते। 14 वीं सदी में दिल्ली सल्तनत प्रादेशिक विद्रोहों के कारण बिखर गयी थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह सब मुहम्मद इब्न तुगलक, 1325-51, के निरंकुश शासन के भड़काने से हुआ था जिसकी कट्टर और विस्तारवादी नीतियों ने बड़े पैमाने पर बैरभाव और आक्रोश फैलाया था।

दिल्ली की सल्तनत के पतन के फलस्वरूप बहुत से प्रादेशिक कुलीनों ने अपनी स्वतंत्राता घोषित की और स्थानीय सल्तनतों की स्थापना कर ली। जौनपुर की शारकी सल्तनत और अहमदाबाद की गुजरात सल्तनत दोनों को भारत में जन्में मुसलमानों ने स्थापित किया था। अहमदनगर और बंगाल अबीसिनियन दास योद्धाओं की पीढ़ियों ने और खानदेश को एक शासक जो अपने को अरब मूल का पीढ़ी का कहता था, ने स्थापित किया था। भारत मूल के मुसलमान शेरशाह सूरी ने गंगा के दुआब में कुछ समय के लिए वैकल्पिक राज्य की स्थापना की चुनौति मुगल साम्राज्य को दी थी।
ये प्रादेशिक सल्तनतें न केवल हिन्दू राजनैतिक और सैन्य सहयोगियों पर विश्वास करतीं थीं वरन् वे भारतीय रिवाजों को अपनाने अथवा देशी परम्पराओं को छूटें देने में ज्यादा उदारवादी थीं। उदाहरण के लिए, न केवल गुजरात के मुसलमान कुलीन परिवारों ने एवं कुछ अन्य सल्तनतों ने हिन्दू कुलीन परिवारों से समानता एवं आदर का व्यवहार किया वरन् मुस्लिम राजकुमारियों का ब्याह हिन्दू सहयोगी परिवारों में उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से हिन्दू राजकुमारियाँ मुस्लिम राजसी घरानों में आईं थीं। यह मुगलों के रिवाजों के विपरीत था। मुगलों ने हिन्दू राजकुमारियाँ वधु की तरह स्वीकार तो कीं परन्तु अपनी राजकुमारियों की शादी हिन्दू परिवारों में नहीं की। मुगलों ने राजपूत भागीदारी को निम्न स्तरीय ढंग से स्वीकारा था जबकि प्रादेशिक सल्तनतों ने संभवतया, अपने हिन्दू सहयोगियों को समान स्तर पर व्यवहार दिया।
हिन्दू और मुसलमान कुलीनों के आपसी सम्बन्धों को शादी ब्याह के द्वारा पक्का किया गया। आम जनता के स्तर पर, भक्ति और सूफी रहस्यमय समानतावादी पंथों के द्वारा एक दूसरे के प्रति अभिमुखता पैदा हुई। दोनों ने मिलकर सामाजिक जाति विभाजन और धार्मिक कठोरता के प्रति अवज्ञा पैदा की। सामाजिक शांति और स्थायित्व को बनाये रखने के लिए प्रादेशिक सल्तनतों ने कुरान की निरंकुशता पर सूफिया लचीलेपन को पालापोसा और दिल्ली के विपरीत, अनेक प्रादेशिक सल्तनतों ने स्थानीय भाषा का समर्थन किया। मातृभाषा के साहित्य को सक्रियता से प्रोत्साहित किया।
साथ ही साथ, पारम्परिकक कलाओं एवं हस्तकौशल को बढ़ावा दिया। बंगाल, गुजरात और कश्मीर में उर्दू की अपेक्षा मातृभाषा में काव्य और साहित्य की रचना शुरू हुई तथा खानदेश, बुरहानपुर एवं अहमदनगर में संस्कृत एवं मराठी साहित्य को उर्दू साहित्य के साथ अनुग्रह मिला। पारम्परिकक पौराणिक विषयों को जौनपुर के लघुचित्रों में जगह मिली और गीत गोविंद के चित्रण तो जौनपुर दरबार में विशेष आकर्षण रखते थे।
दक्खिन के दरबार विभिन्न भारतीय मूल के मुस्लिमों एवं विदेशी मूल के राजवंशों की आपसी दुश्मनी से विदीर्ण हो गये थे। उन्होंने हिन्दुओं से सम्बन्ध सुधारने की कोशिश की। नतीजतन, हिन्दुओं को इस्लामी शासन में सर्वोच्च पदों पर पहुंचने की अनुमति प्राप्त हुई। खासकर, ये राजदरबार देशज हिन्दू कलात्मक प्रभावों के लिए खुल गए थे और सबसे सुंदर लघुचित्रों में विभिन्न भारतीय रागों की व्याख्यायें हुईं। फिर चाहे वे अहमदनगर, औरंगाबाद, बीजापुर या हैदराबाद में क्यों न उत्पन्न हुईं हों। ये लघुचित्रा पूना के मराठा राजदरबारों के और कोल्हापुर और सांवतवाड़ी के लघुचित्रों से बहुत समानतायें रखते हैं। 
इस प्रकार से इन राजदरबारों ने एक विशेष भारतीय-मुस्लिम संस्कृति को विकसित किया जिसने उन्हें उत्तर पश्चिम के विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित संस्कृति से भिन्न पहिचान दी। इन दरबारों ने इस्लाम में परिवर्तित भारतीयों के समग्र चरित्र को प्रतिबिंबित किया, उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती परम्पराओं से अनेक तत्वों को बचा रखा था – सामाजिक रीतिरिवाज, भाषा, साहित्य, संगीत, कला और वास्तुशिल्प से।
इन सल्तनतों में से सबसे समृद्ध गुजरात सल्तनत थी। पहले अहमदाबाद में स्थापित और बाद में चंपानेर में। वहाँ पहले से ही औद्योगीकरण पूर्व के उन्नत उत्पादों का आधार था और 13 वीं शताब्दी तक, विस्तार में फैले हुए बंदरगाहों एवं वाणिज्यक शहरों का जाल था। अहमदशाह 1, 1410-42 के शासनकाल में और बहादुरशाह, 1526-37 तक के अन्य सुलतानों के शासनकाल में ये उन्नत और विकसित होते रहे थे। 18 वीं सदी के “मिराते ए अहमदी” ने देखा कि “तजकिरात उल मुल्क” का लेखक बतलाता है कि “अहमदाबाद के उपनगर उस्मानपुर में लगभग 1000 दुकानें हैं और सभी में हिन्दू और मुस्लिम व्यापारी, दस्तकार, कलाकार, सरकारी मुलाजिम और सैनिक लोग थे।” अन्य यात्रियों ने भी अहमदाबाद के शहर के खुशनुमा विवरण छोड़े हैं कि किस प्रकार से बगीचों और कृत्रिम तालाबों के बीच अनेक महल और रिहायसी प्रतिवास चौड़ी सड़कों एवं बाजारों से युक्त हैं।
गुजरात के शहर वस्त्र उद्योग और अन्य वस्तुओं के निर्माण के न केवल महत्वपूर्ण केंद्र थे वरन् गुजरात के बंदरगाह अन्य वस्तुओं के साथ मसालों एवं इमारती लकड़ी के व्यापार में उन्नत थे, जिन्हें आगे दक्षिण पूर्व एशिया एवं मलाबार तट के बंदरगाहों को और पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा यूरोप को भेजा जाता था। देश के भीतरी भागों के उत्पाद भी गुजरात के बंदरगाहों से बाहर भेजे जाते थे। 15 वीं और 16 वीं सदी में दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में गुजरात के शहरों की गणना होने लगी और सल्तनत के शासकों ने अपनी राजधानियों को सर्वोत्कृष्ट भारतीय वास्तुशिल्पों से सजाया था।

पहले की दोनों राजधानियाँ अहमदाबाद और चंपानेर आकर्षक स्मारक समूहों के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ मायने में ये स्मारक मुगलों से भी आगे थे। हिन्दू और जैन स्थापत्यशिल्प से लिए त्रियामी अलंकृत और विस्मयकारी स्मारक अपने में परम्परागत शुभ संकेतों को संजोये हैं। जैन चिन्हों में “ज्ञान द्वीप”, “कल्पलता” और “कल्पवृक्ष” क्रमशः इच्छापूर्ति, प्रगति एवं समृद्धि के सूचक हैं। अहमदाबाद की सबसे कलात्मक मस्जिदें वे हैं जिन्हें अहमदाबाद के मुस्लिम शासकों की हिन्दू रानियों ने बनवाया था। रानी सिप्री और रानी रूपमति को इसका श्रेय प्राप्त है।
बंगाल दूसरा राज्य था जहाँ सल्तनतों के स्मारकों ने देशज रीति-रिवाजों से प्रचुर मात्रा में उधार लिया था। खासकर यह उधार हिन्दू और बौद्ध से है। 14 वीं सदी में पंडुआ की राजधानी में एवं वारंगल की राजधानी काकतिया में क्रियाशील रहे कलाकारों को नौकरियाँ मिलीं और साथ में पाल और सेना शासकों की सेवा में रहे बुर्जुग कलाकारों की नयी पीढ़ियों को भी काम मिला। इस प्रकार से गुजरात के समान, बंगाल के हिन्दू और बौद्ध रीति-रिवाजों के अनेक चिन्हों को पंडुआ और गौर राजदरबारों के महलों इत्यादि और धार्मिक स्थापत्यशिल्प में समाहित किया गया।
ऐसा कुछ हद तक बिना किसी पूर्व निर्णय के भी होता रहा है क्योंकि अनेक मस्जिदें पहले से बने मठों अथवा मंदिर परिसरों के उपर बनाईं गयी थीं। तब भी, बंगाल की सल्तनत ने मध्य एशिया या परशियन धाराओं से बिना प्रभावित हुए अपने वास्तु सिद्धांतों को बंगाल के रीतिरिवाजों में से अनेक बातों को स्वीकारते और उनका नवीनीकरण करते हुए, गढ़ा था। बंगाल के मुस्लिम रहस्यवादी कवि और गीतकारों ने भी भक्तिधारा के सहपक्षी के सदृश्य ही लोक परम्पराओं में से बहुत कुछ अपने में आत्मसात् किया।
उत्तरी दक्खिन में मुस्लिम किसानों ने कन्नड़ बोलना जारी रखा और ईद और दूसरे मुस्लिम त्यौहार सूफीयों द्वारा मान्य पारम्परिकक गानों एवं उच्चकोटि के लोकनृत्यों के साथ अवसर के अनुसार मनाते रहे। अनेक मौकों पर हिन्दू और मुसलमानों के त्यौहार दोनों समुदाय मिलजुल कर मनाते थे।
इस प्रकार से मुगलों के हाथों पराजित होने के पहले प्रादेशिक सल्तनतें आम तौर पर दिल्ली सल्तनत के आधीन अनुभूत विनाशकारी अतिक्रमण और अभिघात से बचने की कोशिश करतीं थीं और भारतीय राज्यों के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन में ज्यादा उपयोगी योगदान देतीं थीं। व्यापार एवं वाणिज्य शहरों और बंदरगाहों में उन्नत हुआ था। अस्तु इन सल्तनतों द्वारा ललित कलाओं और वास्तुशिल्प के निर्माण को भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के महत्वपूर्ण अंग की तरह से देखा जाना चाहिए और उन्हें भारत के कलात्मक उत्पाद का सर्वोत्तम दर्जा देना चाहिए।