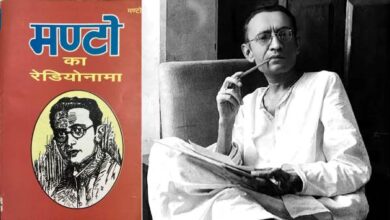23 मार्च 2019 को, प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा चुनावों से ऐन पहले लोहिया जयंती के अवसर पर लोहिया को याद करते हुए एक ब्लॉग लिखा जिसमें कहा गया था कि ‘डॉ. राममनोहर लोहिया यदि जीवित होते तो उन्हें भाजपा की सरकार और नरेन्द्र मोदी पर गर्व होता’। कई समाजवादियों या कहें तो लोहियावादियों ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के इस बयान का काफी बुरा माना। इसके जवाब में राजेंद्र राजन ने 2 मई 2019 को एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था ‘मोदी, लोहिया को चुनावी मौसम में क्यों भुनाना चाहते हैं? वे लिखते हैं: ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने लिखा कि अगर डॉक्टर राममनोहर लोहिया जीवित होते, तो उनकी सरकार पर गर्व करते। मोदी और उनकी पार्टी, लोहिया की राजनीति और विचारधारा के वारिस नहीं हैं। इसलिए मोदी ने जो कहा है वह एक असामान्य या विचित्र दावा ही कहा जाएगा। सवाल यह है कि आखिर लोहिया को अपने पाले में दिखाने की जरूरत मोदी को इस वक्त क्यों महसूस हुई, जब आम चुनाव सिर पर था। क्या इसका चुनाव से कोई वास्ता हो सकता है?
इससे पहले सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक डॉ. प्रेम सिंह ने इसी विषय पर लिखे अपने लेख ‘और अंत में लोहिया! पर विमर्श’ में प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए लिखा, “इस बार लोहिया जयंती के अवसर पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने ब्लॉग पर लोहिया को याद किया जिस पर मेरे एक मित्र ने ध्यान दिलाया और कहा कि मुझे इसका जवाब लिखना चाहिए। लोहिया के बारे में या बचाव में मोदी या आरएसएस के संदर्भ में कुछ भी कहने का औचित्य नहीं है। मित्र ने हामी भरी लेकिन मोदी का खण्डन करने की बात पर अड़े रहे। हार कर मैंने उनसे कहा कि लोहिया के अपहरण के लिए मोदी और आरएसएस को दोष देने का ज्यादा औचित्य नहीं है।
बहरहाल, सुबह अखबार देखा तो मोदी के ब्लॉग पर लोहिया के बारे में लिखी गई टिप्पणी पर अच्छी-खासी खबर पढ़ने को मिली। पता चला कि मोदी ने लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र अंत में लोहिया को हथियार बना कर विपक्ष पर प्रहार किया है। पूरी टिप्पणी में बड़बोलापन और खोखलापन भरा हुआ था । एक स्वतंत्रता सेनानी और गरीबों के हक़ में समानता का संघर्ष चलाने वाले दिवंगत व्यक्ति का उनकी जयंती के अवसर पर चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल अफसोस की बात है। तब और भी ज्यादा जब ऐसा करने वाला शख्स देश का प्रधानमन्त्री हो! जैसा कि मैंने कहा है, लोहिया की विचारधारा, सिद्धांतों, नीतियों पर मोदी के ब्लॉग के संदर्भ में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल उनके गैर-काँग्रेसवाद, जो मोदी के मुताबिक उनके मन-आत्मा में बसा हुआ था, पर थोड़ी बात करते हैं. यह पूरी तरह गलत है कि लोहिया के ‘मन और आत्मा’ में काँग्रेस-विरोध बसा था। मोदी ने नॉन-काँग्रेसिज्म को अपने ब्लॉग में एंटी-काँग्रेसिज्म कर दिया है”।
कोलकाता के एक प्रतिष्ठित समाजवादी परिवार से जुडी सामाजिक कार्यकर्त्ता रुचिरा गुप्ता ने भी इस विषय पर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था “प्रधानमन्त्री श्री मोदी, राममनोहर लोहिया बीजेपी सरकार पर फ़ख़्र नहीं करते क्यूंकि वह फ़ासीवादी विरोधी थे” शायद प्रधानमन्त्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि लोहिया उग्र रूप से फासीवादी विरोधी, साम्राज्यवाद-विरोधी और अधिनायकवाद के विरोधी थे, और उन्होंने हमेशा इन वादों को खारिज किया।
हमारे समाजवादी मित्रों को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से ये शिकायत है की उन्होंने उनके नेता राममनोहर लोहिया के बारे में अपने ये उदगार क्यूँ व्यक्त किये? और चूँकि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉ. लोहिया की राजनीति और विचारधारा के वारिस नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमन्त्री मोदी का यह दावा असामान्य या विचित्र मालूम होता है। वे सवाल करते हैं कि ‘आखिर (उन्हें) लोहिया को अपने पाले में दिखाने की जरूरत इस वक्त क्यों महसूस हुई? और इसका जवाब देते हुए ये लोग खुद ही कहते हैं की “क्यूंकि वे लोग (मोदी और उनकी पार्टी), लोहिया की राजनीति और विचारधारा के वारिस नहीं हैं इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते”।
मेरी राय में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि देते हुए जो श्रेय लेने की कोशिश की थी और कहा था कि यदि वे जीवित होते तो उनकी सरकार पर गर्व करते, उसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। दरअसल नरेन्द्र मोदी ने ऐसा क्यूँ कहा उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं और उनपर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। 50 और 60 के दशक में डॉ. राममनोहर लोहिया पर अक्सर यह आरोप लगे कि उन्होने पंडित नेहरु और काँग्रेस पार्टी के अन्ध विरोध में हिन्दू साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ सांठ-गाँठ की और गैर-काँग्रेसवाद के नाम पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जिससे जनसंघ और बाद में उसकी परवर्ती बीजेपी मजबूत हुई और 1967 तथा 1977 में जनसंघ के लोगों ने ही गैर काँग्रेसवाद के नाम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और अपना राजनीतिक आधार मज़बूत किया। दरअसल इन कारणों पर विस्तार से चर्चा किये जाने की ज़रूरत है।
यह भी पढ़ें – राम मनोहर लोहिया का भाषा चिन्तन
1934 से लेकर 1947 तक की यदि डॉ. राममनोहर लोहिया की राजनीति और उनके विचारों और सिद्धांतों पर गौर करें तो वे काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ज़िम्मेदार नेता होने के साथ साथ काँग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता भी थे। काँग्रेस की विदेश नीति बनाने के साथ साथ साम्प्रदायिकता के सवाल पर उन्होने काँग्रेस पार्टी की रीति-नीति और सिद्धांत को भी बहुत मुखर रूप से पेश किया और राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सदभाव को राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख स्तम्भ बताया। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की पुरजोर मुखालिफत करते हुए डॉ. लोहिया ने मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे मुस्लिम काँग्रेसी नेताओं का समर्थन किया और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन को मजबूत किया। सही मायनों में वह एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता थे और 1947 में भारत विभाजन के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कई बार उन्होने अपनी जान जोखिम में डालकर मुसलमानों की जान बचायी। लेकिन 1947 में सोशलिस्ट पार्टी के कानपुर सम्मेलन के बाद जिसकी अध्यक्षता स्वयं डॉ. लोहिया ने की थी और जिस सम्मेलन के बाद समाजवादियों ने काँग्रेस से अलग होने का फैसला किया, सरहदी गाँधी, खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को छोड़कर लगभग सभी तत्कालीन काँग्रेसी नेताओं के बारे में डॉ. लोहिया की राय बदलने लगी।
जून 1947 में काँग्रेस कार्यसमिति की उस बैठक के बाद जिसमें देश के विभाजन को स्वीकार किया गया और जिसमें जयप्रकाश नारायण और लोहिया भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, काँग्रेस पार्टी के बारे में डॉ. लोहिया की राय बिलकुल बदल गई। देश विभाजन और आजादी के 7-8 माह बाद समाजवादियों ने काँग्रेस पार्टी छोड़ दी और डॉ. लोहिया काँग्रेस पार्टी और सरकार के विरोध में अब खुलकर आ गये। 1952 के आम चुनाव के दौरान डॉ. लोहिया अपने पूर्व नेता जवाहरलाल नेहरू और काँग्रेस पार्टी से इतने बदजन हो गये कि फूलपुर में वह पंडित नेहरू के विरोध में खड़े हिन्दू महासभा के लोकसभा उम्मीदवार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तक का समर्थन करने लगे।
1956 में ‘गिल्टी मैन ऑफ़ इंडियाज़ पार्टीशन’ या ‘भारत विभाजन के गुनहगार’ पुस्तक लिखते हुए जो मूलत: मौलाना अबुल कलम आज़ाद की पुस्तक ‘इंडिया विंस फ़्रीडम’ की समीक्षा है, डॉ. लोहिया ने मौलाना आज़ाद के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए हैं और कई जगह उन्हें झूठा तक करार दिया है। विभाजन के सात कारण गिनाते हुए डॉ. लोहिया ने उनमें से 6 को बरतानवी-अंग्रेजी चाल, और काँग्रेसी नेताओं तथा हिन्दू साम्प्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया है और विभाजन का केवल एक कारण मुस्लिम लीग की राजनीति को बताया है।
हालाँकि 1950 में एक भाषण देते हुए जो बाद मैं ‘हिन्दू बनाम हिन्दू’ के रूप में प्रकाशित हुआ डाक्टर लोहिया कहते हैं की “भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिन्दू धर्म में उदारवाद और कट्टरता की लड़ाई है और उसका अंत अभी दिखाई नहीं पड़ता”. इसी भाषण में वह आगे कहते हैं की “हिन्दू धर्म में कट्टरपंथी जोश बढने पर हमेशा देश सामाजिक और राजनैतिक द्रष्टि से टूटा है और भारतीय राष्ट्र में, राज्य और समुदाय के रूप में बिखराव आया है। मैं नहीं कह सकता की ऐसे सभी काल जिनमें देश टूटकर छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया, कट्टरपंथी प्रभुता के काल थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं की देश में एकता तभी आई जब हिन्दू दिमाग पर उदार विचारों का प्रभाव था”. वह आगे कहते हैं कि “महात्मा गाँधी की हत्या, हिन्दू-मुस्लिम झगडे कि घटना उतनी नहीं थी जितनी हिन्दू धर्म की उदार कट्टरपंथी धाराओँ के युद्ध की। इसके पहले कभी किसी हिन्दू ने वर्ण, स्त्री, संपत्ति और सहिष्णुता के बारे में कट्टरता पर उतनी गहरी चोट नहीं की थी”.
1962 में तीसरे आम चुनाव और भारत पर चीन के हमले के बाद डॉ. लोहिया पंडित नेहरू और उनकी काँग्रेसी सरकार से इस क़दर बदज़न हो गये कि नेहरू सरकार को राष्ट्रीय शर्म की सरकार कहने लगे और काँग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए वह ‘शैतान से भी हाथ मिलाने’ को तैयार हो गये। 1963 में उत्तरप्रदेश में हुए तीन उप चुनावों अमरोहा, जौनपुर और फ़र्रुख़ाबाद में तो डॉ. लोहिया ने न केवल जनसंघ का समर्थन लिया बल्कि जौनपुर में तो जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय के समर्थन में चुनाव सभाओँ को सम्बोधित भी किया। बदले में दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख ने फ़र्रुख़ाबाद में डॉ. लोहिया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और यहीं से जनसंघ का समर्थन लेने और देने की उनकी राजनीति की शुरूआत होती है जिसे ग़ैर-काँग्रेसवाद का नाम दिया गया।
इसी वर्ष कलकत्ते में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. लोहिया ने ‘काँग्रेस हटाओ देश बचाओ’ और गैर-काँग्रेसवाद का नारा दिया। उन्होने सभी विपक्षी दलों जैसे जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों से ऐसी रणनीति बनाने का आहवान किया ताकि आगामी चुनाव में काँग्रेस विरोधी मत बंटने न पावें और काँग्रेस हार जाए। कलकत्ता के इसी सम्मेलन में उनके दो प्रमुख शिष्यों मधुलिमए और जार्ज फ़र्नांडीज़ ने डॉ. लोहिया की पुरजोर मुख़ालिफ़त की। मधुलिमए तो विरोध स्वरूप सम्मेलन में शामिल तक नहीं हुए लेकिन उन्होंने जार्ज फ़र्नांडीज़ के जरिए कहलवाया कि गैर-काँग्रेसवाद के नाम पर साम्प्रदायिक शक्तियों का सहयोग लेने से ‘डॉ. लोहिया का मुंह काला हो जाएगा’।
1964 में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का विलय होकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (संसोपा) का गठन होने और छ: माह बाद ही पुन: प्रसोपा का पुनर्जन्म होने के पीछे डॉ. लोहिया की जनसंघ के साथ सहयोग की नीति भी एक कारण थी।
यह भी पढ़ें – पिछड़ी जाति की जमींदारी व सोशलिस्ट धारा
डॉ. लोहिया ने 1967 के आम चुनावों तक इस नीति को ज़ोरदार ढंग से चलाया। 1967 के आम चुनावों में वामपंथी दलों के अलावा किसी अन्य दल से तो संसोपा का चुनावी गठबंधन या तालमेल नहीं हो पाया लेकिन इन चुनावों के फ़ौरन बाद जब 9 राज्यों में गैर काँग्रेसी सरकार बनीं तो उनमें जनसंघ के साथ दोनों सोशलिस्ट पार्टियाँ, स्वतंत्र पार्टी और वामपंथी दल शामिल हुए। खासकर उ.प्र., बिहार और म.प्र. में संसोपा के लोग जनसंघ के लोगों के साथ मन्त्रीमंडल में शरीक हुए। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में यह मन्त्रीमंडल एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बने थे लेकिन बहुत सारे ऐसे नीतिगत और सिद्धांत के मसले थे जिस पर संसोपा ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाये जाने और उत्तर प्रदेश में कालागढ़ में मजदूरों पर गोली चलाये जाने की घटना जिसपर संसोपा ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमले के बाद डाक्टर लोहिया ने जनसंघ के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें भारत द्वारा परमाणु बम बनाये जाने कि बात कही गयी थी। 12 अप्रैल 1964 को डाक्टर लोहिया और जनसंघ के नेता दीन दयाल उपाध्याय ने भारत-पाक महासंघ बनाये जाने को लेकर एक साझा बयान जारी किया। इसी बयान में कहा गया कि “हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हुए दंगों के बाद दो लाख से भी ज्यादा हिन्दू और दूसरे अल्पसंख्यक भारत आने पर मजबूर हुए हैं। पूर्वी बंगाल में हुई घटनाओं से भारतीयों का क्रुद्ध होना स्वाभाविक है। हमारा यह निश्चित मत है कि पाकिस्तान में हिन्दुओ और अन्य अल्पसंख्यकोँ के जीवन और संपत्ति कि सुरक्षा कि गारंटी की ज़िम्मेदारी भारत सरकार कि है और उसे इस सम्बन्ध में सभी ज़रूरी और कानूनी क़दम उठाने चाहिए”.
यही वह दौर था जब डॉ. लोहिया ने आर एस एस और जनसंघ के शिविरों में जाना शुरू किया और उन्हें देशभक्ति के ‘सर्टिफिकेट’ दिए और भाषा के सवाल पर खास कर हिन्दी के समर्थन के सवाल पर तो उनकी जमकर तारीफ की (देखें विवेकशक्ति मासिक पत्रिका अंक, मार्च 2018 में कानपूर के वरिष्ठ समाजवादी एन के नायर का लेख)। दाड़ी-चोटी के सवाल पर और बीएचयू तथा एएमयू यानि बनारस विश्वविद्यालय से हिन्दू और अलीगढ विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटाये जाने की उनकी मांग को उनके विरोधियों ने साम्प्रदायिक क़रार दिया।
1960 के दशक मैं अरब-इजराइल युद्ध के दौरान भी डाक्टर लोहिया का नजरिया जनसंघ के ही ज्यादा नज़दीक था। जनसंघ इस मुद्दे पर पूरी तरह इजराइल के साथ था और सरकार पर भी इजराइल का पक्ष लेने के लिए दबाव बना रहा था जबकि काँग्रेस पार्टी की नीति राष्ट्रीय आन्दोलन के समय से फलस्तीन का समर्थन करने की रही थी। इस विषय पर डॉ. लोहिया अपने अज़ीज़ दोस्त सिब्ते नकवी की शंकाओं का भी निवारण करने में विफल रहे (लोकसभा में लोहिया खण्ड 15 प्रष्ठ 232-242 में विस्तृत पत्राचार का अवलोकन करें).
1967 के आम चुनावों के दौरान डॉ. लोहिया पर यह भी आरोप लगा गया कि वह मुसलमान विरोधी हैं और इसीलिए वह जनसंघ का साथ दे रहे हैं और यह कि अगर संसोपा की सरकार बनी तो वह कुरान पर पाबंदी लगा देगी और बल पूर्वक मुस्लिम पर्सनल ला को खत्म कर देगी। चुनावों के दौरान ही आल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मशावरत के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व सोशलिस्ट नेता डॉ. ऐ जे फरीदी ने डॉ. लोहिया को एक पत्र लिखा और कहा कि वह तो संसोपा के उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मुस्लिम पर्सनल ला के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए डॉ. लोहिया ने सारनाथ से 25 जनवरी 1967 को डाक्टर फरीदी को एक पत्र लिखा
“प्रिय डाक्टर फरीदी,
आपका ख़त मिला.यह बात सही है की मैने एक ही सिविल जाब्ते की बात कही है और मुसलमानों के निजी कानून को जैसे हिन्दुओं या दीगर लोगों के बदलने की बात कही है। यह ग़लत है की मैने बल के इस्तेमाल की बात कही है। जनराज अथवा जम्हूरियत का मतलब है लोक की रजामंदी। जम्हूरियत में कानून लोक की रजामंदी से बनता-बदलता है। ज़ाहिर है की इसमें मुसलमानों की रजामंदी भी शामिल है। यह सवाल ही नहीं उठता कि मेरे जैसा जनराज का हिमायती मनमानी या ज़बर का इस्तेमाल करेगा। जो कानून बनाएगा वह लोक कि रजामंदी से ही बनाएगा…….. ।
आपका
राममनोहर लोहिया
(लोकसभा में लोहिया भाग-13 प्रष्ठ 350-352)
1967 में ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में काँग्रेस पार्टी के उमीदवार डाक्टर जाकिर हुसैन थे। विपक्षी दलों ने जिनमें डाक्टर लोहिया भी शामिल थे जाकिर हुसैन के मुकाबले सुब्बाराव को अपना उमीदवार घोषित किया और उनका समर्थन किया। जबकि राजनीति से अवकाश ले चुके और उस समय के सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने जाकिर हुसैन का समर्थन किया था।
पर साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है की जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री अब्दुल ग़फ़ूर के तथाकथित भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो आन्दोलन शुरू किया जो ‘बिहार आन्दोलन’ या ‘जेपी आन्दोलन के नाम से भी जाना गया और जिस पर आरएसएस और संघ परिवार की कड़ी पकड़ थी। उस आन्दोलन के दौरान जेपी ने बड़े फ़क़्र से कहा था “आरएसएस को फ़ासिस्ट और साम्प्रदायिक बताया जा रहा है। अगर आरएसएस फ़ासिस्ट और साम्प्रदायिक है तो मैं भी फ़ासिस्ट और साम्प्रदायिक हूं”.
इन सब बातों को लिखने का मक़सद ये है की समाजवादियों को हमेशा गर्व से अपने नेताओं को सिर्फ महिमामंडित करने का काम ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्होंने जो ग़लतियाँ या ‘पाप’ किये हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए और उसका प्रतिवाद करना चाहिए और सिर्फ़ अपने विरोधियों पर यह आरोप लगाकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए की वो समाजवादी नेताओं को उद्धृत करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसी क्रम में ये भी याद रखना चाहिए की वामपंथियों और समाजवादियों ने संविधान सभा के गठन का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उसका बहिष्कार भी किया था और जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक कहा था की ‘क्यूंकि ये संविधान सभा “एडल्ट फ्रैंचाइज़” यानि बालिग़ मताधिकार से चुनी गयी संविधान सभा नहीं है इसलिए इसके द्वारा तैयार संविधान वैध नहीं है’। मज़ेदार बात ये है की जिस संविधान का समाजवादियों और वामपंथियों ने जमकर विरोध किया था और जिसे ग़ुलामी का दस्तावेज़ बताया था, ठीक दो वर्ष बाद उसी संविधान की शपथ लेकर आम चुनावों में हिस्सा लिया। इन चुनावों में अपेक्षा अनुसार नतीजे न मिलने पर जयप्रकाश नारायण तो संसदीय और दलगत राजनीति से ही अलग हो गये और 22 वर्ष बाद उस समय संसदीय और दलगत राजनीति में वापस आये जब उनके आजके ‘मानस पुत्रों’ ने उन्हें अपने कन्धों पर उठा लिया था। उस समय यानि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती इंदिरा गाँधी और उनकी काँग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए न केवल आरएसएस को देशभक्त बताया था बल्कि सेना और अर्ध सैनिक बालों से बग़ावत तक करने की अपील कर डाली थी। जिसके कारण जून 1975 में देश में आपातकाल लगाना पड़ा।
यह भी पढ़ें – कम्युनिस्टों और समाजवादियों की भारी भूलें
डॉ. प्रेम सिंह सरीखे लोग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने ब्लॉग में लोहिया की ‘नॉन-काँग्रेसिज्म’ की राजनीति को ‘एंटी-काँग्रेसिज्म’ कहने पर अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन जिन बैसाखियों के दम पर मोदी और उनके संघ परिवार ने देश की सत्ता पर क़ब्ज़ा किया उन्हें कब तक दोष मुक्त करते रहेंगे? और यह विधवा विलाप भी कब तक कि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी और उनका परिवार उनके नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी विरासत पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं?
वक़्त का तक़ाज़ा है की जिन समाजवादी नेताओं ने अन्ध काँग्रेसवाद और नेहरू-गाँधी परिवार के विरोध के नाम पर जिन सपोलों को दूध पिलाने का काम किया और जिन्हें “राष्ट्र्वाद” के सर्टिफ़िकेट दिए उस पर थोड़ा ‘आत्ममंथन’ और ‘आत्मचिंतन’ होना चाहिए। क्या व्यक्तिगत विरोध के नाम पर हम अपने देश के वजूद उसके संविधान से उसकी एकता से और उसकी सैंकड़ो साल पूरानी सभ्यता के वुजूद से भी समझौता कर लेंगे? आज संघ परिवार और उसके कारिंदे देश की सत्ता पर क़ाबिज़ हैं तो इसकी कुछ ज़िम्मेदारी उन समाजवादियों पर भी आती है जिन्होंने उनकी राजनितिक छुआछूत ख़त्म करके 1967, 1977 और 1989 में उन्हें सत्ता में भागेदारी और बाद में ‘क्रेडिबिलिटि’ दी और 1992 में बाबरी मस्जिद ढाये जाने के बाद जॉर्ज फर्नांडीज़, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान सरीखे तथाकथित समाजवादियों ने आरएसएस के सामने नतमस्तक होकर उन्हें लोहिया और जेपी की विरासत और उनके नाम का इस्तेमाल करने का मौक़ा दिया।
.