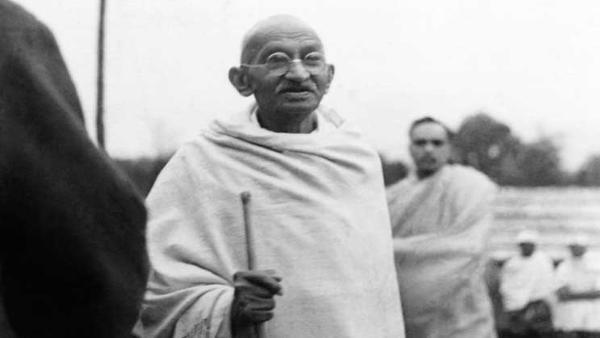तमाम अफ्रिकी, निग्रो, काले लोगों के दड़बेनुमा घरों के पास उन्हीं के बीच उन्हीं के जैसे एक काले, अफ्रिकी, निग्रो व्यक्ति को एक गोरा अमरीकी पोल से बाँधकर एक ऐसे कोड़े से पीट रहा है जिसके दूसरे सिरे पर घातु की मोटी से नुकीली होती कई कीलें बँधी हैं। उस सिरे पर जो मूठ नहीं है और जहाँ से चोट लगनी है। बाकी सभी काले यह सब डरे-सहमे देख रहे हैं और पहले से और अधिक डर रहे रहै हैं। उस काले निग्रो की पीठ पर जो गहरे ज़ख़्म बन रहे हैं उसके दर्द सिसकियाँ बन कर उसके चारों ओर खड़े सभी अफ्रिकी निग्रो काले लोगों की ज़ुबान से बाहर आ रहें हैं। यह रूट्स नामक एक अमरिकी हिस्टॉरिकल ड्रामा का दृश्य है।
यह फिल्म अलेक्स हैले के मशहूर उपन्यास रूट्स : द सागा ऑफ़ एन अमेरिकन फैमिली (1976) के आधार पर एक टी.वी. मीनी सिरीज़ के रूप में बनी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अफ्रिकी, निग्रो और काले लोगों की स्लेव अर्थात् दास के रूप में धड़ल्ले से खरीद फरोख़्त होती थी। वह काला अफ्रिकी निग्रो व्यक्ति जिसे पीटा जा रहा है वह मूलतः एक दास है जिसे अफ्रिका से अपहृत कर के यहाँ अमेरिका में बेच दिया गया है। उसके मालिक ने उसका एक नया नाम टोबी रखा है।
पर वह अपने असली नाम कुन्ता किन्ते के अलावा किसी टोबी सम्बोधन पर रेस्पॉन्स नहीं करता, उसको अनसुना कर देता है। और कई बार वहाँ से भागने की कोशिश भी कर चुका है। वह गोरा व्यक्ति उसे मारते हुए बार–बार उसका नाम पूछता है और वह काला अफ्रिकी निग्रो बार-बार अपना असली नाम ही बताता है। गोरे अमरीकी का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह उसकी पीठ पर बेतहाशा कोड़े बरसाता है।
वह मारते हुए चीख़ता है- ‘तुम अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारे मालिक की बीवी ने तुम्हारे लिए चुना है। यह अफ्रिका नहीं है इसलिए तुम अपना नया नाम बताओ ताकि वह अफ्रिका का न लगे। यह वर्जिनिया है और तुम इन तमाम घोड़ों और सुअरों की तरह जॉन वालर की सम्पत्ति हो और इससे अधिक कुछ नहीं। अब तुम अपना नाम बताओ ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो?’ वह काला अफ्रिकी निग्रो फिर अपना असली नाम कुन्ता किन्ते ही बताता है। वह गोरा अमरीकी उस पर पागलों की तरह कोड़े बरसाने लगता है। कोड़े में लगे नुकीले धातु उस काले व्यक्ति की पीठ पर मोटी रेखाएँ ऐसे बनाते हैं जैसे हल किसी खेत में मिट्टी चीरते हुए निशान बना देते हैं। उन रेखाओं को भरने के लिए उसी का लहू निकल पड़ता है। उसके अपने लहू के अलावा कोई उसका साथ नहीं देता। काफी देर तक यह अमानवीय और असहनीय पीड़ा सहने के बाद वह अपना नाम टोबी बताने को मजबूर होता है। पागलों की तरह कोड़े बरसाते गोरे अमरीकी को यह सुनाई नहीं देता और वह कोड़े बरसाना जारी रखता है। दूसरों के कहने पर कि उसने अपना नाम टोबी कह दिया है, वह उसे ज़ोर से बोलने को कहता है और फिर मारता है। वह काला अफ्रिकी निग्रो ज़ोर से अपना नाम टोबी कहता है।
:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1489481-1251839046.jpeg.jpg)
यह पूरी घटना वर्चस्व की पूरी परिघटना और उसकी सम्पूर्ण संरचना को समझने में काफी मददगार है। यह घटना हमें यह बताती है कि वर्चस्ववादी ताक़तें मातहत व्यक्ति अथवा समुदाय या समूह की पहचान पर सबसे तगड़ा हमला करती हैं। अर्थात् वर्चस्ववादी ताक़तों का मूल लक्ष्य होता है मातहत व्यक्ति अथवा समुदाय या समूह की मूल पहचान को नष्ट करना। वर्चस्व की संरचना में जो तत्व शामिल होते हैं उनमें मातहत की पहचान अथवा अस्मिता का शमन ही सबसे प्रमुख तत्व होता है।
स्पष्ट है कि वर्चस्ववादी ताक़तें हमेशा हाशियाकृत समाज की पहचान को गौण से गौणतर करने की कोशिश करती रहती हैं। उनका अन्तिम ध्येय होता है, उसे पूरी तरह मिटा देना। सत्ताएँ यह राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी करने की भरपूर कोशिश करती हैं। सत्ता हमेशा यह काम दो तरीकों से करती है। एक तो वह अन्याय, ज़बर्दस्ती और हिंसा के निशान मिटा देना चाहती है। यानी वह किसी भी तरह के डॉक्युमेंटेशन को नष्ट कर देने का प्रयत्न करती है जो उसकी इस प्रवृत्ति को सुरक्षित रखती है। ताकि हाशियाकृत समाज को उनकी इस व्यापक हिंसक प्रवृत्ति का पता न चले। यह बौद्धिक तरीका है।
दूसरे, वर्चस्ववादी सत्ता किसी भी तरह की ख़िलाफ़त की आवाज़ को दबाने, दूसरे शब्दों में कहें तो सबक सिखाने का काम करती है ताकि आवाज़ फिर न उठ पाए। यानी वह हाशियाकृत समाज में डर बरकरार रखने के लिए हिंसा के नंगे खेल को उस समूह तक जानबूझकर पहुँचाती है। ये दोनों तरीके बहुत कारगर हैं। और ज़्यादातर एक साथ काम करते हैं और घातक तरीके से। तुरंत असर के लिए और डर कायम करने के लिए सत्ता हिंसा के खेल को हाशियाकृत समाज के लोगों के बीच प्रचारित करती है साथ ही साथ दूरगामी असर के लिए उस हिंसा के डॉक्युमेंटेशन को नष्ट करने का काम भी करती है। ये दोनों तरीके मिलकर डर और अज्ञान (जानकारी का अभाव) को हथियार बनाते हैं। सत्ता के ये राजनीतिक औजार ज़रूरत के मुताबिक निरन्तर पैने किए जाते हैं।
बहरहाल चूँकि वर्चस्व का सबसे मजबूत हमला अस्मिता या पहचान पर होता है इसलिए हाशिए के समाज अथवा व्यक्ति की लड़ाई का केन्द्रबिन्दु वही अस्मिता अथवा पहचान होती है। वर्चस्व की शिनाख़्त का मसला मातहत अतवा पीड़ित व्यक्ति या समुदाय के अधिकारबोध के क्रमशः घने होते जाने से जुड़ा हुआ है। अधिकारबोध का विकास अस्मिता के सवालों से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ। दरअसल अधिकारबोध दोहरी ताक़तों का केन्द्रबिन्दु है। यह एक तरफ वर्चस्व की शिनाख़्त करता है तो दूसर तरफ अस्मिताबोध का विकास करता है। अस्मिताबोध और अधिकारबोध परस्पर पूरक अवधारणाएँ हैं। अधिकारबोध से अस्मिताबोध पनपता है। अस्मिताबोध वर्चस्व की किसी भी अवधारणा से टकराने के सबसे कारगार और मजबूत औजार है। वर्चस्व से टकराने के सभी रास्ते अस्मिताबोध से होकर ही जाते हैं। रूट्स फिल्म इस बात को काफी बारीकी से हमें समझाती है।
अस्मिताबोध आज के बदले हुए समय में अस्मिता की राजनीति का रूप ले चुकी है। आज अगर हम ध्यान से देखें तो पाएँगे कि वर्चस्व के साथ अस्मिता की राजनीति घनिष्ठ रूप जुड़ी हुई है। वर्चस्व की शिनाख़्त और उसका सचेत विरोध- ये दोनों अस्मिता की राजनीति को रूप देते हैं। जहाँ भी वर्चस्व होगा वहाँ हशियाकरण होगा ही। जब जहाँ जिस समूह का वर्चस्व होगा, उसके समक्ष एक ऐसे समूह की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है जो हाशिए पर होती है।
कह सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित करने की पूरक अवधारणा है हशियाकरण की प्रक्रिया। वर्चस्व की पुरानी अवधारणा एक राज्य द्वारा दूसरे समूह अथवा राज्यों पर किए गए आधिपत्य तक सीमित थी पर एंतोनियो ग्राम्शी ने इसकी अवधारणा को एक नया आयाम दिया। ‘अब वर्चस्व का तात्पर्य प्रभुत्व की उस संरचना से है जो सहमति के आधार पर लागू की जाती है या जो प्रकट ज़ोर-ज़बर्दस्ती के बिना नफ़ीस क़िस्म के तौर-तरीक़ों (आर्थिक सत्ता, मीडिया, शिक्षा, प्रचार और लोकोपकारी नीतियाँ) का इस्तेमाल करके समाज में अपने लिए सहमति क़ायम कर लेती है।’ हमारे समाज में कई तरह का वर्चस्व है।
और इसके फलस्वरूप कई तरह का हाशियाकरण भी है। ग्राम्शी के विचारों के अनुसार यह हाशियाकरण एक तरह की सहमति के आधार पर होता है। किसी न किसी तरह लक्ष्य समूह को स्वेच्छा से प्रभुत्व स्थापित करने वाले समूह का आधिपत्य स्वीकार कर लेना पड़ता है। जब यह हाशियाकृत समूह वर्चस्व के ख़िलाफ कोई आवाज़ बुलन्द करता है और वर्चस्व को ठेस पहुँचती है, तो यह अस्मिता की राजनीति होती है। अभय कुमार दुबे ने लिखा है, ‘उदारतावादी लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वयं को हाशियाकृत समझने वाले समुदायों द्वारा अपने सबलीकरण, प्रतिनिधित्व, और मान्यता के लिए किए जाने वाले संघर्ष को अस्मिता की राजनीति की संज्ञा दी जाती है। इस राजनीति के केन्द्र में भाषा, संस्कृति, नस्ल, धर्म, जातीयता, जाति, जेंडर या सेक्शुअलिटी आधारित दावेदारियाँ होती हैं।’ इस राजनीति का कारण यह है कि अस्मिता का सवाल तभी उठता है जब हाशियाकृत समाज किसी न किसी वर्चस्व का शिकार हो, किसी न किसी वर्चस्ववादी सत्ता का उस पर अधिकार हो और अस्मिता के धूमिल हो जाने का ख़तरा उपस्थित हो जाए अथवा अस्मिता संकट ग्रस्त हो जाए। स्पष्ट है वर्चस्व, हाशियाकरण और अस्मिता के सवाल एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
हर आदमी अपनी-अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अस्मिता ही नहीं बल्कि अस्मिताओं से जुड़ा हुआ है। एक ही साथ हम बंगाली, मराठी आदि अस्मिताओं के साथ भारतीय अस्मिता से भी जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय और भाषागत अस्मिता के साथ एक राष्ट्रीय अस्मिता भी है हमारी। इसके साथ ही भारत में तमाम तरह की अस्मिताएँ हैं जो ख़तरे में हैं और जिनकी राजनीति होती है।
अस्मिताएँ हमेशा सापेक्षिक होती हैं। किसी प्रकार का वर्चस्व हाशियाकृत समूह के बिना सम्भव ही नहीं है। पुरुष वर्चस्व के सन्दर्भ में स्त्री अस्मिता, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के सन्दर्भ में दलित अस्मिता, हिंदुत्व के वर्चस्व के सन्दर्भ में धार्मिक अल्पसंख्यकों की अस्मिता (मसलन मुस्लिम अस्मिता), हिन्दी भाषा के वर्चस्व के सन्दर्भ में बांग्ला, तमिल, मराठी अस्मिता, आधुनिक विकास और मुख्यधारा के वर्चस्व के सन्दर्भ में आदिवासी और वंचितों की अस्मिता आदि। लिंग, जाति, धर्म, भाषा, और विकास आधारित वर्चस्वों के बरक्स स्त्री, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक और आदिवासी अस्मिताएँ लंबे समय से संकट में रही हैं। इन संकटों की पहचान और अपने अधिकार की लड़ाई इन्हें अस्मितामूलक आन्दोलनों से जोड़ती है। इनके सामने पहचान का संकट है और ये अपनी पहचान बचाने के प्रति सचेत हैं। अस्मिताओं के लिए संघर्ष वास्तव में किसी न किसी प्रकार के वर्चस्व के ख़िलाफ लड़ाई होती है।
स्त्री, दलित, मुस्लिम और आदिवासी दरअसल हाशियाकृत समाज हैं। वैश्वीकरण के नए दौर में इनका नए ढंग का हाशियाकरण हो रहा है। विश्व की तमाम समृद्धि एक हो रही है। अतः असमृद्ध लोगों का स्वाभाविक रूप से हाशियाकरण हो रहा है। पिछले दिनों अस्मिताओं का नव उभार देखने को मिला। यह दरअसल सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष ही है। हाशिए की सभी आवाज़ें उठीं। हमारी संस्कृति में ही यह बात है कि सभी तरह के वर्चस्व आज भी अपने नंगे रूप में मौजूद हैं। हमारी संस्कृति में इन तमाम वर्चस्वों के पोषक तत्व हैं। इसीलिए तो पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं, ‘सामाजिक न्याय का संघर्ष राजनीतिक सत्ता के संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष परम्परागत सांस्कृतिक वर्चस्व के ख़िलाफ है।’
संस्कृति में ही वर्चस्व के पोषक तत्व होते हैं। स्त्री की लैंगिक अस्मिता पुरुष वर्चस्व की शिकार है। इसके लिए बचपन से ही उसे तैयार किया जाता है। वह सिर्फ जैविक रूप से स्त्री नहीं होती बल्कि समाज और संस्कृति मिलकर उसका स्त्रीत्व गढ़ते है, कुछ इस प्रकार कि वह पुरुष वर्चस्व की पोषक बन सके। स्त्री एक जैविक निर्मिति के बजाय वास्तव में सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति है। ठीक इसी प्रकार जाति-व्यवस्था इसीलिए बनाई गयी की ब्राह्मणवादी वर्चस्व स्थापित हो सके। दलित अस्मिता इसी ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आवाज़ है। वास्तव में दलित राजनीति भी इसको तोड़ने में ठीक से सफल नहीं हो पाई है। दलित राजनीति का वर्तमान स्वरूप तो कहीं-कहीं इस वर्चस्व को चुनौती भी नहीं दे पाता, बल्कि उल्टे गाहे-बगाहे उसका पोषक बन जाता है।
यह इसलिए कि जाति-व्यवस्था पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धान्त पर आधारित है और संस्कार निर्माण की पूरी प्रक्रिया के जरिए जाति-व्यवस्था के शिकार और शिकारी, दोनों इस तर्क को आत्मसात कर लेते हैं। जाति-व्यवस्था सदियों से भारतीय सत्ता-तन्त्र को मजबूत करने का एक उपक्रम साबित हुई है। पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं, ‘असल में तो जाति-व्यवस्था भारतीय सत्ता-तन्त्र की धुरी है। एक सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता, जिसे जबर्दस्त सांस्कृतिक वर्चस्व की ताकत हासिल है। जिसे एक तरफ वर्णाश्रम और अधिकारभेद से बल प्राप्त होता है, दूसरी तरफ सामी नियतिवाद से। जिसका लाभ सिर्फ हिन्दू शासकों ने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, इसाई शासकों ने भी उठाया और धर्म-निरपेक्ष (!) शासकों ने भी।’ दलित और स्त्री की लगभग एक ही कहानी है। दोनों में ब्राह्मणवादी और पुरुषवादी वर्चस्वों को स्वीकार करने के संस्कार निर्मित किए जाते हैं। संस्कार निर्माण की यह प्रक्रिया बचपन से ही चलती है।
आदिवासियों का प्रतिरोध तथाकथित मुख्य धारा के विकास के एजेंडे के प्रति है। विकास के नाम पर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें आदिवासियों की जमीन और उनके जंगल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे रही हैं पूरा का पूरा जीवन उजाड़ कर। कल्याणकरी योजनाओं के नाम पर भी ओड़िसा, छत्तीसगढ़, बंगाल के आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। राष्ट्र-राज्य के बरक्स अब वहाँ भी आवाज़ें आ रही हैं। प्रतिरोध का स्वर उस जगह से भी आ रहा है। यह उनकी अस्मिता का संकट है। उनके प्रतिरोध के भी कई बड़े उदाहरण सामने हैं। नियमगिरि आन्दोलन वास्तव में आदिवासियों के अस्तित्व की ही लड़ाई है।
हाशिए की अस्मिताओं के इस प्रतिरोध का अपना तर्क है। इस पर विचार करते हुए अविजीत पाठक लिखते हैं, ‘अस्मिताएँ समरूप विभेद के रूप में होने के बजाय प्रायः वर्गीकृत और पदानुक्रमिक होती हैं। यह द्वंद्व (या असमान सत्ता सम्बन्ध) गहरी पीड़ा और आक्रोश पैदा करता है। और सम्भवतया ज्यों ही लोकतन्त्रीकरण की भावना बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश करती है अब तक हाशिए पर बैठे समूह जिनकी ‘निम्नतर’ पहचान होती है, प्रतिरोध करने लगते हैं और वे उस पूरी विचारधारा का विरोध करते हैं जो इन पदसोपानों को वैध ठहराती है।’ अस्मिता की राजनीति कहीं न कहीं सत्ता और वर्चस्व के खिलाफ दबे-कुचलों की आवाज है। इस राजनीति में वे सीधे सत्ता और वर्चस्व के तन्त्रों से टकराते हैं।
इसीलिए अस्मिता की राजनीति को राजनीतिक रूप से सही माना जाता है। वास्तव में अस्मिता की राजनीति समाज का लोकतन्त्रीकरण करती है। इसने हमें बहुलतावाद के प्रति जागरूक किया है और विभेदों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है। अविजीत पाठक ठीक ही कहते हैं कि चुँकि यह राजनीति वर्चस्ववादी ताकतों को चुनौती देती है इसलिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अस्मिता की राजनीति अपनी सीमाओं में यह काम करती है। जैसे कि हर विचार, आन्दोलन और प्रतिरोध की अपनी सीमा होती है, अस्मिता की राजनीति की भी अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन यह अपनी सीमाओं के बावजूद लोकतन्त्र को मजबूत बनाने की दिशा की राजनीति है।
.