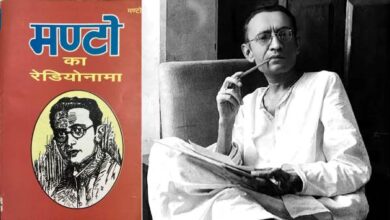पंखों को उड़ान देने वाली अर्चना दी
चंद पलों में धीमे से ऐसे दुनिया छोड़ कर चली गईं अर्चना वर्मा जी जैसे पढ़ते-पढ़ते किसी की आँख लग गई हों और पूरे के पूरे कुनबे को शोक में डुबो गईं। नारियल जैसी व्यक्तित्व वाली प्रभा दीक्षित जी झल्ला कर उलाहने दे रही हैं कि अर्चना के बेटे-बेटियों का कोई ओर-छोर भी है, किस-किस को ढाँढस दिलाती फिरूं? अर्चना जी के हर सुख-दुख की संगिनी प्रभा जी के बिना उनकी बातकतई नहीं की जा सकती। उनके विस्तृत परिवार के सदस्य तो बहुत थे किंतु जीवन का हर उतार-चढ़ाव जिसके साथ एक घर में रहते हुए अर्चना जी ने जिया वे तो उनके बच्चों की प्यारी मौसू प्रभाजी ही थीं। एक-दूसरे की पूरक थीं वे। एक-दूसरे के व्यक्तित्व को जस का तस स्वीकार करके, निहायत खूबसूरती से संगति बिठाना और एक-दूसरे के उठान में निरंतर सहयोगी बने रहना। इतनी मजबूती और इतना ठहराव तो विरले ही सम्बंधों में मिलता है। छोटे-बड़े, ऊपर-नीचे के हिसाब से काम का कोई बँटवारा नहीं।
अपने-अपने मिजाज के अनुरूप काम करते हुए अपना भरपूर विकास करते जाएँ। ऐसी परिस्थिति ही घर न दे सके तो घर का क्या फायदा। एक दिन अर्चना दी ने कहा कि कुछ रचनात्मक लिखना चाहती हूँ कहीं एकांत में जा कर। जैसे मन्नू जी लिखने के लिए कुछ दिन के लिए घर से दूर चली जाती थीं। मैंने पूछा कि आपने भी ऐसा ही घर बसाया है क्या कि कुछ सोचने या रचने के लिए दूर जाना पड़े? कुछ लम्हों के बाद उनकी उन्मुक्त हँसी सुनाई पड़ी। कहने लगीं हाँ मुझे शांति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर संकल्प के मजबूत होने के लिए भी कई बार हम कुछ एक्शन लेते हैं ताकि खुद को राजी कर सकें।वर्ना उनका घर विषम मूल्यों पर थोड़ी आधारित था कि अपने-अपने काम करने के लिए निघर होना पड़े। 
कुछ ही महीने पहले ही उनसे पहली बार मेरा आमना-सामना हुआ था जब कथादेश पत्रिका में स्त्री-प्रश्न पर कॉलम शुरू करने की इच्छा से सिनोप्सेस उन्हें भेजी थी। उसके बाद सारे लेख उन्होंने मँगवा कर पढ़े और मिलने के लिए बुलाया था। ताजा-ताजा परिचय और मेरा शुष्क स्वभाव। उनकी आवाज और उनकी आँखों में औदात्य का, प्रेम का सोता सा बहता है। उसने मेरे भीतर की मरूभूमि को इस कदर शीतल कर दिया कि साहित्यिक जगत में वह मेरी सबसे अधिक अपनी हो गईं। उनके जाने से लगा कि मेरे परिवार का ही कोई चला गया। अब किसकी आँखों में अपने पनपने की खुशी देखूँगी। किसके लिए फलने-फूलने, विकसित होने का मन अब किया करेगा। खुशकिस्मती से निजी संसार में तो अपने शुभचिंतक भरपूर हैं। पितृसत्तात्मक हथकंडों से मुक्त स्त्री के लिए सार्वजनिक परिदृश्य की यहाँ बात की जा रही है। लिखती तो सन 2007 से रही हूँ मैं। पहली बार खुले समाज में नाम की पुकार उनके ही मुँह से सुनी तो लगा अपनी खुदी की कैद से मुक्ति मिल गई। पुरुष को अपनी बात खुद नहीं करनी पड़ती। ‘क’‘ख’ की बात करता है, ‘ख’‘ग’ की, ‘ग’‘ख’ की…… और सबकी बात हो जाती है। हम स्त्रियाँ जो नागरिक की तरह जीना चाहती हैं, उनकी बात कौन करेगा?अंधेरों में डूबना ही नियति हो तो परम्परा के भीतर के अंधेरे क्या बुरे हैं?
कुल 7-8 मुलाकातें ही उनसे हुई होंगी। दो-चार बार ऐसा भी हुआ कि किसी सेमिनार से सीधे उनके घर चली गई। प्रगतिशील लोगों का कार्यक्रम- जिसमें मंच में, मेरे अगल-बगल में सब ओर प्रगतिशील लोग थे। खुद मेरी कुर्सी में भी प्रगतिशील व्यक्ति बैठी थी। वहाँ से उनके घर जाने पर लगा कि मध्य काल से आधुनिक काल में आ गई होऊँ। मैं हक्की-बक्की हो कर देखती रह जाती हूँ कि उनकी फेसबुक पोस्ट लिखने वाली और मेरे सामने बैठी मेरी प्रिय अर्चना दी क्या एक ही व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति केये दो आयाम कैसे हे सकते हैं? पिछले कुछ समय से अपनी ये दुविधा मैं उनसे फोन में कह भी रही थी। मिल कर बात करना तय हुआ था। बदकिस्मती से पिछले 2 महीने से मेरी उनसे मुलाकात हो ही नहीं पाई। पर इस वास्तविकता को रचने वाले मनोविज्ञान और परिस्थितियों को समझने की मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। इन ताने-बानों को समझना अनुकूल देश-काल को निर्मित करने के लिए जरूरी जान पड़ता है।
प्रेम की ऊष्मा से दमकता एकदम नए किस्म का घर-परिवार जिसके दरो-दीवार सबके लिए खुले थे। विषमतामूलक मानसिकता से ऊपर उठ चुकी थी उस घर की सदस्याएँ। जाति, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भाषा की कोई सलवट उनके आचरण में कहीं नहीं। उनकी प्रगाढ़ आत्मीयता और पाना-देना खून के रिश्तों तक सीमित नहीं। कोई अर्थोपार्जन कैसे करता है और अपनी सम्पदा किस पर और कैसे व्यय करता है, इससे भी उनके व्यक्तित्व की खबर मिलती है। घर जाओ तो साधनहीन बच्चों को पढ़ाते हुए मिलेंगी। उनकी घरेलू सहायिकाओं की आँखों मेंजो चमक जुबान मेंजो मिठास होती है, उन्हें डाइनिंग टेबल में बिठाकर जिस चाव से अर्चना-प्रभा जी गरम-गरम पूरी पकौड़े बना कर एक-एक करके परसते जाते हैं।उससे उस घर में उनकी जगह पता चलती है। खबर सुन कर ढाँढस बँधाने गई तो कहा कि अर्चना चली गई तो क्या मैं तो हूँ। इतनी बड़ी घटना की कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पर। दोनों ने एक-दूसरे को अपने साथ से इतना मजबूत और समृद्ध कर दिया है कि अब दिलासा हो या प्यार या कुछ और बस लुटाती ही हैं वे। उन्होंने तो देहदान कर दिया है। अर्चना जी करने वाली थीं। उससे पहले देहांत होने का उन्हें काफी दुख था। जीने का एकदम आधुनिक मुहावरा उनके घर मिलता है। आचरण का रेशा-रेशा आधुनिकता का नया कोड रचता है।
जब भी उनके घर से निकली हूँ यह सवाल मुझे मथता रहा है कि सामाजिक गतिकी अपनी स्वाभाविक लय से भी जिस विकास की ओर ले जाती है। हम प्रगतिशील लोग अपने आचरण का उतना विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्याविरोध करने में जितनी उर्जा जाती है उतनी सही के पक्ष में आगे बढ़ने में नहीं? हम क्यों अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते? जिन शब्दों से मेरे भीतर प्रगतिशील चेतना विकसित हुई और जीवन के नए बोध, नए सपने जगे। उन शब्दों पर अपना दावा करने वाले अधिसंख्य लोगों की रगों में जाति, लिंग, क्षेत्र के भेदभाव को बदस्तूर बहते देखा है।
परिवर्तन तो धीमी गति से होगा मगर आचरण और विचारों में इतनी बड़ी खाई लोगों को किस तरह प्रभावित करती होगी। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? दायित्वबोध सम्पन्न, वृहत सरोकारों की एक खुद्दार शख्सियत जो इतनी पढ़ी-लिखी थी कि किसी भी विषय पर अधिकार के साथ तार्किक ढंग से बात कर सकती थीं। विरोधी व्यक्ति के लिए कण भर भी दुर्भाव लाए बिना बौद्धिक ढंग से बहस को आगे बढाती थीं। उनका हमेशा ये निवेदन रहा कि तर्क का जवाब तर्क से दो नाम के आधार पर नहीं। प्रसिद्धि और पद का या किसी भी तरह का प्रलोभन उन्हें छू तक नहीं गया था। समझनेकी दरकार है कि मानवीय मूल्यों की धुरी पर अडिग, उदात्त, तर्कसम्पन्न विवेकशील व्यक्ति के तर्क उसे इन दिशाओं में क्यों ले जाते हैं और विरोधी तर्क अपना विवेक और सद्भाव कायम रख कर सामने वाले को अपने तर्कों से क्यों नहीं जीत पाता?
स्त्रियों के लिए इस परम्परा में है भी क्या? वह तो परिवर्तन के लिए तैयार ही बैठी रहती है बशर्ते कि प्रगतिगामी परिदृश्य के सरोकारों में समावेशिता हो। स्त्री को व्यक्ति मान कर बराबरी का स्पेस दिया जाए। हम स्त्रियाँ पूरे जोखिम उठा कर घर के बाहर आती हैं तो भी नागरिक न समझा जा कर वही आदर्श बहू, परनिर्भर कातरता ही उनमें खोजी जाए तो? अधिकांशतः सार्वजनिक महत्व के काम करने के लिए बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलता, कोई सराहना नहीं मिलती। ऐसे में बहुत सी स्त्रियाँ सामाजिक जीवन से अलगा कर अचानक अपने भीतर कैद हो जाती हैं, अवसाद में चली जाती हैं। तब कोई नहीं पूछता पर विरोधी बात करने पर विरोध जरूर होता है। कभी अवसाद या निराशा की परिणति अपने भीतर के अंधेरों में डूब कर होती है कभी बाहर के अंधेरों में।
पंख उड़ने के लिए हैं। पहली बार तो यह कोई बताता ही है। मेरे लिए वह पहली अर्चना दी ही थीं। परिवर्तन शील अग्रगामी जिंदगी जीने के लिए अपना होना जरूरी होता है। अपने फलने- फूलने को सराहने वाली नजरों की ऊष्मा चाहिए होती है। अर्चना दी के नर्म ताप ने जाने कितने व्यक्ति रच डाले। विचारधारा उनकी जो भी हो पर सही के पक्ष में खड़े होने वाली जीवंत व्यक्तित्वों की तो उन्होंने पूरी कतार खड़ी कर डाली है। ऐसी उदात्त अर्चना जी को मेरा सलाम।
.