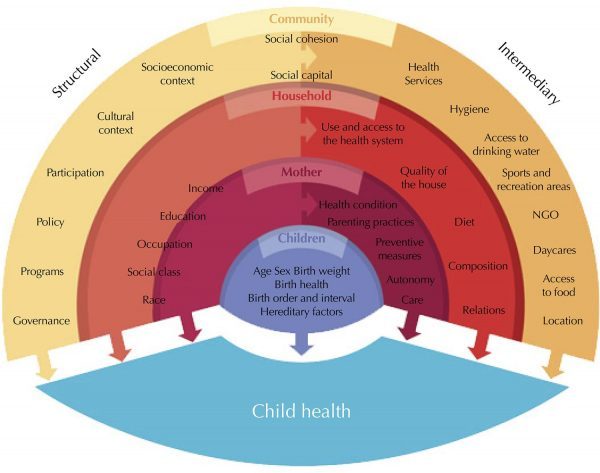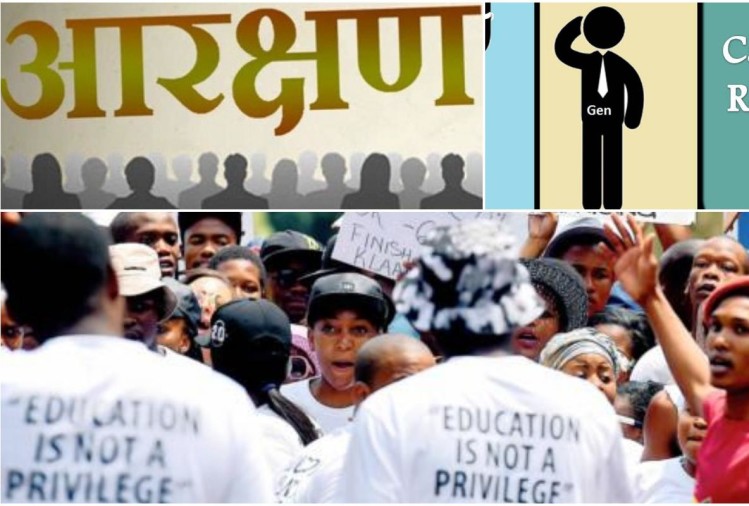वर्चस्व की अवधारणा ही बाजार का मेकानिजम है
बाजार दरअसल जरूरतों और वस्तुओं के बीच की एक जगह का नाम है। वास्तव में जरूरत की चीजों की आपूर्ति के लिए ही बाजार अस्तित्व में आया होगा। बाजार की वास्तविक धुरी लाभ नहीं; बल्कि लेन-देन, परस्पर सहयोग और जरूरत की वस्तुओं की इकट्ठे उपलब्धता की एक भावना रही होगी। लेकिन आज बाजार का स्वरूप बदल गया है, बल्कि एकदम उलट गया है। आज जरूरत की चीजों की उपलब्धता तक सिमटा नहीं है बाजार। लाभ आज बाजार के केन्द्र में है। बाजार आज नयी जरूरतों का उत्पादक बन गया है।
पुराने बाजार में एक सामाजिकता और सामूहिकता थी। लोगों के बीच संवाद थे। परस्पर काम आ पाने की चाह थी। नये बाजार ने सहकारिता के इस भाव को अपदस्थ कर दिया है। आदमी बाजार में होते हुए भी अकेला रह गया है। पुराने बाजार की सामूहिता नये बाजार के अकेलेपन में तब्दील हो गयी है। सामूहिकता अगर पुराने बाजार का मूल चरित्र था तो नये बाजार का मूल चरित्र अकेलापन हो गया है। नया बाजार किसी भी तरह के संवाद के बजाय चीजों से आक्रान्त चेतना का निर्माण करता है।
स्पष्ट है कि बाजार आज अपने सम्पूर्ण चरित्र में आक्रामक हो गया है। यह आक्रामकता भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के चलते आयी है। आज का बाजार और उसका उपभोक्तावाद दरअसल भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया की आड़ में चलने वाली नव साम्राज्यवादी नीति का हथकण्डा बन गया है। उपभोक्तावाद और बाजारवादी अर्थव्यवस्था की मिलीजुली संस्कृति के लिए हिन्दी में ‘बाजारवाद’ शब्द प्रचलित है। जो फर्क बाजार और बाजारवाद में है, वही फर्क उपभोग और उपभोक्तावाद में भी है। बाजारवाद के स्वरूप को सपष्ट करते हुए भगवान सिंह ने लिखा है, ‘बाजारवाद बाजार की तार्किक परिणति है। बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और बाजारवाद उन्हीं समस्याओं को और उग्र करता है जिनसे मुक्ति दिलाने का दावा करता है। बाजारवाद पूँजीवाद की नहीं, अपितु संकटग्रस्त पूँजीवाद या उत्तर-पूँजीवाद की सन्तान है।
बाजार उस यान जैसा है जो नियन्त्रित गति से चलता है और जिसमें क्लच, गीयर और ब्रेक सभी काम करते पाए जाते हैं; बाजारवादी वाहन में ये तीनों फेल हो जाते हैं। काम केवल एक्सीलरेटर करता है।’ बाजारवादी अर्थव्यवस्था भूमण्डलीकरण द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता संस्कृति को पुख़्ता करने का एक उपक्रम है। उपभोक्तावादी संस्कृति दरअसल बाजारवादी अर्थव्यवस्था की पूरक शक्ति है। दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है तो उपभोक्तावादी संस्कृति बदले में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं।
सामान्य जीवन के लिए जिस तरह बाजार की जरूरत होती है ठीक उसी तरह उपभोग अथवा भोग की भी जरूरत होती है। उपभोग और बाजार दोनों एक तरह से मानव जीवन की संचालक शक्तियाँ हैं। भोजन, कपड़ा, मकान, शृंगार और आनन्द आदि के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें संसार में मौजूद हैं, वे वास्तव में मानवीय उपभोग की चीजें ही हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा था, ‘कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन-आनन्द’। आनन्द की प्राप्ति के लिए कर्म से प्राप्त संसाधनों का भोग जरूरी होता है, ठीक उसी तरह भोग के लिए कर्म। भोग के बिना कर्म का महत्त्व नहीं होता। भारतीय परंपरा में उपभोग की एक सम्यक धरणा मिलती है। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति ठीक इसके विपरीत उपभोग को ही सर्वोपरी सच के रूप में स्थापित करने की कोशिश करती है। बाकी सारे मूल्य इसके सामने फीके पड़ जाते हैं।
इस तरह इसका एक परोक्ष हमला मानवीय मूल्यों पर भी पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारी जरूरत की चीजें इकट्ठे उपलब्ध हो सकें बाजार इसी का एक सामूहिक उपक्रम है, जबकि बाजारवाद अपनी शर्तों पर हमारे सामने चीजों का भंड़ार खड़ा कर देता है और प्रचार-प्रसार के विभिन्न हथकंडे अपनाकर हम पर जादुई प्रभाव पैदा करना चाहता ताकि चीजों की ख़रीद-फरोख़्त में बुद्धि का इस्तेमाल करने के बजाय हम बाजार प्रदत्त सेंसेशन से संचालित हों।
सच्चिदानंद सिन्हा का मानना है कि स्वाभाविक उपभोग की वस्तुओं के बरक्स ‘ऐसी वस्तुएँ, जो वास्तव में मनुष्य की किसी मूल जरूरत या कला और ज्ञान की वृत्तियों की दृष्टि से प्रचार के द्वारा उसके लिए जरूरी बना दी गयी हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं’।57 उपभोग का केंद्रीय तत्व ‘जरूरत’ है तो उपभोक्तावाद का केंद्रीय तत्व है ‘व्यावसायिक वृत्ति’। उपभोक्तावादी संस्कृति मनोविज्ञान के नये से नये आविष्कारों का उपयोग लोगों पर किसी गहरे नशे-सा असर बना रहे, इसके लिए करती है।
उपभोक्तावाद का संबंध मूलतः मध्य वर्ग से है। ग़रीब इससे वंचित तो नहीं हैं, असर उनपर भी है लेकिन सीमित आय और अभाव का असर भी उपभोक्तावादी संस्कृति की मार से कुछ हद तक बचाता है। वैसे इक्कीसवीं शताब्दी में इसकी चपेट मे ग़रीब भी आ ही गए हैं किसी न किसी तरह। उपभोक्तावादी संस्कृति पूँजीवादी व्यवस्था की देन है। पूँजीवादी शोषण व्यवस्था ने ही उभोक्तावादी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया है। इससे उसका अपना अस्तित्व भी जुड़ा है।
इस संबंध में सच्चिदनंद सिन्हा लिखते हैं, ‘आज उपभोक्तावाद पूँजीवादी शोषण व्यवस्था का ही परिणाम भर नहीं है बल्कि उसे जिंदा रखने का सबसे कारगर हथियार भी है।’ पूँजीवादी शोषण व्यवस्था और उपभोक्तावादी संस्कृति दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। पूँजीवाद चीजों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया पर टिका हुआ है। अतः स्वाभाविक रूप से उसे पूरी दुनिया में उपभोग की प्रवृति को एक्सीलरेट करना ही होगा वर्ना पूँजीवादी व्यवस्था ढह जाएगी अगर चीजों के बिकने की सूरत न बनी।
विश्व बाज़ार की सांस्कृतिक बर्बरता
इसलिए विश्व के पूँजीवादी उत्पादन को एक विश्व बाजार की भी जरूरत है। स्पष्ट है कि पूँजीवाद के अस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि निरंतर उत्पादन होता रहे और मुनाफा भी होता रहे। सच्चिदानंद सिन्हा ठीक ही लिखते हैं, ‘इस बात का निरंतर प्रयास होता है कि लोगों में उत्तरोत्तर उपभोगवृत्ति को तेज किया जाए जिससे ग्राहकों का अभाव न हो। इस तरह उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोग की प्रवृत्ति को निरंतर उकसाकर पूँजीवादी उत्पादन को जीवित रखती है।’
तीसरी दुनिया का मध्यवर्ग इसका लक्ष्य वर्ग है। वही इसकी चपेट में भी है। इसी का परिणाम है कि चीजों के प्रति एक दीवानगी लोगों में देखने को मिलती है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने लोगों में उपभोग की वस्तुओं को जमा करने की लत लगा दी है। इसी से पूँजीवाद फलफूल रहा है। इस प्रकार वर्तमान पूँजीवादी औद्योगिक सभ्यता उपभोक्तावादी संस्कृति का आधार है। इसने समाज के हर क्षेत्र का व्यावसायीकरण किया। इसने मनुष्य की सहज उपभोगवृत्ति को भी व्यावसायिक रंग में ढालकर अपने लिए आधार तैयार किया।
कहा जाता है- आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति के संदर्भ में इसे नये ढँग से परखने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और चीज़ो की भीड़ की खपत के लिए लोगों की जरूरत में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत थी। पूँजीवादी सभ्यता ने इसी के मद्देनजर तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर इस नयी संस्कृति को जन्म दिया। इस नयी उपभोक्तावादी संस्कृति में चीजें उलट गईं। अब आविष्कार पहले होता है और बाद में प्रचार माध्यमों और विज्ञापनों द्वारा समाज में इसकी जरूरत पैदा की जाती है। फैशन के नाम पर इस नयी चीज को जरूरतों में प्राथमिक बनाया जाता है। इसके लिए तमाम सेलिब्रिटी बड़ी कीमत लेकर झूठा प्रचार करते हैं। विज्ञापन असल में नयी ग़ैरजरूरी चीजों को समाज में प्राथमिक और जरूरी बनाने का ही उपक्रम है। उपभोक्तावादी संस्कृति में विज्ञापन की अहम भूमिका होती है।
नंद भारद्वाज लिखते हैं, ‘तमाम तरह की ग़ैरजरूरी चीजों के लुभावने विज्ञापन आम आदमी को इस या उस चीज को खरीदने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, चाहे लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएँ कुछ भी क्यों न हों।’ श्यामाचरण दुबे ठीक ही कहते हैं, ‘विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तन्त्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी।’ विज्ञापन इस काम के लिए मनुष्य के सेंसेशन का उपयोग करता है। इसका हमला मनुष्य की बुद्धि पर होता है। अब ‘सुंदर’ शब्द का जमाना नहीं रहा, ‘स्मार्ट’ शब्द से वह विस्थापित हो चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा लिखते हैं, ‘सुंदर शब्द भी अब फैशन से बाहर होता जा रहा है, उसका स्थान ‘स्मार्ट’ ने ले लिया है जिसका सीधा संबंध लिबास, सजधज और अप-टू-डेट अदा से है।’ स्पष्ट है कि विज्ञापन बड़ी चालाकी से लोगों में अभाव क्रिएट करता है।
बहरहाल उपभोक्तावादी संस्कृति पूँजीवादी शोषण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हथकण्डा है। उपभोक्तावाद दरअसल पूँजीवादी व्यवस्था का ही चारित्रिक विस्तार है। इसलिए कि यह एक विशेष किस्म की ग़ैरबराबरी पैदा करता है। जाहिर तौर पर विज्ञापन की इसमें भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। एक विज्ञापन आता है जिसका मकसद है एच.डी. चैनल्स की खरीददारी का प्रचार-प्रसार। उसमें कई बच्चे एक साथ झूमते हुए यह गाते नजर आते हैं, ‘डब्बा है डब्बा, अंकल का टी.वी. डब्बा’।
उस आदमी के पास एच.डी. चैनल्स नहीं हैं इसके लिए उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। इस तरह एक महीन लेकिन स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जाती है जिसके पास वह वस्तु है उसके और जिसके पास वह वस्तु नहीं है उसके बीच। इस प्रकार मनुष्य के सेंसेशन का इस्तेमाल करके उपभोक्तावाद एक नया सामाजिक विभाजन पैदा करता है। सच्चिदानंद सिन्हा लिखते हैं, ‘उपभोक्तावादी संस्कृति, समाज को किसके पास क्या उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध हैं, इस आधार पर असंख्य वर्गों में बाँटती जाती है और उनके बीच भावनात्मक भेद पैदा करती है।’ इस प्रकार उपभोक्तावादी संस्कृति और बजार में सामाजिक समतामूलक मूल्यों का निषेध है।
पूँजीवादी व्यवस्था में थोक उत्पादन पर जोर रहता है इसलिए वस्तुएँ बड़े उद्योगों में एक साथ न तैयार होकर अलग-अलग खण्डित रूप में तैयार होती हैं। इससे मजदूर जो उत्पादन के काम से जुड़े होते हैं सिर्फ पैसे के एवज में काम करनेवाले मजदूर बन के रह जाते हैं। सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का जो सुख उन्हें व्यक्तिगत स्तर के छोटे उद्योग और उत्पादन की छोटी प्रणाली से होता था, उसे इस संस्कृति ने उनसे छीन लिया। ख़रीददार भी अब बस उपभोक्ता भर है। यह संस्कृति आदमी को आदमी नहीं रहने देती, उसे मात्र उपभोक्ता बना देती है और दुनिया सिर्फ बाजार हो जाती है। इस तरह यह संस्कृति तमाम सम्बन्धों, सृजनशीलता और कल्पनाशीलता के मूल्यों का भी निषेध रचती है।
बाजार एक तरह की आर्थिक पद्धति है। विनिमय की प्रक्रिया बाजार के समूचे तन्त्र की धुरी है। विनिमय नये सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण के मुख्य आधारों में से एक है। नये बाजार का सीधा हमला हमारी समझ और संवेदना पर है। नया बाजार कहीं अधिक आक्रामक हुआ है। इस नये बाजार को आर्थिक पद्धति के रूप में देखे जाने के बजाय सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से उसके गहरे सरोकारों की पड़ताल की जानी चाहिए। नया बाजार दरअसल सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का कारगर हथियार है।
नये बाजार की इस भूमिका को समझने की कोशिश करते हुए अच्युतानंद मिश्र ने लिखा है, ‘एक ही समय वह प्रतिरोध और समर्थन दोनों को व्यावसायिक मूल्य के रूप में विकसित कर उपभोग में बदल सकता है।’ यही नहीं संवेदनाओं को भी वह प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। नया बाजार प्रतिरोध, समर्थन और संवेदना को उतनी ही जगह देता है जितना कि उनको अपनी जरूरत के मुताबिक कैननाईज कर सके।
बाजार का यह नया स्वरूप समाज की पारम्परिक अवधारणा को नष्ट करता है। गिफ़्ट संस्कृति का इस कदर प्रचलन हुआ है कि ख़ून के रिश्तों को भी अब गिफ़्ट के फेबीकॉल की जरूरत है। बाजार इस कदर हमलावर हो गया है कि उसके बिना अब ‘रिश्तों की मिठास’ नहीं बच सकती। बाजार ने वर्चस्व की अवधारणा से जुड़कर मनुष्य को महज उपभोक्ता में बदल दिया है। इस तरह बाजार की नयी अवधारणा मनुष्य की अवधारणा के खिलाफ़ ठहरती है। मनुष्य की अवधारणा में विचार, तर्क, बुद्धि, सन्देह और प्रतिरोध शामिल होते हैं। नये बाजार का हमला मनुष्य होने की इन्हीं प्रवृत्तियों पर है। मनुष्य की इन्हीं प्रवृत्तियों को नष्ट कर के वर्चस्व की अवधारणा वास्तविक जमीन पा सकती है। दरअसल वर्चस्व की अवधारणा ही बाजार का मेकानिजम है।