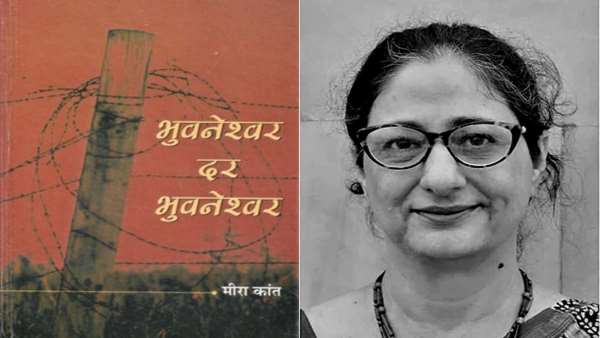नक्सलबाड़ी आन्दोलन और नुक्कड़ नाटक
नुक्कड़ नाटक जो पर्याय है संघर्ष का, व्यवस्था के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कदाचार, धार्मिक कट्ठरता, साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का… वह अचानक आसमान से टपककर रंगजगत में नहीं आ गया है, न किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की उपज है। यह परिकल्पना है निरन्तर चल रहे संघर्ष व उत्तरोत्तर जनोन्मुखी सांस्कृतिक विकास का। आज नुक्कड़ नाटक का जो सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक स्वरुप उपस्थित है उसका पिछली सदी की तीन प्रमुख घटनाओं से सीधा सम्बन्ध है, जिससे न केवल उसने वैचारिक ऊर्जा प्राप्त किया है अपितु रुप के नये-नये आयाम भी ढूंढें हैं। सोवियत क्रांति उन संबंधों की श्रृंखलाओं की पहली कड़ी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत उत्पन्न हुई ग़रीबी, तबाही, बेरोज़गारी, सांस्कृतिक-सामाजिक मूल्यों का विघटन, राजनीतिक अनिश्चितता इसकी दूसरी कड़ी है। तीसरी और महत्वपूर्ण कड़ी 1967 के बंगाल के नक्सलबाड़ी आन्दोलन का वज्रनाद है।
भारत में नाटक को जनता से जोड़ने और जनता को संघर्ष में उतारने, पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताक़तों को शिकस्त देने की दिशा में पहली बार इस तरह का सांस्कृतिक आन्दोलन द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ‘इप्टा‘ की अगुवाई में हुआ था। उस समय एक तरफ़ बंगाल में अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष में लोग मर रहे थे वहीं दूसरी तरफ़ लाखों-करोड़ों लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़ फेंकने में लगे थे, फैली हुई असमानता, धार्मिक कट्ठरता, अंधविश्वास, जाति-पांति का भेदभाव से लड़ने में जुटे थे। तब इप्टा के रंगकर्मी नगरों-महानगरों के हातों, थियेटरों से निकलकर गांवों, कल-कारख़ानों, छोटे-बड़े शहरों में जा रहे थे। अकाल के गीत सुना रहे थे, मुक्ति के गा रहे थे, क्रांति का बिगुल बजा रहे थे। इससे रंगकर्म समृद्ध हुआ। जनता के लोकतत्व नाटकों से जुड़े।
जनता की कहानी का रंग जगत से सीधा संपर्क बना। लोक कलाओं की अनेकों ऐसी विधायें जो सामंती व्यवस्था के साये तले विकृत होती हुई अंतिम सांसें ले रही थी, उन्हें प्राणवायु मिली। एक दिशा प्राप्त हुई। उनका परिमार्जन हुआ। समय से जुड़कर सामयिक हुए। अर्थात जहाँ – जहाँ भी जिस मुल्क में भी शोषण दमन हुआ उसके विरूद्ध संघर्ष छिड़ा, वहाँ के रंगकर्म ने जनता से जुड़ने की आवश्यक्ता को महसूस किया। चाहे स्पेन में गृहयुद्ध हो, वियतनाम में जापानी-फ़्रांसिसी और अमेरीकी मैक्सिको मूल के खेत मज़दूर और काले लोगों का जनवादी अधिकारों का संघर्ष और फ़्रांस में सातवें दशक में उथल-पुथल मचाने वाला युवाओं का लोकप्रिय आन्दोलन, सभी जगह नुक्कड़ नाटकों ने अपना भरपूर योगदान दिया। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्ऱीका के सभी देशों में नुक्कड़ नाटकों ने रंगकर्म और जन आन्दोलन को लोकप्रिय बनाया।
आज़ादी के पहले इप्टा के रंग आन्दोलन में जो धार, पैनापन था वह आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक बरक़रार नहीं रह सका। वामपंथी धाराओं का सतता के समाजवादी भुलभुलैये में फंसने, राजनीतिक और विचारधारात्मक मतभेद बढ़ने, फ़िल्मों के आकर्षण और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण क्रमशः क्षीण होता गया। रंगकर्म की प्रतिबद्धता अवसरवादिता में तब्दील होने लगी। नाटक गांवों से शहरों की तरफ़ वापस लौटने लगा था। नाटक से गाँव-कस्बा छूटता गया। शोषण-उत्पीड़न और लोक से वह दूर होता गया। अब नाटक की परिधि में व्यक्तिगत कुंठा, त्रास, विकृत सेक्स और मध्यवर्गीय आग्राहों-दुराग्रहों का सिलसिला आने लगा।

आज़ादी के लगभग दो दशक गुज़रने के बाद भी देश की बहुसंख्यक जनता को जब लगा कि स्थितियों में विशेष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अमीरी-ग़रीबी की वही खाई अब भी बरक़रार है, किसानों-मज़दूरों पर सामंतों, मिल मालिकों के शोषण में कतई बदलाव नहीं है तो उनमें मोहभंग होने लगा। लोग विरोध में खड़े होने लगे और 1967 आते-आते अंदर का लावा विस्फ़ोट कर गया। चारों तरफ़ फैली ग़रीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण-दमन और मंहगाई के ख़िलाफ़ लोग सड़कों-चैराहों, खेत-खलिहानेां में निकल पड़े। सन 1967 के मई महीने में माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांतिकारियों ने प. बंगाल के तराई इलाके में एक लड़ाकू आन्दोलन छेड़ा। नक्सलबाड़ी, खड़िबाड़ी और फांसीदेवा थाना इलाका 274 मील के दायरे में फैला हुआ है और यहाँ के किसानों में 70 प्रतिशत ग़रीब और भूमिहीन लोग थे। वे बड़े जोतदारों और धनी किसानों के निर्मम शोषण के शिकार थे। ज्यों-ज्यों शोषण अधिक होता गया प्रतिरोध और बढ़ता गया। किसान एकजुट हुए ओर आन्दोलन के तहत ज़मीन पर खेती करना और फ़सल क़ब्ज़ा करना शुरू किया। इस आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने के साथ ही गाँव-गाँव में किसान समीतियाँ उठ खड़ी हुईं किसान सभा के सदस्यों की संख्या पाँच हज़ार से बढ़ाकर चालीस हज़ार हो गयी। किसान समिति के नेतृत्व में किसानों में ज़मीन को बांटा जाने लगा, पुराने काग़ज़ात जला दिये गये। तमाम महाजनी ऋण ख़ारिज किए गए। ज़ालिम जोतदारों का जमा किया हुआ धन और दूसरी चीज़ें लोगों में बांट दी गईं। ज़ालिम जोतदारों को सज़ा दी गयी। किसानों को हथियारबंद किया गया। देहाती इलाक़ों में राष्ट्रीय प्रशासन, क़ानून तथा अदालत को ख़ारिज कर क्रांतिकारी कमेटी के प्राधिकार को कायम किया गया। दमन के लिए जब पुलिस की टुकड़ी गाँव में पहुंची तो तीर-धनुष लेकर किसानों ने उन्हें रोक दिया। सत्ता का जवाब शस्त्र से दिया गया।
प्रतिरोध का यह रूप शोषितों-पीड़ितों को नई प्रदान कर रहा था। नक्सलबाड़ी के किसान संघर्ष ने देशभर की उत्पीड़ित जनता को प्रेरित किया। मज़दूरों और किसानों में धीरे-धीरे यह भावना बढ़ती चली गयी कि नक्सलबाड़ी का रास्ता ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। शहरी मध्यवर्ग और विद्यार्थियों ने भारत की क्रांति के सम्पूर्ण दौर में पहली बार इस संघर्ष से अभूतपूर्व प्रेरणा हासिल किया।
देखते ही देखते नक्सलबाड़ी की चिनगारी देश के कोने-कोने में दावानल बनकर फैल गयी। सरकार ने इस आन्दोलन को पुलिस की टुकड़ियाँ भेजकर कुचलना चाहा, काबिंग ऑपरेशन, मुठभेड़ जैसी शब्दावलियों और नक्सलवादियों की लाश से अख़बार पटने लगे। मुल्क के सबसे अच्छी शिक्षण संस्थान चाहे वे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हो या आईआईटी और प्रेसीडेंसी कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान नक्सलवाद के केंद्र बन गए। साहित्य जो व्यक्तिवाद, पलायनवाद, कुंठा, संत्रास तक सीमित था, अब उसके दायरे में आम लोग उपस्थित हुए। बरसों से जिस किसान-मज़दूर की अवहेलना की गयी थी उन्हें इस आन्दोलन ने नायक का दर्जा देना शुरू किया। रंगमंच जो अभिजात्य ढांचें में जकड़ा हुआ था, चरमरा सा गया। वर्गीय विभाजन स्पष्ट था। एक वर्ग ऐसा था जो कला को कला के लिए मान रहा था तो दूसरा कला को जीवन, समाज और आम लोगों के लिए मान रहा था। एक सत्ता के पक्ष में था तो दूसरा सत्ता के विरोध में। एक के लिए नाटक में प्रतीक, रहस्य, भटकाव महत्वपूर्ण था तो दूसरे के लिए जीवन को स्पष्ट रूप् में प्रस्तुत करना, अशिक्षा-अज्ञान-अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे लोगों को उजाले में ले जाना ज़रूरी पक्ष था।
शुरु में इस प्रकार के नाटक वहीं ज़्यादा हो रहे थे जहाँ नक्सलबाड़ी आन्दोलन का अधिक प्रभाव था। इनमें प.बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेष, उत्तर प्रदेश व पंजाब प्रमुख थे। बंगाल के रंगकर्मियों ने 15-20 मिनट की अवधि वाले ’पोस्टर प्ले’ कलकत्ता और आस-पास के नगरों-कस्बों-गांवों में ख़ूब किये। कलकत्ता के चैरंगी के सामने का मैदान तो इसका ख़ास स्थान था। बिना सूचना के छापामार ढंग से रंगकर्मी अचानक आ जुटते थे और गायन-वादन से लोगों को जुटाकर पोस्टर प्ले शुरु कर देते थे। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती, पूछताछ करती, धर-पकड़ करती… रंगकर्मी मुहल्ले के किसी गली में घुसकर निकल जाते और अगले शो में व्यस्त हो जाते। चूँकि ये नाटक एक आन्दोलन से जुड़े हुए थे इसलिए उनमें एक फ़र्क़ था। कथ्य से अधिक विचार की प्रमुखता थी। दृश्य से अधिक शब्द की प्रधानता थी। कर्म पर बल था। इन्हीं कारणों से पारम्परिक थियेटर करने वालों या उन्हें जो रंगकर्म को पार्टी से जुड़ने से परहेज़ रखते थे, को ये सब नागवार लगा और इन नाटकों पर तरह-तरह के आरोप लगाये। कलावादियों ने नुक्कड़ नाटकों को पार्टी का भोंपू बताया, ‘प्रोपेगैंडा नाटक‘ कहा। ये नाटक दिन के उजाले में होते थे, मुख सज्जा, मंच सज्जा नहीं होता था। नाटक में ज़रूरी नहीं कि मंच, मुख, वस्त्र सज्जा हो ही। अगर नुक्कड़ नाटक दिन में बिना साज-सज्जा के अपने कथा, संवाद, अभिनय के बल पर आ जा रहे लोगों को रोककर नाटक देखने के लिए विवश कर देता है, अपने विचार से उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देता हे तो इसका अर्थ है कि इस नाटक में कला है। कला होने की वजह सी ही नाटक संप्रेषित हो रहा है। थियेटरों के मठाधीशों ने नुक्कड़ नाटक पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए वे एक सोची समझी साज़िश के तहत ही थे।

निःसंदेह उन दिनों के नुक्कड़ नाटक का अंत आक्रामक होता था। इस आन्दोलन के तहत ज़मीन दख़ल, ज़ुल्मी सामंतों का सफ़ाया, चुनाव का बहिष्कार, अदालत से अविश्वास जैसी अनेकों क्रियायें उभर कर सामने आयीं जो उन दिनों के अधिकांश नुक्कड़ नाटकों में स्पष्टतः परिलक्षित हुआ। चाहे वह गुरुशरण सिंह का नुक्कड़ नाटक ‘जंगीराम की हवेली‘, ‘हवाई गोले‘, इंक़लाब जिन्दाबाद‘, ‘तमाशा‘, ‘गढ्ढा‘ हो या अरुण रंजन का ‘पत्ताखोर‘, मधुकर सिंह का ‘दुश्मन‘, शिवराम का ‘कुकड़ू-कूं‘, ‘जनता पागल हो गयी है‘, असग़र वजाहत का ‘सरकारी सांड़‘, राजेश कुमार का ‘जनतन्त्र के मुर्ग़े, ‘जिन्दाबाद-मुर्दाबाद‘ और रमेश उपाध्याय का ‘हरिजन दहन‘। नुक्कड़ों पर सैकड़ों बार प्रस्तुत हुआ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुचर्चित नाटक ‘बकरी‘ का अंत पूर्णरूप से संसदीय व्यवस्था का माखौल उड़ाता नज़र आता है। ‘अब ग़रीबी हटाओ‘ के अंत में नाटक हथियार उठाकर वर्गशत्रु के सफ़ाये की ओर बढ़ता नज़र आता है।
बिहार के गांवों में जहाँ-जहाँ नक्सलबाड़ी आन्दोलन था, वहाँ अघोषित रूप से नाटक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। मसौढ़ी गाँव में जब पटना के रंगकर्मी नाटक कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। 1982 में नवयुवक कला मंच, बक्सर के कलाकार जब उजियार गाँव में ‘इंक़लाब जिन्दाबाद‘ नाटक प्रस्तुत करने पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें ख़ूब परेशान किया। भोजपुर के ‘युवा नीति‘ के कलाकार निर्मल को बक्सर रेलवे पुलिस ने मंचन के दौरान बुरी तरह पीटा। इस संगठन के प्रतिबद्ध रंगकर्मी व कथाकार नवेन्दु, श्रीकांत और सिरिल मैथ्यू के ऊपर पुलिस ने धारा 107 के तहत मुक़दमा दायर किया और उन पर नाटक व गीत के ज़रिए समाज की मर्यादा और शान्ति को नष्ट करने का आरोप लगाया। 1984 में ‘युवानीति‘ के कलाकारों को भोजपुर ज़िले के सहार थाने में बस से उतरते ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। फ़रवरी 1985 में हिरावल, पटना के नाट्य दल के कलाकारों को हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। हिरावल के रंगकर्मी अनिल अंशुमन को यातनाओं के कठिन दौर से गुज़रना पड़ा था। हिरावल के रंगकर्मीयों पर धारा 148, 149, 302, 307, 324 और आम्र्स ऐक्ट 27 लगाया गया।
दिसम्बर 1985 में रोहतास ज़िला के सकला बाज़ार में नवजागरण दल के कलाकारों पर हत्या और राइफ़ल छीनने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। युवा कथाकार और रंगकर्मी डा. विंध्येश्वरी को एक सप्ताह तक विभिन्न थानों में घुमाया गया और पीटा गया। बाद में इन्हें सासाराम भेज दिया गया। 26 पृष्ठों में तैयार किए गए आरोप पत्र में धारा 147, 148, 302, 307, 328 और आम्र्स ऐक्ट 26 के तहत उन्हें ‘कुख्यात नक्सली‘ घोषित कर दिया गया। उनके घर से जो भी पत्रिका, लेखकों के पत्र आदि मिले उन्हें बिहार पुलिस ने नक्सल साहित्य की संज्ञा दी। बहुत सारे जाने माने कथाकारों को भी नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में पुलिस वालों ने एक नाटक मंडली के कलाकारों के साथ दुव्र्यवहार किया। लोगों ने जब इसका प्रतिरोध किया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने थाने में एक महिला रंगकर्मी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपनाध किया।
भगतसिंह के पचासवें बलिदान दिवस पर ‘निशांत‘ द्वारा ग़ाज़ीपुर में ‘इंक़लाब जिन्दाबाद‘ नाटक करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और उन्हें जबरन ज़िला छोड़ने पर मजबूर किया गया। कालीकट में वर्गीस मेमोरियल बुक स्टाल के वार्षिक उत्सव पर ‘नाट्यगीतिका‘ द्वारा ‘स्पार्टकस‘ नाटक के मंचन जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग जुटे थे, पर 200 हथियारबंद पुलिस ने हमला किया और इस संगठन के 23 सदस्यों को गिरफ़्तार कर लिया। इन्होंने जेल के भीतर इसी नाटक का मंचन किया। 20 जुलाई 1974 को कर्ज़न पार्क में साम्राज्यवाद विरोधी कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अचानक हमला कर प्रवीण दत्त, एक युवा संस्कृतिकर्मी को मार डाला।
नुक्कड़ नाटक आन्दोलन की हद केवल गाँव के खेत-खलिहान-चैपालों तक ही सीमित नहीं है, अब वह जंगलों तक पहुँच गया है। जिस तरह ज़मीन के बाद जंगल को आर्थिक शोषण का केंद्र बनाया गया है, कारपोरेट घरानों की गिद्ध नज़र जंगल के छिपे आर्थिक स्रोतों पर पड़ी है, उस शोषण-दमन के विरोध में प्रतिरोध तो उभरना ही था और उभर भी रहा है। भले ही इस प्रतिरोधी संस्कृति का रूप शहरों के सदृश्य न हो लेकिन अभिव्यक्ति तो किसी न किसी माध्यम से व्यक्त हो ही जाती है। जिस तरह सरकार कारपोरेट घरानों से मिलकर जंगलों का दोहन कर रही है, आदिवासियों की उन्नति व प्रगति के नाम पर उन्हें विस्थापित कर रही है, उसके जवाब में आदिवासी का संघर्ष जहाँ एक तरफ़ राजनीतिक रूप से उभर रहा है, वहीं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हर रूप में सामने आ रहा है। निश्चित ही यह सांस्कृतिक रूप लोक के करीब है, लेकिन लोक के रूप में जो भाव आ रहे हैं, वे उसी प्रकार के है जिस तरह के खेत-खलिहानों में अधिकार के लिए लड़ने वाले नुक्कड़ नाट्य आन्दोलन में दिखते थे। वही धार, वही तल्ख़ी यहाँ भी होती है। ये बातों को बिना लाग लपेट, साफ़ और स्पष्ट कहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके लिए वे किसी आयातित बिम्ब-प्रतीक का इस्तेमाल नहीं करते। वे जंगल की, आदिवासी समाज के आस-पास के प्रतीकों के माध्यम से ही अपनी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ते हैं। और इस तरह की लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं। ब्रिटिश सम्राज्यवाद के वक़्त भी बख़ूबी लड़े थे और बदस्तूर आज भी जारी है।
भले इनकी लड़ाई को सत्ता एक ख़ास राजनीति से जोड़ देती हो, नक्सलवादी राजनीति से प्रेरित कह के दमन करने के लिए आधार बनाती हो, लेकिन प्रतिरोध की यह धारा नुक्कड़ नाटक की तरह लगातार बह रही है। मादंल की गूँज तरह जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाह में फैल रही है। सच है कि इस प्रवाह को रोकने के लिए व्यवस्था और कारपोरेट किसी न किसी बहाने इनके अंदर भी घुसने का प्रयास कर रही है। कई सरकारी व अनुदान प्राप्त संस्थाएं लोक रूप धर कर इनकी बोली, इनकी भाषा को अपना हथियार बना कर, इनके सांस्कृतिक आन्दोलन की धार को भोथरा करने की कोशिश कर रही हैं।
समतल की तरह जंगल में भी यही प्रयोग अपनाना चाह रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर लगाया गया यह रूप ज़्यादा दिनों तक बना नहीं रह पाता है। लोग जान जाते हैं, कौन हैं हमारे वास्तविक स्वर देने वाले? कबीर कला मंच तो एक उदाहरण हैं, आज दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जो शहरी प्रचार तन्त्र से दूर जंगलों में एक ऐसी संस्कृति की फ़सल तैयार कर रहे हैं जो भले सत्ता को नागवार लग रहा हो, हक़ीक़त में अवाम की ज़ुबान हैं। और इस आवाज़ को किसी भी सूरत में दबायी नहीं जा सकती। आप उन्हे नक्सलवादी कहकर जेल के सीखचों के पीछे डाल दें, एनकाउंटर कर दें, इनका लहू हर सवाल का जवाब मांगेगा और इस व्यवस्था के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। एक दिन ये जंगलों में इतने बढ़ जायेंगे कि बाहर आकर उन ताक़तों को खुलेआम चुनौती देंगे जो पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के पहरूआ बने उनींद रहे हैं।