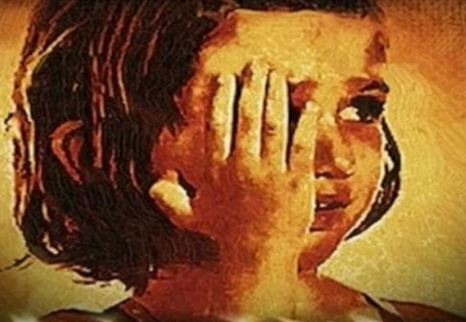राजनैतिक मूल्यों की अनुपस्थिति में – मेधा पाटकर
- मेधा पाटकर
घोषित हुए चुनाव नतीजों से चुनाव पर नजर रखने वाले लोग चकित हैं. जनतन्त्र की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव, सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए आजतक जीवित है. इस पर भरोसा रखकर ही जनता आज तक अपने देश के शासन के साथ संसाधन, संपदा, संस्कृति, संरचना और संविधान चुने गए प्रतिनिधियों को सौंपकर निश्चिंत होती आयी है. इन साधनों से जो साध्य हासिल करने हैं, वे भी जन प्रतिनिधि ही, जो शासक बनेंगे, तय करेंगे, ऐसा मानकर जनता, स्वयं जनार्दन होते हुए भी उन्हें जगन्नाथ के रूप में देखती, स्थान सम्मान देती रही है. 1951 से चलते आये जनप्रतिनिधि क़ानून में चुनावी सुधार परकमजोर आवाज उठती रही है.
इस बार के लोकसभा चुनाव एक चुनौती मानकर लड़े गये. इसके कारण कई सारे थे. एक, पिछले 2014 के चुनाव में चली मोदी हवा (जो तूफ़ान साबित हुई थी) के बावजूद उनके कई निर्णय, विकास की दिशाएँ, विदेश वारियाँ, झूठे दावे, वचन भंग और कॉर्पोरेटी भ्रष्टाचार पर जनता की ओर से आरोप पत्र लगाये गये थे. जाति और मजहब की राजनीति और राष्ट्रवाद का राजनीतिकरण, जो 2014 की जीत के बाद मोदी, शाह और मोदी समर्थकों द्वारा उठाये गये फैक्टर नहीं, फोर्स था, जनता के सामने खुलेआम पेश किया गया, वह भी अभिमान के साथ! इसे असंवैधानिक और अमानवीय कहकर नकारने वालों का जेल भुगतना निश्चित हो चुका था. विचारवंत समझ गए कि संविधान नहीं, तो भी कानूनों में बदलाव लाकर पर्यावरण, श्रमिक अधिकार, आदिवासियों के हक, दलितों का सम्मान, पंचायत राज और ग्राम सभा का स्थान, ये सारे स्तम्भ खोखले किये जा रहे हैं. विकास का ढिंढोरा और सीमावर्ती सुरक्षा के लिए युद्ध का तांडव दोनों हावी होने पर जन-जन को चुभने वाले उपर्युक्त मुद्दों पर कुछ पानी छिड़काया गया. जी.एस.टी. और नोटबन्दी के आघात झेलने वाले भी उसे भूलते गये.
फिर भी बहुत हकीकतें उजागर हुईं. मन की बातों का पर्दाफाश हुआ. फसल बीमा हो या नोटबन्दी, कंपनियों के ही लाभ के आँकड़े सामने आए. मीडिया में अंबानी, अडानी के शेयर्स के हस्तक्षेप के बावजूद दो गुटों में मारामारी और लाचारी दोनों की चली. उसमें पड़े न्यूज़ और प्रचार-प्रसार में पार्टियों के हजारों-करोड़ों के खर्च का हिसाब तो सामने नहीं आया लेकिन सोशल मीडिया में जानकारी का विस्फोट ही नहीं विश्लेषण भी छाया रहा. इस स्थिति में इस बार हवाई नहीं तो चुनावी फायरिंग होगी, ऐसा मानने वालों का विश्वास था कि यह चुनाव किसानों – मजदूरों के, महिला–युवा–बेरोजगारों के मुद्दों पर लड़ा जायेगा! अचानक पुलवामा–बालाकोट से पुकार आई. वहाँ कौन, कितने, कब पहुंचे, फिर कौन, कितने, कैसे शहीद हुए.. यह पता भी नहीं चला! किन्तु उस काण्ड को लेकर प्रधानमन्त्री का सीना, विरोधियों के तमाम हमले झेलकर भी 56 इंच से अधिक चौड़ा हुआ. ‘राष्ट्रवाद’ पर लम्बी, चौड़ी, गहरी बहस को, ‘शहीदवाद’ को उभरते हुए देखा गया और राजनीति के ‘संघीय’ ही नहीं, ‘राष्ट्रीय’ रणनीति के सामने हार स्वीकार करनी पड़ी.
राजनीति में जातिवाद कहीं खुलकर, तो कहीं छुपकर हावी रहता ही आया है. बिहार इत्यादि प्रदेशों में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी जाति के समीकरण का प्रभाव अभिमान के साथ बताया जाता है, अर्थात जाति निर्मूलन की मंजिल दूर रखकर, उसी की ओर चलने का दावा. अब जाति के आधार पर प्रधानमन्त्री जी भी स्वयं वोट की अपील कर चुके तो दलितों, बहुजनों को भी अस्मिता पर अधिक और अस्तित्व के मुद्दों पर कम उर्जा और उद्वेग जताते देखा गया.
लेकिन उससे भी ज्यादा, अब मजहबी स्पर्धा और मूल तत्त्वों के आधार पर हिंसा ही नहीं, अमानवीयता फ़ैलाने की मनीषा भी राजनीतिक हथियार के रूप में काम आने लगी. यह आन्तरिक युद्ध तो राष्ट्र की सीमाओं पर घटित हरकतों से भी ज्यादा भय, आतंक, हिंसा और दुश्मनी का आविष्कार करने की स्थिति है.
इस चुनाव में ईवीएम और ईसी, दोनों के कारनामों पर सन्देह व्यक्त किया गया, जिसके प्रमाण भी पेश हुए. लेकिन सवालात का प्रभाव चुनावी दौड़-धूप में बहुत कम दिखाई दिया, तो कइयों ने इसे आधे पर ही छोड़ दिया. आरबीआई, सीबीआई, न्यायपालिका, एनजीटी आदि को कटघरे में खड़े करने पर ऐसी स्थिति आई जैसे कि इसका जवाब देना तो सवाल करने वालों की ही जिम्मेदारी है.

हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जनता के घोषणा पत्रों की भरमार रही. घोषणा पत्रों में, इसे वचन पत्र या संकल्प पत्र ही क्यों न कहें, महिला, युवा, श्रमिक, आदिवासी या दलितों के मुद्दों में से कुछ चुनकर लिए गये, जो कांग्रेस, राजद, भाकपा जैसी पार्टियों के घोषणा पत्रों में बहुत कुछ दिखाई दिये, फिर भी उनके प्रचार–प्रसार के दौर में ऐसे मुद्दों को, जैसे असुरक्षित रखे गये श्रमिकों के, महिलाओं के साथ हिंसा के, दलितों या आदिवासियों के स्वशासन के, पर्यावरणीय या आर्थिक और बराबरी का कितना स्थान और समय मिला, कितनी लगन दिखाई दी? शायद उतनी ही जितनी आवाज उठी थी. ना केवल चुनाव की, बल्कि दो चुनावों के बीच की भी, राजनीति में, संसदीय और पंचायती राज की प्रक्रिया में भी अवकाश नहीं पाते और राजनीतिक निर्णयों का, जिसमें सामजिक–आर्थिक आयाम भी शामिल रहें जनतान्त्रिक प्रक्रिया का आधार नहीं बनाते. यही कारण है कि जन-जन के संगठित होकर किये गए सारे प्रयास सीमान्त रहते हैं.
वोट बैंक की यह राजनीति जब नशायुक्त अभियान बन जाती है तो, नशा पैदा करने वाली चीजों का, कम या अधिक उपयोग किए बिना वोट नहीं मिल सकता है. राजनीति को नशामुक्त करने की जिम्मेदारी उठाना जरूरी है पर कोई इसके लिए कंधा देने को तैयार नहीं है. इस राज और नीति के नाम परचल रहे खेल में या रण मैदान में उतरे किसी खिलाड़ी से न ही पूरी शुचिता की, न ही कुनीति पर चलने वालों को रोकने का जोखिम लेने की अपेक्षा कर सकते हैं. क्या इस जिन्दगी में हम कुछ हद तक भी बुनियादी परिवर्तन ला पाएंगे, इसका जवाब ढूँढना जरूरी है.
इसीलिए जीत-हार का विश्लेषण, ईवीएम और वीवीपैट की गणना को सही मानकर करें, तो जनतान्त्रिकता के सिकुड़ने के कई कारण सामने आते हैं. जाति–धर्म के नाम पर विभाजन न चाहने वाले एक मंच पर आये, लेकिन मोर्चा नहीं बना पाए… जो समान एजेंडा पर बन सकता था. तो धर्म का बोलबाला इतना बढ़ा और राजधर्म तथा मानव धर्म का इतना कम रहा, कि साध्वी के रूप में उतर आयी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी और उनके राष्ट्र विरोधी बयान भी उनकी पार्टी को अभिमानित करते दिखाई दिए, बस कुछ औपचारिक रूप से विरोध दिखा दिया गया. फिर दिग्विजय सिंह जी के लिए साधू-बाबाओं का रास्ते पर उतर आना भी कइयों–को अपरिहार्य महसूस हुआ. झारखण्ड और महाराष्ट्र तथा गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के समर्थक रहे नेतृत्व को भी नहीं बख्शा, यह कैसे विश्लेषित करें? मीडिया द्वारा सबसे अधिक पापुलर बन गए कन्हैया कुमार को भी हार खानी पड़ी, क्यों? न यूपी में सपा-बसपा एकता के बावजूद भीतरी मनमुटाव छुपा रहा, ना ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस के ही अपने नेताओं के बीच का। ये कहीं विचारहीन बातें करते नज़र आये, तो कहीं इस इवेंट मैनेजमेंट के खेल में अकुशल साबित हुए. बिखराव का यह फैक्टर टकराया अस्मिता भरी एकजुटता से जिसमें राष्ट्र और धर्म एक होकर पेश किया गया.

बंगाल में भाजपा ने जगह बनाई तो इसमें माना जाता है कि वामपन्थी मानी गयी जनता ने भी भाजपा को अपनाया, और कांग्रेस ने केरल में वाममोर्चा को नीचे दिखाया, जिन राज्यों में कुछ ही महीने पहले सत्ता पलट हुआ था उसमें क्या मतदाताओं की राय पलट गयी? इतने कम समय में यह हुआ तो किस आधारपर? कर्ज माफी या बेरोजगार भत्ता के आश्वासनों का पालन नहीं हुआ? जो और जितना हुआ, उसका ठोस प्रचार सत्ता में बैठे नेतृत्व से नहीं कर पाना और विरोधियों द्वारा उसका फायदा उठा लेना यह अनुभव है, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़ और राजस्थान का! कहीं नयी सरकार को फँसाने वाले पुराने शासन के भ्रष्ट अधिकारी थे, और कहीं ऐसे समुदाय थे, जो रुठे थे क्यूंकि उनके सवालों से दो चुनावों के बीच निपटने की कोशिश तक नहीं हुई! राजनीतिक रणनीतियों में क्या कम पड़े ये नये सत्ताधीश? पुरानी पार्टियों के अनुभव की कमी नहीं तो भी उनका कुछ विनाधार आत्मविश्वास आड़े आया? कई क्षेत्रों में प्रचार सभाओं की होड़ में बड़ी पार्टियाँ जिन्हें कोर्पोरेट जगत के साथ कम मात्रा में मदद मिली हो पीछे पड़ी, तो कहीं उम्मीदवारों का चुनाव फंडिंग के आधार पर होता दिखाई दिया. ‘आप’ के मुख्यमन्त्री ने खुद माना कि भाजपा ने दिल्ली के संसदीय प्रत्याशी अच्छे व्यक्तियों को चुना! तो ‘आप’ में क्या कमी थी, अच्छे, ईमानदारों की? आतिशी जैसी उम्मीदवार को बेनामी ताकतों ने बदनामी का दाग लगाकर हराया! इन गन्दी हरकतों को देश ने कोसा लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं.
इस बार यह कहने का मौका नहीं कि कम प्रतिशत वोट लेकर सत्ता कैसे? अगर ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ हो तो 46% वोट पाकर ही सत्ता में आयी है भारतीय जनता पार्टी!
पिछले चुनाव में 31% से बढ़ गया उनका हिस्सा जो जन समर्थन ही माना जायेगा; फिर भी 46% – 54% वाला यह जनतन्त्र कहां तक प्रतिनिधित्व करेगा, उन बेजुबानों का, जिन्होंने वोट किसी को भी दिया हो, अपना हक तो ना छोड़ा है, न छोड़ सकते हैं? उनकी संख्या वोटों से नहीं, कहीं नोटों से, तो कहीं उनकी मेहनत–प्रकृति की पूंजी से गिनो तो वे ही हैं बहुसंख्य! जाति–मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक साबित हुए सब तो भुगत रहे हैं हमला–हिंसा और लूट का, अवमानना और अन्याय का! लेकिन इन विभाजकों के पार बनी बहुसंख्या ही जनतन्त्र की सही ताकत है. भले वोटों की राजनीति की मान्यता बनी रहे, समाज में मूल्यरोपण, हकदारी के संघर्ष, अन्याय की खिलाफत, विनाशकारी विकास की पोल खोल और संविधान की सुरक्षा भी लाने–रखने वाले अपना जनाधार, जनशक्ति चुनाव के पार तभी बना रखेंगे जबकि चुनावी प्रक्रिया में भुलाये, दबाये गये उनके सवाल और समस्याओं को, वे सभी साथी जिन्हें लोकतन्त्र को जीवित रखना है और समता–न्याय की तलाश है, हाथ लेकर टूट पड़ेंगे.
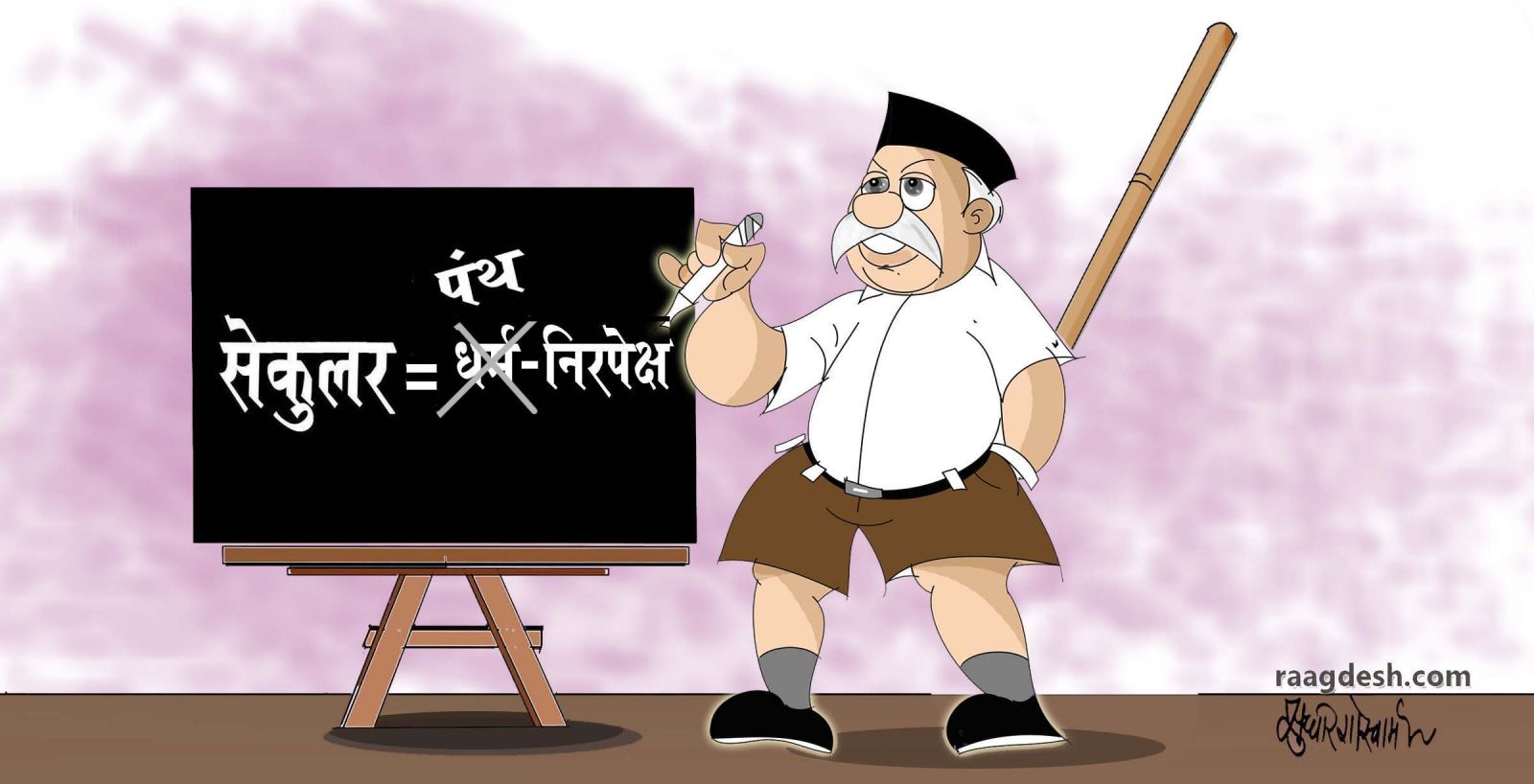
धर्म मूलतत्वाद और धर्म निरपेक्षता के आधार पर चुना जाकर ‘राज्य’ चलाना चाहने वालों ने भी शायद अन्य मुद्दे जैसे विकास, सुशासन, या जनतन्त्र जैसे मुद्दों पर जो परीक्षा देनी है, उसकी भनक ही नहीं प्रत्यक्ष अनुभूति देखकर भी वंचित, शोषित समुदायों ने उन्हें अपना अनोखा डंडा चलाकर तो नहीं दिखाया. सबरी माला जैसे मुद्दें पर हजारों-हजारों महिलाएं कतार में खड़ी हुई. वाममोर्चा के साथ सर्वोच्च अदालत के फैसले के अमल के लिए! लेकिन कांग्रेस ने भाजपा से कुछ अलग याने बीच की भूमिका को लेकर परंपरा को भी सम्मानित किया… क्या भाजपा–कांग्रेस के बीच सेक्युलर लेकिन संवादशील बने रहे कांग्रेसियों को बहुमत से जिताकर केरल की विकास से प्रभावित जनता ने वाम मोर्चा सरकार की संवादहीनता नकारी है, यही मानना है जन संगठनों का? पूरे देश में कांग्रेस ने भी अपने ही लाये हुए जनवादी कानूनों को प्रचारित करने में सफलता नहीं दिखाई.
अब सूचना का अधिकार हो या वन अधिकार, नया भू – अधिग्रहण हो या ‘पैसा’, फेरी वाला कानून हो या पर्यावरणीय क़ानून … इन सब में पुलवामा दौर में बदलाव किए गये हैं या मसौदे तैयार हैं. इसका सामना सत्याग्रही मार्ग पर चलकर करने वालों की देश में कमी नहीं है. जनसंगठनों की एकता के साथ, उन मुद्दों पर समविचारी दलों का आंदोलनकारी बनकर सामने आना, हिम्मत से नि:स्वार्थी, जनवादी वृत्ति से सत्ता–लालच के परे हाथ मिलाना, जनतन्त्र को मजबूत कर सकेगा. सेक्युलर पार्टियों की एकता अगर इन जन आंदोलनों के मुद्दे पर बनती है तो नर्मदा हो या नियमगिरी, फसलों के सही दाम हो या श्रमिकों के क़ानून, पर्यावरणीय से आर्थिक–संवैधानिक संस्थाओं के नीति-नियम भी मुद्दे होंगे, जिन्हें जितने संसद में, उससे अधिक संसद बाह्य राजनीति से चुनौती देते रहेंगे. चुनावी व्यवस्था में विकेंद्रीकरण और ईवीएम ही नहीं, यह वोट बैंक की मशीनरी ही बदलकर अधिक मूल्यवान बनाने की कोशिश प्राथमिकता लेकर बढ़ेगी. चुनावी सुधार नहीं बुनियादी परिवर्तन केवल 1951 के कानून में बदलाव से ही नहीं, जनतन्त्र पर नया नजरिया लाकर ही संभव होगा! पांच साल में यह मौका है उन सबके लिए जिनके मुद्दों पर सही पक्ष जिन्हें कटघरे में नहीं तो भी हाशिये पर खड़ा कर दिया है जनता ने. लेकिन यही जनता स्वयं भी वहीं है, इर्दगिर्द में… साथ लेने–देने के लिए तैयार. आइये–मिलाइये हाथ, दिलायें न्याय!!

लेखिका नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेत्री और प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं|
सम्पर्क- +919423965153, medha.narmada@gmail.com
.