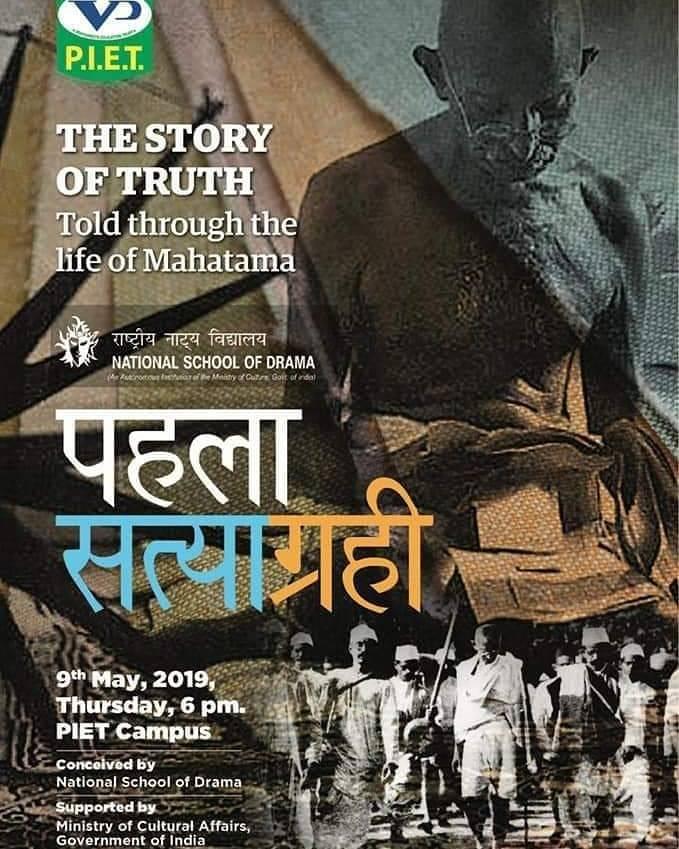हिंदी रंगमंच में फुले-अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रभाव
- राजेश कुमार
फुले ने वर्ष 1855 में ‘तृतीय रत्न’ नाटक को लिखा था। फुले के इस नाटक पर गौर फरमाना क्यों नहीं जरूरी समझा गया? क्या जानबूझकर उपेक्षित रखा गया क्योंकि यह नाटक ब्राह्मणवाद पर सीधा चोट कर रहा है? सन 1853 में बम्बई में दो ही थिएटर का अस्तित्व इतिहास में देखने को मिलता है। एक नाट्यशाला ग्रांट रोड पर था जिसे ‘ग्रांट रोड थिएटर‘ कहा जाता था, दूसरा ‘ खेतवाड़ी थिएटर‘ था जो संभवतः खुला थिएटर था, जिसमें लोकधर्मी परंपरा की शैली द्वारा नाटक अभिनीत हुआ करते थे। ‘बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर ‘ के 27 एवं 31 अक्टूबर 1853 के अंकों से पता चलता है कि बम्बई में इन्हीं दिनों एक ‘पारसी ड्रामेटिक कोर‘ का जन्म हुआ और उसमें गुजराती भाषा में एक नाटक का अभिनय ग्रांट रोड थिएटर में किया जिसका शीर्षक था ‘रुस्तम जबोली और सोहराब’। नाटक के क्षेत्र में प्रमुख रूप से पारसी व्यवसायियों के आने से जिस तरह का देश भर में रंगमंच देखने को मिलता है, वो पारसी थिएटर के नाम से जाना गया। किसी रंगमंचीय अवधारणा के तहत इसका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि सन 1776 में अस्तित्व में आये ‘बम्बई थिएटर ‘ जहां अंग्रेजों के मनोरंजन के लिए अक्सर इंग्लैंड से आये घुमंतू मंडलियों या शौकिया अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश ड्रामा हुआ करते थे, प्रेरणास्रोत थे। सन 1846 तक आते – आते जहां एक तरफ इंग्लैंड से आकर इंग्लिश ड्रामा के मंचन का प्रचलन आर्थिक रूप से फायदेमंद न होने के कारण भले धीमा पड़ गया हो, लेकिन पारसी समुदाय के व्यवसायियों को इस मनोरंजन में वृहद संभावना नजर आई। देश भर के मुख्य शहरों को आधार बनाकर पहले अंग्रजी नाटकों फिर अरबी-ईरानी कहानियों को नाटक में ढाल कर व्यावसायिक रूप से मंचन करने लगी। चूंकि इसके दर्शक ज्यादतर शहरी होते थे इसलिए उनके लिए लाजिमी था कि नाटकों में वही दिखाया जाए जो वे चाहते थे। यही कारण था कि पारसी थिएटर की जो यात्रा शेक्सपियर के नाटकों से शुरू हुई थी, कुछ ही वर्षों के अंतराल बाद भारतीय मिथकों व ऐतिहासिक – धार्मिक गौरव गाथाओं के इर्द – गिर्द घूमने लगी।

लेकिन इसके बरक्स जो नाट्यधारा लोक में व्याप्त थी और जिसकी चर्चा करने, अभिलेख करने में मुख्यधारा के कलमकार जरा संकोच करते हैं, उनकी एक बानगी देखनी है तो पारसी थिएटर के अस्तित्व में आने के दो वर्ष के बाद ही फुले का लिखा नाटक ‘तृतीय रत्न’ पर नजर गड़ाने की जरूरत है। फुले के इस नाटक पर न पाश्चात्य रंगमंच का प्रभाव था, न पारसी थिएटर की तरह किसी तरह की व्यावसायिक प्रमुखता। यह नाटक लोक के बीच लोकप्रिय ‘खेतवाड़ी थिएटर’ के करीब का था जिसके प्रदर्शनों में ‘बम्बई थिएटर’ की तरह केवल अंग्रेजों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, न ‘पारसी थिएटर’ की तरह शुल्क देय जैसी कोई औपचारिकता। किसी भी जाति और वर्ग के लोग नाटक देख सकते थे। फुले का यह नाटक जन सामान्य के बीच से निकला था। यह विदित है, फुले का जो कार्य स्थल था वो पुणे का था और यह शहर पेशवाओं का भी था जहां अस्पृश्य समाज के साथ इन्होंने अतीत में तरह – तरह के अमानवीय बर्ताव किये थे। अंग्रेजों के आने के बाद भले पेशवाओं का राज समाप्त हो गया, लेकिन हिन्दू समाज में जो वर्णव्यवस्था थी, वो बरकरार थी। ब्राह्मणवादी परंपरा खत्म न होने के कारण समाज में छुआ- छूत, अंध विश्वास, कट्टरता यथावत थी।
फुले ने ‘तृतीय रत्न’ नाटक का कथ्य उनदिनों के पारसी थिएटर तर्ज पर आयातित नहीं था। जिस आंदोलन से जुड़े थे, उसी के बीच से निकला हुआ था। दलितों – स्त्रियों को शिक्षा मुहैया कराने के वे जबरदस्त हिमायती थे। इस मिशन में उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्यरत थी। ब्राह्मण समाज से इसका काफी विरोध भी हुआ, पर इन्होंने हार नहीं मानी। ‘सत्यशोधक समाज’ का गठन कर एक वृहद सामाजिक – सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया।  उनके नाटकों का तत्कालीन रंगमंच, विशेषकर लोक में निहित नाट्यशैलियों पर विशेष प्रभाव डाला। लोक मंचों पर पहले हल्के – फुल्के जो हास्य प्रधान नाटक होते थे, धार्मिकता पर जोर होता था; अब उसका स्वर बदल कर आलोचनात्मक होने लगा। फुले ने ‘गुलामगीरी’,’किसान का कोड़ा’ और ‘सत्सार’ के माध्यम से हिन्दू धर्म के परंपरागत मिथकों की जो चीर फाड़ की, नए संदर्भों में जिस तरह विश्लेषित किया; उसका असर तत्काल विभिन्न भाषाओं के रंगमंच पर दिख गया। लोक रंगमंच पर पहले दिखा पर पारसी या हिंदी रंगमंच पर कुछ वर्षों के अंतराल के बाद। सन 1855 में फुले ने ‘ तृतीय रत्न’ से जो लोक नाटक के माध्यम से रंगयात्रा की शुरुआत की थी, कुछ ही वर्षों के बाद उनकी तलाश उससे भी आगे की होने लगी कि कैसे आम लोगों के और करीब पहुंचा जाय। शायद इसी तलाश के कारण सन 1873 में ‘गुलामगीरी’ और सन 1885 में ‘सत्सार’ का लेखन किया। नाटक का जो पारंपरिक रूप होता है, ये कृतियां उस प्रारूप में नहीं है। पंद्रह परिच्छेदों में लिखा ‘गुलामगीरी’ में धोन्डी राव और ज्योति राव का संवाद है जिसमें ब्राह्मणवादी धर्म की छत्रछाया में जो गुलामगीरी फल- फूल रही थी, उसका निर्मम ढंग से पर्दाफाश किया गया है। फुले का मानना था कि जो व्यवस्था अमानवीय है, शोषण पर आधारित है, मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है, उसको बदलना जरूरी है। ब्राह्मणों ने हिन्दू मिथकों, पुराण कथाओं के माध्यम से आम लोगों के बीच भाग्यवाद, यथास्थितिवाद की जड़ को मजबूत किया है, उसे तर्क द्वारा नंगा करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुद्ध ने अपने धम्मोपदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पालि ( मागधी ) अपनाई थी। फुले ने ‘तृतीय रत्न’ में कलाकारों और दर्शकों के बीच संवाद बनाये रखने के लिए विदूषक का जिस तरह इस्तेमाल किया था, उसका तत्काल प्रभाव ‘खेतवाड़ी थिएटर’ में देखने को मिलता है। ‘तृतीय रत्न’ नाटक प्रारम्भ होते ही विदूषक की उपस्थिति मंच पर हो जाती है। और नाटक के अंत तक लगभग सभी दृश्यों में मंच पर विद्यमान रहता है। चल रहे दृश्यों के बीच जब भी मन करता दाखिल हो जाता है। सीधे दर्शको से मुखातिब होने से भी परहेज नहीं करता है। पात्रों पर टिप्पणी करने से भी चुकता नहीं है। उन्हें उकसाता भी है, व्यंग्य भी कसता है। कभी – कभी अपने भाव – भंगिमाओं, ऊलजलूल हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन भी करता है। भले फुले ने विदूषक की इस अभिनय प्रक्रिया को कोई सैद्धान्तिकी रूप न दिया हो, लेकिन लगभग सौ साल बाद ब्रेष्ट जब रंग जगत में ‘अलगाव का सिद्धांत’ लाते हैं तो बरबस फुले की विचारधारा और उनके रंगकर्म के प्रभाव की तरफ ध्यान चला जाता है। भले इसे कोई उल्लेखित न करे, लेकिन ये इतिहास है, अकाट्य तथ्य है कि ब्रेष्ट के इस ‘अलगाव का सिद्धांत’ का उत्स कहीं है तो वो फुले के नाटकीय विचारधारा में है। इसे संयोग कहिये या फुले के नाटक के प्रतिरोधात्मक प्रभाव, जब सन 1873 में फुले मराठी में संवाद शैली में ‘ गुलामगीरी’ लिख रहे थे, उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ‘ सबै जाति गोपाल की ‘ प्रहसन के द्वारा क्षत्री और पंडित दो चरित्रों के संवादों के माध्यम से शास्त्रों के अंतर्विरोधों को उजागर कर वर्ण- जाति व्यवस्था को बेनकाब कर रहे थे। उसी क्रम में सन 1881 में लिखा गया उनका कालजयी प्रहसन ‘अंधेर नगरी ‘ भी है। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि फुले जिस अंदाज से ब्राह्मण वर्ग द्वारा फैलाये जा रहे धार्मिक पाखंडों का भंडाफोड़ कर रहे थे, उसके प्रभाव से हिंदी रंगमंच बचा नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस प्रहसन में बजाप्ते ‘जातवाला(ब्राह्मण)’ नाम से एक पात्र है जो बाजार में चिल्ला – चिल्लाकर अपनी जात बेच रहा है। वो कह रहा है, ‘जात ले जात, टके से जात। एक टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाय और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करै। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिन्दू से क्रिस्तान…’।
उनके नाटकों का तत्कालीन रंगमंच, विशेषकर लोक में निहित नाट्यशैलियों पर विशेष प्रभाव डाला। लोक मंचों पर पहले हल्के – फुल्के जो हास्य प्रधान नाटक होते थे, धार्मिकता पर जोर होता था; अब उसका स्वर बदल कर आलोचनात्मक होने लगा। फुले ने ‘गुलामगीरी’,’किसान का कोड़ा’ और ‘सत्सार’ के माध्यम से हिन्दू धर्म के परंपरागत मिथकों की जो चीर फाड़ की, नए संदर्भों में जिस तरह विश्लेषित किया; उसका असर तत्काल विभिन्न भाषाओं के रंगमंच पर दिख गया। लोक रंगमंच पर पहले दिखा पर पारसी या हिंदी रंगमंच पर कुछ वर्षों के अंतराल के बाद। सन 1855 में फुले ने ‘ तृतीय रत्न’ से जो लोक नाटक के माध्यम से रंगयात्रा की शुरुआत की थी, कुछ ही वर्षों के बाद उनकी तलाश उससे भी आगे की होने लगी कि कैसे आम लोगों के और करीब पहुंचा जाय। शायद इसी तलाश के कारण सन 1873 में ‘गुलामगीरी’ और सन 1885 में ‘सत्सार’ का लेखन किया। नाटक का जो पारंपरिक रूप होता है, ये कृतियां उस प्रारूप में नहीं है। पंद्रह परिच्छेदों में लिखा ‘गुलामगीरी’ में धोन्डी राव और ज्योति राव का संवाद है जिसमें ब्राह्मणवादी धर्म की छत्रछाया में जो गुलामगीरी फल- फूल रही थी, उसका निर्मम ढंग से पर्दाफाश किया गया है। फुले का मानना था कि जो व्यवस्था अमानवीय है, शोषण पर आधारित है, मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है, उसको बदलना जरूरी है। ब्राह्मणों ने हिन्दू मिथकों, पुराण कथाओं के माध्यम से आम लोगों के बीच भाग्यवाद, यथास्थितिवाद की जड़ को मजबूत किया है, उसे तर्क द्वारा नंगा करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुद्ध ने अपने धम्मोपदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पालि ( मागधी ) अपनाई थी। फुले ने ‘तृतीय रत्न’ में कलाकारों और दर्शकों के बीच संवाद बनाये रखने के लिए विदूषक का जिस तरह इस्तेमाल किया था, उसका तत्काल प्रभाव ‘खेतवाड़ी थिएटर’ में देखने को मिलता है। ‘तृतीय रत्न’ नाटक प्रारम्भ होते ही विदूषक की उपस्थिति मंच पर हो जाती है। और नाटक के अंत तक लगभग सभी दृश्यों में मंच पर विद्यमान रहता है। चल रहे दृश्यों के बीच जब भी मन करता दाखिल हो जाता है। सीधे दर्शको से मुखातिब होने से भी परहेज नहीं करता है। पात्रों पर टिप्पणी करने से भी चुकता नहीं है। उन्हें उकसाता भी है, व्यंग्य भी कसता है। कभी – कभी अपने भाव – भंगिमाओं, ऊलजलूल हरकतों से दर्शकों का मनोरंजन भी करता है। भले फुले ने विदूषक की इस अभिनय प्रक्रिया को कोई सैद्धान्तिकी रूप न दिया हो, लेकिन लगभग सौ साल बाद ब्रेष्ट जब रंग जगत में ‘अलगाव का सिद्धांत’ लाते हैं तो बरबस फुले की विचारधारा और उनके रंगकर्म के प्रभाव की तरफ ध्यान चला जाता है। भले इसे कोई उल्लेखित न करे, लेकिन ये इतिहास है, अकाट्य तथ्य है कि ब्रेष्ट के इस ‘अलगाव का सिद्धांत’ का उत्स कहीं है तो वो फुले के नाटकीय विचारधारा में है। इसे संयोग कहिये या फुले के नाटक के प्रतिरोधात्मक प्रभाव, जब सन 1873 में फुले मराठी में संवाद शैली में ‘ गुलामगीरी’ लिख रहे थे, उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ‘ सबै जाति गोपाल की ‘ प्रहसन के द्वारा क्षत्री और पंडित दो चरित्रों के संवादों के माध्यम से शास्त्रों के अंतर्विरोधों को उजागर कर वर्ण- जाति व्यवस्था को बेनकाब कर रहे थे। उसी क्रम में सन 1881 में लिखा गया उनका कालजयी प्रहसन ‘अंधेर नगरी ‘ भी है। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि फुले जिस अंदाज से ब्राह्मण वर्ग द्वारा फैलाये जा रहे धार्मिक पाखंडों का भंडाफोड़ कर रहे थे, उसके प्रभाव से हिंदी रंगमंच बचा नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस प्रहसन में बजाप्ते ‘जातवाला(ब्राह्मण)’ नाम से एक पात्र है जो बाजार में चिल्ला – चिल्लाकर अपनी जात बेच रहा है। वो कह रहा है, ‘जात ले जात, टके से जात। एक टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाय और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच करै। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिन्दू से क्रिस्तान…’।
फुले की तरह अम्बेडकर नाट्यविधा से डायरेक्ट तो नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन रंगमंच के प्रति लगाव राजनीति के क्षेत्र में आने के पूर्व से ही रहा है। जब वे ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस’ में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे तो मराठी रंगमंच की गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखते थे। अखबारों में प्रकाशित नाटकों की समीक्षा पढ़कर अम्बेडकर ने कई बार उन नाटकों की प्रतियां डाक से मंगवाई थी। महाड़ चवदार तालाब के सत्याग्रह हेतु अम्बेडकर धन – संग्रह कर रहे थे तो इस अभियान से जुड़कर मा. बाबूराम पेंढारकर, मा. सखाराम नारायनकाज रोलकर, मा. निर्मल लिबाजी गंगावणे ने अपनी नाटक मंडलियों द्वारा नाटक खेला और धनराशि जमा किया। लेकिन इन मंडलियों द्वारा जिस विषयवस्तु वाले नाटक मंचित किये जाते थे, अम्बेडकर उससे सहमत नहीं हो पा रहे थे। अतएव इस ढंग से धन इकट्ठा किये जाने को उचित नहीं समझा। भक्ति पर आधारित नाटक के मंचन से जमा किये गए धन से अम्बेडकर को सत्याग्रह के तमाशा होने की आशंका लग रही थी। वे नाटक मंडली से दलित – पीड़ितों के अधिकार पाने के लिए संघर्ष के जज्बे की अपेक्षा रखते थे। लेकिन 15 जून 1936 को जब चितरंजन नाटक मंडली ने ‘बॉम्बे थिएटर’ में आप्पा साहब टिपनिस लिखित ‘दक्खन का दीया‘ के मंचन को देखने के लिए अम्बेडकर को आमंत्रित किया तो गए। अम्बेडकर के आने की खबर से थिएटर में दर्शकों की इतनी भीड़ हो गयी कि नाट्यगृह में चींटी को भी प्रवेश करने के लिए जगह नहीं थी। अम्बेडकर का ये कथन गौर तलब है कि ‘मेरे दस भाषणों के बराबर एक नाटक होता है।’ नाटक की ताकत अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे इसलिए जब भी किसी सांस्कृतिक संस्थाओं ने बुलाया, जरूर गए। बोधिमंडल के तत्वाधान में 20 नवम्बर 1955 को जब प्रा0 चिटणीस द्वारा लिखा गया नाटक ‘ युग यात्रा’ होने वाला था, आमंत्रण आने पर स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद नाटक देखने आए थे। सविता अम्बेडकर ने कहा था कि सर्दी में ज्यादा देर तक जगे रहने से तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए बीस – पच्चीस मिनट तक ही रहेंगे। नाटक के आयोजक भालचंद वराले ने कहा कि ‘हम बाबा साहेब के बैठने के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां उन्हें सर्दी नहीं लगेगी।’ चिटणीस ने उस नाटक में रामायण काल से लेकर वर्तमान कालखंड तक अस्पृशयों की जो दीन-हीन दशा थी, उस यथार्थ को इतनी जीवंतता से मंच पर उतारा की अम्बेडकर सर्दी, ठंडी हवाओं को भूल हो गए। 8.30 बजे जो नाटक शुरू हुआ था, जब तक खत्म नहीं हुआ, तन्मय होकर देखते रहे। नाटक पर खुलकर बोले। सभी कलाकारों और चिटणीस की प्रशंसा की। भालचंद की अगुवाई में मंडली के कलाकारों के साथ फोटोग्राफी भी करायी। इस नाटक से इतने अभिभूत थे कि पुनः इसका मंचन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऐतिहासिक धर्मान्तर समारोह में भी मंचित करवाया।
जयशंकर प्रसाद की कहानी ‘विरामचिन्ह’ और प्रेमचंद की ‘सदगति’, ‘ठाकुर का कुआँ’, ‘घासवाली’, ‘मन्त्र’, ‘कफ़न’, ‘मंदिर’ और ‘गोदान’ उपन्यास का ‘मातादीन – सिलिया’ प्रसंग पर अम्बेडकर के राजनीतिक आंदोलनों के असर से इंकार नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता के सवाल पर गांधी और अम्बेडकर के बीच जो बहस या कहे विवाद था, साहित्य उसे अपने एंगल से विश्लेषित कर रही थी। परंतु इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि साहित्यकारों – संस्कृतिकर्मियों का एक बड़ा वर्ग गांधी के पक्ष में ही था जो कहीं न कहीं यथास्थितिवाद को ही स्थापित कर रहा था। कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियों पर प्रहार करने से इन्हें कोई परहेज नहीं था, हां वर्णव्यवस्था को खारिज करने में हिचक जरूर दिख रहा था।
सन 1936 में अम्बेडकर के धर्म छोड़ने की घोषणा से राजनीतिक हलकों में उथल – पुथल तो मचा ही, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भूचाल आ गया था। प्रेमचंद ने ‘मंत्र’ नाम से जो दूसरी कहानी लिखी वो इसी पर केंद्रित थी। नया थिएटर के निर्देशक हबीब तनवीर की ‘जमादारिन’ ( परिवर्तित नाम ‘पोंगा पंडित’)नाटक की प्रस्तुति पर जगह – जगह हिन्दू कट्टरवादियों ने बवाल मचाया था, अवरोध उतपन्न किया था, स्टेज पर चढ़ कर तोड़ – फोड़ की थी, प्रतिबंध लगवाया था, वो इसी काल में रचा गया था। सम्भवतः लोक कलाकारों ने मिलजुल कर सामूहिक रूप से गढ़ा हो। हबीब तनवीर मिजाज के वामपंथी थे लेकिन दूसरे वामपंथियों की तरह वर्ग को लेकर जड़ नहीं थे, वर्ण भी भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा है और इसकी अवधारणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस सत्य को भली- भांति जानते थे। तभी तो वे ‘चरणदास चोर’, ‘आगरा बाजार’,‘सड़क’, ‘बहादुर कलारिन’, ‘हिरमा की अमर कहानी’ और ‘देख रहे हैं नयन’ जैसे नाटक करते हैं, उपेक्षितों – वंचितों – हाशिये के समाज को अपने नाट्य संसार का पात्र बनाते हैं।
शंकर शेष ने ‘एक और द्रोणाचार्य’ में एकलव्य जैसे मिथक के माध्यम से वर्णवादी व्यवस्था को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया था। दूसरा नाटक ‘पोस्टर’ भी इसी तेवर और अप्रोच का था। सन 90 तक आते – आते दलित चेतना का स्वर और तल्ख हो गया। शायद इसकी वजह देश में दलितों पर हो रहे जुल्म और प्रतिरोध में दबे – कुचले लोगों का लामबंद होना हो। स्वदेश दीपक का लिखा नाटक ‘कोर्टमार्शल’ जो सन 90 में साहित्य कला परिषद, दिल्ली द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया था और 1 जनवरी 1991 में रंजीत कपूर के निर्देशन में प्रथम मंचन किया गया था; हिंदी का सम्भवतः पहला नाटक है जिसमें दलित संवेदना इतनी गहराई से व्यक्त है कि हर तबके के दर्शकों के बीच स्वीकार्य है।
स्वामी अछूतानंद ‘हरिहर’ ने सन 1922 से 1932 तक जिस नाटक मंडली के माध्यम से नॉटंकी शैली में फरूखाबाद के आस – पास दलितों को जगाने का अभियान चलाया, उसका नाम भी ‘दलित थिएटर’ ही रखा था। इसमें जो अभिनय करने वाले कलाकार थे, सब दलित समुदाय के ही थे।
आज अगर शहर के रंगमंच पर शरणकुमार लिम्बाले की आत्मकथा ‘अक्करमाशी’ को रणधीर कुमार नए मुहावरे के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस मुहिम में लगे रंगकर्मियों का एक दूसरा तबका है जो इसके समानांतर गांवों में सक्रिय है। वह दलित थिएटर का नया समाजशास्त्र तैयार कर रहा है। अपना सौंदर्यशास्त्र गढ़ रहा है। वह जानता है कि जिस समाज में उसे नाटक करना है वहां शहरों की तरह न स्टेज, प्रकाश, प्रेक्षागृह उपलब्ध होगा न संस्कारी दर्शक। वे जानते हैं कि उन्हें बस्ती के उस उपेक्षित टोले में करना है जहां लोग सदियों से वर्णव्यस्था के यातनागृह में कैद है, उन्हें इंतजार है ऐसे कोरस के स्वर का जो उन्हें जगा सके। अगर जग गए तो ये कहा जा सकता है कि अम्बेडकर की विचारधारा का कुछ तो प्रभाव पड़ा है। चाहे माध्यम रंगमंच ही क्यों न हो?

लेखक धारा के विरुद्ध चलकर भारतीय रंगमंच को संघर्ष के मोर्चे पर लाने वाले अभिनेता,निर्देशक और नाटककार जो हाशिये के लोगों के पुरजोर समर्थक हैं सम्पर्क- +919453737307 rajeshkr1101@gmail.com
.
.
.
सबलोग पत्रिका को फेसबुक पर पढने के लिए लाइक करें|