
इतिहास और साहित्य की चेतनात्मक सम्भावना
दुविधा के इस दौर में एक ओर समाज शास्त्री हैं जो इस परिस्थिति में पैदा हो रही बौद्धिक चुनौतियों को समझने में लगे हैं और दूसरी ओर अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, टेक्नोक्रैट्स, और अन्य विशेषज्ञ हैं जो आने वाली तकनीक की उभरती सम्भावनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और इसकी बहुमूल्यता को समझने में लगे हैं। विचारणीय यह है कि क्या अब इस सब के बीच इतिहास और ऐतिहासिक चेतना अपना मूल्य खो रही है और क्या मानवीय मूल्य अपनी प्रमाणिकता का आधार अब डाटा या फिर तकनीकी दुनिया के हवाले कर अपनी वास्तविकता को नये सिरे से सम्बोधित करेंगे?
पीछे मुड़ कर देखें तो पिछले पचास वर्ष मानवीय इतिहास में बहुत आमूलचूल परिवर्तन वाले दौर रहे हैं। किसी भी दूसरे दौर में ऐसा परिवर्तन सम्भवतया नहीं हुआ होगा। तकनीकी अविष्कार तो प्राचीन काल से ही होते रहे हैं लेकिन जो अविष्कार हाल के पचास वर्षों में हुए हैं,वे महत्त्वपूर्ण हैं। इन आविष्कारों का सामाजिक स्तर पर उनकी मानवीय चेतना पर पड़ते हुए गहरे असर के साथ साथ नैतिक और सामाजिक निष्कर्षों पर गम्भीर राय पूरी तरह से बन ही नहीं पायी है। इन अविष्कारों की चकाचौंद भव्य है और गति अभूतपूर्व तेज़ जिसके वास्तविक, मनोविज्ञानिक और सभ्यागत सन्दर्भ अभी पूरी तरह समझे ही नहीं गये हैं और आगे का दौर सामने खड़ा है। इंस्टाग्राम और यू ट्यूब के दौर में समाज, राजनीति, संस्कृति आदि की हर समय नयी परिभाषा बन रही है जिसमें हर कोई अपनी वास्तविकता और अपने व्यक्तित्व की छवि खोज रहा है। इसलिए डाटा आज केवल साइंस ही नहीं है बल्कि एक बाज़ार भी है और आने वाले समय की चेतना भी। सवाल यह भी है कि क्या बौद्धिक समृद्धि के इस दौर में नये मूल्य केवल एक ऐतिहासिक गलती हैं जो शायद आने वाले समय की आपदा बन सकते हैं या फिर इसमें कुछ ऐसी सम्भावनाएँ भी शामिल हैं जिनसे इतिहास का एक नया दौर शरू हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास और साहित्य की बनती नयी दिशा से लगाया जा सकता है।
इतिहासकार बुद्धिजीवियों की माने तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इतिहास का सरोकार केवल समय की परिस्थिथियों को समझने से नहीं बनता बल्कि हर समय की अपनी महत्वाकांक्षाएँ और चेतनाओं का संग्रह ही इतिहास का रुख तय करती हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि चेतना को सींचने में, सांचने में, और ढालने में इतिहास का बहुमूल्य योगदान हमेशा से ही बना रहा है लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत कुछ ऐसा भी है जो इतिहास द्वारा मिश्रित किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। इसलिये केवल इतिहास को सच का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता जिसमें से वास्तविकता की सभी सम्भावनाएँ तलाश की जा सकें। पर दूसरा पहलू यह भी है कि इतिहास के बिना चेतना अपने आप में क्या है जिससे वो अपनी वास्तविकता की कोई ज़मीन तलाश करने की स्थिति पैदा कर सके।
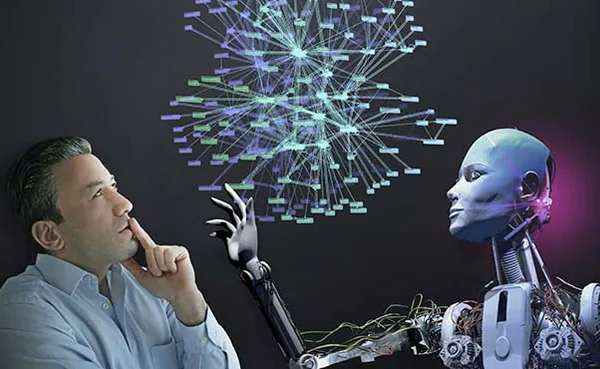
इन परिस्थितियों में ऐतिहासिक चेतना दर्शन यानी फलसफे पर आश्रित हो कर सच को ज़यादा करीब लाने की सम्भावना पैदा कर सकती है। कहा जा सकता है कि कृत्रिम मेधा और डाटा साइंस आने वाले समय में इतिहास के सच को ज़यादा तथ्यात्मक करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारे आत्म चिन्तन में प्रच्छन्न पक्षपाती पूर्वग्रह, पाखंड, निहित रुचियाँ और नस्ली हित, जो हम खुद से भी छिपा कर रखते हैं, इन सब ऋणात्मक भावों को स्पष्ट करने में यह आविष्कार काफी मददगार साबित हो सकता है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता हैं कि इंसानी मूल्यों को सच के करीब पुहंचने के लिये अब ज़यादा तथ्यात्मक होना पड़ेगा जिसको कृत्रिम मेधा और डाटा साइंस बुहत हद तक ज़यादा मुमकिन बना सकते हैं।
एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भाषा, खास कर अंग्रेज़ी भाषा, का प्रयोग अबतक एक खास वर्ग के मूल्यों को स्थापित करने में कार्यगर रहा है और इसके द्वारा ज्ञान की राजनीति भी होती रही है। आने वाले समय में ज्ञान प्राप्त करने की सभी प्रक्रियाएं भाषा के वर्चस्व या फिर भाषा की शिलपकारी पर आधारित नहीं रह सकेंगे बल्कि ज्ञान अब सच मुच प्रयोगसिद्ध आनुभविक प्रमाणों द्वारा निश्चित होगा। इसलिए साहित्य भी अब बदलेगा और काव शास्त्र भी। इस बात के संकेत अभी से नज़र आ रहे हैं कि बिना ठोस तथ्यों का साहित्य या फिर रचनात्मक बोध में छलावी आत्ममुग्धता का आकर्षण पैदा करने वाला साहित्य शायद अब सामाजिक मनोविज्ञान के लिये एक मूर्खता ही नहीं बल्कि बचकानी निरर्थकता का बोध माना जा सकता है। भाषा के पंडितों के लिये भी यह एक चुनौती का विषय है कि अब केवल भाषायी उत्कृष्टता अपने आप में कोई ज्ञान नहीं होगी। अब बहुत से लेखक ऐसे भी होंगे जो भाषा विशेषज्ञता की योगयता को आसानी से पार कर गम्भीर संवाद रचाने में सक्षम हो सकेंगे।

भाषा मनोविज्ञान द्वारा स्थापित विचारात्मक एकाधिकार जो अब तक भाषा के पंडितों के हाथ में रहा है आने वाले समय में ज़यादा सम्भावनाओं के साथ अन्वेषण योग्य होगा। इन पंडितों के लिये बड़ी समस्या यह हो सकती है कि अब संवाद और बोध केवल भाषा पर निर्भर नहीं होगा। अब भाषा विशेषज्ञता का तलिस्म तभी चलेगा जब वह किसी ठोस बौद्धिक उत्कर्ष पर संवाद बनाने लायक होगा। दूर से देखें तो शायद यह ऐसे प्रतीत हो सकता है कि भाषा विशेषज्ञता और भाषा मनोविज्ञान अपना वर्चस्व और शायद अपना मायना ही नये सिरे से तलाश करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन भाषा का संवाद या भाषा पर संवाद अब तभी संभव होगा या यूँ कहें कि होना चाहिये जब भाषा के पंडित अपनी सुस्त पड़ती जिज्ञासा को किसी कठोर परिश्रम द्वारा लगातार सिर्जीवत रखने की चेष्टा करें। बड़ी चुनौती इन विशेषज्ञों के लिये यह भी होगी कि भाषा विशेषज्ञता द्वारा निश्चित किये प्रतीकात्मक विधान को अब कैसे खंडित होने से बचाया जाए। यह प्रतीकात्मक विधान ही तो हैं जो भाषा द्वारा समाज, संस्कृति और राजनीति में अपना वर्चस्व बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि भाषा का वर्चस्व विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अपनी पकड़ सामूहिक मनोविज्ञान को प्रभावित करने में बहुत लम्बे समय तक कामयाब रहा है। लेकिन तकनीकी अविष्कारों ने इस वर्चस्व को कम ही नहीं किया है बल्कि भाषा विशेषज्ञता पर आधारित अहंकार, जो अपने अगले पड़ाव में नस्ली संवेदनाओं को जनम देती है, को एक बड़ा धक्का दिया है। इस लिहाज़ से किसी समतावादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ते एक बड़े कदम की तरह भी तकनीकी अविष्कार की अहम भूमिका हो सकती है।
इस सब के बाद यह सवाल भी है कि तकनीकी विकास की इन खूबियों के इलावा क्या कुछ ऐसा भी है जो अभी हमारे सामने तो हो पर शायद बुहत स्पष्ट तौर पर इस पर गौर नहीं किया गया हो? ऐसी एक समस्या जो हमें देखने को मिल रही है वह यह है कि तकनीक हमारे संवेदनाओं को संकुचित करते हुए स्वयं से विमुख यानी एलेनेट कर रही है। आज का युवक और आने वाले समय का मानव भीड़ में अकेला हो रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड आज की सच्चाई है और शायद आने वाले समय का अभिशाप भी। हमें आज दोस्तों की ज़रुरत नहीं है और शायद आने वाले समय में परीवार की भी नहीं होगी। ऐसा होने की भी सम्भावना है कि परीवार अब एक ज़िम्मेदारियों का बोझ समझा जाए और इंसान कि पूर्ण स्वतन्त्रता में एक रूकावट भी। कॉन्टेंट और फॉर्म यानी ठोस तथ्यात्मक मूल्यों और उनके प्रकट रूप में हम सिर्फ तथ्यात्मकता को ही सर्वश्रेष्ठ पदवी पर देख रहे हैं। आने वाले समय में यह सेल्फ-एलीनेशन यानी आत्म अलगाव एक भव्य रूप धारण कर एक गम्भीर समस्या बन सकती है और आज की प्रगतिवादी मेट्रो संस्कृति में मानसिक स्वास्थ्य से जुडी अवसाद जैसी बीमारियों में इसके लक्षण साफ़ देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक तौर पर मनुष्य और मानवीय अनुभूति में जो फर्क संवेदना की वजह से बनता है वह ही अगर कम हो जाए तो मशीन और मानव में कुछ ख़ास अंतर नहीं रहेगा।

इन चुनौतियों के बीच आज हम उस दोराहे पर खड़े हैं कि जिस पर आगे सिर्फ एक ही ओर बढ़ जाना किसी विकल्प की बात नहीं रही है। यह सच्चाई है जिस से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। हाँ मनुष्य के पास एक ऐसी क्षमता ज़रूर है जिससे वह इतिहास का रुख बदल सकता है और बदलता रहा है। वह क्षमता जिसे हम शायद इतिहास में कहीं पीछे छोड़ आये हैं उसे हम ‘पराभौतिक सूक्षम्ता’ यानी मेटाफिज़िकल इनजैनुइटी के नाम से समझ सकते हैं। इस पराभौतिक सूक्षम्ता से नये निज़ाम और नया दर्शन बनाया जा सकता हैं जो ऐतिहासिक परिस्थितियों में शायद ज़यादा लाभदायक हो सके। ऐसे ही चेतना को पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि स्पाट स्थूलता, जिसकी हमारे चेतना को आदत सी हो चुकी है, से ऊपर उठ कर सहज-ज्ञान की विवेकशील सम्भावना भी पैदा हो सके। यह सहज ज्ञान ही होगा जो चेतना को अपने मूल अस्तित्व कि पहचान करवा सकता है और उसके बढ़ते मशीनीकरण को एक चुनौती देते हुए इतिहास को सर्जनात्मक बनाने में अपनी अहम भूमिका प्रदान कर सकता है। इतिहास शायद अब इन्ही मायनों की नयी तलाश कर रहा है और अब हमें शायद उन मायनों को मूलयवान बनाना होगा जिन पर ऐतिहासिक संदेह करना आज पहली बार एक भूल प्रतीत हो रहा है। हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर तो अभी नहीं पहुंचा जा सकता, हाँ पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि संवेदना का वह दौर शायद आज हमारे सामने है जिसकी हम एक अरसे से तलाश कर रहे हैं।
सारांश में कहें तो यह बात स्पष्ट है कि कृत्रिम मेधा के प्रयोग से उभरती विश्वसनीयता और इसकी संभव चुनौतियों के दो पक्ष हमारी समझ को बाँट रहे हैं। लेकिन पूरी परिस्थिति पर पकड़ बनाने के लिये हमें शायद एक तीसरे पक्ष की भी ज़रुरत है जो इन दोनों पक्षों में मध्यस्थता कर सके। यह तीसरा पक्ष इन दोनों पक्षों की सच्चाई को भी ध्यान में रखे और इन दोनों की विशेषता को मिटाये बिना ज़्यादा पेचीदा सम्भावनाएँ तलाशने की कोशिश करे। यह पेचीदा सम्भावनाएँ अनुभव के विरोधाभास की जटिलता को भी ध्यान में लें लेकिन इनमें सर्जनशीलता की सम्भावना को पहल दें जिसे प्रोफेसर जगदीश सिंह ‘अनुभवी दुपक्षता’ कह कर सम्बोधित करते हैं। यह अनुभवी दुपक्षता एक सरल स्तरीय विश्लेषण की समझ से नहीं पैदा होगी इसके लिये समय के दोनों सिरों को देखने के साथ साथ दोनों स्तर यानी इतिहास और परा-इतिहास में कृत्रिम मेधा की वास्तविकता और प्राभौतिकता दोनों को ध्यान में रख कर ही खोज के नये अनुसंधान पैदा करने होंगे। यह मानवीय क्षमता की परम कठोर और चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी है जिसे उतनी ही पेचीदगी से सुलझाने में बुद्धिजीवियों की तनावपूर्ण परीक्षा होगी। इतिहास, भाषा, साहित्य, और चेतना को अब नयी सम्भावनाएँ तलाशनी होंगी जिसमें इंसानी मन की रोमांचक परवर्तीयों को कुछ समय के लिये पीछे रखना होगा और इस बात पर गम्भीर अध्यन करना होगा कि हमारी परिकल्पना में क्या बाजार ही परम सच्चाई होगी जो कृत्रिम मेधा द्वारा हमारा भविष्य निश्चित करेगी?
