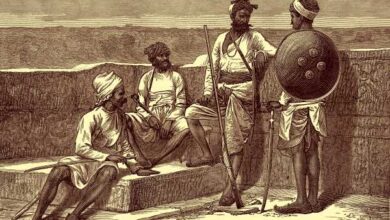कट्टरता का समाजशास्त्र
हमारा समाज बहुत तेज़ी से सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों को घटित होते बेरहमी से देख रहा है और तमाम तरह की महत्त्वपूर्ण विभीषिकाओं को अपने भीतर जज़्ब कर रहा है। इस दौर में चारों तरफ खंजर-ही-खंजर दिखाई पड़ रहे हैं। कट्टरता, क्रूरता, अलगाव और नंगेपन का ज़हर देश की फिजा में इस कदर फैल चुका है कि कोई ठीक से साँस तक नहीं ले पा रहा। मनुष्यता के किसी भी कोने में न नैतिक-बोध दिखाई देता है और न ही दूर-दूर तक असहमति के स्वर सुनाई देते हैं। जाहिर है कि मानवीयता रोज क्रूरता और कट्टरता के सामने रौंदी और कुचली जा रही है। प्रश्नवाचक है तो जबावदेही गायब है। हमारा हर क्षण तनाव और दहशत में बीत रहा है। सत्ता हर चीज को पालतू बना रही है।
हिंसा का दहकता लावा देश और समाज के हर कोने में बह रहा है। असहमति इस दौर का भयावह लोक है। देश के संवैधानिक मूल्य, बहुलता, न्याय के प्रति आस्था और हमारी विविधता को बाँझ बना दिया गया है। विकृतियों को एक संस्थान के रूप में विकसित कर दिया गया है। यदि मूल्यों की बात की जाती है या नैतिकता की तो लगता है कि यह किस ज़माने की बात हो रही है। हम एक बहुत बड़े बाज़ार में हैं। हमारा सब कुछ बाज़ार में बिक रहा है। बाज़ार हमें पूरी तरह से लील रहा है। हम विस्तार से सिकुड़न में आ चुके हैं। जो अभी तक बिक नहीं सका था वह बड़े बाज़ार में आख़िर बिक ही जाएगा। हम संकीर्ण मानसिकता में हैं; विडंबनाओं और अंतर्विरोधों में हैं। हम असहिष्णुता के दायरों में हैं। ग़ालिब ने सच ही कहा है— होता है शाबो रोज तमाशा मेरे आगे। 
इस दौर में भारतीयता की किसी को चिंता नहीं और उसकी व्याख्याएँ मनमाने ढंग से की जा रही हैं; जिनका रिश्ता सत्ता पाने और उसे सुरक्षित रखने का ज्यादा है। भारतीयता पर राष्ट्रभक्ति के जय-जयकार का निरन्तर उद्घोष जारी है। कट्टरता, क्रूरता और नंगापन इस दौर में हमारी जीवन-रेखा बन चुके हैं। जो आतताई, हिंसक मनुष्यता-विरोधी हैं, वही तरह-तरह की बातें हवा में उछालते रहते हैं। अपने को लगाकर बेहतर साबित करने के लिए वे भी मूल्यों की बात करते हैं। हमारी जिन्दगी में आत्मछवियाँ हैं; लेकिन उनके तकाज़े भी हैं। भारतीयता धुप्पल में नहीं हो सकती। सत्ता जिन्दगी की जड़ों को नहीं देखना चाहती। उसका मकसद हमें वास्तविकता से साक्षात्कार करने की जगह भ्रमित करना है। आदर्शों, लक्ष्यों और मूल्यों के लिए हमारे मन में रत्ती भर जगह नहीं। भारत में जो कुछ है उसे हमने बड़े संघर्ष से पाया और आत्मसात किया है। उन कठिनाई से पाई चीज़ों को हम अपने मजे के लिए गँवा रहे हैं।
सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय नहीं होते। बहुस्तरीय पहचान और बहुआयामीपन की ओर उसके कदम भी होते हैं और दिशा भी। समाज और देश कभी भी संकीर्णता से नहीं चल सकते। उनका उदार होना निहायत जरूरी है; क्योंकि अनुदार मनोविज्ञान, संकीर्णताएँ अंततोगत्वा हमारी सांस्कृतिक विरासत को ही ख़त्म कर देगा। जाहिर है कि हमारा बड़बोलापन और चुप्पियाँ हमारे अस्तित्व को ही लील रहे हैं।
कृष्णा सोबती ने इंगित किया था कि— “हम यह न भूलें कि हमारी संस्कृति का प्रमुख पक्ष विचार–स्वातंत्र्य ही रहा है। यह तब भी मौजूद रहा, जब हम दूसरों के अधीन थे। विचार की इस लंबी प्रक्रिया ने ही भारतीय दर्शन और चिंतन को विशेष बनाया है। यही भारतीय संस्कृति और जीवन–शैली का मुखड़ा है। विभिन्न समाजों के प्रभावों को आत्मसात करने की स्वभावगत क्षमता और लचक ने भारतीय संस्कृति को सांस्कृतिक घनत्व प्रदान किया है।“
इस महादेश में बच्चों को शिक्षित करने की समस्या बड़ी विकट है। जब आचरण ही नहीं है तो उनके सामने जो आचरण पेश किया जा रहा है; जिसमें नोच-खसोट और नीचता की पराकाष्ठा भी है और आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चे हवा-हवाई माहौल या यूँ कहें कि बिना आदर्श के शिक्षित नहीं हो सकते। जो ऐसा सोचते हैं वो गीली लकड़ियों में तुरन्त आग या ऊर्जा की परिकल्पना करते हैं। जब आदर्श ही नहीं बचे, नैतिकता का देश-निकाला हो गया तो उनका आचरण ठीक-ठाक हो, यह मात्र धुएँं में लट्ठ मारने जैसा ही है।
नैतिक शिक्षा से बच्चों को आचरणवान नहीं बनाया जा सकता। मैं सत्तर वर्ष पार कर चुका हूँ; अभी भी मेरे बड़े, शिक्षक मेरे आराध्य और आदर्श हैं और मेरी आत्मा में निरन्तर झंकृत होते रहते हैं। जब छात्रों के सामने ही उनके गुरुओं की ठँसाई होती है तो वे क्या सीखते होंगे या उनके सामने माता-पिता और बड़े झूठ बोलें तो बच्चा क्या सीखेगा या ग्रहण करेगा। आचरण पोथियों और ग्रंथों में भले हो; वह यदि हमारे आचरण में नहीं है तो कोई क्या सीख सकता है। किस पवित्रता और और सदाचरण की बात आप कर रहे हैं। ये आसमान से बरसने वाली चीजें नहीं है; बल्कि इसी ठोस धरती में पलती हैं। इनका कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता।
कवि कुमार अंबुज ने सही कहा— “जो हमारे आदर्श थे वे घोड़ों की रेस में तब्दील हो गये।“ अध्यापक पूर्ण सिंह का शायद एक निबंध पढ़ा होगा— आचरण की सभ्यता। उसे मैने हायर सेकंडरी में पढ़ा था— “आचरण केवल मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता। उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिसकर बनता है; उसके फूल तो सूर्य की गरमी और समुद्र के नमकीन पानी से बारंबार भीगकर और सूखकर अपनी लाली पकड़ते हैं।“ (सरदार पूर्ण सिंह)
किसी चीज़ को पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। किस जमाने की बात आप ले बैठे। परम लंठई के महारास में हम आचरण की सुगंध खोज रहे हैं। जैसे कोशिश करने वालों के सपने भी होते हैं और आचरण भी वैसे ही कट्टरता के भी अपने कीर्तिमान और शिखर हैं और कट्टरता के समाजशास्त्र को अपनी सफलता का आधार मानकर जिन्दगी में आगे बढ़ने वाले इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि जब तक उनके पास कट्टरता रूपी महाअस्त्र है वो नीचता और नग्नता के नए मापदंड स्थापित करते रहेंगे और उनके नाम का डंका बजता रहेगा। समाज के लिए कुछ करने की जिजीविषा लेकर जीने वाले कट्टरता के इस समाजशास्त्र का तोड़ ढूँढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं; लेकिन उनकी कोशिशें नक्कारखाने में तूती की आवाज ही साबित हो रही हैं। कट्टरता सत्ता से गले मिलकर अमरबेल की तरह उसके साथ लिपटी हुई है। 
कट्टरता को ठीक-ठीक परिभाषित करना कठिन है। कट्टरता क्रूरता और अमानवीयता के विकट घेरे में है। कट्टरता के दौर में भी कट्टर-से-कट्टर भी अपने को कट्टर नहीं मानना चाहता। फिर सोचिए, उसकी पहचान-परिधि क्या है और उसके साथ-साथ क्या-क्या कनेक्ट है। अपराधी तस्कर माफिया कहता है कि वह ऐसा नहीं है। तड़ीपार झूठे मनोविज्ञान की अपनी स्वनिर्मित दुनिया है। जो हमेशा अपने इशारों पर दंगे कराते थे वे संत-महात्मा का चोला ओढ़कर अच्छे होने को प्रमाणित करने पर तुले हैं। वे यह भी कहते हैं कि देखो, दंगे नहीं हो रहे हैं। उसका रकबा बहुत बढ़ा है; जिसमें हत्याएँ, तस्करी, लूटपाट और न जाने क्या-क्या चीज़ें जुड़ गयी हैं। संविधान, मनुष्य और मीडिया, न्याय की हत्या कोई बड़ी बात नहीं है। गंभीरता उनके पास कभी आ नहीं सकती। कट्टरता क्रूरता और अमानवीयता के मनोविज्ञान से संचालित है। कट्टरता के लिए कोई ठोस परिभाषा हो भी नहीं सकती।
कट्टरता एक फेनोमिना भर नहीं है; वह एक जिन्दा हकीक़त है। सच तो यह है कि कट्टरता अपने अलावा किसी और को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होती। कट्टरता क्रूरता, अमानवीयता, असामाजिकता के साथ नत्थी रहती है। कट्टरता अपनी वास्तविकता छिपा लेती है और अपनी आँखों में पट्टी बाँध लेती है गांधारी की तरह। सभी की अवहेलना करना उसका खास गुण होता है। कट्टरता अपने अलावा किसी की नहीं सुनती। परिभाषा मत कीजिए; बल्कि चारों ओर देखिए— जहाँ मनुष्यता, नैतिकता और आचरण नहीं हैं वहाँ इसे आसानी से खोजा जा सकता है। वर्तमान दौर में भी कट्टरता को गूगल या किसी और सर्च इंजन में नहीं ढूँढ़ा जा सकता। कट्टरता से ही नाजीवाद और हिटलर जैसे मनोविज्ञान पैदा और विकसित हुए। कट्टरता की जुड़वा चीज़ें भी हैं— छल-छद्म, राष्ट्रवाद की अँधेरी सुरंग, अंध राष्ट्रवाद की भयानकता भी।
कट्टरता को हम सिद्धांत बनाकर, कानून लाकर नहीं निपट सकते। अपने मत के अस्वीकार करने पर, अपनी बात और महत्त्व को हरहाल में स्वीकार कराना, दूसरों को भाजी-मूली की तरह काटना और गर्व से लबालब होना। कट्टरता, क्रूरता यानी अतिवाद और दूसरे शब्दों में असहमति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करना, अच्छे की एकदम बुराई करना और उसे नेस्तनाबूद करना। महात्मा गाँधी इसके उदाहरण हैं। कट्टरता क्रूरता, मूर्खता, बर्बरता और अपनी महानता और श्रेष्ठता सिद्ध करने में हमेशा जुटी रहती। किसी की आज़ादी को न मानना जनतंत्र को नेस्तनाबूद करना है। संविधान की हत्या के साथ भी उसका घनघोर रिश्ता है। यूँ तो बातें बहुत हैं। कुमार अंबुज की कविता का यह अंश पढ़ें—
“कुछ लोगों ने आदर्श की तरह चुने दु:स्वप्न/युद्ध, सिंहासन/वे भी आदर्श हुए किसी के/और एक दिन पाए गये/ख़ून और कीचड़ से लथपथ।“
कट्टरता, क्रूरता को मौतें परेशान नहीं करतीं, अव्यवस्था विचलित नहीं करती; केवल उसका सोचा हुआ हरहाल में होता रहे। कट्टरता क्रूरता, नंगापन और मूर्खता को सबसे बड़ा आभूषण मानती है। कट्टरता तानाशाही मनोविज्ञान से सब कुछ अपनी मुठ्ठी में कर लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे मनुष्यता में स्वप्न देखने की सादगी को खुशहाल रखने की इच्छा होती है और संकल्प भी उसी तरह कट्टरता का समाजशास्त्र होता है और उसका मनोविज्ञान भी। यूँ तो हम पूरे कहाँ हो पाते हैं। हम जिन्दगी की अनिवार्यता और प्यास में भटकते हुए यात्रा करते हैं। इसके ठीक उलट कट्टरता अपने अलावा सबके ख़त्म होने की इच्छा और एक अलग तरह का उन्मादी या पागलपंथी मनोविज्ञान है; जहाँ मनुष्यता, नैतिकता, बहुलता और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं होता। कभी गाँधी आज़ादी के लिए करो या मरो की संघर्षशीलता लाए थे। कट्टरता हरहाल में अपना विकास चाहती है। उसके यहाँ भी करो या मरो है और या यह संभव नहीं हो तो मारो काटो खाओ। 
इस दौर की विकट समस्या है कट्टरता। यह मीडिया के लिए भले ही शगल हो, कुछ लोगों के लिए बैठे ठाले का धंधा है और सोशल मीडिया पर विद्वता-प्रदर्शन का गोरखधंधा। कट्टरता ने हमारी जिन्दगी को दोजख बना डाला है और अशांति का ज्वालामुखी भी। कट्टरता बहुधा अपनी श्रेष्ठता की दुहाई देते हुए आती है। इसके मारे लोग एक जाल बिछा चुके हैं। कट्टरता से रिश्ता जोड़े रहने वाला आदमी सब के मत को ग़लत साबित करने में लगा रहता है। वह तो स्वयं को सही साबित करने में ही लगा रहता है; बाक़ी झूठ है। जो पूर्व में किया गया है वह एकदम बेकार। दरअसल कट्टरता कई बार हीनग्रंथि का शिकार भी होती है। कट्टरता उदारता की खुलेआम हत्या करने से भी गुरेज नहीं करती। आक्रांता की तरह वो समूची सही चीज़ों को ख़त्म कर वह एक मुश्त आती है। कट्टरता एक तरह की रंगदारी और अपनी सर्वश्रेष्ठता का उद्घोष भी है। वैसे जिन्दगी, मनुष्यता से बड़ा कुछ नहीं है। कट्टरता के मनोविज्ञान की परिभाषा न तो कर सकते और न पहचान सकते।
यह समय प्रतिदिन कट्टरता की दौड़ और क्रूरता के अट्टहास का है। अच्छे की मुनादी झर रही है और कट्टरता का एरिया दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। कट्टरता अक्सर लंपटता के साए में आती है। छोटे-छोटे पहलुओं, कारकों और उपक्रमों में कट्टरता के रूपांकर दिखने को बाध्य हैं। कट्टरता के उत्स निरन्तर विराट रूपों में देखे जा सकते हैं। बाहर-बाहर अच्छा बनने की उद्घोषणा से भी कोई अपनी कट्टरता नहीं छिपा सकता। इस शर्मनाक घेरे में फँसाने के लिए निरन्तर संगठित रूप में जाल बिछाए जा रहे हैं। दु:खद है कि सार्वजनिक मंचों से हत्या करने की, दूसरों को नष्ट करने की बाकायदा घोषणाएँ हो रही हैं तो उसके सांस्थानिक स्वरूप को रोक पाना सहज संभव नहीं हो सकता।
कट्टरवाद की व्याख्या करते हुए हम आतंकवाद और नक्सलवाद का रम्य गुणगान तो करते हैं; लेकिन जो उसका उन्माद फैला रहे हैं, उन्हें नज़र अंदाज़ कर देते हैं और छिपा भी लेते हैं; सांप्रदायिकता भुला दी जाती है और कट्टरता वादियों के इरादे भी भुला दिए जाते हैं। जानना जरूरी है कि विचार की कट्टरता भी भयावह होती है। सहमतियाँ और असहमतियाँ हमारे जीवन की कोख से पैदा होती हैं। कट्टरता के असंख्य कुतर्क हैं और अनंत योजनाएँ भी। समाज में उठने वाले सवालों पर लोककल्याण की योजनाओं पर चुप्पियाँ भाषा को, बोली को और इरादों को जहर का पर्यायवाची बना देना आख़िर क्या साबित करता है? सांप्रदायिकता का जहर और उसकी परिणितियाँ हम सब निरन्तर भुगत रहे हैं और उसका खूनी रूप अरसे से हमें अशांति से भर रहा है। कठमुल्लापन हमारी नस-नस में टहल रहा है। आख़िर यह कब तक चलता रहेगा?