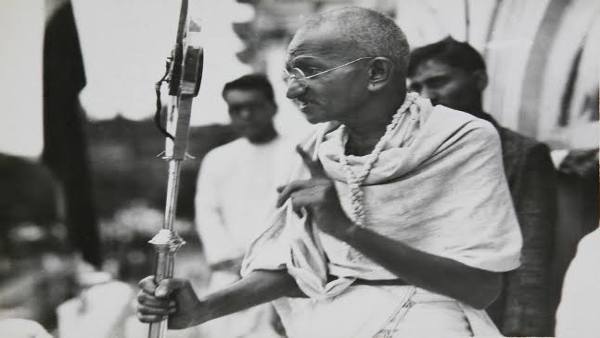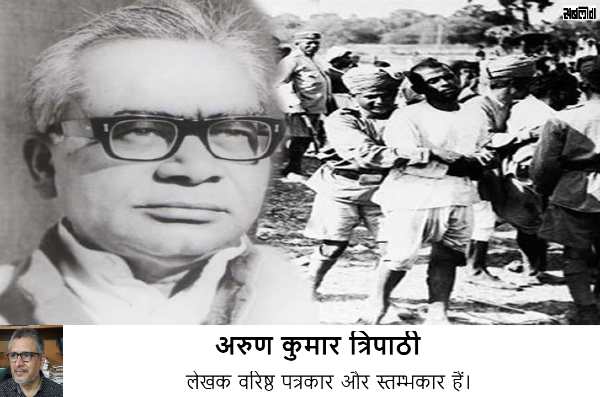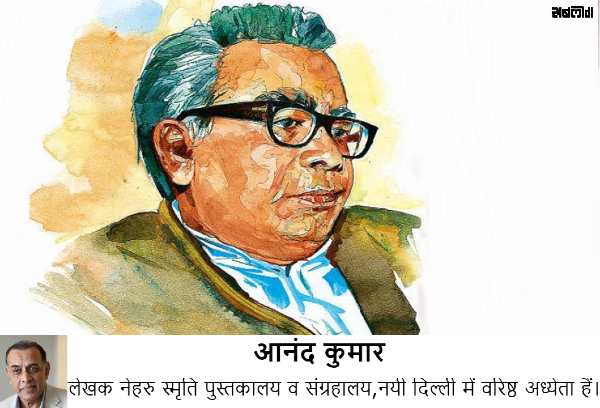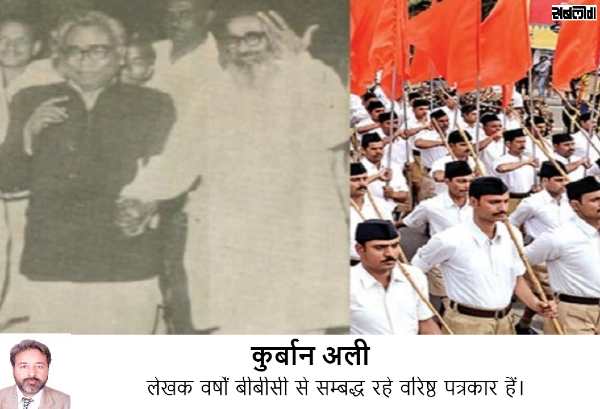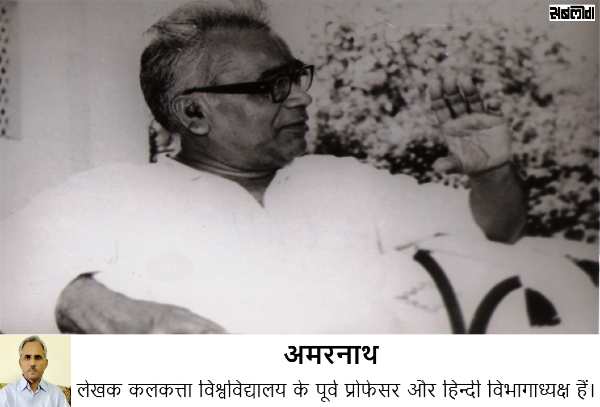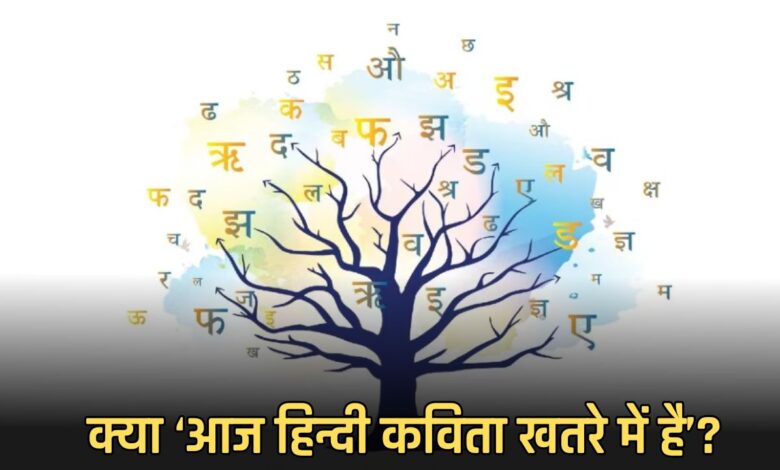
क्या ‘आज हिन्दी कविता खतरे में है’?
इस समय विपुल मात्रा में लिखी जा रही हिन्दी कविताओं पर कुछ भी कहना-लिखना बेहद कठिन है। किसी भी सजग पाठक और आलोचक के लिए इन कवियों की नाम-सूची भी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। कवियों और कविताओं की भीड़ है। कविता-संग्रह अधिक संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं और कथा-पत्रिकाओं में ही नहीं, विचार एवं चिन्तन-प्रमुख पत्रिकाओं में भी कविताओं के लिए अब अच्छी-खासी जगह है। काव्य-पाठ का सिलसिला भी अधिक है और फेसबुक पर भी कविताएँ छायी हुई हैं। कुछ कहानीकार और उपन्यासकार भी कविता की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। निश्चित रूप से इसके सामाजिक-सांस्कृतिक कारण भी हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।
इस समय खतरे में लोकतन्त्र और संविधान है, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है या कविता? क्या सचमुच ‘आज हिन्दी कविता खतरे में है’? यह सोच-समझकर व्यक्त की गयी चिन्ता है या फेसबुक पर नियमित रूप से कुछ भी लिख देने का बौद्धिक विलास? कुछ कवियों-लेखकों को छोड़ कर अधिसंख्य कवि लेखक फेसबुक पर सक्रिय हैं। क्या कभी-कभार हमें फेसबुक पर भी नजर नहीं डालना चाहिए कि इन दिनों वहाँ क्या कहा और लिखा जा रहा है?
सोशल मीडिया में कविता अथवा साहित्य की उपस्थिति पर कुछ भी लिखते समय मुझे विश्व-प्रसिद्ध इतालवी उपन्यासकार, (‘द नेम ऑफ द रोज’ उपन्यास के लेखक) सांस्कृतिक आलोचक,राजनीतिक-सामाजिक टिप्पणीकार उम्बर्तो इको (5.1.1932-19.2.2016) का यह कथन याद आता है कि सोशल नेटवर्क ने उन मूर्खों के एक समूह को बोलने का अधिकार दिया है, जो पहले केवल ‘बार’ (शराबघर) में एक ग्लास वाईन पीकर बोलते और बात करते थे और समुदाय को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अब फेसबुक पर कवियों और कविताओं पर भी बात की जा रही है। जब एक जाना-पहचाना समकालीन हिन्दी कवि अपने फेसबुक वॉल पर यह लिखे कि ‘आज हिन्दी कविता खतरे में है’, तो कविता के सजग पाठकों और आलोचकों के लिए यह कथन विचारणीय है या उपेक्षणीय?
रंजीत वर्मा ने 22 अक्टूबर 2025 को अपने वॉल पर हिन्दी कविता के खतरे में होने की जो बात कही है, क्या हमें उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए? अगर कोई नया कवि कहता तो इसे छोड़ा जा सकता था क्योंकि उसका काव्यानुभव और अध्ययन अभी एक प्रक्रिया में है, पर रंजीत वर्मा चार दशकों से कविताएँ लिख रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ एवं प्रमुख (लगभग) कवि के कथन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। उनकी अपनी काव्य-समझ भी है, जिससे हम सहमत हों या असहमत।
वे हिन्दी कविता को लेकर कुछ अधिक चिन्तित हैं- “आज हिन्दी कविता खतरे में है। यह खतरा हिन्दुत्ववाद का है यानी कि कविता के साम्प्रदायिक होने का है। वैसे यह खतरा नया नहीं है बल्कि यह पैदाइशी खतरा है, मतलब कि तब से जब हिन्दी साहित्य अस्तित्व में आता है।” हिन्दी साहित्य अस्तित्व में कब आया? हिन्दी साहित्य का सामान्य छात्र भी यह जानता है कि यह हजार वर्ष का साहित्य है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा (769 ई.) को हिन्दी का पहला कवि माना है। क्या हिन्दी साहित्य अपने जन्म से ही ‘साम्प्रदायिक’ है?
रंजीत वर्मा हिन्दी साहित्य के जानकार नहीं हैं। वे ‘हिन्दुत्ववाद’ के भी कम जानकार हैं। ‘हिन्दुत्व’ शब्द के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिन्दुत्व विचारधारा के संस्थापक कट्टर हिन्दू, बंगाल में आर्थिक एवं भारतीय राष्ट्रवाद के अगुआ चन्द्रनाथ बसु (31.8.1844 – 20.6.1910) थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘हिन्दुत्व- हिन्दूर प्राकृत इतिहास’ (1892) में इस पद (हिन्दुत्व) का प्रयोग एक पारम्परिक हिन्दू सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया है। चन्द्रनाथ बसु ने इसका प्रयोग ‘हिन्दू धर्म की प्रकृति’ के रूप में किया। ‘हिन्दुत्व’ एवं ‘हिन्दुत्ववाद’ पद के प्रयोक्ताओं को इसके बारे में भी जानने की जरूरत है क्योंकि यह सामान्य पद (टर्म) नहीं है। चन्द्रनाथ बसु का ‘हिन्दुत्व’ सावरकर और संघ-परिवार के ‘हिन्दुत्व’ से भिन्न है।
चन्द्रनाथ बसु के सामने हिन्दू अनुष्ठान, परम्पराएँ और दर्शन था, जबकि सावरकर (28.5.1883- 26.2.1966) ने ‘हिन्दुत्व’ को एक सामाजिक-राजनीतिक अर्थ प्रदान किया। सावरकर का लक्ष्य ‘हिन्दुत्व’ को सामाजिक-राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के एक हथियार के रूप में था। ‘हिदुत्व’ का प्रयोग एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 की अपनी पुस्तिका ‘एसेंशियल्स ऑफ हिन्दुत्व’ में किया है- चंद्रनाथ बसु के प्रयोग से लगभग इकतीस वर्ष बाद। सावरकर ने अपनी इस पुस्तिका का 1928 में पुनर्मुद्रण ‘हिन्दुत्व: हू इज ए हिन्दू’ शीर्षक से किया। 31 छोटे-छोटे अध्यायों (या शीर्षकों) में विभाजित इस पुस्तिका के एक अध्याय का शीर्षक है- ‘हिन्दुत्व इज डिफरेंट फ्रॉम हिन्दूइज्म’।
रंजीत वर्मा जब ‘हिन्दुत्ववाद’ के कारण हिन्दी कविता के खतरे में होने की बात करते हैं, तब उन्हें यह भी जानना चाहिए कि ‘हिन्दुत्व’ और ‘हिन्दूइज्म’ में अन्तर है। हिन्दी कविता किसी भी काल-खण्ड में कभी साम्प्रदायिक नहीं रही। ‘हिन्दूइज्म’ और ‘हिन्दुत्व’ के अन्तर को सावरकर ने स्वीकारा है। ‘हिन्दूइज्म’ पद की निर्मिति ब्रिटिश लेखकों ने 19वीं सदी में की है। अँग्रेजी में चार्ल्स ग्रांट (16.4.1746-31.10.1823) ने 1789 में अपने एक पत्र में इस पद का प्रयोग किया है। ‘हिन्दूइज्म’ के प्रथम प्रयोग के लगभग सौ वर्ष बाद ‘हिन्दुत्व’ पद अस्तित्व में आया। चार्ल्स ग्रांट भारतीय और घरेलू मामलों में प्रभावशाली ब्रिटिश राजनेता थे, जिन्होंने भारत में ‘सामाजिक सुधार’ और ईसाई मिशन के लिए कार्य किया।
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय (22.5.1772-27.9.1833) ने 1816 में ‘हिन्दूइज्म’ का प्रयोग किया। हिन्दू धर्म और ‘हिन्दुत्व’ में अन्तर है, हिन्दू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। यह विभिन्न परम्पराओं और विश्वासों का मिश्रण है, जो ईसा पूर्व लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहले से मौजूद है। सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना जहाँ एक व्यक्ति-विशेष से जुड़ी हुई है, वहाँ हिन्दू धर्म किसी एक व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय से न जुड़कर अनेक ऋषियों, सन्तों और गुरुओं से जुड़ा है। हिन्दू धर्म विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं का मेल है। यह शैव, वैष्णव और शाक्त सम्प्रदायों का संगम है।
रंजीत वर्मा ‘हिन्दूइज्म’ और ‘हिन्दुत्व’ में अन्तर नहीं करने के कारण आरम्भ से ही हिन्दी साहित्य में ‘हिन्दुत्ववाद’ का खतरा देखते हैं। हिन्दी के अनेक कवियों में हम हिन्दू तत्त्व देख सकते हैं, पर उनमें ‘हिन्दुत्व’ और ‘हिन्दुत्ववाद’ देखना कोरा बकवास है। इन पंक्तियों के लेखक ने सावरकर की पुस्तिका ‘एसेंशियल्स ऑफ हिन्दुत्व’ (1923) की प्रकाशन शती (2023) पर लखनऊ से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र – ‘जनसंदेश टाइम्स’ में (17 मार्च 2023) हिन्दुत्व पर विस्तार से विचार किया था। ( देखें, ‘फासीवाद की दस्तक’ 2024, सेतु प्रकाशन, पृष्ठ 191-96)। रंजीत वर्मा ने कुछ समय तक वकालत भी की है। पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 1966 के केस ‘शास्त्री यज्ञ पुरुष दास और अन्य बनाम मूल दास भूदरदास वैश्य और अन्य’ (1966 (3) SCR 242) की अवश्य जानकारी होगी।
इस केस में यह सवाल उठा था कि स्वामी नारायण पन्थ ‘हिन्दूइज्म’ का एक हिस्सा है या नहीं? इस केस में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. वी. गजेन्द्र गड़कर (सातवें मुख्य न्यायाधीश, फरवरी 1964 से मार्च 1966 तक) ने अपने निर्णय में यह लिखा था कि ‘हिन्दूइज्म’ को परिभाषित करना कठिन लगता है, क्योंकि यह दुनिया के अन्य धर्मों की तरह किसी एक ‘प्रोफेट’ में विश्वास नहीं करता और न किसी एक ईश्वर की पूजा करता है। यह न तो किसी एक दार्शनिक विचारधारा का समर्थक है, और न किसी एक धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान का। हम इसे एक जीवन-पद्धति (वे ऑफ लाइफ) के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और कुछ नहीं। स्वामी नारायण केस की सुनवाई पाँच सदस्यीय पीठ ने की थी। मुख्य न्यायाधीश गजेन्द्र गड़कर के अलावा इस बेंच में के. एन. वांचू, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वी.रामास्वामी और न्यायमूर्ति पेनमेत्सा सत्यनारायण राजू थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्वामी नारायण सम्प्रदाय के मन्दिर को हिन्दू मन्दिर माना था और उसमें हरिजनों को प्रवेश का अधिकार दिया था।
कविता पर विचार करने के क्रम में ‘हिन्दुत्व’ और सुप्रीम कोर्ट आदि पर विचार इसलिए आवश्यक है कि कवि रंजीत वर्मा ने ‘हिन्दुत्व’ और ‘हिन्दुत्ववाद’ की बात की है। उनके अनुसार प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन (1936) ने ‘इसी हिन्दुत्ववाद के परखच्चे उड़ा कर रख दिये थे।’ क्या प्रेमचन्द ने 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में कहीं भी हिन्दुत्ववाद का जिक्र किया था? प्रेमचन्द की पंक्तियाँ उद्धृत कर रंजीत वर्मा को अब यह बताना चाहिए कि प्रेमचन्द ने किस तरह अपने भाषण में ‘हिन्दुत्ववाद के परखच्चे उड़ाकर रख दिये थे।’ रंजीत वर्मा के अनुसार “शायद यही वजह रही होगी कि हिन्दी के तथाकथित बड़े नामों की जमात इस सम्मेलन से खुद को बाहर रखे रही।” ‘तथाकथित बड़े नामों’ में से उन्होंने केवल एक नाम ‘निराला’ का लिया है।
रंजीत वर्मा का कथन देखें- “महाकवि कहे जाने वाले निराला तक इसमें शामिल नहीं हुए थे, जब कि स्थापना- सम्मेलन बहुत दूर नहीं, बल्कि लखनऊ में हो रहा था, जो उनके शहर इलाहाबाद के करीब ही पड़ता था। आज हम इन्हें प्रगतिशील कवि मानते हैं।” रंजीत वर्मा निराला को ‘महाकवि’ और ‘प्रगतिशील’ नहीं मानते। ‘महाकवि कहे जाने वाले’ और ‘प्रगतिशील कवि मानने’ की ध्वनि देखें। उन्होंने निराला को पढ़ा नहीं है। उनकी आपत्ति प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन में निराला की अनुपस्थिति के कारण है। बिना उस सम्मेलन में गये निराला ‘प्रगतिशील’ कैसे हुए? कवि कथन है- “आज हम इन्हें प्रगतिशील कवि मानते हैं।”
‘बादल-राग’ कविता 1923 की है, जिसमें निराला ने जन-संघर्ष की ओर संकेत किया था। कवि की पहचान केवल उसकी कविता है। अभी हिन्दी के जो कवि प्रलेस, जलेस और जसम में नहीं हैं, क्या उनमें कुछ कवि प्रगतिशील नहीं हैं? रंजीत वर्मा इस समय किसी भी लेखक संगठन में नहीं हैं। क्या उन्हें ‘प्रगतिशील’ कवि नहीं कहा जा सकता? निराला लगभग दस वर्ष लखनऊ में रहे थे- 1929 से 1939 तक। फिर वे प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन में क्यों नहीं गये? ‘प्रगतिशील आन्दोलन और सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला’ लेख (हिन्दी कविता की परम्परा, वाणी प्रकाशन, 2024) में नामवर सिंह ने लिखा है- “प्रगतिवादी आन्दोलन से न जुड़कर भी निराला प्रगतिशील भूमि से जुड़े थे। निराला की रचना उसी भूमि से उत्पन्न हुई थी।
निराला उसी भूमि से रस लेते थे, जिससे प्रगतिशील आन्दोलन। निराला उस आन्दोलन से न जुड़ सके तो इसका कारण आन्दोलन में शामिल विविध प्रवृत्तियाँ थीं। वह कुछ बौद्धिक लोगों का समूह हो गया था, जो भारतीय जनता की समस्याओं को न समझते हुए भी आन्दोलन कर रहे थे।” (हिन्दी कविता की परम्परा, वही, पृष्ठ 45) लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में निराला क्यों नहीं गये थे? निराला प्रगतिशील आन्दोलन के समर्थक नहीं थे। नामवर सिंह ने लिखा है- “वे आमन्त्रित भी नहीं किये गये थे” (वही, पृष्ठ 44)।
रंजीत वर्मा के अनुसार 1936 के बाद “दूसरी बार हिन्दुत्ववाद के परखच्चे उड़ते हैं 1967 में, जब नक्सल आन्दोलन तेज आँधी की तरह हिन्दी साहित्य में प्रवेश करता है और एक बार फिर हम देखते हैं कि तथाकथित बड़े नाम चुपचाप घर के दरवाजे खिड़कियाँ बन्द कर इस आँधी के गुजरने का इन्तजार करते रहे।” वे तथाकथित बड़े नामों में से एक का भी नाम नहीं लेते। नक्सलवाड़ी आन्दोलन ‘हिन्दुत्ववाद’ के खिलाफ नहीं था। 1967 में चौथे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ के सांसद 14 से बढ़कर 35 हो गये थे, फिर भी उस समय ‘हिन्दुत्ववाद’ की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती।
उन्हें भ्रम है कि 1936 और 1967 का महत्त्व ‘हिन्दुत्ववाद’ के विरुद्ध होने के कारण है, जबकि प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में और नक्सलवाड़ी आन्दोलन 1967 में ‘हिन्दुत्ववाद’ के खिलाफ नहीं था। रंजीत वर्मा ने नक्सलवाड़ी आँधी के गुजरने के बाद बाहर आने वाले कवियों में से केवल अशोक वाजपेयी का नामोल्लेख किया है – “वे वापस आये और तितलियों को पकड़ते हुए कहा- कविता की वापसी। ‘कविता की वापसी’ का नारा अशोक वाजपेयी ने दिया था, जो आज खुद को प्रतिरोध का कवि मनवाने पर तुले हैं और लोग भी हैं कुछ ऐसे कि मान रहे हैं।” नाम लेने से डर क्यों?
फेसबुक के पोस्ट पर इतने विस्तार से लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अब हिन्दी के कुछ कवि और लेखक गलत माहौल बनाने में लग गये हैं। हिन्दी कविता का संसार बड़ा है। समकालीन कवि इतने हैं कि सबको पढ़ना भी सबके लिए सम्भव नहीं है। जो मन में आया, लिख- बोल दिया। यह गलत ढंग का प्रचार है। रंजीत वर्मा ने अपने पोस्ट में जिस ‘हिन्दुत्ववाद’ की बात कही है और उसके लपेटे में निराला को लिया है, वह उनकी नासमझी और बदनीयती का एक ‘उत्कृष्ट’ प्रमाण है। वे निराला के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयत्न दो-तीन साल से कुछ बोलकर और कभी कभी फेसबुक पर सक्रिय होकर कर रहे हैं।
उनके अनुसार अभी हिन्दी साहित्य में ‘हिन्दुत्ववाद’ है। “जिस ‘हिन्दुत्ववाद’ को प्रगतिशील साहित्य ने दो बार परास्त किया, वही ‘हिन्दुत्ववाद’ फिर इधर हाल के वर्षों में सिर उठा कर सामने आ गया है।” उन्हें ‘हिन्दी साहित्य और हिन्दी कविता में हिन्दुत्ववाद’ शीर्षक से एक लेख लिखकर किसी मासिक पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेज देना चाहिए। वे साहित्य में ‘हिन्दुत्ववाद’ लाने के लिए मोदी को दोषी नहीं मानते। शायद वे यह भी मानें कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काव्यप्रेमी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 नवम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में रायपुर पहुँचने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, 2 नवम्बर को रामदरश मिश्र के निधन पर शोक जताया और इसी तारीख को पटना में राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाया(रोड शो के पहले)।
रंजीत वर्मा ने लिखा है कि ‘हिन्दुत्ववाद’ को “लाने का श्रेय उन्हीं तथाकथित बड़े नामों को जाता है, जो 1936 में स्थापना-सम्मेलन में शामिल न होकर और 1967 में घरों में बन्द होकर ‘हिदुत्ववाद’ या कहिए कि साम्प्रदायिक घृणा के बीज को बचाने का काम कर रहे थे। ऐसे प्रगतिशील कहे जाने वाले कवियों और प्रतिरोध के स्वयंभू कवियों से छुटकारा पाने की आज जरूरत है।” कौन है प्रगतिशील कहा जाने वाला और प्रतिरोध का स्वयंभू कवि? उन्होंने केवल निराला और अशोक वाजपेयी के नाम लिये हैं। वे फेसबुक पर आह्वान करते हैं, आइए इनसे छुटकारा पाइए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि फेसबुक पर समर्थकों की भीड़ जुटाने से वे कविता की नेतृत्वकारी भूमिका में नहीं आएँगे।
वे जिस ‘हिन्दुत्व’ की बात बार-बार करते हैं, उसके बारे में यह नहीं जानते कि ‘हिन्दुत्व’ आरएसएस की ‘मार्गदर्शक विचारधारा’ है। निराला और अशोक वाजपेयी इस विचारधारा के साथ नहीं हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने (31 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे) तक उनके पोस्ट को 8 लोगों ने ‘शेयर’ किया है, 63 ने कमेंट्स दिये हैं और 57 ने लाइक किया है। गलत बातें तुरत फैलती हैं, इसलिए भी इन्हें रोकना जरूरी है। फेसबुक पर सक्रिय लोगों मे से बहुत कम लोग पढ़ते-सोचते हैं। निराला के बारे में उनमें से कुछ को छोड़कर अधिक नहीं जानते, वे क्या जानेंगे उन्हें तो रंजीत वर्मा भी नहीं जानते।
निराला की कविताएँ पढ़ना और समझना आसान नहीं है। हिन्दी में ‘स्वीपिंग रीमार्क्स’ अधिक बढ़ रहा है। आत्ममुग्धता चरम पर है। अपने को तीसमार खाँ समझने वालों की संख्या बढ़ रही है।
निराला की ‘तुलसीदास’ कविता को ‘साम्प्रदायिक कविता’ कहना गलत है। “गौरतलब यह है कि निराला 1936 में ‘साम्प्रदायिक कविता’ ‘तुलसीदास’ लिखकर प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन का जवाब दे रहे थे, प्रगतिशीलता को चुनौती दे रहे थे।” यह कविता 1936 की नहीं है और न ‘साम्प्रदायिक’ है। ‘तुलसीदास’ कविता का रचना- काल 1934 है। यह लखनऊ से प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘सुधा’ के फरवरी मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई 1935 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसके एक वर्ष बाद लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन हुआ था।
‘तुलसीदास’ कविता को पढ़े और समझे बिना इस प्रकार की की गयी टिप्पणी यह बताती है कि इस समय बाजार और प्रचार के मोह एवं आकर्षण में हमारे कुछ कवि किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसी टिप्पणी हिन्दी का वह समकालीन कवि कर रहा है, जिसे हम ‘प्रगतिशील’, ‘मार्क्सवादी’ और ‘क्रान्तिकारी’ भी मान रहे हैं। “राम मन्दिर तो वे आज बना रहे हैं, हमने बहुत पहले ही ‘राम की शक्ति-पूजा’ शुरू कर दी थी। आपको क्या लगता है कि बाबर से नफरत करना हम मोदी से सीखे हैं, बिलकुल नहीं। यह नफरत हम कविता में बहुत पहले से पाले हुए थे। विश्वास नहीं होता है, तो ये पंक्तियाँ देखिए-
“मोगल दल बल के जलद-यान / दर्पित पद उन्हें पठान या इसी तुलसीदास, कविता की ये पंक्तियाँ पढ़ें- यों मांगल पद तल, प्रथम तूर्ण / समबद्ध देश – बल चूर्ण – चूर्ण / इस्लाम कलाओं से परिपूर्ण आदि आदि आदि ”
‘तुलसीदास’ कविता को सम्पूर्णता में समझने की जरुरत है।
‘सुधा’ (जुलाई 1933) की सम्पादकीय टिप्पणी एक (1) में निराला ने लिखा था- “आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है। अत: साहित्य के विकास का श्रेय अनेक अंशों में उसे ही प्राप्त है।” आलोचना में-‘शैशव-संलाप’ के लिए स्थान नहीं है। काव्य की बारीकियाँ समझने वाले अब कम हिन्दी कवि और आलोचक बचे हैं।
‘तुलसीदास’ और ‘राम की शक्ति-पूजा’ कविता ‘द्वितीय अनामिका’ में संकलित हैं। ‘राम की शक्ति-पूजा’ इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक पत्र ‘भारत’ में 26 अक्टूबर 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। निराला की सभी कविताएँ नन्द किशोर नवल द्वारा सम्पादित ‘निराला रचनावली’ (राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली,1983) के पहले और दूसरे खण्ड में संकलित हैं। ‘रचनावली’ के पहले खण्ड (1983) में ‘तुलसीदास’ कविता कुल 23 पृष्ठों (पृष्ठ 267 से 289) में और ‘राम की शक्ति- पूजा’ कुल 10 पृष्ठों (पृष्ठ 310 से 319) में हैं। ये दोनों कविताएँ निराला की ही नहीं, हिन्दी की भी महान कविताएँ हैं, जिनपर आलोचकों ने विस्तारपूर्वक विचार किया है।
रंजीत वर्मा ने ‘तुलसीदास’ कविता के जो दो संक्षिप्त अंश उद्धृत किये हैं, वे तीसरे और सातवें चरण के हैं। ‘तुलसीदास’ 100 चरणों की एक लम्बी कविता है। ‘तुलसीदास’ और ‘राम की शक्ति-पूजा’ एक-दो बार पढ़कर समझ में नहीं आएगी। ‘तुलसीदास’ कविता का सजग-सावधान और गम्भीर पाठक उसके 28 वें चरण की इन पंक्तियों – “चलते-फिरते, पर निस्सहाय/ वे दीन, क्षीण, कंकाल काय”, 32वें चरण की ‘दीनों की भी दुर्बल पुकार’ और 96 वें चरण की इन पंक्तियों- “देश-काल के शर से बिंधकर/ यह जागा कवि अशेष छवि धर/ इसका स्वर भर भारती मुखर होयेंगी” को भी याद रखेगा।
‘तुलसीदास’ कविता को पढ़े – समझे बिना ही उसकी दो-चार पक्तियाॅं अपने मनोनुकूल चयन कर उसे ‘साम्प्रदायिक’ कहना स्वयं अपना उपहास करना है। और ‘राम की शक्ति-पूजा’? आश्चर्य है कि हिन्दी का एक वरिष्ठ समकालीन कवि यह लिखता है- “राम मन्दिर तो वे आज बना रहे हैं, हमने बहुत पहले ही राम की शक्ति पूजा शुरू कर दी थी।” अभी प्रियदर्शन ने ‘राम की शक्ति-पूजा’ की उदात्तता से प्रभावित होने की बात कही है।
‘हिन्दुत्ववाद’ की चिन्ता करते हुए आरएसएस, भाजपा और नरेन्द्र मोदी की बात न करने का अर्थ स्पष्ट है। रंजीत वर्मा ने अपने पोस्ट में तीन बार मोदी की सकारात्मक चर्चा की है और एक बार भी आरएसएस और संघ परिवार का उल्लेख तक नहीं किया है। “आपको क्या लगता है कि साहित्य में इस हिन्दुत्ववाद को मोदी लाया है, जी नहीं” और “आपको क्या लगता है कि बाबर से नफरत करना हम मोदी से सीखे हैं, बिलकुल नहीं।” सभी जानते हैं कि मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और ‘हिन्दुत्व’ का सम्बन्ध केवल आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों से है। रंजीत वर्मा ने अपने पोस्ट में मोदी पर कुछ भी नहीं कहा है। उन्हें क्लीन चिट दी है और हिन्दुत्ववाद का दोषी निराला को ठहराया है। वे हिन्दी कविता को ‘साम्प्रदायिक’ और ‘हिन्दुत्ववाद’ से जुड़ा मानते हैं।
ऐसा आरोप लगाने से पहले उन्हें उन हिन्दी कवियों का नाम लेना चाहिए जिनकी कविता ‘साम्प्रदायिक’ है या ‘हिन्दुत्व’ के रंग में रंगी है। उनके सामने ऐसा एक ही कवि है और वे हैं निराला। उन्होंने लिखा है कि निराला “आगे भी हिन्दी कविता में हिन्दुत्ववाद की जमीन तैयार करने में लगे थे।” वे मोदी को दोष नहीं देते। “मोदी को मत दोष दीजिए कि उसके कारण साहित्य का सम्प्रदायीकरण हो रहा है, बल्कि उन तथाकथित बड़े प्रगतिशील कहे जाने वाले और प्रतिरोध के स्वयंभू कवियों को कटघरे में खड़ा कीजिए, जिनके कारण मोदी का सत्ता तक पहुँचना सुगम हुआ।” कविता और राजनीति की उनकी समझ ठीक नहीं है। पहली बात यह है कि हिन्दी कविता को खतरा आत्ममुग्ध कवियों से है, न कि हिन्दुत्ववाद से।
दूसरी बात यह है कि न तो 1936 में और न 1967 में हिन्दुत्ववाद के परखच्चे उड़े। तीसरी बात यह है कि हिन्दी साहित्य और हिन्दी कविता कहीं भी हिन्दुत्ववाद से प्रभावित नहीं है। हिन्दी के कितने कवि ‘हिन्दुत्ववादी’ हैं? चौथी बात यह है कि ‘तुलसीदास’ कविता ‘साम्प्रदायिक’ नहीं है और ‘राम की शक्ति-पूजा’ का राममन्दिर से कोई सम्बन्ध नहीं है। पाँचवीं बड़ी बात, जिसे अब सभी जानते हैं कि मोदी हिंदुत्व और कॉर्पोरेट की जुगलबन्दी के कारण सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे।
अपने पोस्ट में ‘हिन्दुत्व’ और ‘हिन्दुत्ववाद’ से रंजीत वर्मा न तो आरएसएस को जोड़ते हैं, न सावरकर-गोलवलकर को। इस समय उनकी चिन्ता में हिन्दी की समकालीन कविता है, आरएसएस, भाजपा, हिन्दू राष्ट्र का एजेंडा नहीं है। पटना में पिछले दिनों चार दिनों का (25-28 सितम्बर 2025) जो अन्तरराष्ट्रीय साहित्योत्सव हुआ था उसमें सचिव के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में वे शामिल थे, जो अच्छी बात है, पर उन्होंने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है कि चुनाव के पहले ही उन प्रदेशों में ऐसे आयोजन क्यों किये जाते हैं ।
जहाँ भाजपा की सरकार है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादेमी संयुक्त रूप से अन्तरराष्ट्रीय साहित्योत्सव क्यों कर रहा है? क्या सचमुच सरकार को साहित्य से अनुराग है? हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले शिमला में (16 से 18 जून 2022) ऐसा पहला आयोजन हुआ था। दूसरा अन्तरराष्ट्रीय साहित्योत्सव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले (3 से 6 अगस्त 2023 तक) भोपाल में हुआ था और तीसरा ऐसा आयोजन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना में हुआ है, जहाँ उद्घाटन-सत्र और समापन सत्र में मंच पर एक भी लेखक की उपस्थिति नहीं थी। यह सब मोदी के कार्य-काल में ही हो रहा है।
अच्छी बात यह है कि हिन्दी के कई कवि आज भी निराला का महत्त्व समझते हैं। अभी भी हिन्दी में अनेक ऐसे कवि हैं जिनमें आत्ममुग्धता नहीं है। ‘आवाज़ भी एक जगह है’ (2000) ‘में मंगलेश डबराल की एक कविता है ‘ब्रेश्ट और निराला’ (1999)। निराला ब्रेश्ट से बोलते हैं- “मैं लड़ा कुलीनों से ब्राह्मण के घर के व्यंजन छोड़े/ जो असली जन हैं समाज के महॅंगू और झींगुर जैसे/ या इलाहाबाद के पथ की वह मजदूरिन/ उन पर जब लिखा मैंने/ आलोचक बरसे मुझ पर, कइयों ने कहा मुझे पागल/ मरा हूँ हजार मरण।” निराला ने ‘गहन है यह अन्धकारा’ 1942 में लिखी थी और संजय कुंदन ने इसी शीर्षक से इस सदी के 25 साल के 20 कवियों की 75 कविताओं का एक संकलन प्रकाशित किया है। (वाम प्रकाशन, फरवरी 2025) एक ही समय में हिन्दी के दो कवि (रंजीत वर्मा और संजय कुंदन) निराला को जिस तरह देखते हैं, उसे देखा और समझा जाना चाहिए।
संजय कुंदन की चिन्ता में निराला नहीं हैं। उनकी चिन्ता में उदारीकरण की परियोजना, बाजार, सूचना क्रान्ति, साम्प्रदायिक- फासीवाद, भूमंडलीकरण – उदारीकरण, जीवन के बुनियादी मुद्दे, औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट समूह, वित्तीय पूंजी, अधिनायकवादी शासक, लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद, हिन्दुत्व, विकास, गुजरात मॉडल सब है। क्या इन सबका ‘हिन्दुत्व’ और ‘हिन्दुत्ववाद’ से ही सम्बन्ध है? संजय कुंदन ने ‘हिन्दी कविता के प्रतिरोधी स्वर की एक मुकम्मल तस्वीर’ रखने की कोशिश की है। रंजीत वर्मा को चाहिए कि वे 20 ‘साम्प्रदायिक’ और ‘हिन्दुत्ववादी’ कवियों का एक संकलन उनकी कविताओं के साथ निकालें। यह सचमुच एक बड़ा काम होगा,जिसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए।