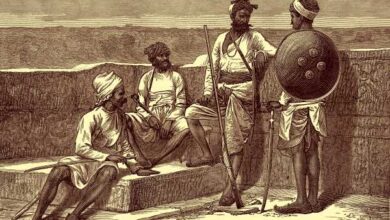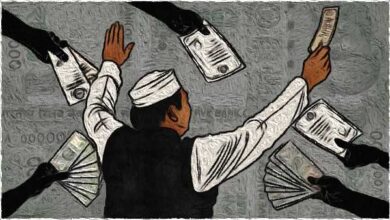गंगा मुक्ति आन्दोलन: समकालीन विमर्श
22-23 फ़रवरी, 2025 को कहलगाँव (भागलपुर) में गंगा मुक्ति आन्दोलन की 43वीं वर्षगांठ का आयोजन हुआ। इस दो दिवसीय समारोह में देश के अन्य हिस्सों में पानी और पर्यावरण पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। लोगों ने गंगा में दीप प्रवाहित कर और नौका जुलूस निकालकर नदी के प्रति अपना सम्मान जताया।
यह आन्दोलन शुरू से ही मनुष्य व् नदी (प्रकृति) के परस्पर आश्रितता के मुद्दे पर बल देता रहा है। अस्सी के दशक से शुरू हुए इस आन्दोलन का मुख्य नारा रहा है – ‘गंगा को अविरल बहने दो’ और सही मायनों में यह नारा उतना ही या उससे कहीं ज्यादा आज भी प्रासंगिक है। किसी आन्दोलन का चार दशक से भी अधिक समय तक समाज में बना रहना उसकी प्रासंगिकता को ही दर्शाता है। हालाँकि इस लम्बे अन्तराल में आन्दोलन की प्रकृति एवं इसके मुद्दों में आए बदलावों पर भी गौर करने की ज़रूरत जान पड़ती है।
आन्दोलन का ऐतिहासिक महत्त्व:
अंग जनपद अर्थात भागलपुर, बिहार का अनुमण्डलीय क्षेत्र है कहलगाँव, जो उत्तरायणी गंगा (सुलतानगंज) से लगभग, 40 कि मी पूरब और पीरपैंती प्रखण्ड के पश्चिम में स्थित है। 1982 में कहलगाँव के कागज़ी टोला नामक मछुआरों की बस्ती से गंगा मुक्ति आन्दोलन शुरू हुआ था । यह सामाजिक आन्दोलन सत्तर के दशक में हुए जे पी आन्दोलन से प्रेरित था जो मुख्य रूप से जलकर जमींदारी के विरोध में आरम्भ हुआ पर धीरे धीरे इसने अन्य सामाजिक मुद्दों को भी अपना हिस्सा बना लिया।
जलकर जमींदारी या पानीदारी कर की प्रथा 300 सालों से इस क्षेत्र (सुल्तानगंज प्रखण्ड से पीरपैंती प्रखण्ड तक का 80 किमी का गंगा क्षेत्र) में चल रही एक विशेष प्रकार की परम्परा थी। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से इस कर का उन्मूलन सम्भव हुआ, जिसे गंगा मुक्ति आन्दोलन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
इस आन्दोलन की दूसरी बड़ी जीत थी घोघा (ग्राम पंचायत) और कहलगाँव के बीच स्थित शंकरपुर दियारे में 513 एकड़ बेनामी जमीन का भूमिहीनों के बीच में बाँटा जाना।
जब 1991 में जलकर उन्मूलन के बाद नदी को फ्री फिशिंग या निर्बाध मछली मारने का क्षेत्र घोषित कर दिया गया, उसी साल कुछ महीनों बाद सुल्तानगंज से कहलगाँव तक का 60 किमी लम्बा हिस्सा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया जो एशिया में लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के लिए मुख्य संरक्षित क्षेत्र है।
डॉल्फिन संरक्षण के कारण स्थानीय मछुआरों द्वारा मछली मारने पर पाबन्दी लग गयी। जिस कारण गंगा मुक्ति आन्दोलन को मछुआरों के हित में आगे भी काम करने की ज़रूरत जान पड़ी। कालांतर में जल श्रमिक संघ नामक एक सामाजिक संस्था का निर्माण किया गया जो मछुआरों की समस्याओं के समाधान हेतु पिछले चार दशकों से प्रयासरत है।
इस वर्ष हुए समारोह में डॉ. फ़ारूक़ अली (पूर्व कुलपति) ने कहा कि बहती नदियों को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। डॉ. पवन सिंह ने बताया कि अभयारण्य की जगह इसका नाम आश्रयणी होना चाहिए था क्योंकि अभयारण्य हमेशा भूमि पर होता है जबकि यह क्षेत्र बहती नदी का एक हिस्सा है, जो गांगेय डॉल्फिन के प्रश्रय के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक निर्धारित क्षेत्र में डॉल्फिन को बाँधकर रखने का विचार भी अपने में अनूठा और गलत है क्योंकि डॉल्फिन निश्चित ही इस क्षेत्र से आगे और पीछे के हिस्सों में जाने के लिए स्वतन्त्र है।
जनपक्षीय मुद्दे एवं प्रयास:
यह आन्दोलन न केवल एक पर्यावरणीय आन्दोलन है बल्कि कला एवं संस्कृति के संरक्षण तथा समाज सुधार के भी प्रयास करता रहा है। यह शरू से ही समतामूलक समाज की स्थापना के विचार से प्रेरित रहा है। मछुआरों की स्थिति में सुधार से लेकर शराबबन्दी (घरेलू हिंसा का मुख्य कारण) तथा जाति उन्मूलक मूल्यों को समाज में शामिल करने का इस आन्दोलन का प्रयास रहा है। वर्तमान में यह आन्दोलन मुख्य रूप से मछुआरों के अधिकारों के लिए – ख़ासकर उन्हें आरक्षण दिलाने के लिए – ‘जल श्रमिक संगठन’ के माध्यम से भागलपुर के साथ साथ अन्य जिलों (जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, इत्यादि) के मछुआरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है।
हाल में हुए आयोजन में शामिल लोगों के लिए डॉल्फिन अभ्यारण्य से जुड़े कुछ अहम मामलों के विरोध में आन्दोलन को मजबूत बनाने का प्रयास एक प्रमुख मुद्दा रहा। उनका कहना है कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए क्रूज़ चलने तथा बाँध और बराज बनाने पर पाबन्दी लगाने की ज़रूरत है न कि स्थानीय मछुआरों को मछली मारने से रोकने की। वर्तमान में मछुआरों पर वन विभाग द्वारा डॉल्फिन संरक्षण के नाम पर मछली मारने पर पाबन्दी है। केवल कुछ ही मछुआरों के पास ज़िला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर मछली मारने का अधिकार है। ऐसे में कई बार बिना पहचान पत्र वाले स्थानीय मछुआरों के पकडे जाने पर उनपर एफ। आई। आर। तथा पुलिस द्वारा मारपीट, इत्यादि की घटनाएँ होती हैं। अनेक मछुआरे अपने परम्परागत पेशे को छोड़कर जीविकोपार्जन के अन्य स्रोत ढूँढने को बाध्य हो रहे हैं। इस आन्दोलन के जारी रहने का एक बड़ा कारण फ्री फिशिंग एक्ट का सही रूप से लागू नहीं हो पाना है।
इस आयोजन के तीन अन्य प्रमुख मुद्दे थे – पहला, गंगा नदी की लगातार बदतर होती स्थिति, दूसरा, गंगा के इलाके में बढ़ता अपराधीकरण अर्थात माफ़िया के लोगों द्वारा स्थानीय मछुआरों पर होने वाले हमले और तीसरा, बाढ़ आने पर कागज़ी टोला तथा भागलपुर के अन्य इलाकों में बढ़ रही भूमि कटाव की समस्या। लोगों ने लगभग हर साल और कभी कभी एक ही साल में दो-तीन बार बाढ़ आने पर होने वाली समस्याओं पर भी चिंता जाहिर की।
अन्य मुद्दे:
एनटीपीसी की राख
शुरुआत में जलकर जमींदारी के विरोध के अलावा एनटीपीसी कहलगाँव के निर्माण को रोकने का प्रयास इस आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य था। हालाँकि, तब इस निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सका और अब इसका दुष्परिणाम कई किलोमीटर में फैले पोंड ऐश (थर्मल प्लांट से निकला मलबा या राख जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है) के रूप में देखा जा सकता है। अब इस राख को आस पास के क्षेत्रों में सड़क निर्माण के काम में लाया जा रहा है। इस क्षेत्र में कैंसर पीड़ितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। डॉ. पवन सिंह ने बताया कि एनटीपीसी के राख के कारण थाली के चावल का रंग भूरा हो जाता है। स्वास्थ्य कारणों से कई लोग अपना निवास स्थान कहलगाँव से बदलकर भागलपुर या अन्य सुरक्षित जगहों की तरफ़ पलायन कर रहे हैं।
फरक्का बराज
यह गौरतलब है कि भागलपुर बिहार के सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित इलाकों में से एक है और यहाँ के स्थानीय लोग इन बाढ़ों का एक प्रमुख कारण फ़रक्का बराज को मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस बराज के बनने से गंगा में गाद की समस्या कई गुणा बढ़ गयी है और नदी की गहराई काफी घट गयी है। साथ ही कई अन्य जलीय जीवों जैसे कछुए, प्रॉन और हिलसा मछली की गंगा नदी में निर्बाध आवाजाही भी बाधित हुई है। ऐसे में फ़रक्का बराज को तोड़ने पर विगत कुछ वर्षों से विमर्श हो रहा है। बंगाल में गंगा भांगन एक्शन समिति नामक संस्था भी इस दिशा में प्रयासरत है और इसके एक सदस्य तरीकुल इस्लाम ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया । सबने एकमत से केंद्र सरकार से फ़रक्का बराज पर छह महीने के अन्दर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। अगर इस दिशा में कारगर प्रयास से बात कुछ आगे बढे तो यह इस आन्दोलन की एक बड़ी जीत होगी।
उपलब्धि और सुझाव
गंगा मुक्ति आन्दोलन का अध्ययन वर्तमान में सामाजिक आन्दोलनों के समक्ष चुनौतियों को समझने में भी मदद करता है। इसमें कोई शक नहीं कि विगत वर्षों में नदी-केन्द्रित इस क्षेत्रीय जन-आन्दोलन ने मछुआरों की आजीविका तथा पर्यावरणीय मुद्दों की जटिलता को लेकर आम जनमानस में जागरूकता बढायी है।
इस आन्दोलन में मूल्यों की व्यापकता है पर सम्भव है उद्देश्यों की यही व्यापकता आन्दोलन को किसी ख़ास दिशा में अधिक प्रयासरत रहने में बाधित भी कर रहा हो। चार दशक से समाज में इसका जारी रहना जहाँ एक ओर इसे निश्चित ही एक शांतिमय आन्दोलन की मिशाल बनाता है वहीँ दूसरी तरफ लगता है कि समय के साथ इसमें एक तरह का ठहराव सा आ गया है। मसलन, हर साल इस आन्दोलन की वर्षगाँठ मनाने की परम्परा कमोबेश एक प्रतीकात्मक घटना जान पड़ती है। साथ ही साल दो साल में एकाध क्षेत्रीय कार्यक्रम करके आगे कोई बड़ा आयोजन करने की योजना बनती है पर इस दिशा में जितनी एकजुटता, नेतृत्व और धन की आवश्यकता है, उसका नितांत ही अभाव जान पड़ता है। एक व्यवहारिक सोच इस लोकपक्षीय आन्दोलन को गति देगा।