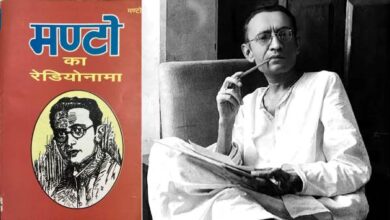एक सच्चे अयोध्यावासी थे शीतला सिंह
शीतला सिंह नहीं रहे। शीतला सिंह अमर हैं। 1947 के भारत विभाजन और फिर 1971 के पाकिस्तान विभाजन (कश्मीर इन्हीं दोनों के भीतर का विवाद है) के बाद इस उपमहाद्वीप के सबसे बड़े विवाद रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के केन्द्र में खड़े होकर उसे देखने, उसके साक्षी और भुक्तभोगी बनने और उसके समाधान के लिए एक सूत्रधार व पंच की भूमिका निभाने वाले शीतला सिंह सिर्फ पत्रकार नहीं थे। वे सिर्फ `जनमोर्चा’ अखबार के सम्पादक ही नहीं थे। वे उससे कहीं ज्यादा थे। वे हमारे समाज के सद्असदविवेक थे। अगर हम उनकी पत्रकार वाली भूमिका को प्रधान मानेंगे तो भी वे पराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह उन मनीषी पत्रकारों की श्रेणी में पहुँच जाएँगे जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में कभी क्रान्तिकारियों का साथ दिया तो कभी गाँधी जी का। कभी जान पर खेलकर अखबार निकाला तो कभी राजनीति में कूद कर अपनी वाणी और कर्म के बीच की दूरी मिटायी।

अयोध्या आन्दोलन के समय पत्रकारों ने तमाम भूमिकाएँ निभायीं। कुछ तो आन्दोलन को भड़काने और बाबरी मस्जिद को गिरवाने में लगे थे। कुछ समाधान के लिए केन्द्र सरकार और पक्षकारों से सम्पर्क में थे और मानते थे कि अगर समय रहते पहल नहीं की गयी तो विवादों के चलते संवैधानिक सद्भाव का प्रतीक बन चुका बाबरी मस्जिद का ढाँचा कभी भी गिराया जा सकता है। तो कुछ इन सब से अलग धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव पर आधारित जनमत के निर्माण में संलग्न थे और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को लेकर आश्वस्त थे। शीतला सिंह को हम समाधान ढूँढने वाले और धर्मनिरपेक्ष व सद्भाव वाले ढाँचे को मजबूत करने वाले पत्रकार के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वे पत्रकार निखिल चक्रवर्ती और प्रभाष जोशी की तरह से राजधानी दिल्ली में बैठकर अपनी भूमिकाएँ नहीं निभा रहे थे। बल्कि शीतला सिंह और उनकी सहयोगी सुमन गुप्ता, निर्मला देशपांडे जैसे गाँधीवादियों के साथ ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रह कर और अपनी जान जोखिम में डालकर उस समस्या और विवाद का समाधान ढूँढ रहे थे। इसी के साथ वे स्थानीय नागरिकों और साधु सन्तों के विवेक को भी अपना अवलम्ब बनाए हुए थे।
तात्कालिकता से अलग अयोध्या विवाद के बहाने अस्सी के दशक के मध्य से खड़ी हुई राजनीति को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं। एक तो वह चिन्तन धारा है जिसका सम्बन्ध मार्क्सवाद से है और जो धर्म को राजनीति से दूर रखने की हिमायती है। वह किसी भी तरह से धार्मिक मामलों पर न तो राजनीतिक बात करना पसन्द करती है और न ही उसे अपने विमर्श में शामिल करके उससे कुछ सीखना या उस पर किसी को कुछ सिखाना चाहती है। उस धारा के तमाम लोग छह दिसम्बर 1992 तक यह मानते रहे कि फैजाबाद और अयोध्या की जनता पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। राम मन्दिर आन्दोलन कुछ लोगों का शिगूफा है और उसका कोई असर होने वाला नहीं है। अगर किसी ने ढाँचे को तोड़ने की कोशिश की तो लोग उसे स्वयं ही रोक लेंगे। दूसरी धारा अयोध्यावादियों की है। जिसने योजनाबद्ध तरीके से अयोध्या विवाद को भारतीय राजनीति का केन्द्रीय एजेंडा बनाया और पूरे समाज को हिन्दू- मुस्लिम, उदार और कट्टर और इतिहास और मिथक के आधार पर विभाजित कर दिया। उसके लिए अयोध्या विवाद पूरी इतिहास दृष्टि का विवाद है, राजनीतिक दृष्टि का विवाद है, राष्ट्रवाद का विवाद है और इसके माध्यम से उस हिन्दू राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है जो 1947 में महात्मा गाँधी की हत्या के बाद जागृत लोकविवेक के कारण बनने से रह गया था।

तीसरी धारा अयोध्यावासियों की है। यह धारा पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक सभी को स्थानीय आधार पर निर्धारित करने और उससे विकास और समाज नीति तैयार करने के पक्ष में रहती है। यह ग्राम स्वराज की धारा है, यह विकेन्द्रीकरण की धारा है और यह राष्ट्रीय विवेक को क्षेत्रीय विवेक का विस्तार ही मानती है न कि क्षेत्रीय विवेक को राष्ट्रीय विवेक का मातहत कारकून। किसी ने ठीक ही कहा है कि `न्यूज इज लोको लोको लोको।’ इसी के तहत शीतला सिंह मानते थे कि खबर स्थानीय ही होती है। बाद में उसके राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयाम विकसित होते हैं। फैजाबाद जिले में महात्मा हरगोविंद जी द्वारा 5 दिसम्बर 1958 को सहकारिता के आधार पर शुरू किए गये `जनमोर्चा’ के पत्रकारीय प्रयोग की स्थानीय शक्ति को वे पहचानते थे क्योंकि वे उससे शुरू से ही जुड़े थे। वे यह भी जानते थे कि यह स्थानीयता अपने में राष्ट्रीयता की सम्भावना रखती है। वे आये थे धर्मनिरपेक्षता की वामपन्थी धारा से लेकिन अयोध्या में रहते हुए और भाँति- भाँति के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों से गुजरते हुए धर्म और धार्मिक संस्थाओं के महत्त्व को समझते थे। वे अयोध्यावासी इस मायने में थे कि वे चाहते थे कि अयोध्या विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व के सहयोग से हो जाए और इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं और शक्तियों की आवश्यकता ही न पड़े न ही राष्ट्रीय वातावरण विषाक्त हो। लेकिन अयोध्यावादियों की शक्ति उन पर भारी पड़ी और अयोध्यावासी हार गये।
एक अयोध्यावासी के रूप में शीतला सिंह के प्रयासों का साक्षी उनका अपना ग्रन्थ `अयोध्याः रामजन्मभूमि-बाबरी-मस्जिद का सच’ तो है ही साथ ही अयोध्या के निवासी और उनका अपना अखबार जनमोर्चा भी है। वे लिखते हैं—`रामजन्मभूमिःबाबरी मस्जिद विवाद को निपटाने के लिए बनी समिति की पहली बैठक जनमोर्चा कार्यालय के सभाकक्ष में 26 फरवरी 1986 को हुई। उसमें लगभग पचास लोगों ने उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत किये।’ इसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग थे। इस बैठक में तमाम बातों के अलावा जो आदर्श उभर रहा था वह था वर्धा के सत्यार मन्दिर का आदर्श। वर्धा के सत्यार मन्दिर के लिए भूमि गाँधी के सहयोगी जमनालाल बजाज ने दी थी। उसमें एक ही मंच पर राम, सीता, कृष्ण, ईसा मसीह, जरथुस्र, शिव पार्वती और लक्ष्मी विराजमान हैं। इसी मंच पर मक्का मदीना की तस्वीरें भी लगी हैं। गौतम बुद्ध और मार्क्स को भी स्थान दिया गया है। इसकी एक अनुकृति अयोध्या के गुजरात भवन में बनाई गयी थी। उसका अयोध्यावासियों ने स्वागत किया था। लगता है शीतला सिंह के मन में कुछ ऐसा ही था।

शीतला सिंह ने अपनी इस पुस्तक में मन्दिर निर्माण के लिए होने वाली कई महत्त्वपूर्ण पहल का जिक्र किया है। उसमें उप्र के तत्कालीन मुख्यमन्त्री वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी से वार्ता का जिक्र है तो प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंहराव और अर्जुन सिंह से हुई वार्ताओं का वर्णन है। वे बताते हैं कि किस प्रकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर की पहल पर दोनों पक्षों में बात बन गयी थी और विहिप के नेता अशोक सिंघल भी तैयार हो गये थे लेकिन दिल्ली से भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि हमें मन्दिर थोड़े ही बनाना है। वह तो कभी भी और कहीं भी बन जाएगा। हमें तो दिल्ली में सरकार बनानी है। इस तरह एक बार फिर अयोध्यावासी हार गये और वहाँ की शान्ति और सद्भाव को भंग करने का मार्ग तथाकथित राष्ट्रवाद की संकीर्ण राजनीति ने प्रशस्त कर दिया। इसी के साथ वे यह भी लिखते हैं कि पत्रकारिता का काम आग लगाना नहीं बल्कि समाज की रचना और मानवतावादी स्वरूप का निर्माण करना है। शीतला सिंह के पास अयोध्या आन्दोलन पर इतनी जानकारी और इतना अनुभव था कि वे चाहते तो इस पर विदेशी प्रकाशकों के लिए पुस्तकें लिखकर भारी रायल्टी और नाम कमा सकते थे। ऐसे प्रस्ताव पड़े ही हुए थे। क्योंकि जनमोर्चा का कार्यालय तमाम विदेशी पत्रकारों का अड्डा हुआ करता था। लेकिन उन्होंने अयोध्या को बेचा नहीं। उनके लिए अयोध्या की समस्या प्रोफेशन से ज्यादा एक मिशन से सम्बन्धित थी। वे उसका समाधान चाहते थे न कि उस पर धन्धा करना।
वास्तव में जब लोग यह कहते हैं कि पत्रकार लोकतन्त्र का पहरेदार है वे उसकी भूमिका को कम करके आँकते हैं। पत्रकार तो सामाजिक ताने बाने को रोज बुनने वाला एक जुलाहा है। जो जानता है कि कौन सा धागा किस धागे के साथ बुनना है और कौन सा रंग कहाँ चढ़ाना है। वह इंगला, पिंगला ताना भरनी और सुषमन तार को भी चीन्हता है। इस तरह शीतला बाबू सद्भावपूर्ण समाज के एक जुलाहे थे जो अपने सहकारी संस्थान के करघे पर रोज एक सद्भावपूर्ण समाज की चादर बुनते थे। यह बात अलग है कि अयोध्यावादियों की हिंसा और घृणा की राजनीति ने अयोध्या के इस जुलाहे की बुनाई को अप्रासंगिक कर दिया। उसकी चादर को चीर डाला। ऊँची ऊँची काटन मिलों के पॉलियस्टर के कपड़ों के आगे मेहनत और ईमानदारी से बुने गये सहकारिता के वस्त्रों कीमत इस समाज में निरन्तर घटने लगी।
पत्रकारों के पैकेज बढ़ने लगे, गाड़ियाँ लम्बी होने लगीं। वे सत्ता के उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों से शीतला बाबू की तरह यह कहने के लिए नहीं मिलते कि अयोध्या में उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया जो विहिप के विरोधी थे? या जिन लोगों ने मुस्लिम घरों को तहस नहस किया और उसमें रह रहे लोगों को जिन्दा जलाया वे खुले आम क्यों घूम रहे हैं? बाजारवादी पत्रकार इसलिए मिलते हैं कि उनके समूह का विज्ञापन औरों से कम क्यों है। ऐसे ही लोगों के कारण आज नवीकरण के नाम पर अयोध्या और फैजाबाद जैसी नगरी ध्वस्त हो जाती है और कोई बोलने वाला नहीं रहता। अयोध्यावासियों की यह हार देश की स्थानीयता की हार है। न्याय और विवेक की हार है। यह पराड़कर जी के 1925 में वृंदावन में दिए गये मसीहाई वक्तव्य का सच होना है। जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता समृद्ध होगी पत्रकार अमीर बनेंगे लेकिन उनकी स्वाधीनता नहीं होगी। इस बदलते माहौल में भी शीतला बाबू जब तक रहे एक सच्चे अयोध्यावासी की तरह स्थानीयता, मानवीय संवेदना, सद्भाव और सत्य के लिए लड़ते रहे। उनकी पत्रकारिता हर गाढ़े अँधेरे समय में समाज को प्रेरणादायक रोशनी देती रहेगी।