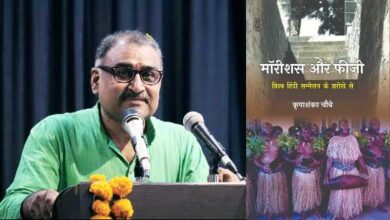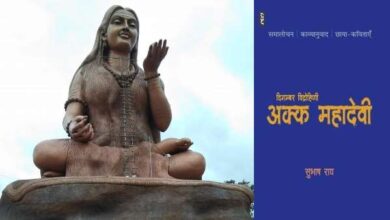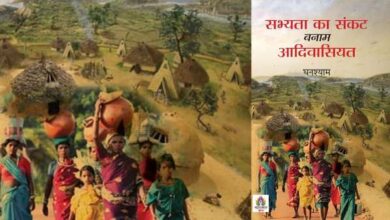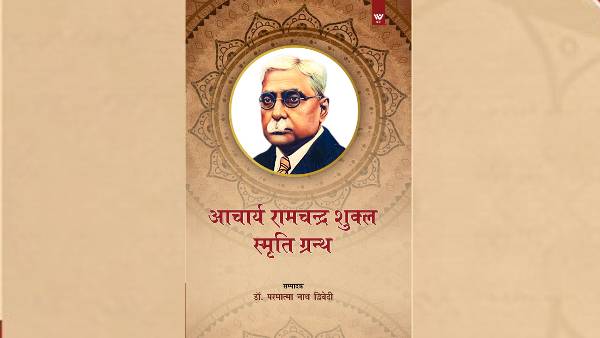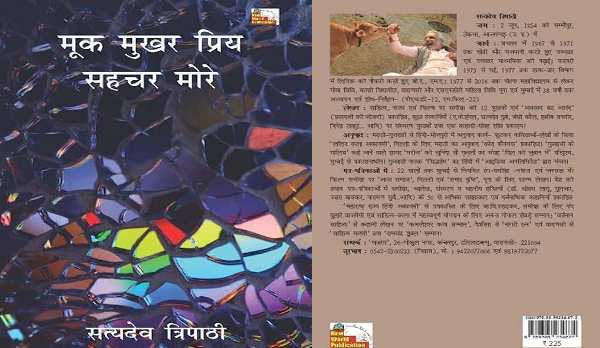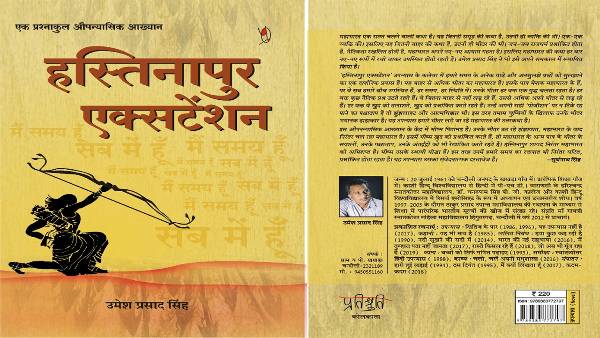
महाभारत की केंद्रीय नारी-दृष्टि पर उठते सवाल…
‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ : एक काव्यात्मक पुनराख्यान
डॉ. उमेश प्रसाद सिंह लिखित ‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ ‘महाभारत’ की कथा का विवेचनात्मक आख्यान है। यह साहित्य की एक अभिनव विधा भी है और रूप एवं प्रवृत्ति भी। हालाँकि लेखक ने मुख पृष्ठ पर इसे ‘एक प्रश्नाकुल औपन्यासिक आख्यान’ कहा है, लेकिन आरम्भ कविता से होता है। फिर आगे का पूरा आख्यान सच ही बेहद प्रश्नाकुल है, परंतु औपन्यासिक नहीं। अपनी प्रकृति में ही व्याख्यापरक है और भाषा तो लगभग काव्यमय है और कथा तो क्लासिक है ही। शुरुआत के अध्याय तो नितांत काव्यमयता से पूर्ण हैं, जो धारा उत्तरार्ध में काफ़ी क्षीण हुई है। और अंतिम हिस्सों में तो काव्यत्व काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि महाभारत पर आधृत आख्यान में ऐसी ही भावाकुलता पूरी पुस्तक हो भी नहीं सकती। लिहाज़ा आगे के काव्यत्व की कमतरता विषयानुरूप है। फिर भी सिर्फ़ भाषिकता के लिए भी इसे पढ़ा जा सकता है और पढ़ने वाला क़तई निराश नहीं, बल्कि समृद्ध होगा। और वह यदि ज़रा भी साहित्यिक रुचियों वाला हुआ, तब तो अद्भुत आनंद आ जायेगा…। यह भाषा का भी कमाल है कि बहव: प्रचलित महाभारत की कथा ‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ में अभिनव हो उठी है..।लेकिन इसी से नितांत असाहित्यिक याने आम पाठक के लिए नहीं है यह कृति।
दूसरे, इसमें भरी पड़ी हैं – लेखक की अंतर्दृष्टि से उपजी उद्भावनाएँ, जिनके बिना सब कुछ के बावजूद इस पर लिखने की बात मुझसे शायद न बनती…। यह लिखना ‘अकोरहा’ – याने न किसी पत्रिका ने समीक्षार्थ भेजा है, न ही लेखक ने कहा है – याने मामला बिलकुल स्वैच्छिक है। चोपड़ाजी के ‘महाभारत’ की तरह पूरी कथा को देखने का माध्यम यहाँ भी समय है, जिसे ‘समय की आँखें’ कर दिया गया है, जो कृति में है तो काफ़ी, लेकिन छायी नहीं है – सभद्रा कुमारीजी के ‘है भादों घटा, किंतु छायी नहीं है’ की तरह…।
शुरुआत ऋषि पाराशर की औचक ही सत्यवती नामक धीवर-कन्या के साथ भेंट से होती है – ज़मीन पर नहीं, जल पर। सो, परिवेश व मिलन-प्रसंग दोनो ही नितांत भावात्मक हैं। ऊपर मेघ-आच्छादित आकाश…नीचे उफनती नदी…तिरती नौका में निबिड़ एकांत…और अकस्मात भेंट का कुतूहल…। इस प्रकार यह भेंट तप के ताप का नैसर्गिक सौंदर्य की तरलता से साक्षात्कार है। इन सबसे उद्दीप्त काम के आवेग और ऋषित्व के आभिजात्य का मनोरम सुयोग है…। फिर भाषा भला काव्यमय न होती, तो क्या होती….!! ऋषि के आमंत्रण में यह भावमयता मुखर होती है – ‘रूपसि, मै भाव को जानता हूं। मुझे भाव को धारण करने में, भाव में निमग्न होने में कोई ग्लानि नहीं है। कोई हीनता-बोध नहीं है। मुझे अपने भाव से अतीत स्थिति में कोई गर्व नहीं है। सब कुछ सहज है प्रिये! मै काम के वश में नहीं हूँ। कामिनि, मैंने काम को स्वीकार किया है। काम को अपने में आश्रय का दान दिया है हृदय-हारिणि! आपकी कृपा के बिना मेरा दान सफल नहीं होगा…’ आदि-आदि। इस पर सत्यवती की तरफ़ से सांसारिकता की बाधा मुखरित होती है, जिसे निरस्त करती हैं – ऋषित्व की महिमा… पहले तो सत्यवती की देह से उठती मछली की गंध, जिसके कारण उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी है, ऋषि के तप-बल से कमल की सुवास में बदल जाती है। उसका नाम ‘सुगंधा’ हो जाता है। यह सुगंध योजन दूर तक जाती है, जिससे वह ‘योजनगंधा’ अभिधान से भी विलसती है। ऋषि के अनुसार ‘सृष्टि में कुछ भी असम्भव नहीं है। इसका रचयिता परम स्वतंत्र है’। सो, इनका समागम भी संसारी होने के बावजूद संसारेतर, देह में निवसित होकर भी देहेतर सिद्ध होता है। दो प्राणों के इस महामिलन से ‘तीसरा महाप्राण प्रकट’ हुआ – इस आख्यान का बीज। ऋषि ने काल को कीलित कर दिया, जिससे दस माह का समय दस घड़ी में समाहित हो गया और तीसरा प्राणी जन्मा ही पाँच वर्ष का। इस ‘विस्तारित (बढ़ी हुई) स्थिति’ को लक्ष्य करके ऋषि ने उसे व्यास कहा। इसी तरह काश, लेखक भी कृति को हस्तिनापुर ‘एक्सटेंशन’ न कहके विस्तार कहता…!! अर्थ व प्रभाव बिलकुल कमतर न होता और फ़ालतू की अंग्रेजियत से बच जाती हिंदी, जो आज इसी शोभाचार (फ़ैशन) के चलते नाहक वर्णसंकर हुई ज़ा रही है…। ख़ैर, बालक व्यास को मां के स्तन-पान की ज़रूरत नहीं। सो, बालक को ऋषि अपने साथ ले जा सके और ‘सुगंधा का शील बना रहा, सत्यवती कुमारी ही रही – अक्षत-योनि’।
विवेच्य कृति में लेखक-प्रसूत दोनो –भाषिकता व उद्भावना– विशेषताएँ ही इसकी ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ हैं। यूँ तो यह वैशिष्ट्य व्याप्त है पूरे कृतित्व में, लेकिन जायज़े के लिए उदाहरण लूँगा मैं – भीष्म के गांधार जाने के प्रसंग का…। गांधार-नरेश अपनी सभा को बताते हैं – ‘हस्तिनापुर साम्राज्य के संरक्षक-संचालक महा पराक्रमी, अप्रतिहत योद्धा महामहिम गंगानंदन भीष्म हमारी गांधारी को अपने जन्मान्ध राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए माँगने आये हैं’। सुनते ही राजकुमार शकुनि की अगुआई में सभा का मत – ‘यह असहनीय अत्याचार है, गांधार देश का अपमान है…किसी के घर में घुसकर उसका मान-मर्दन आपराधिक आचरण है…हम उन्हें उनकी कुटिलता का मज़ा चखा देंगे। युद्ध करेंगे…बूढ़े भीष्म को धूल चटा देंगे। हम वीर हैं, मरना जानते हैं’।
इस पर नरेश कहते हैं – ‘मर मिटने का साहस उत्तम है। यह क्षत्रिय की शोभा है…मगर मर जाने भर से आत्मगौरव की रक्षा नहीं हो सकती…ये वही भीष्म हैं, जिन्होंने काशी भूमंडल के सारे सम्राटों को अकेले जीत लिया था। द्वंद्व युद्ध में भगवान परशुराम को भी पीछे हटना पड़ा था।…आज भी उनकी भुजाओं का बल क्षीण नहीं हुआ है, शर-संधान शिथिल नहीं हुआ है। वे गांधारी को माँगने नहीं, हड़पने आये हैं…’। इस प्रकार हस्तिनापुर के नितांत नामाकूल प्रस्ताव एवं महाराज की ग्लानि के असहनीय परिताप के बीच भीष्म के शौर्य के आतंक से पूरा राज्य, राज-समाज पस्त हो रहा होता है…
कि उसी वक्त ‘आँखें बंद किये गांधारी ने देखा’…के विधान का सूत्र बनता है, जिसके साथ भाषा की प्रांजलता का सोता फूटता है और आयाम-दर-आयाम खुलती जाती हैं उद्भावनाएँ – “असमर्थ की आँख नहीं होती…व्यवस्था, विधान, नैतिकता, धर्म…सब केवल शक्ति के श्रिंगार हैं। आँखें केवल हस्तिनापुर के पास हैं, भीष्म के पास हैं। आँख न होने के बावजूद कुमार धृतराष्ट्र के पास हैं। अपने समूचे समय में आँखें सिर्फ़ और सिर्फ़ गंगानदन के पास हैं। देखने के एकमात्र अधिकारी वही हैं।…आँखों को छीनने वाली आँखों को देखने की कल्पना से गांधारी का हृदय काँप गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब गांधारी कभी नहीं देखेगी…। भीष्म का दर्प उसे नहीं देखना। माता-पिता की विवशता उसे नहीं देखनी…गांधार की लज्जा उसे नहीं देखनी…अब वह देखने के लिए नहीं, बस दिखने के लिए है…”। उसने अपने दुपट्टे की तह बनाकर आँखों पर बांध लिया और कहा – ‘सुचरिते, मेरी सखि, मेरा हाथ थाम ले – मुझे सभा भवन की तरफ़ ले चल और राजसभा से कह दे कि वह गांधारी को गांधार की तरफ़ से महामहिम भीष्म के हाथों हस्तिनापर के श्रिंगार के लिए समर्पित कर दे…’
और आप पढ़ते चले जाइए – न विक्षोभ थमता, न पढ़ना विलमता… और न शमित होता शकुनि के विक्षोभ का प्रतिशोध एवं लेखकीय उद्भावना का चरम यह कि समय ने देखा – ‘गांधार से हस्तिनापुर की तरफ़ तीन रथ जा रहे थे –
-भीष्म का रथ, उसके पीछे गांधारी का रथ और सबसे पीछे शकुनि का रथ… याने
-आतंक का रथ, उसके पीछे परिणय का रथ और उसके पीछे प्रतिशोध का रथ…।
और देखने के सूत्र का समापन – ‘एक दूसरे को कोई नहीं देख रहा था – आतंक अंधा, परिणय अंधा, प्रतिशोध अंधा’…!! एक अंधे के लिए एक अंधा दो अंधा उपहार लेकर लौट रहा था…’।
ऐसे तर्क-भाव-भाषा-उद्भावनाओँ से भरी-अँटी पड़ी है किताब। उक्त उदाहरण में भी मैं तो बानगी ही दे पाया हूँ…। उस दो-ढाई पृष्ठों (56-58) का वर्णन पूरा पढ़ लिया जाये, तो भाषा व लेखकीय उद्भावना का स्पष्ट व सहज हृदयंगम हो जाने वाला आस्वाद मिल जाये…।
लेकिन असली उद्भावना या सर्जनात्मकता तो महाभारत की घटनाओं व विशेष रूप से चरित्रों के उद्घाटन में है, जिनका अध्याय-विभाजन भी प्राय: चरित्रानुसार ही है। यदि चरित्रों के नामों से ही अध्यायों के शीर्षक भी दे दिये जाते, तो कृति कर रूप-विधान के सोने में सुहागा हो जाता। इन चरित्रों-प्रसंगों की उद्भावनाओ से निकले मर्म चमत्कृत करते हैं – हाय, यह सब तो हम जानते थे, पर इसमें यह भी निहित है, कभी क्यों न जान पाये…!!
इसका सबसे बड़ा, थोक में मिलता ख़ज़ाना है भीष्म का चरित्र। इसी ने सिंह साहब से ‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ लिखवाया है, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति न होगा, क्योंकि उसके बाद के हिस्सों में न वह आकर्षण आता, न वैसी तल्लीनता बनती…। और हालाँकि प्रायः सभी चरित्रों के अंतस् में झांकने का प्रयत्न हुआ है, लेकिन प्रमुखता के अनुसार इस पूरे कथायोजन को ‘भीष्म बनाम नारी’ या ‘नारियों के प्रति भीष्म-सलूक’ जैसा कोई नाम दे दिया जाये, तो भी बिलकुल असंगत न होगा। सत्यवती, अम्बा-अम्बिका-अम्बालिका, गांधारी-द्रौपदी तक…को मिलाकर तीन पीढ़ियों की स्त्रियों की पीड़ा-अपमान-बर्बादी की ऐसी श्रिंखला बनती है, जो भीष्म की ही करी-धरी (कारस्तानी) है। मैं महाभारत और उस पर लिखे साहित्य व विवेचन का कोई अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए ग़लत हो सकता हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है – व्यास पर्व, युगांत, पर्व, नरेंद्र कोहली की कथा-श्रिंखला एवं क. मा. मुंशीजी लिखित सात भागों में कृष्णावतार …आदि, में याद नहीं आता कि कहीं इस तरह भीष्म को देखा गया हो। सो, यह उमेश प्रसादजी की अपनी मौलिक उद्भावना है। और पढ़ने पर बिना किसी आश्चर्य-शंका-सोच के ये सब सच आईने की तरह साफ़-साफ़ दिखने लगते हैं…।
सत्यवती-प्रसंग को लें, तो इतिहास-पुराण में भीष्म जैसा पिता-प्रेमी पुत्र कोई न हुआ, जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो, लेकिन सिंह साहब के अनुसार ‘सत्यवती के लिए भीष्म का त्याग किसी भीषण अपराध से कम न था। यह त्याग सत्यवती की स्वाधीनाता का हरण करने वाला सिद्ध हुआ। महाराज शांतनु के समक्ष ‘सत्यवती व उसके पिता की हैसियत न थी कि वे इनकार करते…। सत्यवती ने शान्तनु का वरण नहीं किया था, वह भीष्म के त्याग के चलते वरण करने के लिए विवश हुई थी। धीवर की शर्त जितनी कठोर थी भीष्म के लिए, उससे कम न थी सत्यवती के लिए – बूढ़े के साथ जीवन बिताना तो धीवर को नहीं, उस अनिंद्य सुंदरी युवती को ही था। सो, वह भीष्म का अपराध कभी भूल न सकी। भीष्म ने अपने त्याग को बड़ी चीज़ मान लिया। भूल गये कि सिर्फ़ त्याग ही धर्म नहीं होता’।
इसी श्रिंखला में उमेशजी की सत्यवती यह भी सोचती है कि शान्तनु को छोड़कर गंगा गयी न होती, तो शायद वह शांतनु की पुत्रवधू बनकर इस घर में आती – याने त्यागी पुत्र में पति की कल्पना, जो उस उम्र व उन स्थितियों में अस्वाभाविक न थी। सत्यवती की जानिब से शांतनु को भी ठीक ही ढोंगी कहलवाया गया है – ‘तुम ढोंगी हो शांतनु – तुम धर्म का, वात्सल्य का, करुणा का ढोंग रचते हो, जब हत्यारा ही बनना था, हत्या ही करानी थी भीष्म की, तो उस दिन तुमने गंगा को क्यों रोका था? वह तो जनमते ही उन्हें अपने जल में ड़ुबा रही थी…’। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता था कि तब पुत्र-सुख चाहिए था और जब बिना पत्नी के हो गये और अकूत सौंदर्य दिख गया, तो उसी पुत्रेष्णा की तिलांजलि दे दी।
इसके बाद ख़ानदान की भावी नारियों के प्रति भीष्म के किये या उनसे हुए का निष्कर्ष यह – ‘स्त्री क्या कोई वस्तु है, जिसे कभी प्रभुत्व की धौंस से, कभी बल के आतंक से, कभी पराक्रम की प्रचण्डता से, कभी त्याग के दबाव से अपने प्रिय व्यक्ति के लिए भेंट कर दिया जाये…’? और सिंह साहब पूरी पुस्तक में क़रीने से दिखाते हैं कि भीष्म ने जीवन भर यही किया। उनके लिए ‘नारी एक सजीव अस्मिता नहीं, एक वस्तु, एक उपादान बनकर रह गयी। अपने सारे आदर्शों की उच्चता के बावजूद मातृ शक्ति के प्रति भीष्म के अनादर पूर्वक किये कर्म उनकी सारी महत्ता को वस्तुतः महत्त्वहीन बना देते हैं’।
यहीं भीष्म के अचेतन में पनपे उस मनोविज्ञान को भी देख लें, जिसे उमेश प्रसादजी ने सोपान-दर-सोपान उद्घाटित किया है… ‘अपने वृद्ध पिता शांतनु की उद्दाम काम-पिपासा ने भीष्म के भीतर नारी के प्रति कहीं बहुत गहरे वितृष्णा के भाव भर दिये थे। इस भाव ने उनके हृदय से स्त्री के गरिमामय सम्मोहनपूर्ण अस्तित्त्व को विस्थापित कर दिया था। और यह कि वे स्वयं एक प्रणय के अनुबंध के ध्वंस की धरोहर थे – शांतनु ने गंगा के साथ की वचनबद्धता को तोड़कर इस बेटे भीष्म को प्राप्त किया था। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए लेखक कहता है कि शांतनु ने क्या वात्सल्य के लिए प्रेम को ठुकराया था…? नहीं, साम्राज्य की विरासत को सम्भालने याने ‘हस्तिनापुर की वंश-परम्परा की रक्षा और राजगद्दी की सुरक्षा’ का उद्देश्य ही उनके जीवन में शेष रह गया था। इसी के फेर में और सब कुछ बह गया। सिंह साहब ने कहा नहीं, पर क्या ज़िंदगी भर उनका यही करना भी पैतृक देन ही था?
लेकिन इसी रौ में उमेशजी यह तक कह देते हैं – ‘स्त्री के प्रति वितृष्णा के बोध ने भीष्म को स्त्री जाति के प्रति कठोर व क्रूर बना दिया था। अपनी क्रूरता को ढँकने के लिए उन्होंने अपने त्याग का एक आकर्षक आस्तरण पा लिया था। अपनी निस्पृहताओं के आवरण में अपने आचार को छिपाकर उन्हें धर्मसम्मत बनाना उनकी आदत बनती गयी…’। यह बहुत संगत व सही इसलिए नहीं बनता कि यह प्रक्रिया अचेतन की नहीं, चेतन की है और ऐसा कुछ जानबूझकर करने वाला तो भीष्म जैसे महनीय चरित्र के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर अंत में यह कहना किंचित संतुलित भी कर देता है – ‘भीष्म का स्वभाव, उनके स्वभाव के विरुद्ध एक जटिल निर्मिति बनता गया। वह निरंतर बनता ही रहा – बढ़ता ही रहा’…।
भीष्म के ऐसे इरादे व उनकी ऐसी छबि के चित्र उनके हर उस पराक्रम में निहित व प्रयुक्त हैं, जो अपनी वंश परम्परा व हस्तिनापुर राज्य को सुरक्षित रखने के लिए भीष्म ने किये…। इसी क्रम में सत्यवती के बाद जब उसके पुत्र व राज्य के उत्तराधिकारी अपने मरणासन्न भाई विचित्रवीर्य की मृत्यु से पूर्व भोग के लिए एक नहीं तीन-तीन राजकुमारियों (काशी-नरेश की कन्याओं – अम्बा-अम्बिका-अम्बालिका) को लेने जा रहे थे, तो ‘उस लज्जाजनक मार्ग पर तीव्रगति से जाते हुए तनिक भी लज्जित न थे’।…उन्हें भेजने वाला उनका अपराजेय पौरुष था। उनका अप्रतिहत कौशल था। उनका अमित बल था। उनके अमोघ-अचूक अस्त्र-शस्त्र थे। पिता का दिया इच्छा-मृत्यु का वरदान था’। और इसी बल सबको विजित की भाँति निरुत्तर कर देने के बाद भीष्म ने जब तीनो कन्याओं को रथ पर बैठने के आदेश दिये, तो शाल्व से प्रेम करने वाली अम्बा से सिंह साहब ने फिर जो कहलवाया, वह आधुनिक दृष्टि है। आज के सोच व समाज का ज्वलंत सच है – ‘स्त्री, राज्य की तरह कोई वस्तु है क्या भीष्मजी, जिसे आप अपने पराक्रम से जीतकर चाहे जिसे भेंट कर दें? स्त्री एक सजीव सत्ता है महाराज, उसे वरण का प्राकृतिक अधिकार है। आप स्त्री जाति की स्वतंत्रता के प्रति अपराध कर रहे हैं’। इस सिंह-दृष्टि का तब के समाज को भान भी था और यही तो उद्भावना का स्रोत व सर्जक है।
इस प्रकार ‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ भीष्म के समक्ष अम्बिका…आदि पात्रों के माध्यम से महाभारत-युग की आधुनिक व्याख्या है। इसे अम्बा के माध्यम से ही उस युग की भाषा में भी व्यक्त कराया गया है – ‘आपका आचरण एक शूरवीर राजपुरुष का नहीं, एक बलशाली दस्यु का है’। और अम्बा के विरोधी स्वर का अंत इस प्रसंग की आख़िरी परिणति के आलोक में यूँ होता है – ‘आप भूमंडल के समस्त राजाओं को भले अकेले रणभूमि में पराजित कर लें, मगर अम्बा आपसे कभी पराजित न होगी – अम्बा से आपको हारना ही होगा, हारना ही होगा…’। और महाभारत में शिखंडी-प्रकरण इस सच का आधार भी है और प्रमाण भी। पुस्तक में नहीं आया यह सच कि प्रतिज्ञाओं का पालन ही यदि भीष्म का जीवन था, तो अम्बा के अवतार शिखंडी पर वाण न चलाने की प्रतिज्ञा ही उनकी मृत्यु का निमित्त भी बनी…।
इसके बाद की पीढ़ी में गांधारी को भीष्म जिस तरह लाये, उसका वर्णन यहाँ शुरू में ही भाषा व उद्भावना के प्रमाण में आ गया है। अतः अब ‘नारी जाति और भीष्म’ के इस विमर्श के अंतिम सोपान पर द्रौपदी के पास चलें…। चीर-हरण के समय दुर्योधन-दुशासन-कर्ण…आदि सबसे बुरी तरह अपमानित होते हुए वह भीष्म से मुख़ातिब होती है और अपने को पांडवों की पत्नी, कुरूवंश की सम्मानित कुल वधू, पुत्रवधू और उनकी पौत्र वधू होने की हैसियत से उनके अपने वंश व राज्य की सुरक्षा के प्रण के हवाले से राज्य के बँटवारे, द्यूत-क्रीड़ा के अनाचार और अब कुल की ऐसी वीभत्स नंगई को लेकर सारे प्रश्न करती है, जिसमें लेखक के सम्यक् नियोजन व तीक्ष्ण दृष्टि का बेबाक़ कौशल देखते ही बनता है…प्रतिक्रिया में एक बार भीष्म हिलते हैं – लगता है कि उठेंगे, कुछ कहेंगे, पर फिर अपनी जगह बैठे रहकर सिर झुकाए हुए इतना ही कहते है – ‘बेटी, धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। मैं तुम्हारे प्रश्नों के सम्यक्-विवेचन में अपने को असमर्थ पा रहा हूं’…। फिर द्रौपदी द्वारा कृष्ण का आवाहन व आगे की द्रौपदी-कथा जो होती है…के बाद ‘कट टु’ करके…वहाँ चलें….
जहां शर-शय्या पर पड़े हैं भीष्म और वहाँ खड़े हैं समूचे ख़ानदान के लोग। और उन सबके समक्ष डॉ सिंह ने द्रौपदी से पुछवाने का नियोजन किया है – ‘पितामह, चीर-हरण के समय जब मैं बार-बार आपसे धर्म की दुहाई दे रही थी, उस समय धर्म के निर्णय में आपकी धर्मबुद्धि क्यों नहीं प्रवृत्त हो सकी थी? और तब भीष्म से बड़ा ही दक़ियानूसी उत्तर दिलवाते हैं उमेशजी – ‘बेटी, उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरा रक्त और उससे मेरी बुद्धि दूषित हो गयी थी’। लेकिन इस नियोजन का राज़ खुलता है – द्रौपदी के प्रति-उत्तर में। वह भीष्म के दकियानूसीपने को निरस्त करती हुई बड़ी ही वैज्ञानिक टिप्पणी करती है – ‘पितामह! महात्मा विदुर भी तो दुर्योधन का वही अन्न खा रहे थे। क्या अलग-अलग शरीरों में अन्न अलग-अलग रक्त का निर्माण करता है’? और तब पितामह अपने अंतिम क्षण में आज के युग के समक्ष पूरी तरह बेपर्द हुए बिना नहीं रह पाते…।
द्रौपदी का चीरहरण-प्रकरण पूरे युग, समूची मनुष्यता पर जिस कदर भारी है, उसका अहसास महाभारत पढ़ते हुए उतना नहीं होता, जितना ‘हस्तिनापुर एक्सटेंशन’ पढ़ते हुए होता है। यह फ़र्क़ एक के क्लासिक व दूसरे के सामाजिक रचना होने का भी है। इसमें लेखक लाता है – पिता शांतनु व माता गंगा को भीष्म के सपनों (पाप-बोधी चेतना) में। और वे लोग ‘तीखे-तीखे सवालों से चिथड़े-चिथड़े’ कर डालते हैं भीष्म के। दोनो से द्रौपदी-विषयक प्रश्न पुछवाये गये हैं…, क्योंकि दोनो अपने सुयोग्य पुत्र भीष्म के (कु)कृत्य से स्वर्ग की देवसभा में लज्जित-अपमानित महसूस करते हैं। गंगा सवाल करती है – ‘यदि मेरा कोई इसी तरह अपमान करता, तो तुम क्या चुप बैठते’? इस पर भीष्म की फ़ुंकार आती है, तब पूछती हैं – ‘वही राजरानी का पद तो द्रौपदी का भी था…द्रौपदी तो नंगी न हुई, मैं ज़रूर नंगी हो गयी’।
इसलिए उनकी तमाम योग्यताओं व पौरुषों के बावजूद इस कृति में उनके इस कुकृत्य को बार-बार उजागर किया गया है – शांतनु ने तो भीष्म को धृतराष्ट्र के समकक्ष खड़ा करते हुए यहाँ तक कह दिया है – ‘तुम्हारी त्रुटिपूर्ण राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीयता का उपयोग धृतराष्ट्र व दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ‘पुत्र प्रेम में अंधा, तुम राष्ट्र-प्रेम में अंधे…। क्या फ़र्क़ पड़ता है – अंधा तो अंधा’…’।
इस प्रकार पांचाली के माध्यम से भीष्म के नारी-विषयक एकांगी सोच व सामंतवादी कर्म की अंतिम आहुति का लेखकीय निष्कर्ष सप्रमाण सामने आता है – ‘कुछ चीजों को देखने में बहुत कुछ को बिलकुल न देख पाने की योग्यता का अभाव भीष्म के अधूरेपन का सबसे बड़ा कारण था। उनका अंतस् अपने ख़ालीपन की झंकृति से हमेशा बजता रहा…। अभेद्य पराक्रम के आवरण में बजता हुआ एक करुण गीत का अनुवाद संभवत: भीष्म (के चरित्र) की मूल पूँजी है। ‘राष्ट्र के लिए विश्व समुदाय के हित की उपेक्षा, परिवार की प्रतिष्ठा के लिए दूसरों के मर्यादा की अप्रतिष्ठा…भीष्म के सारे ज़रूरी गुणों के बावजूद उन्हें अपने समय का नायक नहीं बनने देती’…!!
उमेशजी इस कथा के अनुसार सही ही उद्घाटित करते हैं कि ‘नियति ने भीष्म के सामने नारी की स्वतंत्रता व उसकी गरिमा के दलन के नये-नये अवसर उपस्थित किये – अवसर आते गये और भीष्म अवमानना करते गये…’। उनके किये के अनुसार ‘वंश-परम्परा की रक्षा, उसका विकास ही नारी के अस्तित्व का अर्थ है’। नारी अपने लिए नहीं, वंश के लिए है। वह वंश कैसे चलता है, यह गौण है। उदाहरण के रूप में विचित्रवीर्य के मरने के बाद ‘अंबिका-अम्बालिका से वंश-वृद्धि कराना है…पर कैसे कराना है, यह जानना नारी के लिए ज़रूरी नहीं’। इसी सामंतवादी दृष्टि व सलूक का नतीजा है कि व्यास जैसा कोई आदमी उनके साथ गमन करने आयेगा, का उन नारियों को ठीक से पता तक न था और इसी से परिणाम इतने भयंकर हुए…।
लेकिन इस पूरे प्रकरण के लिए एकमात्र भीष्म को ज़िम्मेदार ठहराना इतना उचित नहीं – किंचित अतिरंजना तो है, क्योंकि उस युग में नियोग-प्रथा थी। व्यास के रूप में बड़े भाई व ऋषि को लाना उस प्रथा का एक तरह से परिष्कृत रूप था। इरावती कर्वे की संगत उद्भावना यह भी है कि किसी राजा…आदि को लाने से वह संतति के साथ राज्य पर अपना दावा पेश करता, जिस मानसिकता का सबसे विचित्र रूप मुग़ल शासन में रहा कि दावा न पेश कर पायें, इसके लिए शहजादियों की शादियाँ ही वर्जित कर दी गयीं – उन्हें आजीवन राजसी सुख-सुविधाएँ मुहय्या की जाती थीं। इस प्रथा का एक रूप यह भी था कि नियोग के लिए स्वयंवर होता था। उसकी घोषणा होती थी। प्रतिस्पर्धी आते थे। स्त्री को अपनी पसंद के पुरुष का एक-एक रात के लिए तीन बार के वरण का अधिकार होता था। कुल मिलाकर यह कि चली आती परम्पराओं का निरापद उपयोग किया भीष्म ने…। बस, इस युगीन जड़ता की सीमाओं को तोड़ न सके, जो उनके व्यक्तित्व की युगीन मातहती अवश्य है, पर इसके कर्त्ता भीष्म नहीं, युग था – वे तो उसके प्रयोक्ता मात्र थे – नियंता नहीं।
फिर इसके आगे जाकर उमेशजी भीष्म के अस्तित्व को ही धृतराष्ट्र-पांडु-विदुर में संतरित-विकसित पाते हैं…, जो थोड़ा द्रविड़ प्राणायामी ज़रूर है, पर निराधार नहीं। सिंह साहब धृतराष्ट्र को ‘भीष्म की आंतरिक अंधता का संवाहक और पांडु को भीष्म की बाह्य निर्भीकता की छाया में छिपी नैतिक पांड़ुरता और उनके त्याग के नीचे दबी उनके मोह की पांडुरता का विग्रह’ मानते हैं। इसी क्रम में विदुर को ‘भीष्म की धर्म की शूद्रता का प्रतिनिधि’ – एक शूद्र धर्मात्मा, विवश धर्मात्मा…। कहना होगा कि ये उद्भावनाएँ सिंह साहब की तर्क-विश्लेषण शक्ति व सोच-संगति की प्रतिभा का पुख़्ता प्रमाण अवश्य हैं, सुनने में रोचक हैं, तारीफ़ के लायक़ हैं…। पर इसे विचार्य-स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसका बिस्मिला ही उलटा व अवांतर हो गया है। ये प्रवृत्तियाँ जैविक हैं – अभिमन्यु के लिए कही गयी ‘पिता वै जायते पुत्र:’ वाली। भीष्म के साथ इन तीनो का ऐसा कुछ है ही नहीं। पालन-पोषण से विकसित होने वाली होतीं, तो विचार्य व कदाचित स्वीकार्य होतीं। असल में काम कोई भी हो, लगातार करते-करते वह अपनी रासायनिक प्रक्रिया की नियति का शिकार हो जाता है, तो कभी अतिरंजना हो ही जाती है। और इतनी सारी बातों की उद्भावनाएं करते-करते सिंह साहब की भी यह करने की वृत्ति बन गयी है। इसी तरह जुए में एक पर एक सम्पत्ति हारते हुए भाइयों व पत्नी तक को हार जाने वाले युधिष्ठिर भी जब आत्म-मनन करते हैं, तो सिंह साहब इसी रासायनिक प्रक्रिया में उसके अंतस् से निकले सवाल के जवाब में इसका ठीकरा भी भीष्म के सर फोड़वा देते हैं – ‘पितामह ने आमंत्रण रोकवा क्यों नहीं दिया’!! ज़ाहिर है कि खेलने वाले का दोष ज्यादा है, तो उसका इस तरह बचाव बेज़ा है। फिर पितामह की तो इसमें सम्मति भी न थी…। क्या भीष्म को तरह-तरह से निबेरना भी उसी रासायनिक प्रक्रिया का शिकार होकर ही हर जगह उन्हीं को दोषी देख रहा है!! इत्यलम् भीष्म-प्रकरण।
उमेश सिंह की ‘समय की आँख’ प्रच्छन्न रूप से सभी प्रमुख पात्रों के पास पहुँचती है। इस श्रिंखला में द्रोणाचार्य के पास तब पहुँचती है, जब पांडव-वनवास के उपरांत इंद्रप्रस्थ के समस्त कार्यभार के दायित्व को सम्भालने का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन उनके पास आया है। और पहले तो गुरु इनकार करते हैं, फिर स्वीकार लेते हैं। इसी सूत्र को पकड़े संक्षेप में उनका पूरा जीवन आता है – धनुर्विद्या के महान ज्ञाता-प्रयोक्ता होने के बावजूद एक गाय न पाने और सारे संघर्षों के बाद निष्कर्ष वही कि ‘एक कटोरे दूध के लिए विद्या बेच दी, विवेक बेच दिया, अपना धर्म छोड़ दिया’!! जी रहे हैं ‘समय के अभिशाप की तरह’…। फिर वह खुद ही क़बूलते हैं – ‘मेरे जीवन में गर्व करने लायक कुछ है नहीं…मै भी अंधा हूँ। और कहना होगा कि इस विवेचन में ख़ास कुछ नया नहीं, लेकिन मुद्दे में सीधे घुसकर बात कह देने का वह कौशल (डाइरेक्टनेस) है, जो अपने लुभावनेपन में नवता बन जाती है…।
बच गये निष्कासित महात्मा विदुर। उनके पास पहुँचती है ‘समय की आँख’, तो इन चरित्रों के सारे नग्न सत्य कैप्सूल की तरह उजागर हो जाते हैं – पांडु वानप्रस्थ को जाते हुए साम्राज्य धरोहर के रूप में रख गये थे अंधे धृतराष्ट्र के पास। उसने हथिया लिया। उसके हाथ बने – दुर्योधन-शकुनि-कर्ण। उन्होंने तातश्री भीष्म व आचार्य द्रोण के हाथों को भी अपने हाथ कर रखे हैं। तातश्री अपनी प्रतिज्ञा के पगहे से सिंहासन के खूँटे के साथ बंधे हैं। आचार्य सोने के पिंजरे में बंधे शेर हैं। पिंजरे से निकाल कर उन्हें ज़रूरत पड़ने पर शिकार के काम में लगाया जा सकता है’ – उनका इंद्रप्रस्थ चलाना और युद्ध में लड़ना…ऐसा ही था। काश, सिंह साहब उस प्रसंग को भी ले पाते, जब वे अपने सेनापतित्व में एक दिन युधिष्ठिर को युद्ध-बंदी बनाने की साज़िश (रणनीति) रचते हैं। इसमें सत्य (पांडवों) के पक्ष में उनकी निष्ठा एवं प्रियतम शिष्य अर्जुन के प्रति उनका प्रेम खूब उघड़ता (एक्सपोज़ के लिए नंगा कहना बेज़ा लग रहा है) है और इसकी मनोवैज्ञानिक उद्भावना भी रोचक होती – कि उनक अपार शस्त्र-ज्ञान कभी कोई बड़ा काम न कर सका था, जिसके हीन भाव का मार्जन था युधिष्ठिर को बंदी बनाकर कुछ कर भावी समय के लिए कुछ कर दिखाना…। यह तो रहा उनका आंतरिक सत्य था, जो उनकी कुंठा से उपजा था और बाहरी सत्य था – कौरवों के नमक की अदायगी…। बहरहाल,
बस, इतने सारे अंधों के बीच अंधे न होने की सजा मिली विदुर को – मंत्रि-पद के निष्कासन की…। सिंहजी के विदुर सोचते हैं – ‘क्या अंधा-बहरा-गूँगा न होना मेरा अपराध था? राजा की दुर्बलताओं को मंत्री का जान लेना क्या अपराध था’? हाँ, था – ‘क्योंकि अंधे राजा को अंधा-बहरा-गूँगा मंत्री चाहिए, जो मैं न था। और तब हस्तिनापुर का ऐसा एक्सटेंशन सामने आता है – ‘चाहे जितना बड़ा वेतन हो, जितना बड़ा पद हो, ग़ुलाम बनकर उसे पकड़े रहने से अच्छा है – अकिंचन बनकर (बिदुर की तरह) बन में रह लेना – अपनी मर्यादा, अपने विवेक और अपने धर्म के साथ…।
इस बीच गांधारी-धृतराष्ट्र संवाद में धृतराष्ट्र के उसी धारित पुत्र-मोह का स्वीकार आता है, जो बहव: कथित व बहुश्रुत है। बस, चरम पर जाकर गांधारी का भी पुत्र-मोह स्वीकारना यहाँ किंचित अलग है, वरना वह वक्त आने पर (दुर्योधन का सारा शरीर बज्र करने जैसा काम) कर कर तो दी थी, पर कभी कहती न थी।
सबकी बात लेखक ने कही-कहलायी है, पर विदुर व युधिष्ठिर में ‘समय से साक्षात्कार’ नहीं, उनके ‘आत्म-स्वीकार’ प्रमुख बन कर आये हैं, जो उनकी चारित्रिकता के अनुरूप होकर छजते हैं। युधिष्ठिर अपनी पौराणिक पहचान के साथ है – कि उसमें दोष-मुक्त होने की कोशिश नहीं है। बस, एक बात है कि क्षात्र-धर्म में युद्ध व द्यूत से किसी राजा के इनकार न करने के अभिलेख के हवाले से अपने कृत्य को बचाने का एक कदम उठा है। लेकिन लेखक इस प्रसंग में युधिष्ठिर की उस लत को लाना भूल गया है, जिसमें वह भाइयों व पत्नी तक को वस्तु बनाकर दांव पर लगाकर हार देता है। अभिलेख में यह निर्देश तो न होगा। हाँ, खुला स्वीकार कृष्ण को लेकर है कि तातश्री सीधे व साधिकार जुड़े होकर और गूरु द्रोण सामने रहकर, जो न कर सके, वह कृष्ण ने किया – आज यदि मैं हूँ और जो भी हूँ, उन्हीं के कारण हूँ।
इन बातों के अलावा मुझे विवेच्य व उल्लेख्य ऐसे प्रसंग न मिले, जो कोई नवता व ख़ास विवेचनीयता लिये हों…और यदि ऐसे हैं और मुझसे छूट रहे हैं, तो मैं अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता स्वीकार लूँगा…। अत: इस आलेख को यहीं विराम देते हुए एक छोटा-सा उल्लेख भी ज़रूरी समझता हूँ…उत्तर भारतीय बोलियों में ‘ने’ के प्रयोग के निहित (इन बिल्ट) अभाव से उसी अंचल में रह जाने वालों से खड़ी हिंदी के बोल-चाल में तो ढेरों, पर प्रकृतित: लेखन में भी क्वचित् भूल हो जाती है। और ऐसी दो च्युतियाँ मुझे मिलीं, जो लिखने के प्रवाह के बाद दुहराने में मार्जन की अवश्यमेव अधिकारिणी थीं – अगर आप छल को जान लिये होते (99) और तुम न माने (101)।
लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसी व्याख्यापरक पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला, जिसका आह्लाद चिर-स्थायी है। महाभारत की यह व्याख्या अपनी पूर्वज व्याख्याओं की सरणि में सम्मान्य स्थान पाने की अधिकारिणी है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं।