
विभ्रम और बिखरावग्रस्त विपक्ष और भविष्य की राजनीति!
आज भारत के विपक्षी दलों में आपसी अविश्वास और बिखराव है। विपक्ष का क्रमशः सिकुड़ते जाना लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालाँकि, यह भी सत्य है कि आज जो कांग्रेस हाशिये पर है, उसने भी लगभग 50 वर्ष तक विपक्ष-विहीन शासन किया है। कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह को दरकिनार करते हुए स्वाधीनता आन्दोलन की विरासत और समयांतराल में गाँधी ‘सरनेम’ तक को हथिया लिया। परिणामस्वरूप, वह स्वान्त्र्योत्तर भारत की केन्द्रीय और सर्व-सत्तावादी राजनीतिक पार्टी बन बैठी। विपक्ष की नगण्य उपस्थिति ने ही कांग्रेस के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को पैदा किया और अंततः 25 जून,1975 के दिन आपातकाल को संभव किया।
संभवतः कांग्रेस की इन्हीं अधिनायकवादी प्रवृत्तियों और नेहरू परिवार केन्द्रित राजनीति की प्रतिक्रियास्वरूप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ की परियोजना पर कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि उन्हें अपने इस अभियान में चाहे-अनचाहे जबर्दस्त सफलता भी मिल रही है। सन् 2014 और सन् 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि वह नेता प्रतिपक्ष पदप्राप्ति की संवैधानिक अर्हता को भी पूरा न कर सकी। साथ ही,आज वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों और तेलंगाना, उड़ीसा, झारखण्ड, दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में अप्रासंगिक और विलुप्तप्राय हो गयी है। गौरतलब है कि इन राज्यों में लोकसभा की आधी सीटें हैं।
कांग्रेस की क्रमशः डूबती लुटिया के लिए सोनिया गाँधी का धृतराष्ट्री पुत्रमोह जिम्मेदार है। उन्हें अपने सु-पुत्र और कांग्रेस के युवराज राहुल गाँधी के अलावा कोई अन्य नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं लगता। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष और जननेता के रूप में राहुल गाँधी की योग्यता और क्षमता भारत-विख्यात है। दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर उनका ‘दोचित्तापन’ भी जगजाहिर है। यह भी एक सर्वज्ञात तथ्य है कि वे सर्वाधिक निर्णायक अवसरों पर ‘विदेश यात्रा’ पर चले जाते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं, जिन्हें बाद में G-23 कहा गया, ने सार्वजनिक पत्र लिखकर इन्हीं सब बातों पर चिंता व्यक्त करते हुए 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी में अंतरिम व्यवस्था की जगह स्थायी अध्यक्ष और आंतरिक लोकतन्त्र की बहाली की दरख्वास्त की थी। इस पत्र ने गाँधी परिवार और उनके दरबारियों को नाराज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव (2019) में मिली करारी हार के बाद राहुल गाँधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और सोनिया गाँधी तबसे अंतरिम अध्यक्षा हैं। अभी कांग्रेस ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ और तदर्थवाद की शिकार है। अध्यक्ष न होते हुए भी कांग्रेस के सारे सांगठनिक फैसले राहुल गाँधी और उनकी विश्वसनीय ‘मित्र-मण्डली’ लेती है। यह यूपीए-। और यूपीए–।। जैसी ही व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के सभी निर्णय 7 रेसकोर्स रोड से न होकर 10 जनपथ से हुआ करते थे। इस जवाबदेहीमुक्त व्यवस्था के अपने लाभ हैं। परन्तु इस उत्तरदायित्वहीन सत्ता-सुख के नुकसान भी बहुतेरे हैं, जो कभी सार्वदेशिक और सर्वाधिक सशक्त पार्टी रही कांग्रेस की पंगुता, क्रमिक अवसान, आंतरिक असंतोष, भयावह गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की हताशा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। बिहार के विधान-सभा चुनाव, हैदराबाद के महानगरनिगम चुनाव, राजस्थान के नगर निकाय और पंचायत चुनाव और जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद् चुनाव परिणामों ने इस हताशा और निराशा को और भी घनीभूत कर दिया है।
मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ-दिग्विजय सिंह की खेमेबंदी और वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ गयी। अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जनाधार और संभावनाओं वाले नेता को कांग्रेस के बाहर अपना भविष्य देखने को विवश होना पड़ा। पिछले दिनों राजस्थान में भी मप्र की पटकथा का दुहराव होते-होते बचा है। हालाँकि, अभी इस राजनीतिक प्रहसन का पटाक्षेप नहीं हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट ‘छब्बे बनने चले थे और दुबे बनकर’ रह गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन में अशोक गहलोत और उनके चहेते प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने जिसप्रकार सचिन पायलट समर्थकों को ठिकाने लगाया गया है और सचिन पायलट के ‘पुनर्वास की प्रतीक्षा’ लम्बी होती जा रही है, उससे उनका धैर्य चुक रहा है।
वे कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल सकते हैं और अशोक गहलोत सरकार की परिणति भी कमलनाथ सरकार जैसी हो जाएगी। पंजाब में मुख्यमन्त्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू-प्रताप सिंह बाजवा की खींचतान और हरियाणा में भूपिंदर सिंह हूडा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा आदि की गुटबाजी पार्टी को निरन्तर कमजोर कर रही है। अशोक तंवर जैसे उभरते हुए दलित नेता को निर्विकल्प होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। असम सहित उत्तर-पूर्व के अधिकांश राज्यों में कभी कांग्रेस नेता रहे हेमंत विश्वा शर्मा ने अकेले कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ कर दिया है।
बिहार विधान-सभा चुनाव परिणाम के बाद तमाम विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी के प्रति अविश्वास और संशय और भी गहरा हो गया है। यह अकारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में मिली हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा है। उसने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गाँधी ‘पिकनिक’ मना रहे थे। राजद ने जहाँ 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीतीं, वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई। उसका चुनावी प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक था और इसकी वजह से बिहार में विपक्ष की सरकार बनते-बनते रह गयी।
अब राजद जदयू पर डोरे डालने की फिराक में है। लेकिन चतुर सुजान नीतीश कुमार राजनीति के मँजे हुए खिलाड़ी हैं और वे 2015-16 में जदयू-राजद की महागठबन्धन सरकार के कड़वे अनुभवों को भूले नहीं हैं। निश्चय ही, वे आपसी अविश्वास के चलते टूटे महागठबन्धन की विदाई बेला में तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें दी गयी संज्ञा ‘पलटू चाचा’ का स्थायीकरण नहीं करना चाहेंगे। इसी आपसी अविश्वास के चलते महागठबन्धन के पुराने सहयोगी दलों- जीतनराम मांझी के हम और मुकेश साहनी के वी आई पी ने भी चुनाव से ठीक पहले महागठबन्धन से किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी और अंततः उनका निर्णय सही साबित हुआ।
उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों के कारण चुनावी दृष्टि से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिर-प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने महागठबन्धन बनाकर चुनाव लड़ा। इस महागठबन्धन में पश्चिमी उप्र में प्रभावी राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुआ। लेकिन मात्र 15 सीटों पर सिमटकर यह महागठबन्धन बिखर गया और आपसी आरोप-प्रत्यारोप का लम्बा दौर चला। बुआ-भतीजे के बीच एकबार फिर इतनी गहरी खाई पैदा हो गयी है कि ‘पुनर्मिलन’ की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं है। उधर चाचा-भतीजे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की टकराहट से समाजवादी पार्टी में भी गृह-कलह और टूट-फूट जारी है।
असदुद्दीन ओवैसी स्वातन्त्रोत्तर भारत के मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाह रहे हैं। उनकी पार्टी ऑल इण्डिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलिमीन मुस्लिम लीग की तर्ज पर मुसलमानों में गहरी घुसपैठ करते हुए उनकी एकमात्र सरपरस्त पार्टी बनती जा रही है। ओवैसी और उनकी पार्टी की अखिल भारतीय सक्रियता और उपस्थिति ने तथाकथित सेक्युलर पार्टियों-कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा, सी पी एम और तृणमूल कांग्रेस आदि की नींद उड़ा दी है। अभी तक ये दल मुसलमानों को एकमुश्त वोट बैंक की तरह अपने खाते में जोड़कर अपना चुनावी गणित साधते आये हैं। किन्तु मुसलमानों के मसीहा के रूप में ओवैसी के उभार ने उनके चुनावी समीकरण और संभावनाओं को गड़बड़ा दिया है। अभी उप्र में भाजपा का कोई आसन्न और विश्वसनीय विकल्प नहीं है।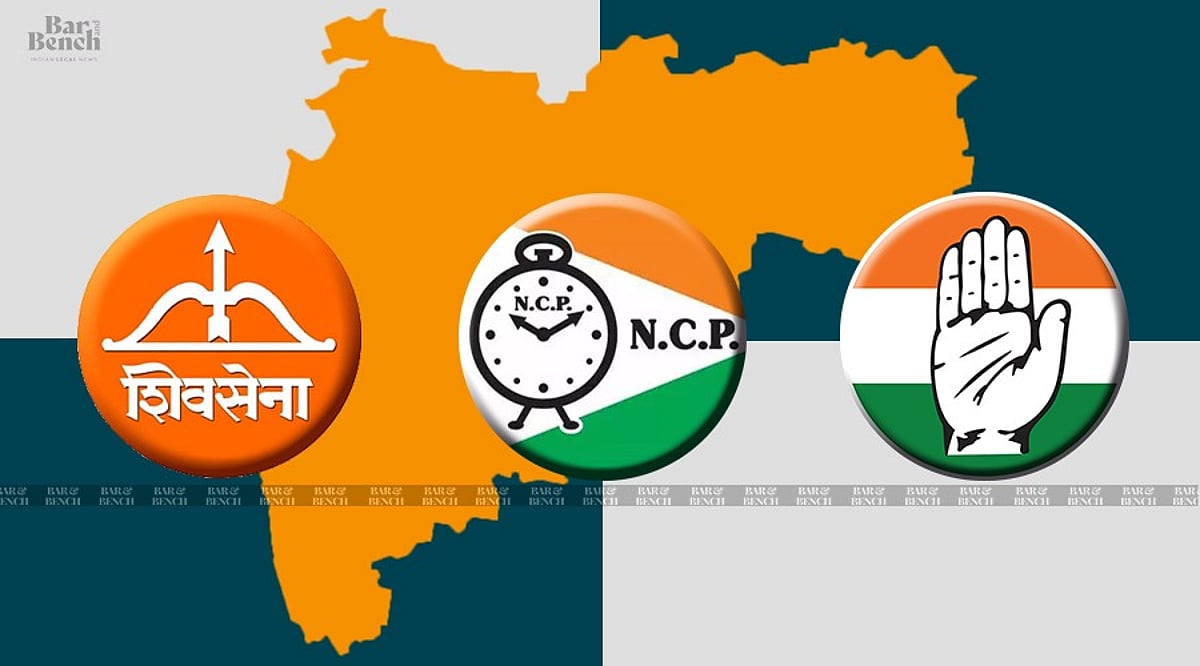
महाराष्ट्र एक और बड़ा राज्य है। वहाँ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार है। यह जनादेश की चोरी से बनी हुई अंतर्विरोधों की सरकार है। इसके घटक दलों में अंदरूनी कलह और खींच-तान वक्त-बेवक्त दिखाई-सुनाई पड़ती रहती है। पिछले दिनों सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गाँधी ने मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक पत्र लिखकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों आदि वंचित वर्गों की विकास योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने की माँग की। यह पत्र शिवसेना और एन सी पी को सख्त नागवार लगा क्योंकि यह कांग्रेस अध्यक्षा की उपरोक्त वर्गों का बड़ा हितैषी दिखकर उनका वोट बैंक साधने की जुगत थी। महाराष्ट्र में पारस्परिक बढ़त हासिल करने की इसप्रकार की जद्दोजहद जारी है। आपसी अविश्वास और अंतर्विरोधों के कारण एक समय मुंबई शहर ‘कोरोना कैपिटल’ बन गया और महाराष्ट्र की बढ़ी हुई कोरोना मृत्युदर के कारण वहाँ की सरकार को विपक्ष ने ‘महाविनाश अघाड़ी’ की संज्ञा दे डाली।
कर्नाटक की कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) सरकार भी इसीप्रकार के अविश्वास और अंतर्विरोधों की शिकार हुई। एक संवाददाता सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमन्त्री एच डी कुमारस्वामी को अपनी सरकार चलाने और जरूरी निर्णय लेने में विवशता जाहिर करते हुए रोना तक पड़ा। एस सिद्धरमैया और देवगौड़ा परिवार का पारस्परिक द्वेष और वैमनस्यता जनता दल के जमाने का है। उसीकी परिणति अंततः कुमारस्वामी सरकार के पतन में हुई और आज सिद्धरमैया और कुमारस्वामी का आपसी वैर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली भारी चुनावी सफलता से दीदी बौखलायी हुई हैं। वहाँ वामपंथी दल और कांग्रेस गठबन्धन बनाकर विधान सभा चुनाव लड़ने वाले हैं।
त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को लाभ मिलना स्वाभाविक है। तृणमूल कांग्रेस और वाम-कांग्रेस गठजोड़ जैसी सेक्युलर और हिंसावादी पार्टियों के कारिंदे और जनाधार काफी हद तक ‘कॉमन’ है, जबकि भाजपा इनसे अलग जमीन और जनाधार तलाशने में कामयाब हुई है। तमिलनाडु की राजनीति लम्बे समय से दो ध्रुवीय है। वहाँ दो चिर-प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल- डी एम के और ए आई डी एम के सत्ता की अदला-बदली करते रहते हैं। हालांकि, इन दलों के सर्वमान्य नेताओं एम करुणानिधि और जे जयललिता के निधन के बाद नयी राजनीतिक संभावनाओं और समीकरणों का सूत्रपात हो सकता है। केरल और तमिलनाडु में जमीन तलाशती भाजपा की नज़र इस नए ‘स्पेस’ पर है। कांग्रेस लम्बे समय से तमिलनाडु में पिछलगुआ पार्टी है। दरअसल, विपक्षी एकता की सबसे बड़ी बाधा क्षेत्रीय क्षत्रपों की लपलपाती महत्वाकांक्षा और एक-दूसरे के जनाधार को हथियाने की प्रतिस्पर्धा है। नीति और नीयत का यह दोष किसी विश्वसनीय विकल्प की संभावनाओं को निरस्त करता है।
पिछले दिनों मोदी सरकार द्वारा लिए गए तीन बड़े निर्णयों- नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की बेदखली और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से सम्बन्धित अनुच्छेद 370 एवं 35 ए की समाप्ति पर तमाम विपक्षी दल अपनी-अपनी ढपली पर अपना–अपना राग अलापते नज़र आये। हालाँकि, कांग्रेस आदि कुछ विपक्षी दल पहले नागरिकता संशोधन कानून और अब कृषि विधेयकों के विरोध की आड़ में दूसरों के कन्धों से बंदूक चलाकर अपना लक्ष्य साधने की फ़िराक में हैं। लेकिन ये लुकी-छिपी वाली कोशिशें बड़े बदलाव के लिए नाकाफी हैं।
डॉ. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। विपक्ष को इस बात को समझते हुए अवसरवादी और विद्वेषात्मक राजनीति का परित्याग करते हुए साझा नीति और कार्यक्रमों के आधार पर आपसी विश्वास और एकता कायम करनी चाहिए और साजिशों की जगह संघर्ष का रास्ता अपनाकर भारतीय लोकतन्त्र को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। विपक्षी दलों को ‘मोदी मेनिया’ से भी बाहर निकलकर भाजपा-विरोध की नकारात्मक राजनीति की जगह नीतियों और मुद्दों पर आधारित रचनात्मक राजनीति करनी चाहिए। इसी से उनका और भारतवासियों का कल्याण होगा।
केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को भी सत्तामद से बचते हुए अधिकाधिक जनोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों को धरातल पर लागू करना चाहिए। उसे विपक्ष और अन्यान्य स्टेकहोल्डर्स के साथ भी निरन्तर संपर्क और संवाद की स्वस्थ परम्परा विकसित करनी चाहिए। यह सत्य है कि आज भारतीय संसदीय व्यवस्था में सत्तासीन भाजपा के सामने विपक्ष और विकल्प के नाम पर गहरा शून्य है। किन्तु भाजपा को सन् 1977 और सन् 2004 के अनुभवों से सबक लेते हुए विकल्पहीनता को अपनी शक्ति और उपलब्धि मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। राजनीति में निर्विकल्पता का सीमित महत्व है क्योंकि असंतुष्ट जनता अपना विकल्प खुद तलाश लेती है। ऐसा ही उसने 1977 और 2004 के चुनावों में किया था।
.











