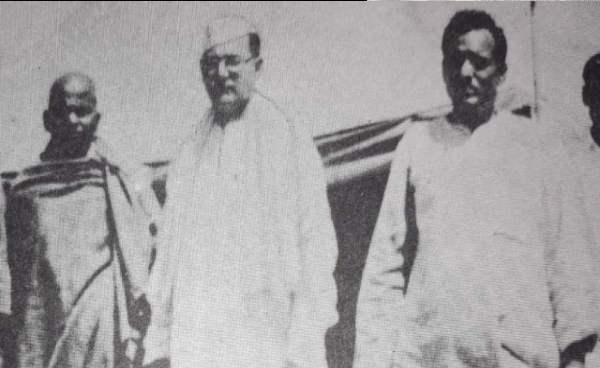दास्तान-ए-दंगल सिंह (52)
- पवन कुमार सिंह
हमारी मंडली के साथी कोचिंग सेंटर को जमाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। धीरे-धीरे आमदनी बढ़ने के साथ हम आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। इसी बीच पाठक जी को गोड्डा कॉलेज से और मुझे कहलगाँव, नौगछिया और खगड़िया कॉलेज से तदर्थ नियुक्ति के लिए बुलावा आया। थोड़े उधेड़-बुन के बाद पाठक जी बेमन से गोड्डा चले गए और मित्रों ने मेरे लिए कहलगाँव का विकल्प चुना, क्योंकि वहाँ से रोज ट्रेनयात्रा करके कोचिंग सेंटर से जुड़े रहने की गुंजाइश थी। कहलगाँव के पास त्रिमुहान गाँव में मेरी बड़की दिदिया का घर था तथा शहर में ही मेरे गोतियारी के नंद चाचा के साढू जगद्धात्री बाबू बीइओ थे। उनके पुत्र ध्रुव जी (अभी हाल में स्वर्गवासी हुए हैं) हमारी मंडली के सदस्य थे। सभी अनुकूलताएँ देखकर हमने कहलगाँव आने की योजना बनाई। अनिल जी मुझे लेकर इस तरह चले जैसे कोई अभिभावक अपने आश्रित छात्र को कहीं एडमिशन कराने ले जाता है। हम सुबह की गाड़ी से आए थे, इस कारण ध्रुव जी के यहाँ नाश्ता करने के बाद कॉलेज जाने की योजना थी। ट्रेन से उतरकर मौसा जी के आवास पर जाने के रास्ते में ही सुधा जी का घर था। उसी दिन अनिल जी को छत पर टहलती हुई सुधा दिख गयी थीं और उन्होंने चौंककर कहा था कि यह लड़की तो शादी करने लायक है। पता लगाया जाए कि स्वजातीय है क्या? मैं सुधा को देख नहीं पाया था क्योंकि अनिल के चौंकने और मुझे देखने के लिए टोकने का उपक्रम देखकर वे कमरे में घुस गयी थीं। उत्साहित मित्र का ध्यान हटाने के लिए मैंने कहा था कि यह तो बंगाली टोला है, यहाँ स्वजातीय लोग कहाँ होंगे! पर अनिल ने ध्रुव जी से पूछकर मालूम कर ही लिया था कि वह घर शारदा पाठशाला के साइंस टीचर श्रीधर बाबू का है जो राजपूत ही हैं। आगे विधाता की मर्जी और अनिल के दुस्साहसी सहयोग से मेरा विवाह उसी लड़की से हुआ। उस प्रसंग पर पहले लिख चुका हूँ।


एसएसवी कॉलेज कहलगाँव शहर के मध्य एक छोटी पहाड़ी पर स्थित अंग्रेजों की कोठी ‘हिल हाउस’ या ‘बावन दरवाजा’ में संचालित था, जिसमें कालांतर में और कई नये भवन जुड़ गये। लगभग ग्यारह बजे हम दोनों प्रधानाचार्य प्रो0 संसारधर झा के वेश्म में उनसे मिले। दोनों का परिचय लेने के बाद उन्होंने अफसोस जताया कि यहाँ इतिहास में कोई खाली पद नहीं है इस कारण अनिल जी को जगह नहीं दे सकते। उन्होंने बड़ा बाबू को बुलवाकर मेरा योगदान करवा लिया। हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रो0 रामसागर प्रसाद सिंह लम्बी छुट्टियों पर थे। उनकी लीव वेकेंसी पर मेरी नियुक्ति की गयी थी। प्रो0 झा ने हमारे कॅरिअर की प्रशंसा और अपने कॉलेज के शिक्षकों की निंदा करते हुए कहा था कि “यहाँ खूब चेतकर और सोच-समझकर लोगों से मिलिएगा। आप पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं। यहाँ कोई घोड़े का डॉक्टर था तो कोई नर्स, जमीन का दलाल या स्टाम्प वेंडर आदि। सभी अपने-अपने आका की कृपा से प्रोफेसर बन गये हैं।” उनकी इस बात से हम काफी अचंभित हुए थे। दोपहर का खाना फिर ध्रुव जी के यहाँ खाकर हम भागलपुर लौट आए थे।
अगले दिन कॉलेज आया तो झा साहब ने प्राध्यापक कक्ष में साथ ले जाकर सबसे मेरा परिचय कराया और मुझे सहयोग करने का आग्रह सहकर्मियों से किया। कार्यकारी विभागाध्यक्ष प्रो0 हीरा लाल श्रीवास्तव से अनुरोध करके मैंने वर्ग आबंटित करने में सहूलियत मांगी थी। यदि सुबह की गाड़ी से आऊँ तो दोपहर को लौट सकूँ या यदि दोपहर में आऊँ तो शाम की गाड़ी पकड़ लूँ। क्लासरूम की कमी के चलते कॉलेज सुबह 7:30 बजे से शाम के 4:50 तक चलता था। हीरा बाबू ने मेरा अनुरोध मानकर मुझे वर्ग बाँट दिये थे। दो अन्य प्राध्यापक विभाग में और थे डॉ0 लखनलाल सिंह आरोही(सम्प्रति अध्यक्ष, अंगिका अकादमी) और डॉ0 अजबलाल पंडित नीलकुसुम(स्वर्गीय)। मुझे राष्ट्रभाषा हिन्दी की कक्षाएँ अधिक दी गयी थीं इस कारण अधिकाधिक छात्रों को पढ़ाने का सुअवसर अनायास ही मिल गया था। एक माह बीतने तक मैं विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। इसका पता तब चलता था जब मेरे क्लास में अन्य कक्षाओं के छात्र बिना बताए घुस जाते थे या पढ़ाई शुरू करने के बाद वर्ग में घुसने के लिए अनुमति माँगते थे। बीए अंतिम वर्ष का एक लड़का तो ऐसा दीवाना हो गया था कि वह रोज एक गुलाब लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर खड़ा रहता। दूर से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करता फिर चरणस्पर्श करता तब फूल देता था। मैंने पूछा था कि वह ऐसा क्यों करता है तो उसने कहा था कि उसे आत्मिक खुशी और शांति मिलती है। यह सब तो बहुत अच्छा लगता था, किन्तु एक भारी दिक्कत थी। ताजा-ताजा एमए पास करके आया दुबला-पतला युवक बरामदे या सीढ़ियों से गुजरती छात्रों की भीड़ में घुलमिलकर खो जाता। कद-काठी से कमजोर होने के कारण भीड़ में अलग पहचान नहीं बन पाती थी और कई बार धक्का-मुक्की खाने तक की नौबत आ जाती थी। इस संकट के समाधान के लिए मैं चॉक-डस्टर और रजिस्टर के साथ एक-दो मोटी किताब हाथ में कंधे से ऊपर उठाकर भीड़ में चलने लगा था ताकि दूर से ही लड़के जान जाएँ कि शिक्षक हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाने का खूब आनंद ले रहा था। बच्चे भी नये शिक्षक के वर्ग के मजे लेने लगे थे।
शंकर साह विक्रमशिला महाविद्यालय की संकल्पना भागलपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण सिन्हा की थी। उनके नेतृत्व में जनसहयोग से 3 दिसंबर 1967 को विक्रमशिला कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में उदाकिशुनगंज वासी दयाशंकर साह द्वारा भूमि और पैसे दान करने के कारण उनके पिता शंकर साह का नाम जोड़ा गया। दुर्भाग्यवश स्थापनाकाल से ही इस कॉलेज के मानव संसाधन में विभेद का ज़हर घुल गया था। उस समय क्षेत्र के दो दिग्गज राजनेताओं में गंभीर प्रतिद्वंद्विता थी। अलग-अलग समय और परिस्थितियों में ये दोनों कॉलेज की प्रबंधन समिति के सचिव रहे थे। दोनों ने अपने लोगों को नियुक्त किया था। दोनों के चहेते प्रिन्सिपल भी अलग-अलग थे, जिनमें पद को लेकर लम्बे समय तक मुकदमेबाजी चली थी। स्टाफ में गुटबंदी और अलगाव का असर साफ-साफ कैम्पस में महसूस किया जा सकता था। किंतु मैं इस गुटबाजी से प्रभावित नहीं होने के लिए अतिरिक्त रूप से सतर्क था। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से खुलकर मिलता और बातचीत में तटस्थ रहने का प्रयास करता था। प्रधानाचार्य डॉ0 झा मुझे बहुत स्नेह देते थे, क्योंकि डूबकर पढ़ाने वाले शिक्षक उन्हें पसंद थे। उनसे मिलने जाता तो हर बार वे अपने पनबट्टे से पान जरूर खिलाते थे।
कुल मिलाकर सबकुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि दुर्योग की तरह एक घटना घटित हो गयी, जिसने मेरी तटस्थता को ही मेरा सबसे बड़ा दुर्गुण सिद्ध कर दिया। कॉलेज के शिक्षक संघ के पुनर्गठन के लिए चुनाव था। कुल 45 स्वीकृत पदों में से 44 पर स्थाई शिक्षक कार्यरत थे। मैं अकेला तदर्थ शिक्षक था। तीन-चार माह साथ गुजारने के बाद मैं जान गया था कि 22-22 लोग विरोधी गुटों में बँटे हुए हैं। चुनाव के दिन सभी शिक्षक उपस्थित थे। संघ के पाँच पदों के लिए दोनों पक्ष से अलग-अलग उम्मीदवार उतारे गये थे। मैं समझ रहा था कि मेरा मत निर्णायक हो जाएगा। विवाद से बचने का एक ही उपाय था कि मैं परहेज करके मतदान में भाग न लूँ। इसके पूर्व एक सप्ताह से दोनों पक्ष के लोग मुझे वोट के लिए फुसलाने का प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्यवश प्रिन्सिपल साहब खुद निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने मेरी नियुक्ति की थी। इस कारण मेरे वोट पर वे अपना अधिकार मानते थे। उन्होंने भी मुझे अपने गुट के लोगों को वोट देने के लिए कहा था। इस तरह मैं चुनाव के दिन भारी धर्मसंकट में फँस गया था। मीटिंग शुरू हुई तो मैंने खड़े होकर सदन से निवेदन किया कि मैं एडहॉक टीचर हूँ इसलिए मुझे वोट नहीं डालना चाहिए। प्रिन्सिपल साहब ने जोरदार तरीके से मेरी बात यह कहकर काट दी कि “हमारे यहाँ जिस शिक्षक ने चॉक-डस्टर के साथ क्लास ले लिया, वह शिक्षक है। अस्थाई के बाद ही कोई स्थाई होता है। पवन बाबू वोट डालेंगे।”
जान छुड़ाने के लिए मैंने भी एक पासा फेंका, “मैं किसी गुटबंदी में विश्वास नहीं करता, इसलिए गुट को नहीं, मनपसंद चेहरे को वोट दूँगा।”
इसपर दोनों पक्षों ने सहमति दे दी। मतदान हुआ और जिसका डर था वही हो गया। एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के दो पदाधिकारी चुनाव जीत गये। चार लोगों को एक-एक अधिक मत मिले थे। एक प्रो0 मोईनुद्दीन को पाँच मतों के अंतर से जीत मिली थी। संघ के लिए तो जो हुआ सो हुआ, पर मेरे लिए तो जैसे भूचाल आ गया। दोनों गुट के लोगों ने मुझसे मुँह फुला लिया, मुझे निशाना बनाकर व्यंग्य करने लगे और फब्तियाँ कसने लगे। खाली समय में स्टाफरूम में बैठना मुश्किल हो गया। लीजर में पहाड़ से उतरकर बाजार घूमकर आ जाता फिर क्लास लेता। मेरी तकलीफ को और भारी बनाने के लिए प्रिन्सिपल साहब ने एक और उपाय किया। हिंदी के विभागाध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने मेरा रूटीन अपने से सेट कर दिया। पहली घंटी से लेकर अंतिम घंटी तक। यानी कि मैं सुबह 5 बजे की गाड़ी भागलपुर में पकड़ूँ और 6 बजे शाम तक लौट सकूँ। अध्यक्ष जी ने अगले दिन वह रूटीन थमा दी। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की और कहलगाँव में रोज सुबह से शाम होने लगी। हाँ, मजबूरी में मौसी की वह बात माननी पड़ी कि रोज नाश्ता और भोजन उनके घर करूँ। लेकिन परेशानी तो बहुत हो रही थी। इसी क्रम में एक दिन क्रॉसिंग के कारण सुबह की ट्रेन लेट हो गयी। कैम्पस घुसने से पहले ही पहली घंटी बज गयी थी। उबड़-खाबड़ रास्ते से पहाड़ी चढ़ते मेरी साँसें फूल रही थीं। मैं तेजी से स्टाफरूम की तरफ जा रहा था कि चेम्बर से प्रिन्सिपल साहब ने आवाज दी, “पवन बाबू जरा मिलकर जाइए।”
मैं पलटकर उनके पास आया और बोला, “सर, क्लास छूट रहा है।”
“क्लास तो दस मिनट पहले ही छूट गया। बैठिए।” उन्होंने हँसकर कहा फिर पूछा, “बहुत परेशान दिख रहे हैं?”
“सर, परेशान हूँ इसलिए परेशान दिख रहा हूँ।”
“मुझे अच्छा लगता है जब टीचर को परेशान देखता हूँ। टीचर के माथे पर पसीना देखकर लगता है कि मेरा काम ठीक चल रहा है।” पता नहीं, उनकी मंशा क्या थी, किन्तु उनकी इस टिप्पणी ने गहरी नींद में सोए दंगल सिंह को चिकोटी काटकर जगा दिया, जो नहीं जानता था ‘दैन्य और विनय’।
“सर, यह पसीना इस सड़े हुए कॉलेज के लिए नहीं बना है। आप रद्दी, आपके स्टाफ रद्दी। सब जात-पाँत करते हैं।मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। भारी भूल हुई जो मैं यहाँ आया। बस, अब और नहीं।”
वे ‘हाँ-हाँ, क्या-क्या’ करते रहे और मैंने उनके सामने पड़े कॉलेज के लेटरपैड से एक पन्ना लेकर एक वाक्य का त्यागपत्र लिख डाला, “प्रधानाचार्य महोदय, मैं व्यक्तिगत कारणों से व्याख्याता का पद त्याग रहा हूँ।” वे कसमसाकर रह गये। मैंने पेपरवेट से पन्ने को दबाया फिर उनका पनबट्टा खोलकर एक खिल्ली पान और जर्दा लेकर खा लिया और कहा, “सर, भूल-चूक लेनी-देनी। माफ करिएगा, चलता हूँ। अब यहाँ नहीं आऊँगा। प्रणाम!” चलते हुए अपने पीछे से उनकी आवाज सुनी, “गुस्सा थूक दीजिए पवन बाबू। फिर आइएगा… …” पर दंगल सिंह कहाँ रुकने वाला था। वह तो संघर्ष के अग्निकुंड में छलांग लगा चुका था।
(क्रमशः)