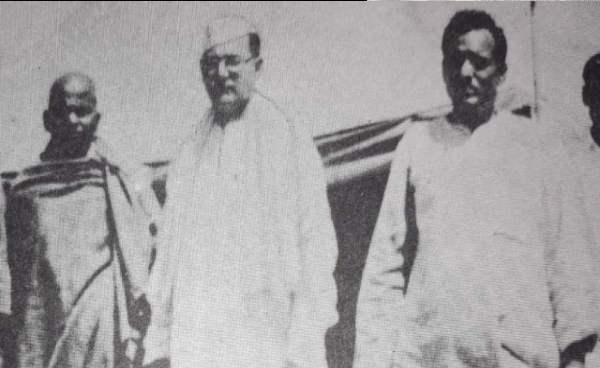दास्तान-ए-दंगल सिंह (48)
- पवन कुमार सिंह
पीजी कैम्पस की कहानी उन दोनों पात्रों के बिना पूरी नहीं हो सकती, जो थे तो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, किन्तु मेरी नजरों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। एक थे हिंदी विभाग के आदेशपाल स्व0 अमर राय और दूसरे पीजी होस्टल के वार्ड सर्वेंट दाहू मुखिया। अमर जी सम्पूर्ण विभाग की धुरी और गार्जियन थे। हम सभी उनको ‘अमर बाबू’ बुलाते थे और वे हमें साधिकार डाँट सकते थे। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित और समय के पाबंद। समय की कीमत हमने उनसे समझी। एक बानगी देखिए। क्लास की घण्टी लगाकर अमर जी हमारे कक्षाकक्ष में आकर हमें डाँटते हैं, “हल्ला क्यों कर रहे हैं आपलोग? किनका क्लास है?”
“हेड सर का।”
“शांत रहिये, भेजते हैं।” उधर अध्यक्ष प्रो0 शिवनंदन प्रसाद अपने चेम्बर में दो-तीन प्राध्यापकों के साथ बैठे बात कर रहे हैं। अमर जी उनके सामने अटेंडेंस रजिस्टर पटकते हुए कहते हैं, “सर आपका क्लास है। आप गप्प कर रहे हैं और लड़का लोग हल्ला मचा रहा है।”
अध्यक्ष जी हँसते हुए जवाब देते हैं, “अरे अमर साँस भी नहीं लेने दोगे?”
“क्लास में जाकर साँस लीजिए न! कौन मना करता है?” अध्यक्ष जी रजिस्टर उठाकर चुपचाप क्लास चले जाते हैं। भारी वृद्ध शरीर और घुटनों की तकलीफ के बावजूद हमेशा सक्रिय अमर जी विभाग के सभी सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखते। कमरों और फर्नीचरों की सफाई से लेकर घंटी बजाने और पानी पिलाने तक। गुरुजी लोगों के लिए चाय, पान, सुरती सबका जुगाड़ वे करते। एक दिन क्लास लगने से पहले हम आठ-दस साथी बरामदे में गप्पें लड़ा रहे थे कि अमर जी ने आकर कहा, “…***जी खैनी दीजिए, दामोदर बाबू मांग रहे हैं।”
“क्या मेरा नाम बोलकर माँगे?”
“नहीं तो क्या हम अपने से बोल रहे हैं?”
“उनको कैसे मालूम?”
“अरे एक नशेड़ी दूसरे नशेड़ी को खूब पहचानता है। चलिए, जल्दी दीजिए नहीं तो वे क्लास लेने में देरी करेंगे।”
फाइनल परीक्षा के पहले दो-तीन साथियों की उपस्थिति कम हो रही थी। हमें अंदेशा था कि उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। हम चार-पाँच साथियों ने मिलकर अमर जी से आग्रह किया कि वे आवश्यक उपस्थिति बना दें। उन्होंने साफ मना कर दिया और हेड सर को कह देने की धमकी भी दे डाली। एक-दो दिन के अंतराल पर हमने उनकी खूब खुशामद की पर वे राजी नहीं हुए। एक दिन मौका ताड़कर हमने रजिस्टर चुरा लिया और विभाग के बगल में स्थित अंधे कुएँ में डाल दिया। इस कृत्य की जानकारी केवल शरारती कोर कमेटी को ही थी। किन्तु अमर जी ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने हेड सहित सभी प्राध्यापकों को हम चार छात्रों का नाम बता दिया, जिन्होंने उनसे हाजिरी बनाने का अनुरोध किया था। हमें खूब डाँट पड़ी। विभाग से निकाल देने की धमकी भी दी गयी, किन्तु हमने बिल्कुल मुँह नहीं खोला। कुछ दिनों तक बहुत तनाव रहा फिर बात आयी-गयी हो गयी। इस कांड के चोर सभी तो जीवित हैं पर सिपाही और न्यायाधीश सब स्वर्गवासी हो गये हैं। तभी तो वह रहस्य खोलने का मैंने साहस किया है।
अमर जी से मिले स्नेह को मैंने उनके जीवित रहने तक निभाने की कोशिश की। उनकी संतानों की शादी से लेकर खुद उनकी अस्वस्थता तक उनके घर जाता-आता रहा। उनका इकलौता बेटा बालकृष्ण किशोरावस्था में ही मुझसे काफी जुड़ गया था। होस्टल में भैया-भैया करता आता और ठेकुआ-भूजा जो मिलता अधिकार से खाता। बाद में उसे विश्वविद्यालय में नौकरी मिली। मेरे घर कहलगाँव दर्जनों बार आया और भौजी के हाथ का खाना खाये बिना कभी नहीं लौटा। अपनी पुत्री को मैट्रिक परीक्षा देने मेरे घर छोड़ गया था बालकृष्ण। उसके स्नेह के आगे सहोदर भाई का स्नेह भी फीका पड़ जाता। पता नहीं, वैसे पिता और अमर जी जैसे दादा के घर कैसा कुलंगार बच्चा पैदा हो गया जिसके चलते बालकृष्ण को मौत चुननी पड़ी। मैं उस कुपुत्र का मुँह भी देखना नहीं चाहता हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा।
पीजी होस्टल के 110 कमरों के लिए चार वार्ड सर्वेंट नियुक्त थे- दाहू, मिसरी, लक्ष्मण और महेश। सहरसा निवासी दाहू मुखिया उनमें से वरिष्ठ थे। वे हमारे हिस्से में आते थे। दुबली-पतली काया में गज़ब की फुर्ती। पैदल चलते तो साइकिल की गति होती। सभी अधिवासियों की सेवा में तत्पर। एक मजेदार व्यक्तित्व। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। दोपहर बाद घूमकर पूछते, “यौ मालिक परवत्ती चौक जाय छी। किछ लाबय के ऐछ?” यदि पूछकर जाते तो सबका सामान सिलसिलेवार ले आते। किन्तु जब छात्र अपनी जरूरतों के हिसाब से फरमाइश करते तो वे गड़बड़ा जाते थे। मसलन किसी ने पुकारकर कहा, “दाहू धोबी के यहाँ से कपड़े ला दो।” कोई बोला, “दाहू बर्तन साफ कर दो।” “नमक ले आओ।” “सब्जी काट दो।” “आटा गूंध दो।” “पीने का पानी ले आओ।” या और ऐसे ही कुछ और तो हश्र यह होता कि अंतिम छात्र की बात पूरी हो जाती और बाकी की वे भूल जाते। इस भुलक्कड़ी में कई बार छात्र गुस्सा हो जाते तो जवाब देते, “यौ सर एक्के बेर एतना बात कोना याद राखबै?”
दाहू मुखिया परिवार नहीं रखते थे, किन्तु एक बेटा साथ रहता था, जिसे जांघ में लाल फूलगोभी जैसे आकार-प्रकार का दुर्गंध युक्त घाव था। एक साथी के रिश्तेदार सदर अस्पताल में सर्जन थे। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और बालक चंगा हो गया था। सभी छात्रों के अंशदान से दाहू ने गाँव में थोड़ी जमीन भी खरीद ली थी। एमए के बाद भी उसी होस्टल के रिसर्च विंग में हम तीन साथी तीन साल और रह गये थे। इस तरह दाहू से हमारा सानिध्य पाँच साल से भी अधिक का रहा। इस क्रम में हमारा रिश्ता बहुत प्रगाढ़ हो गया था। हम साथ ही पकाने-खाने लगे थे। टोस्ट जैसी मोटी रोटी को तवे पर कपड़े से दबा-दबाकर पकाने की कला उनसे सीखी थी। दाहू की उस भूरी अनोखी रोटी का स्वाद अबतक मन में बसा है। होस्टल छोड़ने के लगभग दस साल बाद दाहू से अजन्ता टॉकिज के सामने भेंट हुई थी। सुधा जी साथ थीं। कुछ हालचाल के बाद विदा लेते हुए मैंने उनके हाथ में एक नोट पकड़ाया तो वे अत्यंत भावुक हो गये और आँसुओं में भींगकर बोले, “लछमी यौ, अखैंन तक प्रेम कैर रहल छी ई दरिद्र सँ। कहाँ पायब ई दुलार आब? आब त लोक गारिए सँ बात करै छत। आहाँ के बाल-बच्चा सब सुखी रहैत। जीअ लछमी।” मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। सुधा जी और मेरी आँखें जरूर गीली हो गयीं। दाहू मुखिया से यह मेरी अंतिम मुलाकात थी। बहुत याद आते हैं दाहू मुखिया!😢
(क्रमशः)